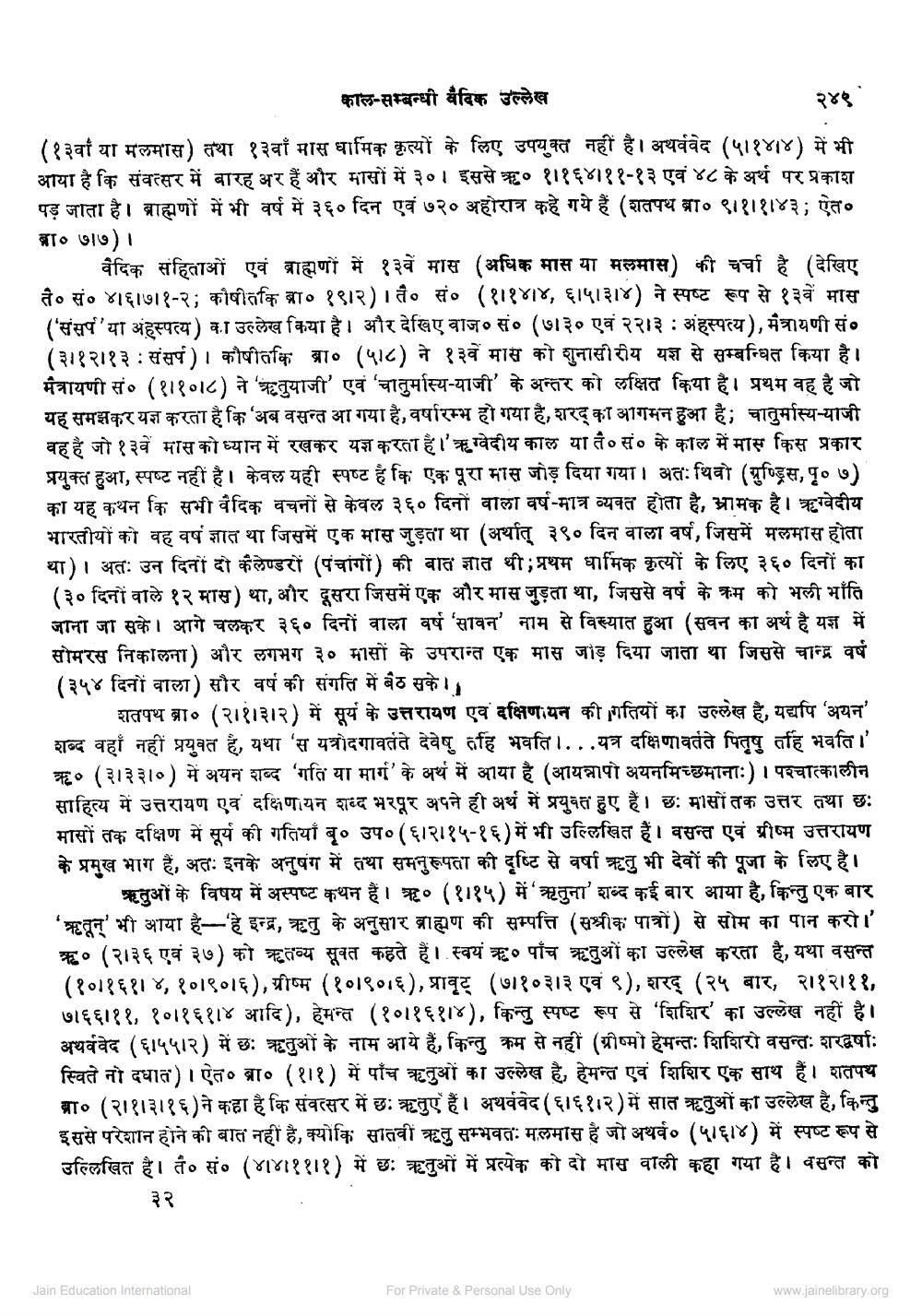________________
काल-सम्बन्धी वैदिक उल्लेख
२४९
(१३वा या मलमास) तथा १३वाँ मास धार्मिक कृत्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। अथर्ववेद (५।१४।४) में भी आया है कि संवत्सर में बारह अर हैं और मासों में ३०। इससे ऋ० १६१६४।११-१३ एवं ४८ के अर्थ पर प्रकाश पड़ जाता है। ब्राह्मणों में भी वर्ष में ३६० दिन एवं ७२० अहोरात्र कहे गये हैं (शतपथ ब्रा० ९।१।११४३; ऐत. ब्रा० ७७)।
वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों में १३वें मास (अधिक मास या मलमास) की चर्चा है (देखिए तै० सं० ४।६।७।१-२; कौषीतकि ब्रा० १९।२) । तै० सं० (१।१४।४, ६।५।३।४) ने स्पष्ट रूप से १३वें मास ('संसर्प' या अंहस्पत्य) का उल्लेख किया है। और देखिए वाज० सं० (७।३० एवं २२१३ : अंहस्पत्य), मैत्रायणी सं. (३।१२।१३ : संसर्प)। कौषीतकि ब्रा० (५।८) ने १३वें मास को शुनासीरीय यज्ञ से सम्बन्धित किया है। मैत्रायणी सं० (१।१०८) ने 'ऋतुयाजी' एवं 'चातुर्मास्य-याजी' के अन्तर को लक्षित किया है। प्रथम वह है जो यह समझकर यज्ञ करता है कि अब वसन्त आ गया है, वर्षारम्भ हो गया है, शरद् का आगमन हुआ है; चातुर्मास्य-याजी वह है जो १३वें मास को ध्यान में रखकर यज्ञ करता है। ऋग्वेदीय काल या तै० सं० के काल में मास किस प्रकार प्रयुक्त हुआ, स्पष्ट नहीं है। केवल यही स्पष्ट है कि एक पूरा मास जोड़ दिया गया। अतः थिवो (ग्रुण्डिस, पृ०७) का यह कथन कि सभी वैदिक वचनों से केवल ३६० दिनों वाला वर्ष-मात्र व्यक्त होता है, भ्रामक है। ऋग्वेदीय भारतीयों को वह वर्ष ज्ञात था जिसमें एक मास जुड़ता था (अर्थात् ३९० दिन वाला वर्ष, जिसमें मलमास होता था)। अतः उन दिनों दो कैलेण्डरों (पंचांगों) की बात ज्ञात थी; प्रथम धार्मिक कृत्यों के लिए ३६० दिनों का (३० दिनों वाले १२ मास) था, और दूसरा जिसमें एक और मास जुड़ता था, जिससे वर्ष के क्रम को भली भाँति जाना जा सके। आगे चलकर ३६० दिनों वाला वर्ष 'सावन' नाम से विख्यात हुआ (सवन का अर्थ है यज्ञ में सोमरस निकालना) और लगभग ३० मासों के उपरान्त एक मास जोड़ दिया जाता था जिससे चान्द्र वर्ष (३५४ दिनों वाला) सौर वर्ष की संगति में बैठ सके।।
शतपथ ब्रा० (२।१।३।२) में सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की गतियों का उल्लेख है, यद्यपि अयन' शब्द वहाँ नहीं प्रयुक्त है, यथा ‘स यत्रोदगावर्तते देवेषु तहि भवति ।...यत्र दक्षिणावर्तते पितृषु तहि भवति।' ऋ० (३।३३।०) में अयन शब्द 'गति या मार्ग' के अर्थ में आया है (आयन्नापो अयनमिच्छमानाः)। पश्चात्कालीन साहित्य में उत्तरायण एवं दक्षिणायन शब्द भरपूर अपने ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। छ: मासों तक उत्तर तथा छः मासों तक दक्षिण में सूर्य की गतियाँ बु० उप० (६।२।१५-१६) में भी उल्लिखित हैं। वसन्त एवं ग्रीष्म उत्तरायण के प्रमुख भाग हैं, अतः इनके अनुषंग में तथा समनुरूपता की दृष्टि से वर्षा ऋतु भी देवों की पूजा के लिए है।
ऋतुओं के विषय में अस्पष्ट कथन हैं। ऋ० (१।१५) में ऋतुना' शब्द कई बार आया है, किन्तु एक बार 'ऋतून्' भी आया है-हे इन्द्र, ऋतु के अनुसार ब्राह्मण की सम्पत्ति (सश्रीक पात्रों) से सोम का पान करो।' ऋ० (२।३६ एवं ३७) को ऋतव्य सूक्त कहते हैं। स्वयं ऋ० पाँच ऋतुओं का उल्लेख करता है, यथा वसन्त (१०।१६१। ४, १०।९०।६), ग्रीष्म (१०।९००६),प्रावृट् (७।१०३।३ एवं ९), शरद् (२५ बार, २।१२।११, ७।६६।११, १०।१६१।४ आदि), हेमन्त (१०।१६११४), किन्तु स्पष्ट रूप से 'शिशिर' का उल्लेख नहीं है। अथर्ववेद (६।५५।२) में छः ऋतुओं के नाम आये हैं, किन्तु क्रम से नहीं (ग्रीष्मो हेमन्तः शिशिरो वसन्तः शरवर्षाः स्विते नो दधात)। ऐत० ब्रा० (१११) में पाँच ऋतुओं का उल्लेख है, हेमन्त एवं शिशिर एक साथ हैं। शतपथ ब्रा० (२।१।३।१६)ने कहा है कि संवत्सर में छः ऋतुएँ हैं। अथर्ववेद (६।६१०२) में सात ऋतुओं का उल्लेख है, किन्तु इससे परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि सातवीं ऋतु सम्भवतः मलमास है जो अथर्व० (५।६।४) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। त० सं० (४।४।११।१) में छः ऋतुओं में प्रत्येक को दो मास वाली कहा गया है। वसन्त को
३२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org