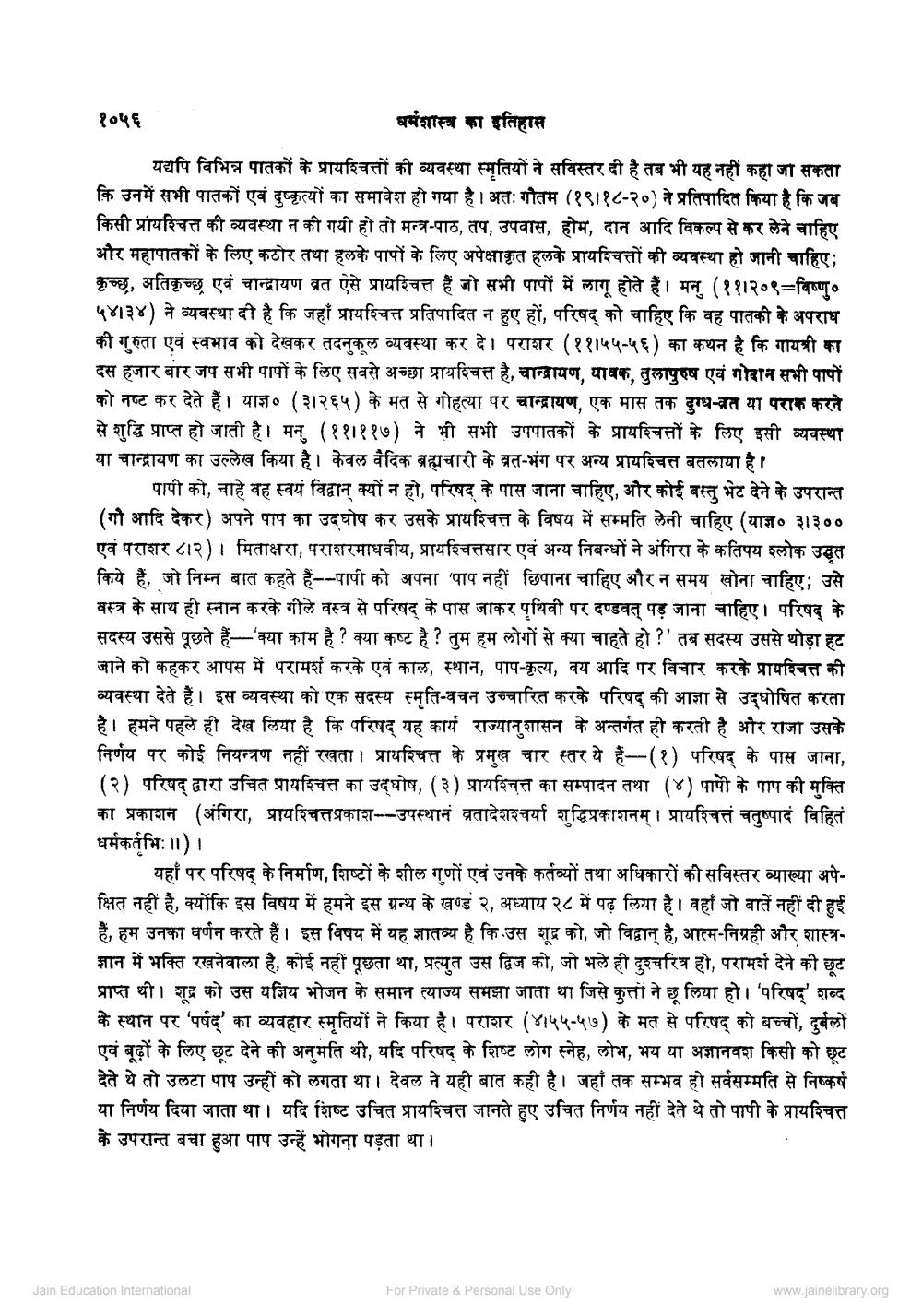________________
१०५६
धर्मशास्त्र का इतिहास यद्यपि विभिन्न पातकों के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था स्मृतियों ने सविस्तर दी है तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें सभी पातकों एवं दुष्कृत्यों का समावेश हो गया है। अतः गौतम (१९।१८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जब किसी प्रायश्चित्त की व्यवस्था न की गयी हो तो मन्त्र-पाठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विकल्प से कर लेने चाहिए और महापातकों के लिए कठोर तथा हलके पापों के लिए अपेक्षाकृत हलके प्रायश्चित्तों की व्यवस्था हो जानी चाहिए; कृच्छ, अतिकृच्छ एवं चान्द्रायण व्रत ऐसे प्रायश्चित्त हैं जो सभी पापों में लागू होते हैं। मनु (११२०९ विष्णु० ५४१३४) ने व्यवस्था दी है कि जहाँ प्रायश्चित्त प्रतिपादित न हुए हों, परिषद् को चाहिए कि वह पातकी के अपराध की गुरुता एवं स्वभाव को देखकर तदनकल व्यवस्था कर दे। पराशर (१११५५-५६) का कथन है कि गायत्री का दस हजार बार जप सभी पापों के लिए सबसे अच्छा प्रायश्चित्त है, चान्द्रायण, यावक, तुलापुरुष एवं गोदान सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। याज्ञ० (३३२६५) के मत से गोहत्या पर चान्द्रायण, एक मास तक दुग्ध-व्रत या पराक करने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु (११११७) ने भी सभी उपपातकों के प्रायश्चित्तों के लिए इसी व्यवस्था या चान्द्रायण का उल्लेख किया है। केवल वैदिक ब्रह्मचारी के व्रत-भंग पर अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है।
पापी को, चाहे वह स्वयं विद्वान् क्यों न हो, परिषद् के पास जाना चाहिए, और कोई वस्तु भेट देने के उपरान्त (गौ आदि देकर) अपने पाप का उद्घोष कर उसके प्रायश्चित्त के विषय में सम्मति लेनी चाहिए (याज्ञ० ३१३०० एवं पराशर ८१२)। मिताक्षरा, पराशरमाधवीय, प्रायश्चित्तसार एवं अन्य निबन्धों ने अंगिरा के कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं, जो निम्न बात कहते हैं--पापी को अपना 'पाप नहीं छिपाना चाहिए और न समय खोना चाहिए; उसे वस्त्र के साथ ही स्नान करके गीले वस्त्र से परिषद् के पास जाकर पृथिवी पर दण्डवत् पड़ जाना चाहिए। परिषद् के सदस्य उससे पूछते हैं--'क्या काम है ? क्या कष्ट है ? तुम हम लोगों से क्या चाहते हो?' तब सदस्य उससे थोड़ा हट जाने को कहकर आपस में परामर्श करके एवं काल, स्थान, पाप-कृत्य, वय आदि पर विचार करके प्रायश्चित्त की व्यवस्था देते हैं। इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचन उच्चारित करके परिषद् की आज्ञा से उद्घोषित करता है। हमने पहले ही देख लिया है कि परिषद् यह कार्य राज्यानुशासन के अन्तर्गत ही करती है और राजा उसके निर्णय पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता। प्रायश्चित्त के प्रमुख चार स्तर ये हैं-(१) परिषद् के पास जाना, (२) परिषद् द्वारा उचित प्रायश्चित्त का उद्घोष, (३) प्रायश्चित्त का सम्पादन तथा (४) पापो के पाप की मुक्ति का प्रकाशन (अंगिरा, प्रायश्चित्तप्रकाश---उपस्थानं व्रतादेशश्चर्या शुद्धिप्रकाशनम् । प्रायश्चित्तं चतुष्पादं विहितं धर्मकर्तृभिः॥)।
यहाँ पर परिषद् के निर्माण, शिष्टों के शील गुणों एवं उनके कर्तव्यों तथा अधिकारों की सविस्तर व्याख्या अपेक्षित नहीं है, क्योंकि इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में पढ़ लिया है। वहाँ जो बातें नहीं दी हुई हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि उस शूद्र को, जो विद्वान् है, आत्म-निग्रही और शास्त्रज्ञान में भक्ति रखनेवाला है, कोई नहीं पूछता था, प्रत्युत उस द्विज को, जो भले ही दुश्चरित्र हो, परामर्श देने की छूट प्राप्त थी। शूद्र को उस यज्ञिय भोजन के समान त्याज्य समझा जाता था जिसे कुत्तों ने छू लिया हो। 'परिषद्' शब्द के स्थान पर 'पर्षद्' का व्यवहार स्मृतियों ने किया है। पराशर (४१५५-५७) के मत से परिषद् को बच्चों, दुर्बलों एवं बूढ़ों के लिए छूट देने की अनुमति थी, यदि परिषद् के शिष्ट लोग स्नेह, लोभ, भय या अज्ञानवश किसी को छूट देते थे तो उलटा पाप उन्हीं को लगता था। देवल ने यही बात कही है। जहाँ तक सम्भव हो सर्वसम्मति से निष्कर्ष या निर्णय दिया जाता था। यदि शिष्ट उचित प्रायश्चित्त जानते हए उचित निर्णय नहीं देते थे तो पापी के प्रायश्चित्त के उपरान्त बचा हआ पाप उन्हें भोगना पड़ता था।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org