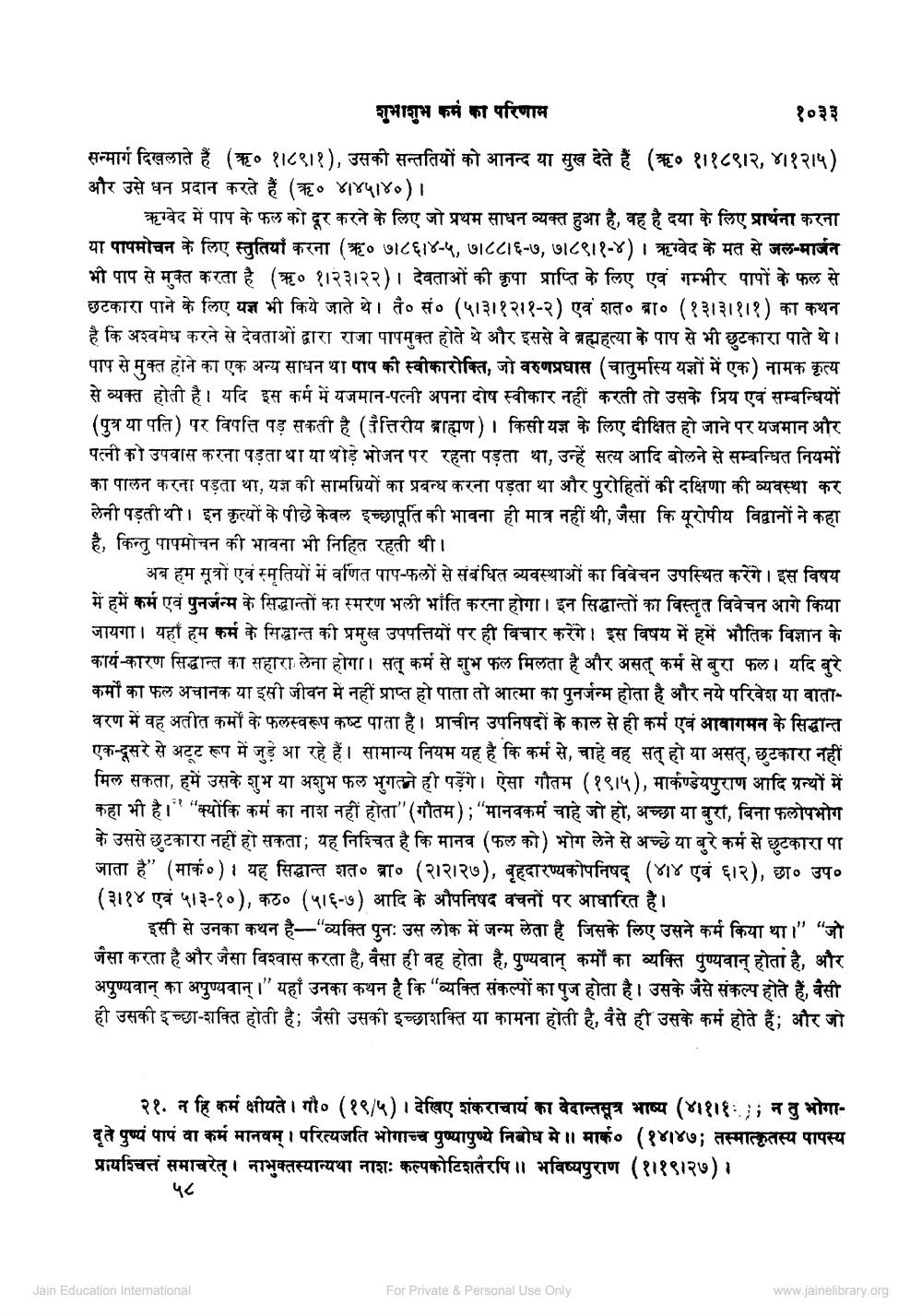________________
शुभाशुभ कर्म का परिणाम
१०३३ सन्मार्ग दिखलाते हैं (ऋ० ११८९।१), उसकी सन्ततियों को आनन्द या सुख देते हैं (ऋ० १११८९।२, ४।१२।५) और उसे धन प्रदान करते हैं (ऋ० ४।४५।४०)।
ऋग्वेद में पाप के फल को दूर करने के लिए जो प्रथम साधन व्यक्त हुआ है, वह है दया के लिए प्रार्थना करना या पापमोचन के लिए स्तुतियाँ करना (ऋ० ७।८६।४-५, ७।८८।६-७, ७८९।१-४) । ऋग्वेद के मत से जल-मार्जन भी पाप से मुक्त करता है (ऋ० १।२३।२२)। देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एवं गम्भीर पापों के फल से छटकारा पाने के लिए यज्ञ भी किये जाते थे। तै० सं० (५।३।१२।१-२) एवं शत० ब्रा० (१३।३।१।१) का कथन है कि अश्वमेध करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्त होते थे और इससे वे ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पाते थे। पाप से मुक्त होने का एक अन्य साधन था पाप को स्वीकारोक्ति, जो वरुणप्रघास (चातुर्मास्य यज्ञों में एक) नामक कृत्य से व्यक्त होती है। यदि इस कर्म में यजमान-पत्नी अपना दोष स्वीकार नहीं करती तो उसके प्रिय एवं सम्बन्धियों (पुत्र या पति) पर विपत्ति पड़ सकती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण)। किसी यज्ञ के लिए दीक्षित हो जाने पर यजमान और पत्नी को उपवास करना पड़ता था या थोड़े भोजन पर रहना पड़ता था, उन्हें सत्य आदि बोलने से सम्बन्धित नियमों का पालन करना पड़ता था, यज्ञ की सामग्रियों का प्रबन्ध करना पड़ता था और पुरोहितों की दक्षिणा की व्यवस्था कर लेनी पड़ती थी। इन कृत्यों के पीछे केवल इच्छापूर्ति की भावना ही मात्र नहीं थी, जैसा कि यूरोपीय विद्वानों ने कहा है, किन्तु पापमोचन की भावना भी निहित रहती थी।
अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों में वर्णित पाप-फलों से संबंधित व्यवस्थाओं का विवेचन उपस्थित करेंगे। इस विषय में हमें कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्तों का स्मरण भली भांति करना होगा। इन सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा। यहाँ हम कर्म के सिद्धान्त की प्रमुख उपपत्तियों पर ही विचार करेंगे। इस विषय में हमें भौतिक विज्ञान के कार्य-कारण सिद्धान्त का सहारा लेना होगा। सत् कर्म से शुभ फल मिलता है और असत् कर्म से बुरा फल। यदि बुरे कर्मों का फल अचानक या इसी जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है और नये परिवेश या वातावरण में वह अतीत कर्मों के फलस्वरूप कष्ट पाता है। प्राचीन उपनिषदों के काल से ही कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त एक-दूसरे से अटूट रूप में जुड़े आ रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि कर्म से, चाहे वह सत् हो या असत्, छुटकारा नहीं मिल सकता, हमें उसके शुभ या अशुभ फल भुगतने ही पड़ेंगे। ऐसा गौतम (१९।५), मार्कण्डेयपुराण आदि ग्रन्थों में कहा भी है।' "क्योंकि कर्म का नाश नहीं होता" (गौतम); “मानवकर्म चाहे जो हो, अच्छा या बुरा, बिना फलोपभोग के उससे छुटकारा नहीं हो सकता; यह निश्चित है कि मानव (फल को) भोग लेने से अच्छे या बुरे कर्म से छुटकारा पा जाता है" (मार्क०)। यह सिद्धान्त शत० ब्रा० (२।२।२७), बृहदारण्यकोपनिषद् (४१४ एवं ६।२), छा० उप० (३॥१४ एवं ५।३-१०), कठ० (५।६-७) आदि के औपनिषद वचनों पर आधारित है। __इसी से उनका कथन है-"व्यक्ति पुनः उस लोक में जन्म लेता है जिसके लिए उसने कर्म किया था।" "जो जैसा करता है और जैसा विश्वास करता है, वैसा ही वह होता है, पुण्यवान् कर्मों का व्यक्ति पुण्यवान् होता है, और अपुण्यवान् का अपुण्यवान्।" यहाँ उनका कथन है कि "व्यक्ति संकल्पों का पुज होता है। उसके जैसे संकल्प होते हैं, वैसी ही उसकी इच्छा-शक्ति होती है; जैसी उसकी इच्छाशक्ति या कामना होती है, वैसे ही उसके कर्म होते हैं; और जो
२१. न हि कर्म क्षीयते। गौ० (१९/५)। देखिए शंकराचार्य का वेदान्तसूत्र भाष्य (४११०६न तु भोगादृते पुण्यं पापं वा कर्म मानवम् । परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुण्ये निबोध मे॥ मार्क० (१४॥४७; तस्मात्कृतस्य पापस्य प्रायश्चित्तं समाचरेत् । नाभुक्तस्यान्यथा नाशः कल्पकोटिशतैरपि ॥ भविष्यपुराण (१।१९।२७)।
५८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org