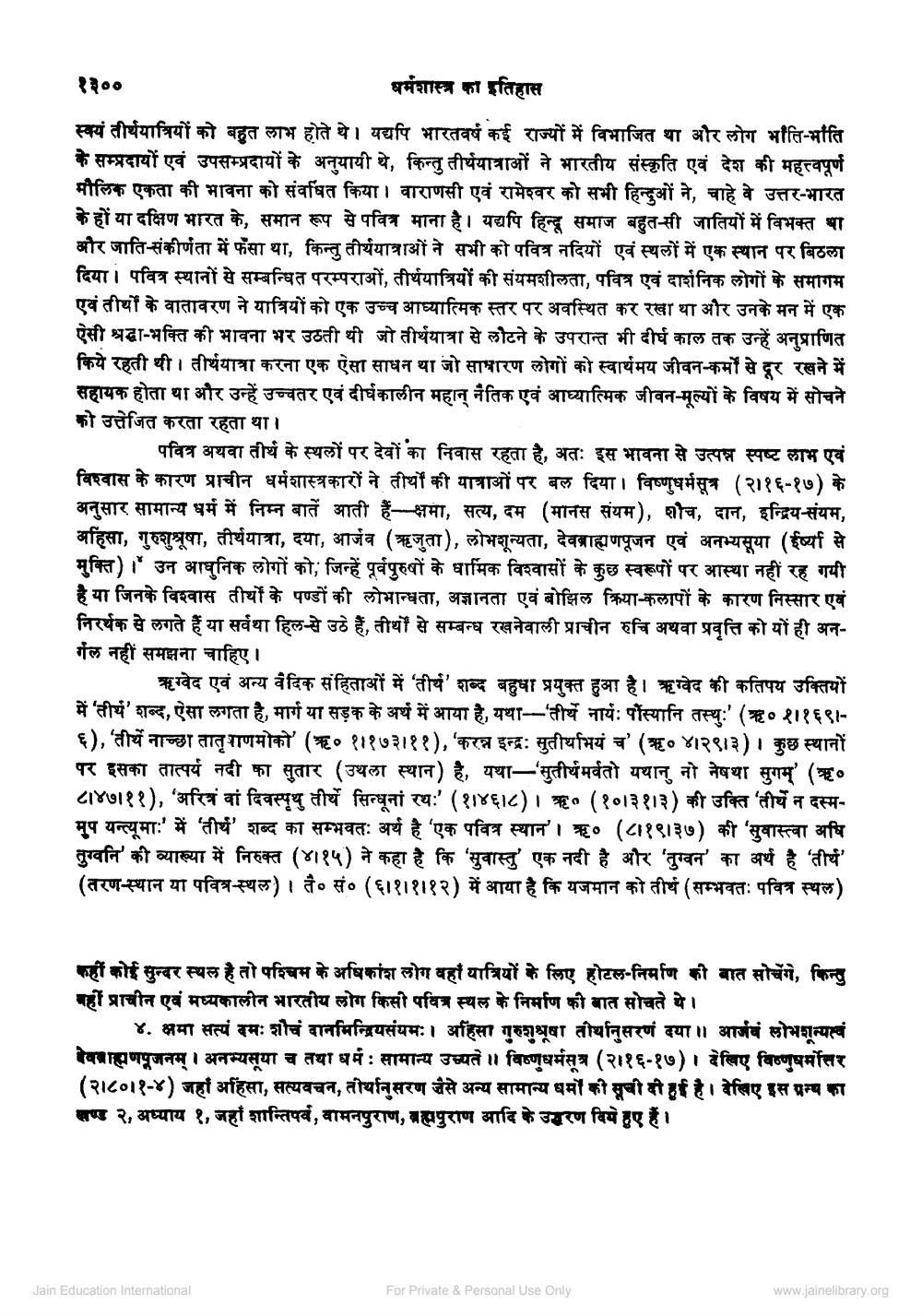________________
धर्मशास्त्र का इतिहास स्वयं तीर्थयात्रियों को बहुत लाभ होते थे। यद्यपि भारतवर्ष कई राज्यों में विभाजित था और लोग भांति-भांति के सम्प्रदायों एवं उपसम्प्रदायों के अनुयायी थे, किन्तु तीर्थयात्राओं ने भारतीय संस्कृति एवं देश की महत्त्वपूर्ण मौलिक एकता की भावना को संवधित किया। वाराणसी एवं रामेश्वर को सभी हिन्दुओं ने, चाहे वे उत्तर-भारत के हों या दक्षिण भारत के, समान रूप से पवित्र माना है। यद्यपि हिन्दू समाज बहुत-सी जातियों में विभक्त था
और जाति-संकीर्णता में फंसा था, किन्तु तीर्थयात्राओं ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्थलों में एक स्थान पर बिठला दिया। पवित्र स्थानों से सम्बन्धित परम्पराओं, तीर्थयात्रियों की संयमशीलता, पवित्र एवं दार्शनिक लोगों के समागम एवं तीर्थों के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रखा था और उनके मन में एक ऐसी श्रद्धा-भक्ति की भावना भर उठती थी जो तीर्थयात्रा से लौटने के उपरान्त भी दीर्घ काल तक उन्हें अनुप्राणित किये रहती थी। तीर्थयात्रा करना एक ऐसा साधन था जो साधारण लोगों को स्वार्थमय जीवन-कर्मों से दूर रखने में सहायक होता था और उन्हें उच्चतर एवं दीर्घकालीन महान् नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के विषय में सोचने को उत्तेजित करता रहता था।
पवित्र अथवा तीर्थ के स्थलों पर देवों का निवास रहता है, अतः इस भावना से उत्पन्न स्पष्ट लाभ एवं विश्वास के कारण प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने तीर्थों की यात्राओं पर बल दिया। विष्णुधर्मसूत्र (२०१६-१७) के अनुसार सामान्य धर्म में निम्न बातें आती हैं-क्षमा, सत्य, दम (मानस संयम), शौच, दान, इन्द्रिय-संयम, अहिंसा, गरुशश्रषा, तीर्थयात्रा, दया, आर्जव (ऋजता), लोभशन्यता, देवब्राह्मणपूजन एवं अनभ्यसूया (ईर्ष्या से मक्ति)। उन आधनिक लोगों को, जिन्हें पूर्वपुरुषों के धार्मिक विश्वासों के कुछ स्वरूपों पर आस्था नहीं रह गयी है या जिनके विश्वास तीर्थों के पण्डों की लोभान्धता, अज्ञानता एवं बोझिल क्रिया-कलापों के कारण निस्सार एवं निरर्थक से लगते हैं या सर्वथा हिल-से उठे हैं, तीर्थों से सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन रुचि अथवा प्रवृत्ति को यों ही अनगंल नहीं समझना चाहिए।
ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक संहिताओं में 'तीर्थ' शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद की कतिपय उक्तियों में 'तीर्थ' शब्द, ऐसा लगता है, मार्ग या सड़क के अर्थ में आया है, यथा-'तीर्थे नार्यः पौंस्यानि तस्थुः' (ऋ० ११६९।६), 'तीर्थे नाच्छा तातृपाणमोको' (ऋ० १११७३।११), 'करन्न इन्द्रः सुतीर्थाभयं च' (ऋ० ४।२९।३)। कुछ स्थानों पर इसका तात्पर्य नदी का सुतार (उथला स्थान) है, यथा-'सुतीर्थमर्वतो यथानु नो नेषथा सुगम्' (ऋ० ८१४७।११), 'अरित्रं वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथः' (११४६१८)। ऋ० (१०॥३१॥३) की उक्ति तीर्थे न दस्ममुप यन्त्यूमाः' में 'तीर्थ' शब्द का सम्भवतः अर्थ है 'एक पवित्र स्थान'। ऋ० (८।१९।३७) की 'सुवास्त्वा अधि तुग्वनि' की व्याख्या में निरुक्त (४।१५) ने कहा है कि 'सुवास्तु' एक नदी है और 'तुग्वन' का अर्थ है 'तीर्थ' (तरण-स्थान या पवित्र स्थल)। तै० सं० (६।१२।१२) में आया है कि यजमान को तीर्थ (सम्भवतः पवित्र स्थल)
कहीं कोई सुन्दर स्थल है तो पश्चिम के अधिकांश लोग वहां यात्रियों के लिए होटल-निर्माण की बात सोचेंगे, किन्तु नहीं प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय लोग किसी पवित्र स्थल के निर्माण की बात सोचते थे।
४. क्षमा सत्यं दमः शौचं दानमिन्द्रियसंयमः। अहिंसा गुरुशुश्रूषा तीर्थानुसरणं दया॥ आर्जवं लोभशन्यत्वं देवबाह्मणपूजनम् । अनम्यसूया च तथा धर्म : सामान्य उच्यते ॥ विष्णुधर्मसूत्र (२०१६-१७)। देखिए विष्णुधर्मोत्तर (२।८०।१-४) जहाँ अहिंसा, सत्यवचन, तीर्थानुसरण जैसे अन्य सामान्य धर्मों की सूची दी हुई है। देखिए इस अन्य का सण २, अध्याय १, जहाँ शान्तिपर्व, वामनपुराण, ब्रह्मपुराण आदि के उद्धरण विये हुए हैं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org