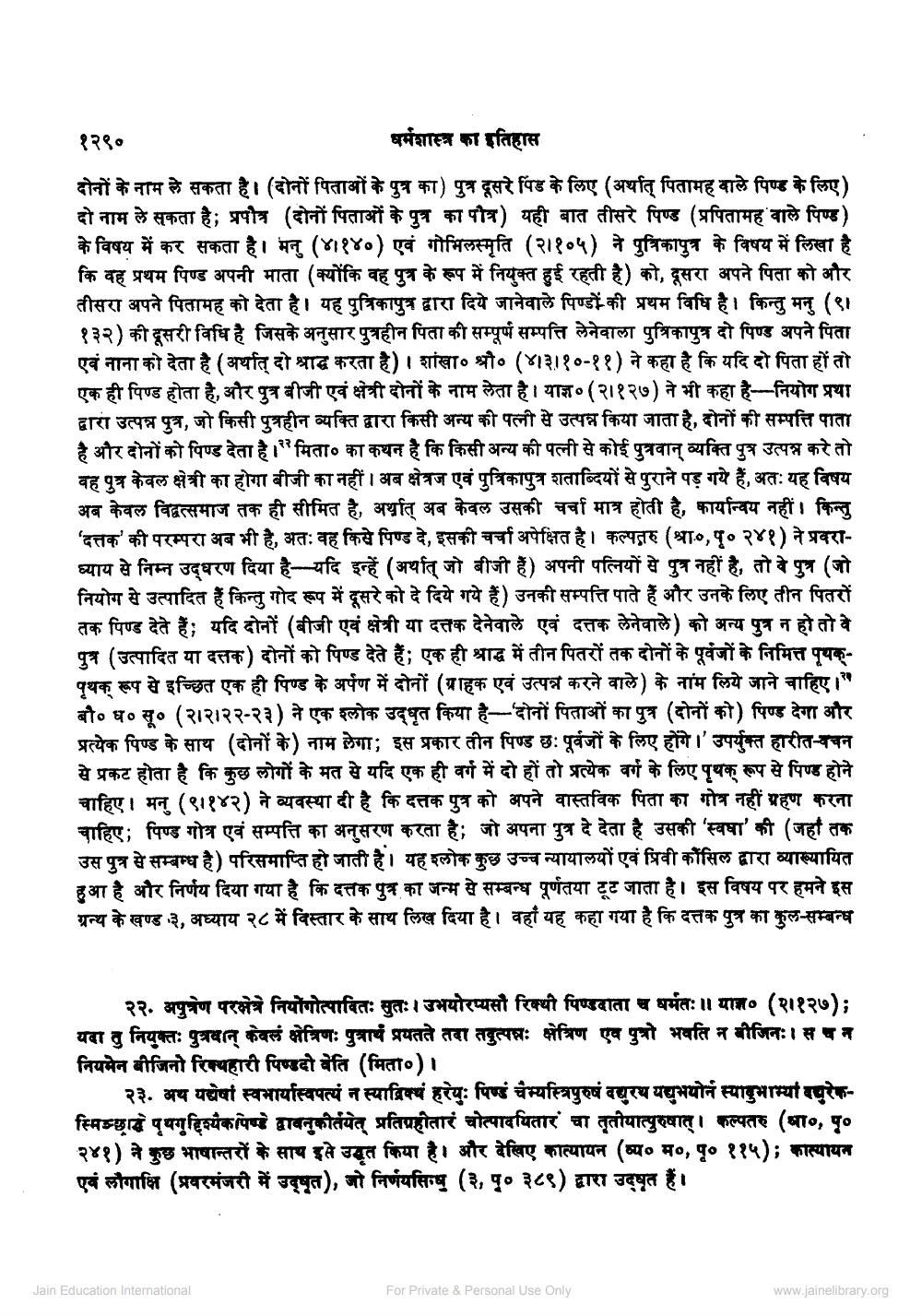________________
१२९०
धर्मशास्त्र का इतिहास दोनों के नाम ले सकता है। (दोनों पिताओं के पुत्र का) पुत्र दूसरे पिंड के लिए (अर्थात् पितामह वाले पिण्ड के लिए) दो नाम ले सकता है। प्रपौत्र (दोनों पिताओं के पुत्र का पौत्र) यही बात तीसरे पिण्ड (प्रपितामह वाले पिण्ड) के विषय में कर सकता है। मनु (४।१४०) एवं गोभिलस्मृति (२।१०५) ने पुत्रिकापुत्र के विषय में लिखा है कि वह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योंकि वह पुत्र के रूप में नियुक्त हुई रहती है) को, दूसरा अपने पिता को और तीसरा अपने पितामह को देता है। यह पुत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवाले पिण्डों की प्रथम विधि है। किन्तु मनु (९। १३२) की दूसरी विधि है जिसके अनुसार पुत्रहीन पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति लेनेवाला पुत्रिकापुत्र दो पिण्ड अपने पिता एवं नाना को देता है (अर्थात दो श्राद्ध करता है)। शांखा. श्री० (४।३।१०-११) ने कहा है कि यदि दो पिता हों तो एक ही पिण्ड होता है, और पुत्र बीजी एवं क्षेत्री दोनों के नाम लेता है। याज्ञ० (२।१२७) ने भी कहा है-नियोग प्रथा द्वारा उत्पन्न पत्र, जो किसी पत्रहीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दोनों की सम्पत्ति पाता है और दोनों को पिण्ड देता है। मिता० का कथन है कि किसी अन्य की पत्नी से कोई पुत्रवान् व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करे तो वह पत्र केवल क्षेत्री का होगा बीजी का नहीं। अब क्षेत्रज एवं पत्रिकापुत्र शताब्दियों से पुराने पड़ गये हैं, अतः यह विषय अब केवल विद्वत्समाज तक ही सीमित है, अर्थात अब केवल उसकी चर्चा मात्र होती है, कार्यान्वय नहीं। किन्त 'दत्तक' की परम्परा अब भी है, अतः वह किसे पिण्ड दे, इसकी चर्चा अपेक्षित है। कल्पतरु (श्रा०,१०२४१) ने प्रवराध्याय से निम्न उद्धरण दिया है-यदि इन्हें (अर्थात् जो बीजी हैं) अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं है, तो वे पुत्र (जो नियोग से उत्पादित हैं किन्तु गोद रूप में दूसरे को दे दिये गये हैं) उनकी सम्पत्ति पाते हैं और उनके लिए तीन पितरों तक पिण्ड देते हैं। यदि दोनों (बीजी एवं क्षेत्री या दत्तक देनेवाले एवं दत्तक लेनेवाले) को अन्य पुत्र न हो तो वे पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दोनों को पिण्ड देते हैं; एक ही श्राद्ध में तीन पितरों तक दोनों के पूर्वजों के निमित्त पृथक्पृथक् रूप से इच्छित एक ही पिण्ड के अर्पण में दोनों (ग्राहक एवं उत्पन्न करने वाले) के नाम लिये जाने चाहिए।" बौ० ध० सू० (२।२।२२-२३) ने एक श्लोक उद्धृत किया है-'दोनों पिताओं का पुत्र (दोनों को) पिण्ड देगा और प्रत्येक पिण्ड के साथ (दोनों के) नाम लेगा; इस प्रकार तीन पिण्ड छः पूर्वजों के लिए होंगे।' उपर्युक्त हारीत-वचन से प्रकट होता है कि कुछ लोगों के मत से यदि एक ही वर्ग में दो हों तो प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक् रूप से पिण्ड होने चाहिए। मनु (९।१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को अपने वास्तविक पिता का गोत्र नहीं ग्रहण करना चाहिए; पिण्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुसरण करता है; जो अपना पुत्र दे देता है उसकी 'स्वधा' की (जहाँ तक उस पुत्र से सम्बन्ध है) परिसमाप्ति हो जाती है। यह श्लोक कुछ उच्च न्यायालयों एवं प्रिवी कौंसिल द्वारा व्याख्यायित हुआ है और निर्णय दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जन्म से सम्बन्ध पूर्णतया टूट जाता है। इस विषय पर हमने इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २८ में विस्तार के साथ लिख दिया है। वहाँ यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र का कुल-सम्बन्ध
२२. अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोंगोत्पावितः सुतः। उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः॥याज (२१२७); यदा तु नियुक्तः पुत्रवान् केवलं क्षेत्रिणः पुत्रार्थ प्रयतते तदा तदुत्पन्नः क्षेत्रिण एव पुत्रो भवति न बीजिनः। सपन नियमेन बीजिनो रिफ्यहारी पिण्डदो वेति (मिता०)।
२३. अथ योषां स्वभार्यास्वपत्यं न स्याद्रिक्यं हरेयुः पिण्डं चैम्यस्त्रिपुरुषं वारथ यद्युभयोर्न स्यादुभाम्या बयुरेकस्मिञ्छा पृथगुद्दिश्यकपिण्डे द्वावनुकीर्तयेत् प्रतिग्रहीतारं चोत्पादयितार चा तृतीयात्पुरुषात्। कल्पतरु (मा०, पृ० २४१) ने कुछ भाषान्तरों के साथ इसे उब्त किया है। और देखिए कात्यायन (व्य० म०, पृ० ११५); कात्यायन एवं लौगाक्षि (प्रवरमंजरी में उद्धृत), जो निर्णयसिन्धु (३, पृ० ३८९) द्वारा उद्धृत हैं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org