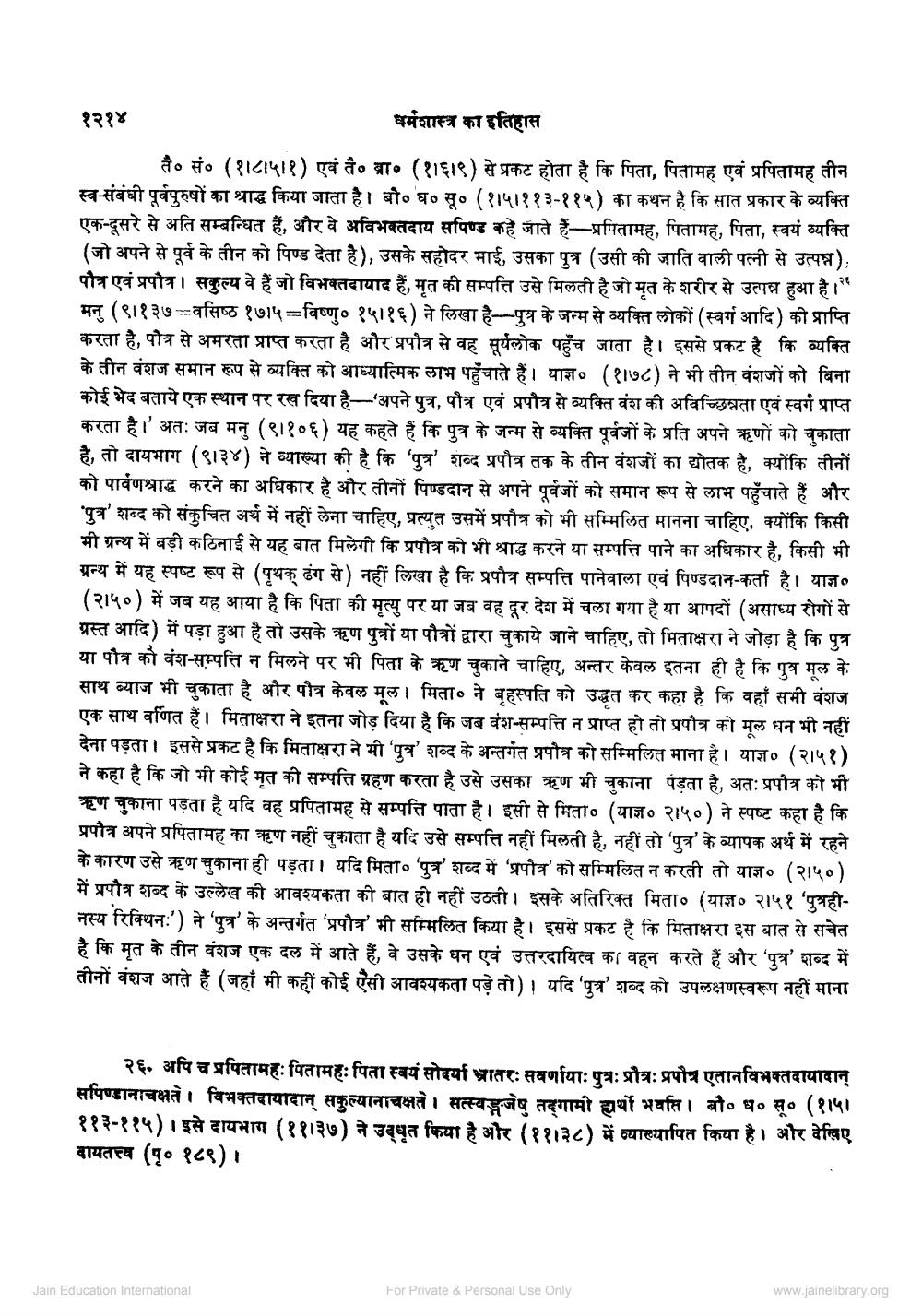________________
धर्मशास्त्र का इतिहास
तै० सं० ( १/८/५/१) एवं तै० ब्रा० (१।६।९ ) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह तीन स्व-संबंधी पूर्वपुरुषों का श्राद्ध किया जाता है। बो० घ० सू० (१।५।११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति एक-दूसरे से अति सम्बन्धित हैं, और वे अविभक्तदाय सपिण्ड कहे जाते हैं--प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं व्यक्ति ( जो अपने से पूर्व के तीन को पिण्ड देता है), उसके सहोदर भाई, उसका पुत्र ( उसी की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न ): पौत्र एवं प्रपौत्र । सकुल्य वे हैं जो विभक्तदायाद हैं, मृत की सम्पत्ति उसे मिलती है जो मृत के शरीर से उत्पन्न हुआ है । " मनु ( ९ | १३७ = वसिष्ठ १७१५ = विष्णु० १५ ।१६) ने लिखा है - पुत्र के जन्म से व्यक्ति लोकों (स्वर्ग आदि) की प्राप्ति करता है, पौत्र से अमरता प्राप्त करता है और प्रपोत्र से वह सूर्यलोक पहुँच जाता है। इससे प्रकट है कि व्यक्ति के तीन वंशज समान रूप से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाते हैं। याज्ञ० ( १।७८) ने भी तीन वंशजों को बिना कोई भेद बताये एक स्थान पर रख दिया है - ' अपने पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र से व्यक्ति वंश की अविच्छिन्नता एवं स्वर्ग प्राप्त करता है ।' अतः जब मनु ( ९।१०६ ) यह कहते हैं कि पुत्र के जन्म से व्यक्ति पूर्वजों के प्रति अपने ऋणों को चुकाता है, तो दायभाग ( ९।३४ ) ने व्याख्या की है कि 'पुत्र' शब्द प्रपौत्र तक के तीन वंशजों का द्योतक है, क्योंकि तीनों को पार्वणश्राद्ध करने का अधिकार है और तीनों पिण्डदान से अपने पूर्वजों को समान रूप से लाभ पहुँचाते हैं और 'पुत्र' शब्द को संकुचित अर्थ में नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उसमें प्रपौत्र को भी सम्मिलित मानना चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रन्थ में बड़ी कठिनाई से यह बात मिलेगी कि प्रपौत्र को भी श्राद्ध करने या सम्पत्ति पाने का अधिकार है, किसी भी ग्रन्थ में यह स्पष्ट रूप से ( पृथक् ढंग से) नहीं लिखा है कि प्रपौत्र सम्पत्ति पानेवाला एवं पिण्डदान-कर्ता है। याज्ञ० (२/५० ) में जब यह आया है कि पिता की मृत्यु पर या जब वह दूर देश चला गया है या आपदों (असाध्य रोगों से ग्रस्त आदि) में पड़ा हुआ है तो उसके ॠण पुत्रों या पौत्रों द्वारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोड़ा है कि पुत्र या पौत्र को वंश- सम्पत्ति न मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवल इतना ही है कि पुत्र मूल के साथ ब्याज भी चुकाता है और पौत्र केवल मूल । मिता० ने बृहस्पति को उद्धृत कर कहा है कि वहाँ सभी वंशज एक साथ वर्णित हैं । मिताक्षरा ने इतना जोड़ दिया है कि जब वंश-सम्पत्ति न प्राप्त हो तो प्रपौत्र को मूल धन भी नहीं देना पड़ता। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा ने मी 'पुत्र' शब्द के अन्तर्गत प्रपौत्र को सम्मिलित माना है । याज्ञ० (२।५१ ) ने कहा है कि जो भी कोई मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है उसे उसका ऋण भी चुकाना पड़ता है, अतः प्रपोत्र को भी ऋण चुकाना पड़ता है यदि वह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है। इसी से मिता० ( याज्ञ० २१५०) ने स्पष्ट कहा है कि प्रपौत्र अपने प्रपितामह का ऋण नहीं चुकाता है यदि उसे सम्पत्ति नहीं मिलती है, नहीं तो 'पुत्र' के व्यापक अर्थ में रहने के कारण उसे ऋण चुकाना ही पड़ता । यदि मिता० 'पुत्र' शब्द में 'प्रपोत्र' को सम्मिलित न करती तो याज्ञ० (२/५० ) में प्रपौत्र शब्द के उल्लेख की आवश्यकता की बात ही नहीं उठती। इसके अतिरिक्त मिता० ( याज्ञ० २।५१ 'पुत्रही - नस्य रिक्थिनः') ने 'पुत्र' के अन्तर्गत 'प्रपौत्र' भी सम्मिलित किया है। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा इस बात से सचेत है कि मृत के तीन वंशज एक दल में आते हैं, वे उसके धन एवं उत्तरदायित्व का वहन करते हैं और 'पुत्र' शब्द में तीनों वंशज आते हैं (जहाँ भी कहीं कोई ऐसी आवश्यकता पड़े तो ) । यदि 'पुत्र' शब्द को उपलक्षणस्वरूप नहीं माना
१२१४
२६. अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या भ्रातरः सवर्णायाः पुत्रः प्रौत्रः प्रपौत्र एतानविभक्तदायादान् सपिण्डानाचक्षते । विभक्तदायादान् सकुल्यानाचक्षते । सत्स्वङ्गजेषु तद्गामी ह्यर्थो भवति । बौ० ध० सू० (१14) ११३-११५) । इसे दायभाग (११।३७) ने उद्धृत किया है और (११।३८) में व्याख्यापित किया है। और देखिए दायतत्त्व ( पृ० १८९ ) ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org