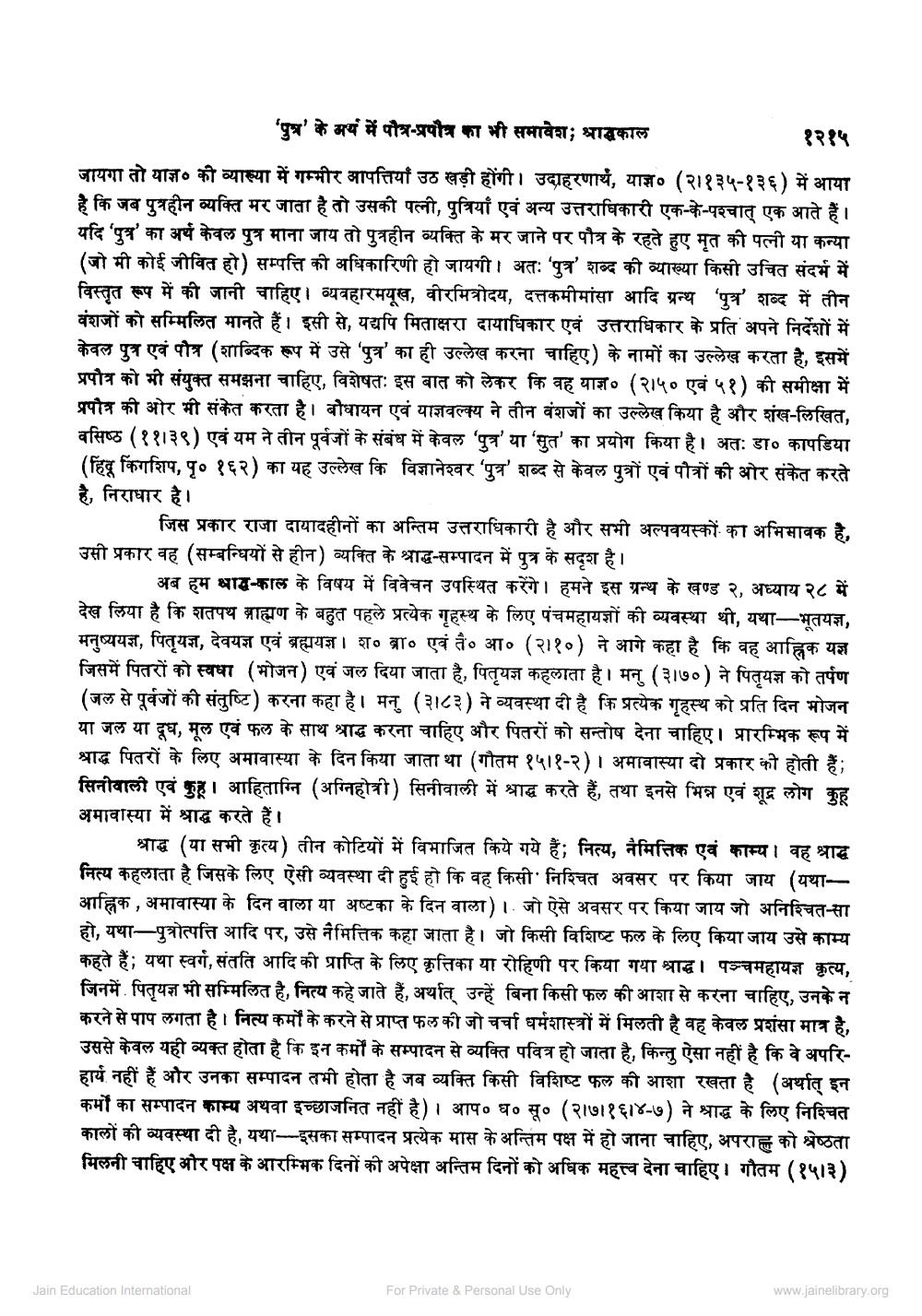________________
'पुत्र' के मयं में पौत्र-प्रपौत्र का भी समावेश; श्राद्धकाल
१२१५ जायगा तो याज्ञ० की व्याख्या में गम्भीर आपत्तियाँ उठ खड़ी होंगी। उदाहरणार्थ, याज्ञ० (२११३५-१३६) में आया है कि जब पुत्रहीन व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी, पुत्रियाँ एवं अन्य उत्तराधिकारी एक-के-पश्चात् एक आते हैं। यदि 'पुत्र' का अर्थ केवल पुत्र माना जाय तो पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र के रहते हुए मृत की पत्नी या कन्या (जो भी कोई जीवित हो) सम्पत्ति की अधिकारिणी हो जायगी। अतः 'पुत्र' शब्द की व्याख्या किसी उचित संदर्भ में विस्तृत रूप में की जानी चाहिए। व्यवहारमयूख, वीरमित्रोदय, दत्तकमीमांसा आदि ग्रन्थ 'पुत्र' शब्द में तीन वंशजों को सम्मिलित मानते हैं। इसी से, यद्यपि मिताक्षरा दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के प्रति अपने निर्देशों में केवल पुत्र एवं पौत्र (शाब्दिक रूप में उसे 'पुत्र' का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामों का उल्लेख करता है, इसमें प्रपौत्र को भी संयुक्त समझना चाहिए, विशेषतः इस बात को लेकर कि वह याज्ञ० (२।५० एवं ५१) की समीक्षा में प्रपौत्र की ओर भी संकेत करता है। बौधायन एवं याज्ञवल्क्य ने तीन वंशजों का उल्लेख किया है और शंख-लिखित, वसिष्ठ (११।३९) एवं यम ने तीन पूर्वजों के संबंध में केवल 'पुत्र' या 'सुत' का प्रयोग किया है। अतः डा० कापडिया (हिंदू किंगशिप, पृ० १६२) का यह उल्लेख कि विज्ञानेश्वर 'पुत्र' शब्द से केवल पुत्रों एवं पौत्रों की ओर संकेत करते है, निराधार है।
जिस प्रकार राजा दायादहीनों का अन्तिम उत्तराधिकारी है और सभी अल्पवयस्कों का अभिभावक है, उसी प्रकार वह (सम्बन्धियों से हीन) व्यक्ति के श्राद्ध-सम्पादन में पुत्र के सदृश है।
_अब हम धाड-काल के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में देख लिया है कि शतपथ ब्राह्मण के बहुत पहले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञों की व्यवस्था थी, यथा-भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ। श० ब्रा० एवं तै० आ० (२०१०) ने आगे कहा है कि वह आह्निक यज्ञ जिसमें पितरों को स्वधा (भोजन) एवं जल दिया जाता है, पितृयज्ञ कहलाता है। मनु (३।७०) ने पितृयज्ञ को तर्पण (जल से पूर्वजों की संतुष्टि) करना कहा है। मनु (३।८३) ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक गृहस्थ को प्रति दिन भोजन या जल या दूध, मूल एवं फल के साथ श्राद्ध करना चाहिए और पितरों को सन्तोष देना चाहिए। प्रारम्भिक रूप में श्राद्ध पितरों के लिए अमावास्या के दिन किया जाता था (गौतम १५।१-२)। अमावास्या दो प्रकार की होती हैं; सिनीवाली एवं कुहू । आहिताग्नि (अग्निहोत्री) सिनीवाली में श्राद्ध करते हैं, तथा इनसे भिन्न एवं शूद्र लोग कुहू अमावास्या में श्राद्ध करते हैं।
श्राद्ध (या सभी कृत्य) तीन कोटियों में विभाजित किये गये हैं; नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। वह श्राद्ध नित्य कहलाता है जिसके लिए ऐसी व्यवस्था दी हुई हो कि वह किसी निश्चित अवसर पर किया जाय (यथाआह्निक , अमावास्या के दिन वाला या अष्टका के दिन वाला)। जो ऐसे अवसर पर किया जाय जो अनिश्चित-सा हो, यथा-पुत्रोत्पत्ति आदि पर, उसे नैमित्तिक कहा जाता है। जो किसी विशिष्ट फल के लिए किया जाय उसे काम्य कहते हैं; यथा स्वर्ग, संतति आदि की प्राप्ति के लिए कृत्तिका या रोहिणी पर किया गया श्राद्ध। पञ्चमहायज्ञ कृत्य, जिनमें पितृयज्ञ भी सम्मिलित है, नित्य कहे जाते हैं, अर्थात् उन्हें बिना किसी फल की आशा से करना चाहिए, उनके न करने से पाप लगता है। नित्य कर्मों के करने से प्राप्त फल की जो चर्चा धर्मशास्त्रों में मिलती है वह केवल प्रशंसा मात्र है, उससे केवल यही व्यक्त होता है कि इन कर्मों के सम्पादन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, किन्तु ऐसा नहीं है कि वे अपरिहार्य नहीं हैं और उनका सम्पादन तभी होता है जब व्यक्ति किसी विशिष्ट फल की आशा रखता है (अर्थात् इन कर्मों का सम्पादन काम्य अथवा इच्छाजनित नहीं है)। आप० ध० स० (२७।१६।४-७) ने श्राद्ध के लिए निश्चित कालों की व्यवस्था दी है, यथा-इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हो जाना चाहिए, अपराह्ण को श्रेष्ठता मिलनी चाहिए और पक्ष के आरम्भिक दिनों की अपेक्षा अन्तिम दिनों को अधिक महत्त्व देना चाहिए। गौतम (१५।३)
www.jainelibrary.org
For Private & Personal Use Only
Jain Education International