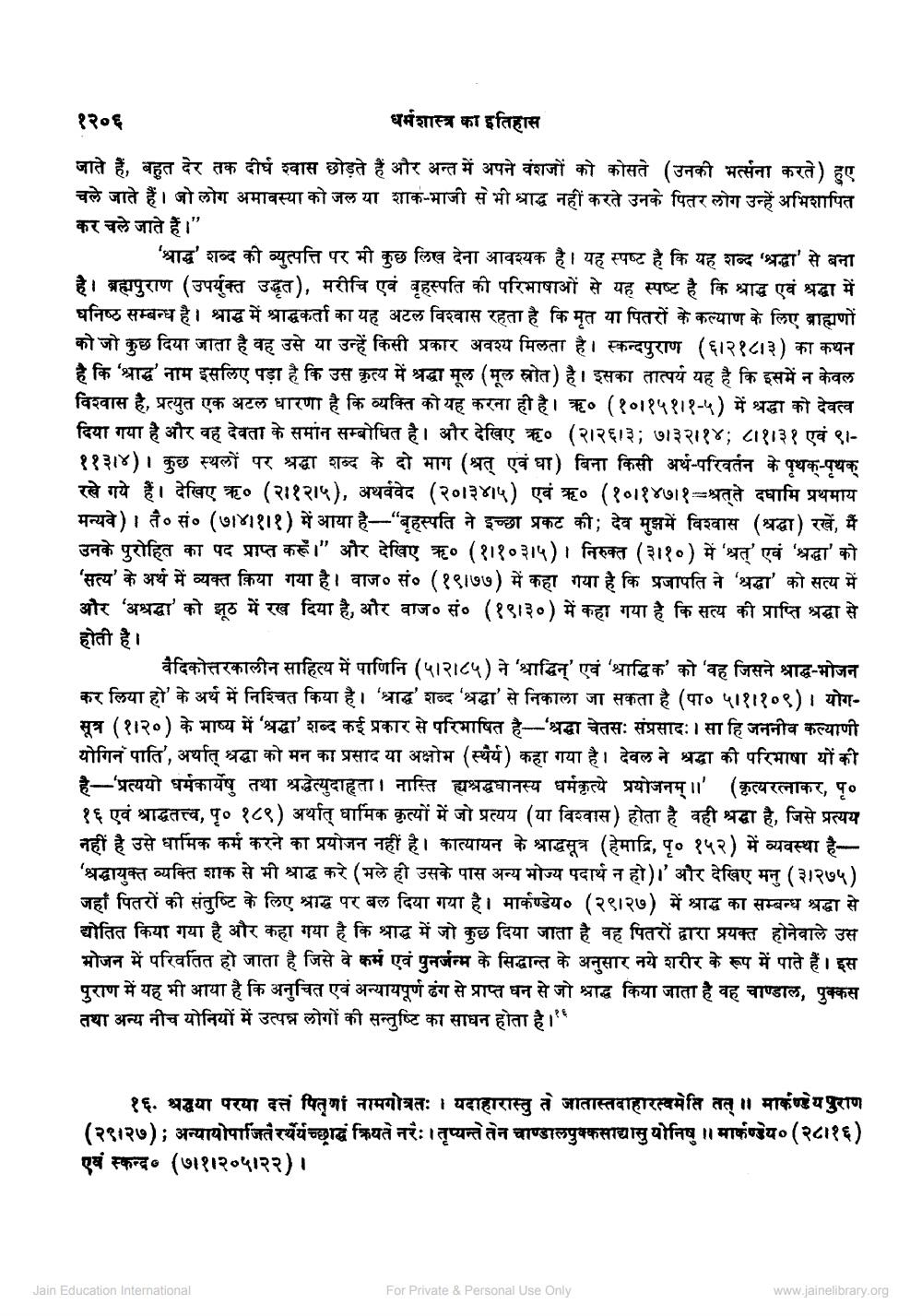________________
१२०६
धर्मशास्त्र का इतिहास
जाते हैं, बहुत देर तक दीर्घ श्वास छोड़ते हैं और अन्त में अपने वंशजों को कोसते (उनकी भर्त्सना करते हुए चले जाते हैं। जो लोग अमावस्या को जल या शाक-भाजी से भी श्राद्ध नहीं करते उनके पितर लोग उन्हें अभिशापित कर चले जाते हैं।"
'श्राद्ध' शब्द की व्युत्पत्ति पर भी कुछ लिख देना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि यह शब्द 'श्रद्धा' से बना है। ब्रह्मपुराण (उपर्युक्त उद्धृत), मरीचि एवं बृहस्पति की परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि श्राद्ध एवं श्रद्धा में घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्राद्ध में श्राद्धकर्ता का यह अटल विश्वास रहता है कि मृत या पितरों के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को जो कुछ दिया जाता है वह उसे या उन्हें किसी प्रकार अवश्य मिलता है। स्कन्दपुराण (६।२१८१३) का कथन है कि 'श्राद्ध' नाम इसलिए पड़ा है कि उस कृत्य में श्रद्धा मूल (मूल स्रोत) है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें न केवल विश्वास है, प्रत्युत एक अटल धारणा है कि व्यक्ति को यह करना ही है। ऋ० (१०।१५१४१-५) में श्रद्धा को देवत्व दिया गया है और वह देवता के समान सम्बोधित है। और देखिए ऋ० (२।२६।३; ७।३२॥१४; ८1१।३१ एवं ९।११३।४)। कुछ स्थलों पर श्रद्धा शब्द के दो भाग (श्रत् एवं धा) बिना किसी अर्थ-परिवर्तन के पृथक्-पृथक् रखे गये हैं। देखिए ऋ० (२।१२।५), अथर्ववेद (२०१३४१५) एवं ऋ० (१०।१४७।१-श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवे)। तै० सं० (७।४।१।१) में आया है-“बृहस्पति ने इच्छा प्रकट की; देव मुझमें विश्वास (श्रद्धा) रखें, मैं उनके पुरोहित का पद प्राप्त करूँ।" और देखिए ऋ० (१।१०३।५)। निरुक्त (३।१०) में 'श्रत्' एवं 'श्रद्धा' को 'सत्य' के अर्थ में व्यक्त किया गया है। वाज० सं० (१९।७७) में कहा गया है कि प्रजापति ने 'श्रद्धा' को सत्य में
और 'अश्रद्धा' को झूठ में रख दिया है, और वाज० सं० (१९।३०) में कहा गया है कि सत्य की प्राप्ति श्रद्धा से होती है।
वैदिकोत्तरकालीन साहित्य में पाणिनि (५।२।८५) ने 'श्राद्धिन्' एवं 'श्राद्धिक' को 'वह जिसने श्राद्ध-भोजन कर लिया हो' के अर्थ में निश्चित किया है। 'श्राद्ध' शब्द 'श्रद्धा' से निकाला जा सकता है (पा० ५।१११०९)। योगसूत्र (२२०) के भाष्य में 'श्रद्धा' शब्द कई प्रकार से परिभाषित है-'श्रद्धा चेतसः संप्रसादः । सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति', अर्थात् श्रद्धा को मन का प्रसाद या अक्षोभ (स्थैर्य) कहा गया है। देवल ने श्रद्धा की परिभाषा यों की है-'प्रत्ययो धर्मकार्येषु तथा श्रद्धेत्युदाहृता। नास्ति ह्यश्रद्धधानस्य धर्मकृत्ये प्रयोजनम् ॥' (कृत्यरत्नाकर, पृ० १६ एवं श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) अर्थात् धार्मिक कृत्यों में जो प्रत्यय (या विश्वास) होता है वही श्रद्धा है, जिसे प्रत्यय नहीं है उसे धार्मिक कर्म करने का प्रयोजन नहीं है। कात्यायन के श्राद्धसूत्र (हेमाद्रि, पृ० १५२) में व्यवस्था है'श्रद्धायुक्त व्यक्ति शाक से भी श्राद्ध करे (भले ही उसके पास अन्य भोज्य पदार्थ न हो)।' और देखिए मनु (३।२७५) जहाँ पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध पर बल दिया गया है। मार्कण्डेय० (२९।२७) में श्राद्ध का सम्बन्ध श्रद्धा से द्योतित किया गया है और कहा गया है कि श्राद्ध में जो कुछ दिया जाता है वह पितरों द्वारा प्रयक्त होनेवाले उस भोजन में परिवर्तित हो जाता है जिसे वे कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार नये शरीर के रूप में पाते हैं। इस पुराण में यह भी आया है कि अनुचित एवं अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त धन से जो श्राद्ध किया जाता है वह चाण्डाल, पुक्कस तथा अन्य नीच योनियों में उत्पन्न लोगों की सन्तुष्टि का साधन होता है।
१६. श्रद्धया परया दत्तं पितृमां नामगोत्रतः । यदाहारास्तु ते जातास्तवाहारस्वमेति तत् ॥ मार्कण्डेय पुराण (२९।२७); अन्यायोपाजित रथैर्यच्छ्राद्धं क्रियते नरैः। तृप्यन्ते तेन चाण्डालपुक्कसाधासु योनिषु ॥मार्कण्डेय० (२८।१६) एवं स्कन्द० (७१२२०५।२२)।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org