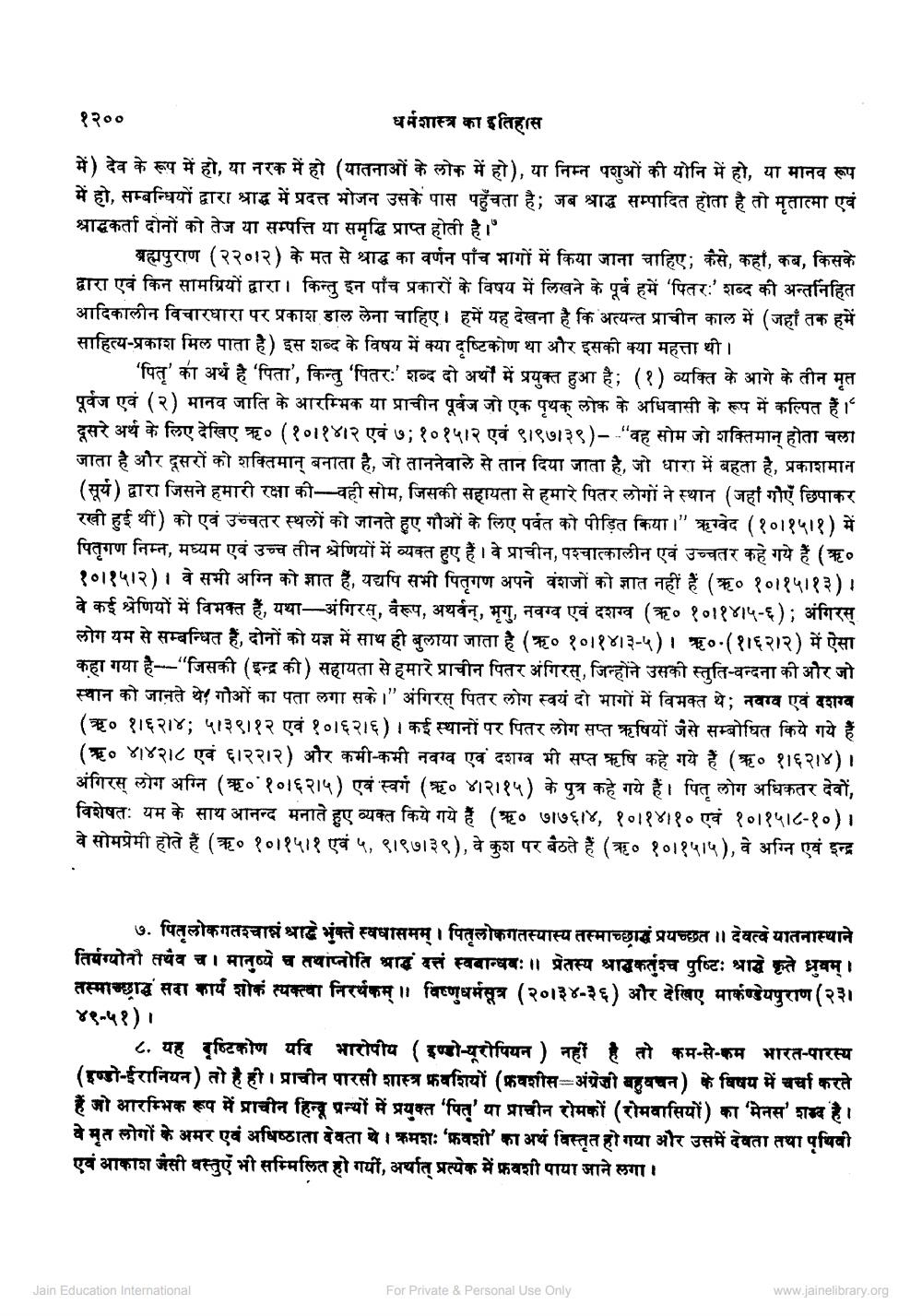________________
१२००
धर्मशास्त्र का इतिहास
में) देव के रूप में हो, या नरक में हो (यातनाओं के लोक में हो), या निम्न पशुओं की योनि में हो, या मानव रूप में हो, सम्बन्धियों द्वारा श्राद्ध में प्रदत्त भोजन उसके पास पहुँचता है; जब श्राद्ध सम्पादित होता है तो मृतात्मा एवं श्राद्धकर्ता दोनों को तेज या सम्पत्ति य
ब्रह्मपुराण (२२०१२) के मत से श्राद्ध का वर्णन पाँच भागों में किया जाना चाहिए; कैसे, कहाँ, कब, किसके द्वारा एवं किन सामग्रियों द्वारा। किन्तु इन पाँच प्रकारों के विषय में लिखने के पूर्व हमें 'पितरः' शब्द की अन्तर्निहित आदिकालीन विचारधारा पर प्रकाश डाल लेना चाहिए। हमें यह देखना है कि अत्यन्त प्राचीन काल में (जहाँ तक हमें साहित्य-प्रकाश मिल पाता है) इस शब्द के विषय में क्या दृष्टिकोण था और इसकी क्या महत्ता थी।
'पितृ' का अर्थ है 'पिता', किन्तु 'पितरः' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है; (१) व्यक्ति के आगे के तीन मृत पूर्वज एवं (२) मानव जाति के आरम्भिक या प्राचीन पूर्वज जो एक पृथक् लोक के अधिवासी के रूप में कल्पित हैं।' दूसरे अर्थ के लिए देखिए ऋ० (१०।१४१२ एवं ७; १०१५।२ एवं ९।९७।३९)- "वह सोम जो शक्तिमान् होता चला जाता है और दूसरों को शक्तिमान् बनाता है, जो ताननेवाले से तान दिया जाता है, जो धारा में बहता है, प्रकाशमान (सूर्य) द्वारा जिसने हमारी रक्षा की वही सोम, जिसकी सहायता से हमारे पितर लोगों ने स्थान (जहाँ गौएँ छिपाकर रखी हुई थीं) को एवं उच्चतर स्थलों को जानते हुए गौओं के लिए पर्वत को पीड़ित किया।" ऋग्वेद (१०।१५।१) में पितृगण निम्न, मध्यम एवं उच्च तीन श्रेणियों में व्यक्त हुए हैं। वे प्राचीन, पश्चात्कालीन एवं उच्चतर कहे गये हैं (ऋ० १०।१५।२)। वे सभी अग्नि को ज्ञात हैं, यद्यपि सभी पितृगण अपने वंशजों को ज्ञात नहीं हैं (ऋ० १०.१५।१३)। वे कई श्रेणियों में विभक्त हैं, यथा-अंगिरस्, वैरूप, अथर्वन्, भृगु, नवग्व एवं दशग्व (ऋ० १०११४१५-६); अंगिरस् लोग यम से सम्बन्धित हैं, दोनों को यज्ञ में साथ ही बुलाया जाता है (ऋ० १०।१४।३-५)। ऋ० (११६२।२) में ऐसा कहा गया है---"जिसकी (इन्द्र की) सहायता से हमारे प्राचीन पितर अंगिरस्, जिन्होंने उसकी स्तुति-वन्दना की और जो स्थान को जानते थे, गौओं का पता लगा सके।" अंगिरस पितर लोग स्वयं दो भागों में विभक्त थे; नवग्व एवं दशग्व (ऋ० ११६२।४, ५।३९।१२ एवं १०।६२।६)। कई स्थानों पर पितर लोग सप्त ऋषियों जैसे सम्बोधित किये गये हैं (ऋ० ४।४२१८ एवं ६।२२।२) और कमी-कमी नवग्व एवं दशग्व भी सप्त ऋषि कहे गये हैं (ऋ० ११६२।४)। अंगिरस् लोग अग्नि (ऋ० १०॥६२।५) एवं स्वर्ग (ऋ० ४।२।१५) के पुत्र कहे गये हैं। पितृ लोग अधिकतर देवों, विशेषतः यम के साथ आनन्द मनाते हुए व्यक्त किये गये हैं (ऋ० ७७६।४, १०।१४।१० एवं १०।१५।८-१०)। वे सोमप्रेमी होते हैं (ऋ० १०।१५।१ एवं ५, ९।९७।३९), वे कुश पर बैठते हैं (ऋ० १०।१५।५), वे अग्नि एवं इन्द्र
७. पितृलोकगतश्चानं श्राद्धे भुंक्ते स्वधासमम् । पितृलोकगतस्यास्य तस्माच्छादं प्रयच्छत ॥ देवत्वे यातनास्थाने तिर्यग्योनौ तथैव च । मानुष्ये च तथाप्नोति श्राद्धं दत्तं स्वबान्धवः॥ प्रेतस्य श्रारकर्तुश्च पुष्टिः श्राखे कृते ध्रुवम् । तस्माच्छावं सदा कार्य शोकं त्यक्त्वा निरर्थकम् ॥ विष्णुधर्मसूत्र (२०१३४-३६) और देखिए मार्कण्डेयपुराण (२३॥ ४९-५१)।
८. यह दृष्टिकोण यदि भारोपीय (इण्डो-यूरोपियन ) नहीं है तो कम-से-कम भारत-पारस्य (इण्डो-ईरानियन) तो है ही। प्राचीन पारसी शास्त्र वशियों (वशीस अंग्रेजी बहुवचन) के विषय में चर्चा करते हैं जो आरम्भिक रूप में प्राचीन हिन्दू प्रन्यों में प्रयुक्त 'पित' या प्राचीन रोमकों (रोमवासियों) का मेनस' शब्द है। वे मृत लोगों के अमर एवं अधिष्ठाता देवता थे। क्रमशः 'झवशी' का अर्थ विस्तृत हो गया और उसमें देवता तथा पृथिवी एवं आकाश जैसी वस्तुएँ भी सम्मिलित हो गयीं, अर्थात् प्रत्येक में फवशी पाया जाने लगा।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org