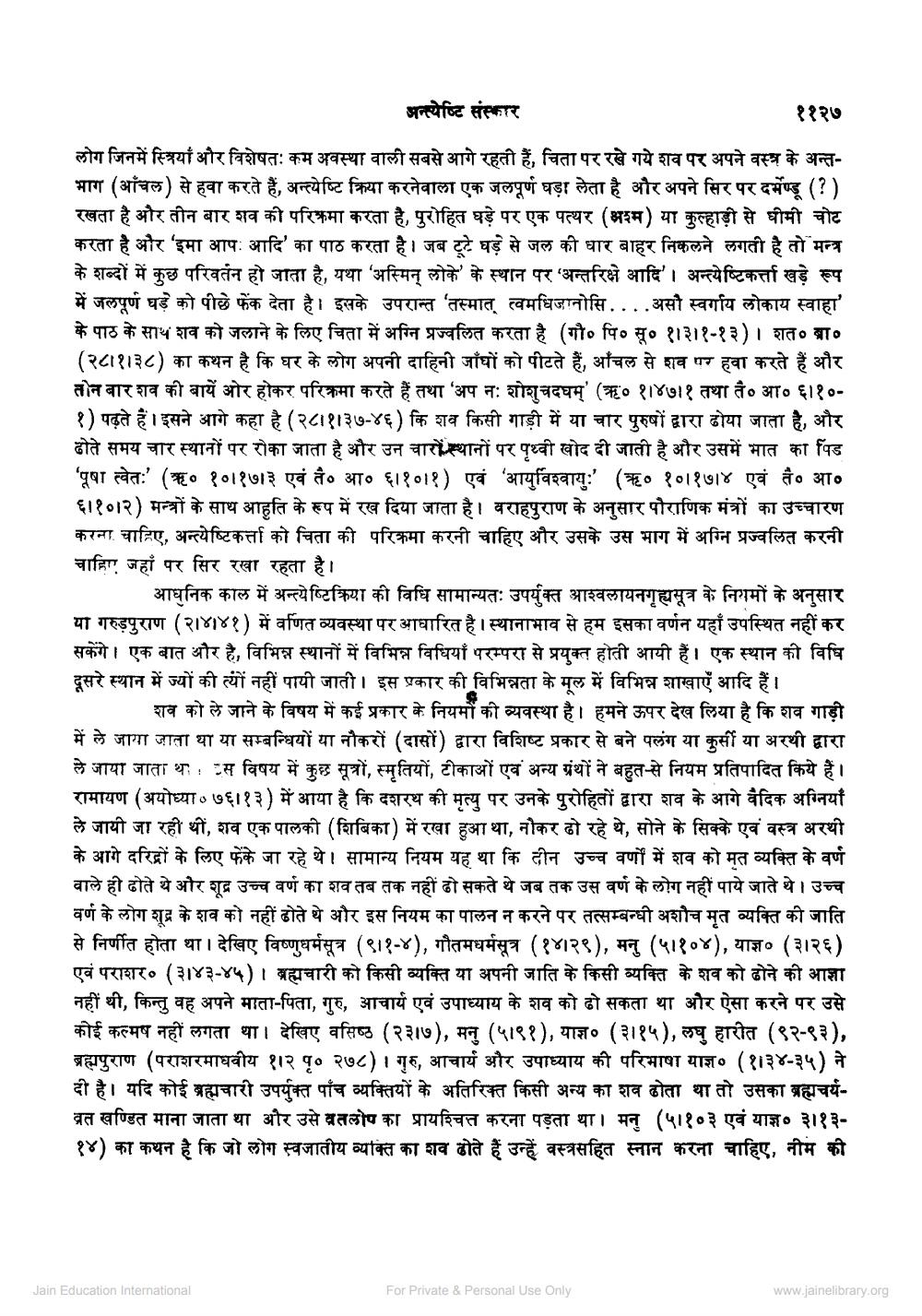________________
अन्त्येष्टि संस्कार
११२७
लोग जिनमें स्त्रियाँ और विशेषतः कम अवस्था वाली सबसे आगे रहती हैं, चिता पर रखे गये शव पर अपने वस्त्र के अन्तभाग (आँचल) से हवा करते हैं, अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाला एक जलपूर्ण घड़ा लेता है और अपने सिर पर दर्भण्डू (?) रखता है और तीन बार शव की परिक्रमा करता है, पुरोहित घड़े पर एक पत्थर (अश्म) या कुल्हाड़ी से धीमी चोट करता है और 'इमा आपः आदि' का पाठ करता है। जब टूटे घड़े से जल की धार बाहर निकलने लगती है तो मन्त्र के शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, यथा 'अस्मिन् लोके' के स्थान पर 'अन्तरिक्षे आदि'। अन्त्येष्टिकर्ता खड़े रूप में जलपूर्ण घड़े को पीछे फेंक देता है। इसके उपरान्त 'तस्मात् त्वमधिजातोसि....असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा'
ठ के साथ शव को जलाने के लिए चिता में अग्नि प्रज्वलित करता है (गौ० पि० सू०१॥३॥१-१३)। शत० ब्रा० (२८।१।३८) का कथन है कि घर के लोग अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं, आँचल से शव पर हवा करते हैं और तोन बार शव की बायें ओर होकर परिक्रमा करते हैं तथा 'अप नः शोशुचदघम्' (ऋ० ११४७।१ तथा ते० आ०६।१०१) पढ़ते हैं। इसने आगे कहा है (२८११३७-४६) कि शव किसी गाड़ी में या चार पुरुषों द्वारा ढोय ढोते समय चार स्थानों पर रोका जाता है और उन चारों स्थानों पर पृथ्वी खोद दी जाती है और उसमें भात का पिंड 'पूषा त्वेतः' (ऋ० १०।१७।३ एवं तै० आ० ६।१०।१) एवं 'आयुर्विश्वायुः' (ऋ० १०।१७।४ एवं तै० आ० ६।१०।२) मन्त्रों के साथ आहुति के रूप में रख दिया जाता है। वराहपुराण के अनुसार पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, अन्त्येष्टिकर्ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके उस भाग में अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए जहाँ पर सिर रखा रहता है।
आधुनिक काल में अन्त्येष्टिक्रिया की विधि सामान्यतः उपर्युक्त आश्वलायनगृह्यसूत्र के नियमों के अनुसार या गरुडपुराण (२१४१४१) में वर्णित व्यवस्था पर आधारित है। स्थानाभाव से हम इसका वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे। एक बात और है, विभिन्न स्थानों में विभिन्न विधियाँ परम्परा से प्रयुक्त होती आयी हैं। एक स्थान की विधि दूसरे स्थान में ज्यों की त्यों नहीं पायी जाती। इस प्रकार की विभिन्नता के मूल में विभिन्न शाखाएँ आदि हैं।
शव को ले जाने के विषय में कई प्रकार के नियमों की व्यवस्था है। हमने ऊपर देख लिया है कि शव गाड़ी में ले जाया जाता था या सम्बन्धियों या नौकरों (दासों) द्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग या कुर्सी या अरथी द्वारा ले जाया जाता था। इस विषय में कुछ सूत्रों, स्मृतियों, टीकाओं एवं अन्य ग्रंथों ने बहुत-से नियम प्रतिपादित किये हैं। रामायण (अयोध्या ०७६।१३) में आया है कि दशरथ की मृत्यु पर उनके पुरोहितों द्वारा शव के आगे वैदिक अग्नियाँ ले जायी जा रही थीं, शव एक पालकी (शिबिका) में रखा हुआ था, नौकर ढो रहे थे, सोने के सिक्के एवं वस्त्र अरथी के आगे दरिद्रों के लिए फेंके जा रहे थे। सामान्य नियम यह था कि दीन उच्च वर्गों में शव को मत व्यक्ति के वर्ण वाले ही ढोते थे और शूद्र उच्च वर्ण का शव तब तक नहीं ढो सकते थे जब तक उस वर्ण के लोग नहीं पाये जाते थे। उच्च वर्ण के लोग शूद्र के शव को नहीं ढोते थे और इस नियम का पालन न करने पर तत्सम्बन्धी अशौच मृत व्यक्ति की जाति से निर्णीत होता था। देखिए विष्णुधर्मसूत्र (९।१-४), गौतमधर्मसूत्र (१४।२९), मनु (५।१०४), याज्ञ० (३।२६) एवं पराशर० (३।४३-४५)। ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने की आज्ञा नहीं थी, किन्तु वह अपने माता-पिता, गुरु, आचार्य एवं उपाध्याय के शव को ढो सकता था और ऐसा करने पर उसे कोई कल्मष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (२३६७), मनु (५।९१), याज्ञ० (३।१५), लघु हारीत (९२-९३), ब्रह्मपुराण (पराशरमाधवीय १२ १० २७८) । गुरु, आचार्य और उपाध्याय की परिभाषा याज्ञ० (११३४-३५) ने दी है। यदि कोई ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का शव ढोता था तो उसका ब्रह्मचर्यव्रत खण्डित माना जाता था और उसे बतलोप का प्रायश्चित्त करना पड़ता था। मनु (५।१०३ एवं याज्ञ० ३३१३१४) का कथन है कि जो लोग स्वजातीय व्यक्ति का शव ढोते हैं उन्हें वस्त्रसहित स्नान करना चाहिए, नीम की
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org