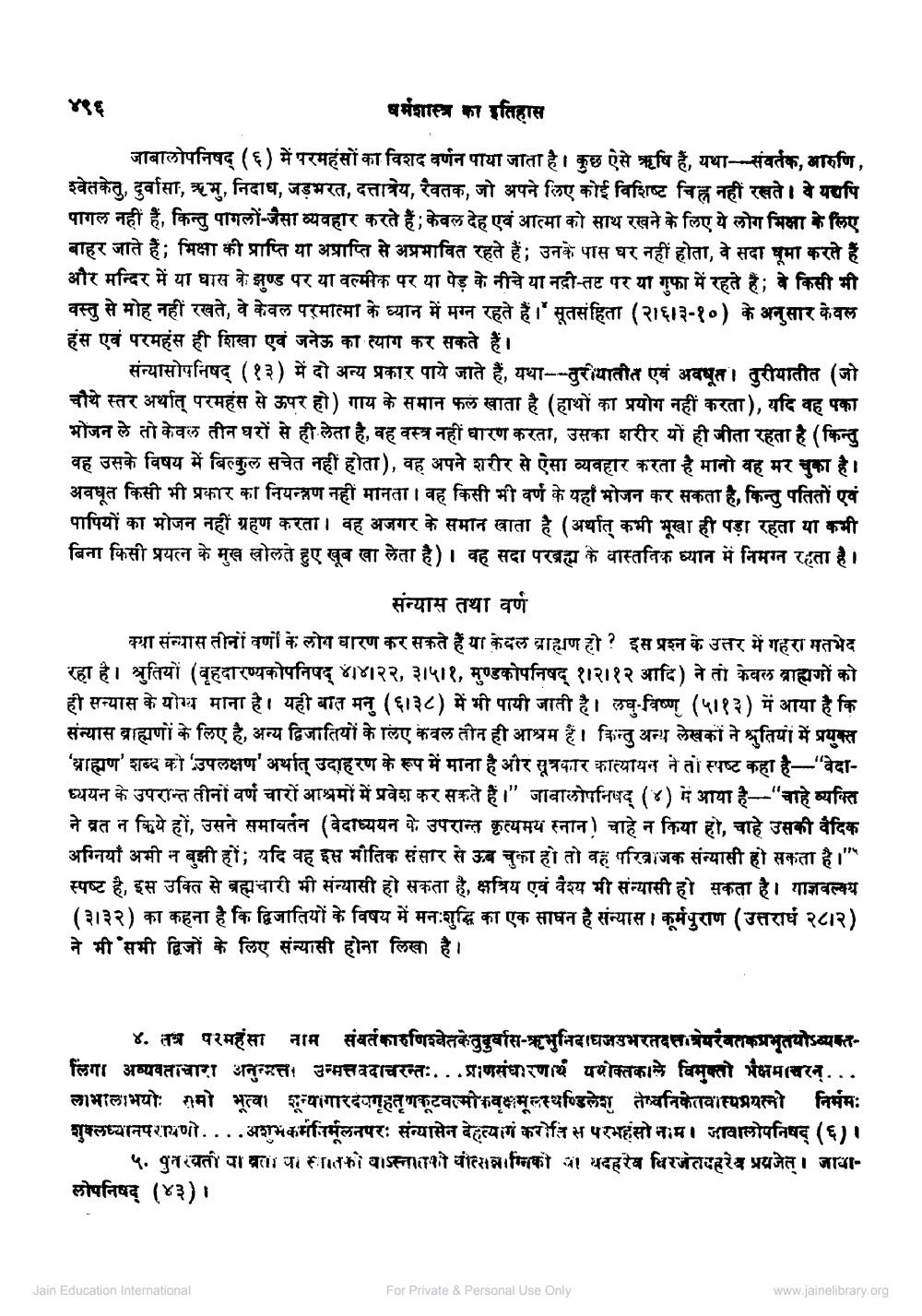________________
धर्मशास्त्र का इतिहास
जाबालोपनिषद् (६) में परमहंसों का विशद वर्णन पाया जाता है। कुछ ऐसे ऋषि हैं, यथा---संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासा ऋभु, निदाघ, जड़भरत, दत्तात्रेय, रैवतक, जो अपने लिए कोई विशिष्ट चिह्न नहीं रखते । वे यद्यपि पागल नहीं हैं, किन्तु पागलों जैसा व्यवहार करते हैं; केवल देह एवं आत्मा को साथ रखने के लिए ये लोग मिक्षा के लिए बाहर जाते हैं; भिक्षा की प्राप्ति या अप्राप्ति से अप्रभावित रहते हैं; उनके पास घर नहीं होता, वे सदा घूमा करते हैं। और मन्दिर में या घास के झुण्ड पर या वल्मीक पर या पेड़ के नीचे या नदी-तष्ट पर या गुफा में रहते हैं; वे किसी भी वस्तु से मोह नहीं रखते, वे केवल परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं । * सूतसंहिता ( २।६।३-१०) के अनुसार केवल हंस एवं परमहंस ही शिखा एवं जनेऊ का त्याग कर सकते हैं।
४९६
संन्यासोपनिषद् (१३) में दो अन्य प्रकार पाये जाते हैं, यथा--- -- तुरीयातीत एवं अवधूत । तुरीयातीत (जो चौथे स्तर अर्थात् परमहंस से ऊपर हो ) गाय के समान फलं खाता है (हाथों का प्रयोग नहीं करता), यदि वह पका भोजन ले तो केवल तीन घरों से ही लेता है, वह वस्त्र नहीं धारण करता, उसका शरीर यों ही जीता रहता है (किन्तु वह उसके विषय में बिल्कुल सचेत नहीं होता), वह अपने शरीर से ऐसा व्यवहार करता है मानो वह मर चुका है। अवधूत किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं मानता। वह किसी भी वर्ण के यहाँ भोजन कर सकता है, किन्तु पतितों एवं पापियों का भोजन नहीं ग्रहण करता। वह अजगर के समान खाता है ( अर्थात् कभी भूखा ही पड़ा रहता था कभी बिना किसी प्रयत्न के मुख खोलते हुए खूब खा लेता है ) । वह सदा परब्रह्म के वास्तविक ध्यान में निमग्न रहता है ।
संन्यास तथा वर्ण
क्या संन्यास तीनों वर्णों के लोग धारण कर सकते हैं या केवल ब्राह्मण हो ? इस प्रश्न के उत्तर में गहरा मतभेद रहा है। श्रुतियों (वृहदारण्यकोपनिषद् ४।४।२२, ३।५।१, मुण्डकोपनिषद् १।२।१२ आदि) ने तो केवल ब्राह्मणों को ही सन्यास के योग्य माना है। यही बात मनु ( ६।३८) में भी पायी जाती है । लघु-विष्णु ( ५1१३ ) में आया है कि संन्यास ब्राह्मणों के लिए है, अन्य द्विजातियों के लिए केवल तीन ही आश्रम हैं । किन्तु अन्य लेखकों ने श्रुतियों में प्रयुक्त 'ब्राह्मण' शब्द को 'उपलक्षण' अर्थात् उदाहरण के रूप में माना है और सूत्रकार कात्यायन ने तो स्पष्ट कहा है-"वेदाध्ययन के उपरान्त तीनों वर्णं चारों आश्रमों में प्रवेश कर सकते हैं।" जाबालोपनिषद् (४) में आया है- " चाहे व्यक्ति
व्रत न किये हों, उसने समावर्तन ( वेदाध्ययन के उपरान्त कृत्यमय स्नान ) चाहे न किया हो, चाहे उसकी वैदिक afrat अभी नबुझी हों; यदि वह इस भौतिक संसार से ऊब चुका हो तो वह परिव्राजक संन्यासी हो सकता है।"" स्पष्ट है, इस उक्ति से ब्रह्मचारी भी संन्यासी हो सकता है, क्षत्रिय एवं वैश्य भी संन्यासी हो सकता है । याज्ञवल्क्य (३।३२) का कहना है कि द्विजातियों के विषय में मनः शुद्धि का एक साघन है संन्यास । कूर्मपुराण (उत्तरार्ध २८।२ ) ने भी सभी द्विजों के लिए संन्यासी होना लिखा है ।
४. तंत्र परमहंसा नाम संवर्तकारुणिश्वेतकेतुदुर्वास ऋभुनिदाघजउभरतद सः श्रेयश्वतकप्रभृतयोऽव्यक्तलिंगा अव्यक्ताचारा अनुन्मत्तः उन्मत्तवदाचरन्तः प्राणसंधारणार्थ ययोक्तकाले विमुक्तो भैक्षम (चरन्... लाभालाभयोः रामो भूत्वा शून्यागारदेवगृहतृणकूटवल्मीकवृक्षमूलस्थण्डिलेश तेवनिकेतवास्यप्रयत्नो निर्ममः शुक्लध्यानपरायणो अशुभ कर्मनिर्मूलनपरः संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसो नाम । जावालोपनिषद् ( ६ ) । ५. ततीव्रताको वास्नातक वत्सन्नग्निको वा यदहरेव विरजेतदहरेव प्रव्रजेत् । जावालोपनिषद् (४३) ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org