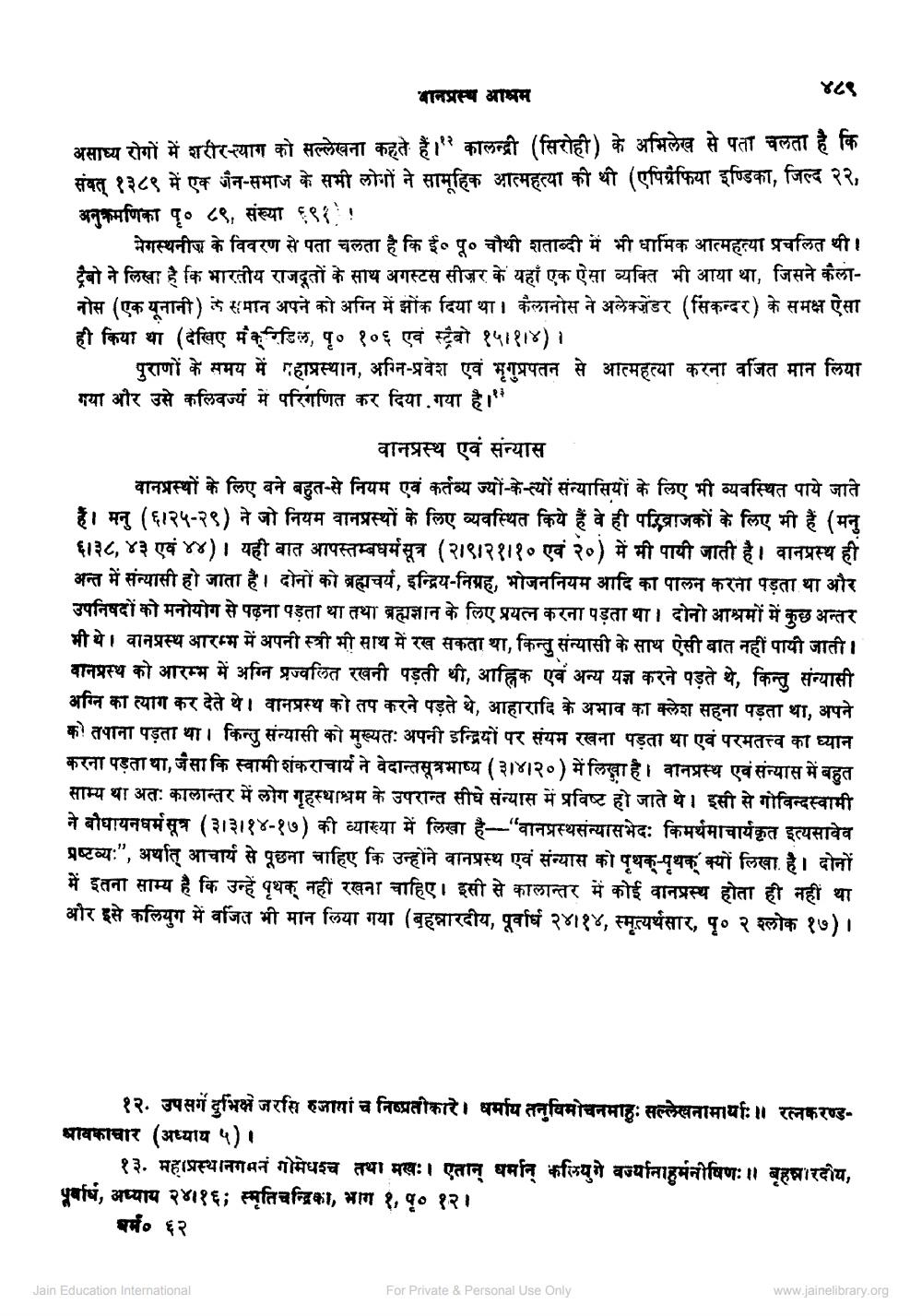________________
४८९
वानप्रस्थ आश्रम
असाध्य रोगों में शरीर त्याग को सल्लेखना कहते हैं।२ कालन्द्री (सिरोही) के अभिलेख से पता चलता है कि संवत् १३८९ में एक जन-समाज के सभी लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की थी (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द २२, अनुक्रमणिका पृ० ८९, संख्या ६९१ ।
मेगस्थनीज के विवरण से पता चलता है कि ई० पू० चौथी शताब्दी में भी धार्मिक आत्महत्या प्रचलित थी। ट्रैबो ने लिखा है कि भारतीय राजदूतों के साथ अगस्टस सीज़र के यहाँ एक ऐसा व्यक्ति भी आया था, जिसने कैलानोस (एक यूनानी) के समान अपने को अग्नि में झोंक दिया था। कैलानोस ने अलेक्जेंडर (सिकन्दर) के समक्ष ऐसा ही किया था (देखिए मरिडिल, पृ० १०६ एवं स्ट्रैबो १५।१।४)।
पुराणों के समय में महाप्रस्थान, अग्नि-प्रवेश एवं भृगुप्रपतन से आत्महत्या करना वजित मान लिया गया और उसे कलिवयं में परिगणित कर दिया. गया है।
वानप्रस्थ एवं संन्यास वानप्रस्थों के लिए बने बहुत-से नियम एवं कर्तव्य ज्यों-के-त्यों संन्यासियों के लिए भी व्यवस्थित पाये जाते हैं। मनु (६।२५-२९) ने जो नियम वानप्रस्थों के लिए व्यवस्थित किये हैं वे ही परिव्राजकों के लिए भी हैं (मनु ६॥३८, ४३ एवं ४४)। यही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।९।२१।१० एवं २०) में भी पायी जाती है। वानप्रस्थ ही अन्त में संन्यासी हो जाता है। दोनों को ब्रह्मचर्य, इन्द्रिय-निग्रह, भोजननियम आदि का पालन करना पड़ता था और
निषदों को मनोयोग से पढना पडता था तथा ब्रह्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना पड़ता था। दोनो आश्रमों में कुछ अन्तर भी थे। वानप्रस्थ आरम्भ में अपनी स्त्री भी साथ में रख सकता था, किन्तु संन्यासी के साथ ऐसी बात नहीं पायी जाती। वानप्रस्थ को आरम्भ में अग्नि प्रज्वलित रखनी पड़ती थी, आह्निक एवं अन्य यज्ञ करने पड़ते थे, किन्तु संन्यासी अग्नि का त्याग कर देते थे। वानप्रस्थ को तप करने पड़ते थे, आहारादि के अभाव का क्लेश सहना पड़ता था, अपने को तपाना पड़ता था। किन्तु संन्यासी को मुख्यतः अपनी इन्द्रियों पर संयम रखना पड़ता था एवं परमतत्त्व का ध्यान करना पड़ता था, जैसा कि स्वामी शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्रभाष्य (३।४।२०) में लिखा है। वानप्रस्थ एवं संन्यास में बहुत साम्य था अतः कालान्तर में लोग गृहस्थाश्रम के उपरान्त सीधे संन्यास में प्रविष्ट हो जाते थे। इसी से गोविन्दस्वामी ने बौधायनधर्मसूत्र (३।३।१४-१७) की व्याख्या में लिखा है-“वानप्रस्थसंन्यासभेदः किमर्थमाचार्यकृत इत्यसावेव प्रष्टव्यः", अर्थात् आचार्य से पूछना चाहिए कि उन्होंने वानप्रस्थ एवं संन्यास को पृथक्-पृथक् क्यों लिखा है। दोनों में इतना साम्य है कि उन्हें पृथक् नहीं रखना चाहिए। इसी से कालान्तर में कोई वानप्रस्थ होता ही नहीं था और इसे कलियुग में वर्जित भी मान लिया गया (बृहन्नारदीय, पूर्वार्ध २४।१४, स्मृत्यर्थसार, पृ० २ श्लोक १७)।
१२. उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे। धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः॥ रलकरण्डभावकाचार (अध्याय ५)।
१३. महाप्रस्थानगमनं गोमेधश्च तथा मखः। एतान् धर्मान् कलियुगे वानाहुर्मनीषिणः ॥ बृहन्नारदीय, पूर्वार्ष, अध्याय २४३१६; स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, पृ० १२।
धर्म० ६२
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org