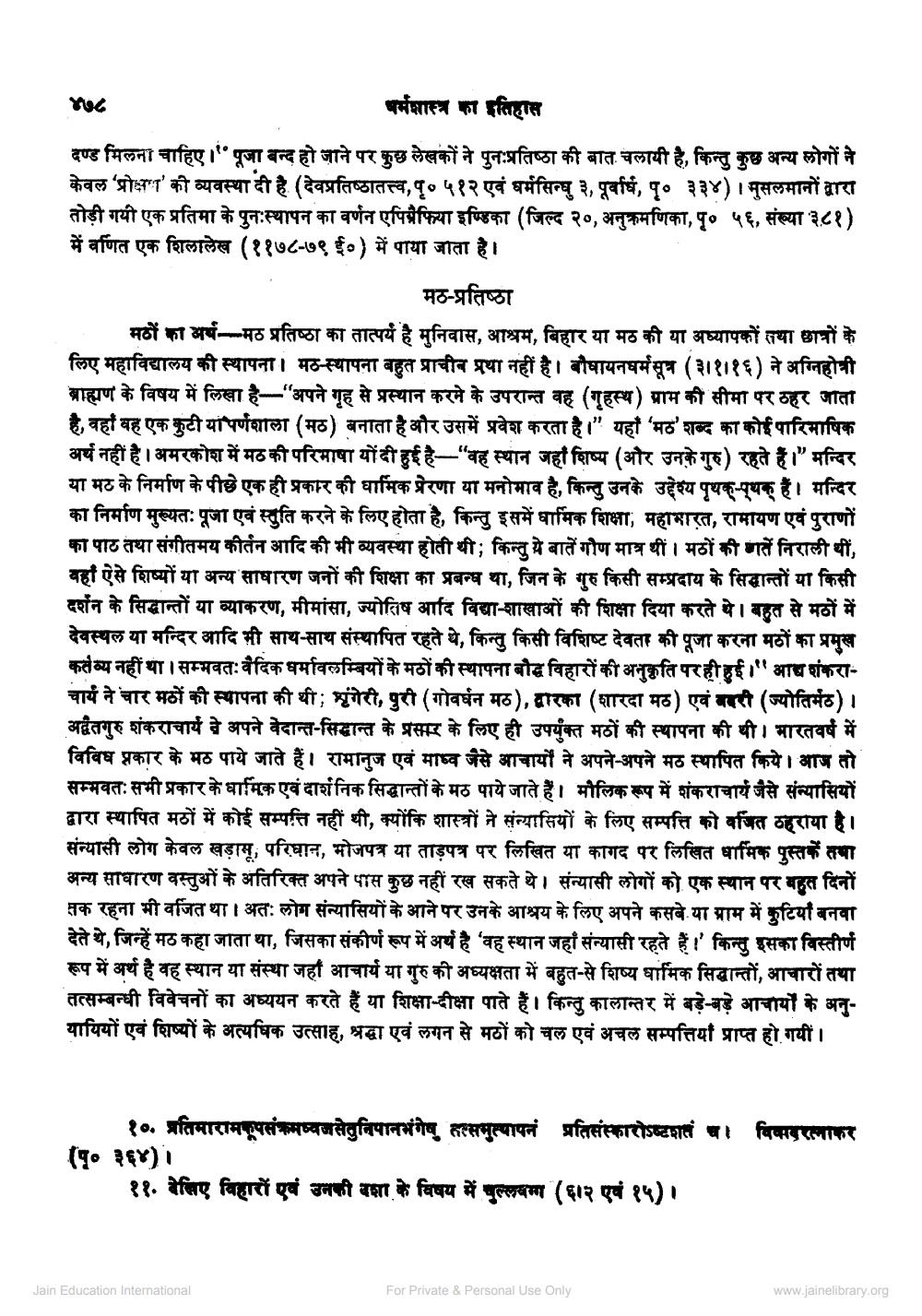________________
१७८
धर्मशास्त्र का इतिहास दण्ड मिलना चाहिए। पूजा बन्द हो जाने पर कुछ लेखकों ने पुनःप्रतिष्ठा की बात चलायी है, किन्तु कुछ अन्य लोगों ने केवल 'प्रोक्षण' की व्यवस्था दी है (देवप्रतिष्ठातत्त्व, पृ० ५१२ एवं धर्मसिन्धु ३, पूर्वार्ष, पृ० ३३४) । मुसलमानों द्वारा तोड़ी गयी एक प्रतिमा के पुनःस्थापन का वर्णन एपिप्रैफिया इण्डिका (जिल्द २०, अनुक्रमणिका, पृ० ५६, संख्या ३.८१) में वर्णित एक शिलालेख (११७८-७९ ई०) में पाया जाता है।
मठ-प्रतिष्ठा मठों का अर्थ-मठ प्रतिष्ठा का तात्पर्य है मुनिवास, आश्रम, बिहार या मठ की या अध्यापकों तथा छात्रों के लिए महाविद्यालय की स्थापना। मठ-स्थापना बहुत प्राचीच प्रथा नहीं है। बौधायनधर्मसूत्र (३।१।१६) ने अग्निहोत्री ब्राह्मण के विषय में लिखा है-"अपने गृह से प्रस्थान करने के उपरान्त वह (गृहस्थ) ग्राम की सीमा पर ठहर जाता है, वहां वह एक कुटी यापर्णशाला (मठ) बनाता है और उसमें प्रवेश करता है।" यहाँ 'मठ' शब्द का कोई पारिभाषिक अर्थ नहीं है । अमरकोश में मठ की परिभाषा योंदी हुई है-"वह स्थान जहाँ शिष्य (और उनके गुरु) रहते हैं।” मन्दिर या मठ के निर्माण के पीछे एक ही प्रकार की धार्मिक प्रेरणा या मनोभाव है, किन्तु उनके उद्देश्य पृथक्-पृथक् हैं। मन्दिर का निर्माण मुख्यतः पूजा एवं स्तुति करने के लिए होता है, किन्तु इसमें धार्मिक शिक्षा, महाभारत, रामायण एवं पुराणों का पाठ तथा संगीतमय कीर्तन आदि की भी व्यवस्था होती थी; किन्तु ये बातें गौण मात्र थीं। मठों की गते निराली थीं, वहां ऐसे शिष्यों या अन्य साधारण जनों की शिक्षा का प्रबन्ध था, जिन के गुरु किसी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों या किसी दर्शन के सिद्धान्तों या व्याकरण, मीमांसा, ज्योतिष आदि विद्या-शाखाओं की शिक्षा दिया करते थे। बहुत से मठों में देवस्थल या मन्दिर आदि भी साथ-साथ संस्थापित रहते थे, किन्तु किसी विशिष्ट देवता की पूजा करना मठों का प्रमुख कर्तव्य नहीं था। सम्भवतःवैदिक धर्मावलम्बियों के मठों की स्थापना बौद्ध विहारों की अनुकृति परहीहुई।" आद्य शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी; शृंगेरी, पुरी (गोवर्धन मठ), द्वारका (शारदा मठ) एवं बबरी (ज्योतिर्मठ)। अद्वैतगुरु शंकराचार्य ने अपने वेदान्त-सिद्धान्त के प्रसार के लिए ही उपर्युक्त मठों की स्थापना की थी। भारतवर्ष में विविध प्रकार के मठ पाये जाते हैं। रामानुज एवं माध्व जैसे आचार्यों ने अपने-अपने मठ स्थापित किये। आज तो सम्भवतः सभी प्रकार के धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तों के मठ पाये जाते हैं। मौलिक रूप में शंकराचार्य जैसे संन्यासियों द्वारा स्थापित मठों में कोई सम्पत्ति नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों ने संन्यासियों के लिए सम्पत्ति को वर्जित ठहराया है। संन्यासी लोग केवल खड़ामू, परिधान, भोजपत्र या ताड़पत्र पर लिखित या कागद पर लिखित धार्मिक पुस्तकें तथा अन्य साधारण वस्तुओं के अतिरिक्त अपने पास कुछ नहीं रख सकते थे। संन्यासी लोगों को एक स्थान पर बहत दिनों तक रहना भी वर्जित था। अतः लोग संन्यासियों के आने पर उनके आश्रय के लिए अपने कसबे या ग्राम में कुटियां बनवा देते थे, जिन्हें मठ कहा जाता था, जिसका संकीर्ण रूप में अर्थ है 'वह स्थान जहाँ संन्यासी रहते हैं। किन्तु इसका विस्तीर्ण रूप में अर्थ है वह स्थान या संस्था जहाँ आचार्य या गुरु की अध्यक्षता में बहुत-से शिष्य धार्मिक सिद्धान्तों, आचारों तथा तत्सम्बन्धी विवेचनों का अध्ययन करते हैं या शिक्षा-दीक्षा पाते हैं। किन्तु कालान्तर में बड़े-बड़े आचार्यों के अनुयायियों एवं शिष्यों के अत्यधिक उत्साह, श्रद्धा एवं लगन से मठों को चल एवं अचल सम्पत्तियां प्राप्त हो गयीं।
१०. प्रतिमारामकूपसंक्रमध्वजसेतुनिपानभंगेषु तत्समुत्थापनं प्रतिसंस्कारोऽष्टशतं च। विवादरत्नाकर (पृ. ३६४)।
११. बेलिए विहारों एवं उनकी बशा के विषय में बुल्लबग्ग (६।२ एवं १५)।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org