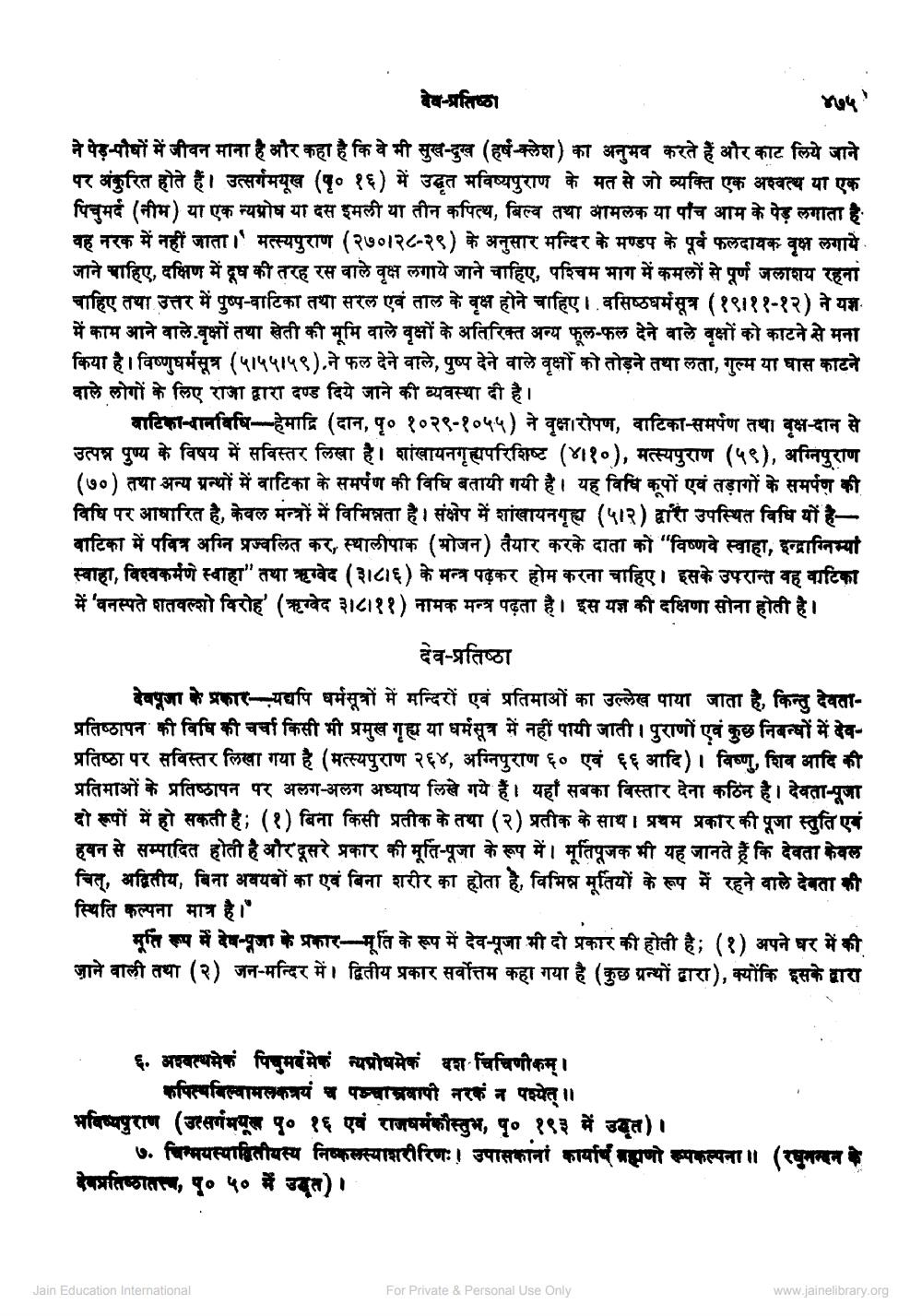________________
देव-प्रतिष्ठा
४७५
पेड़-पौधों में जीवन माना है और कहा है कि वे भी सुख-दुख (हर्ष -क्लेश) का अनुभव करते हैं और काट लिये जाने पर अंकुरित होते हैं । उत्सर्गमयूख ( पृ० १६ ) में उद्धृत भविष्यपुराण के मत से जो व्यक्ति एक अश्वत्थ या एक पिचुमर्द (नीम) या एक न्यप्रोष या दस इमली या तीन कपित्थ, बिल्व तथा आमलक या पाँच आम के पेड़ लगाता है. वह नरक में नहीं जाता।' मत्स्यपुराण (२७०।२८-२९ ) के अनुसार मन्दिर के मण्डप के पूर्व फलदायक वृक्ष लगाये. जाने चाहिए, दक्षिण में दूध की तरह रस वाले वृक्ष लगाये जाने चाहिए, पश्चिम भाग में कमलों से पूर्ण जलाशय रहना चाहिए तथा उत्तर में पुष्प वाटिका तथा सरल एवं ताल के वृक्ष होने चाहिए । वसिष्ठधर्मसूत्र ( १९।११-१२ ) ने यज्ञआने वाले वृक्ष तथा खेती की भूमि वाले वृक्षों के अतिरिक्त अन्य फूल-फल देने वाले वृक्षों को काटने से मना किया है। विष्णुधर्मसूत्र (५।५५/५९). ने फल देने वाले, पुष्प देने वाले वृक्षों को तोड़ने तथा लता, गुल्म या घास काटने वाले लोगों के लिए राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की व्यवस्था दी है।
वाटिका - वानविधि - हेमाद्रि (दान, पृ० १०२९-१०५५) ने वृक्षारोपण, वाटिका - समर्पण तथा वृक्ष-दान से उत्पन्न पुण्य के विषय में सविस्तर लिखा है। शांखायनगृह्यपरिशिष्ट (४११० ), मत्स्यपुराण (५९), अग्निपुराण ( ७० ) तथा अन्य ग्रन्थों में वाटिका के समर्पण की विधि बतायी गयी है। यह विधि कूपों एवं तड़ागों के समर्पण की विधि पर आधारित है, केवल मन्त्रों में विभिन्नता है। संक्षेप में शांखायन गृह्य (५।२) द्वारा उपस्थित विधि यों हैवाटिका में पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर, स्थालीपाक (भोजन) तैयार करके दाता को "विष्णवे स्वाहा, इन्द्राग्निभ्यां स्वाहा, विश्वकर्मणे स्वाहा” तथा ऋग्वेद (३२८२६ ) के मन्त्र पढ़कर होम करना चाहिए। इसके उपरान्त वह वाटिका में 'वनस्पते शतवल्शो विरोह' (ऋग्वेद ३।८।११) नामक मन्त्र पढ़ता है। इस यज्ञ की दक्षिणा सोना होती है।
देव-प्रतिष्ठा
देवपूजा के प्रकार यद्यपि धर्मसूत्रों में मन्दिरों एवं प्रतिमाओं का उल्लेख पाया जाता है, किन्तु देवताप्रतिष्ठापन की विधि की चर्चा किसी भी प्रमुख गृह्य या धर्मसूत्र में नहीं पायी जाती। पुराणों एवं कुछ निबन्धों में देवप्रतिष्ठा पर सविस्तर लिखा गया है (मत्स्यपुराण २६४, अग्निपुराण ६० एवं ६६ आदि) । विष्णु, शिव आदि की प्रतिमाओं के प्रतिष्ठापन पर अलग-अलग अध्याय लिखे गये हैं। यहाँ सबका विस्तार देना कठिन है । देवता-पूजा दो रूपों में हो सकती है; (१) बिना किसी प्रतीक के तथा (२) प्रतीक के साथ । प्रथम प्रकार की पूजा स्तुति एवं हवन से सम्पादित होती है ओर दूसरे प्रकार की मूर्ति पूजा के रूप में। मूर्तिपूजक भी यह जानते हैं कि देवता केवल चित्, अद्वितीय, बिना अवयवों का एवं बिना शरीर का होता है, विभिन्न मूर्तियों के रूप में रहने वाले देवता की स्थिति कल्पना मात्र है।
मूर्ति रूप में देव पूजा के प्रकार-मूर्ति के रूप में देव-पूजा भी दो प्रकार की होती है; (१) अपने घर में की जाने वाली तथा (२) जन-मन्दिर में । द्वितीय प्रकार सर्वोत्तम कहा गया है (कुछ ग्रन्थों द्वारा ), क्योंकि इसके द्वारा
६. अश्वत्थमेकं पिचुमर्वमेकं न्यप्रोषमेकं दश - चिचिणीकम् । कपित्थबिल्वामलकत्रयं च पञ्चानवापी नरकं न पश्येत् ॥
भविष्यपुराण ( उत्सर्गमयूल ५० १६ एवं राजधर्मकौस्तुभ, पृ० १९३ में उद्धृत ) ।
७. चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः । उपासकानां कार्यां ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ ( रघुनन्दन के देवप्रतिष्ठातत्त्व, पु० ५० में उबूत) ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org