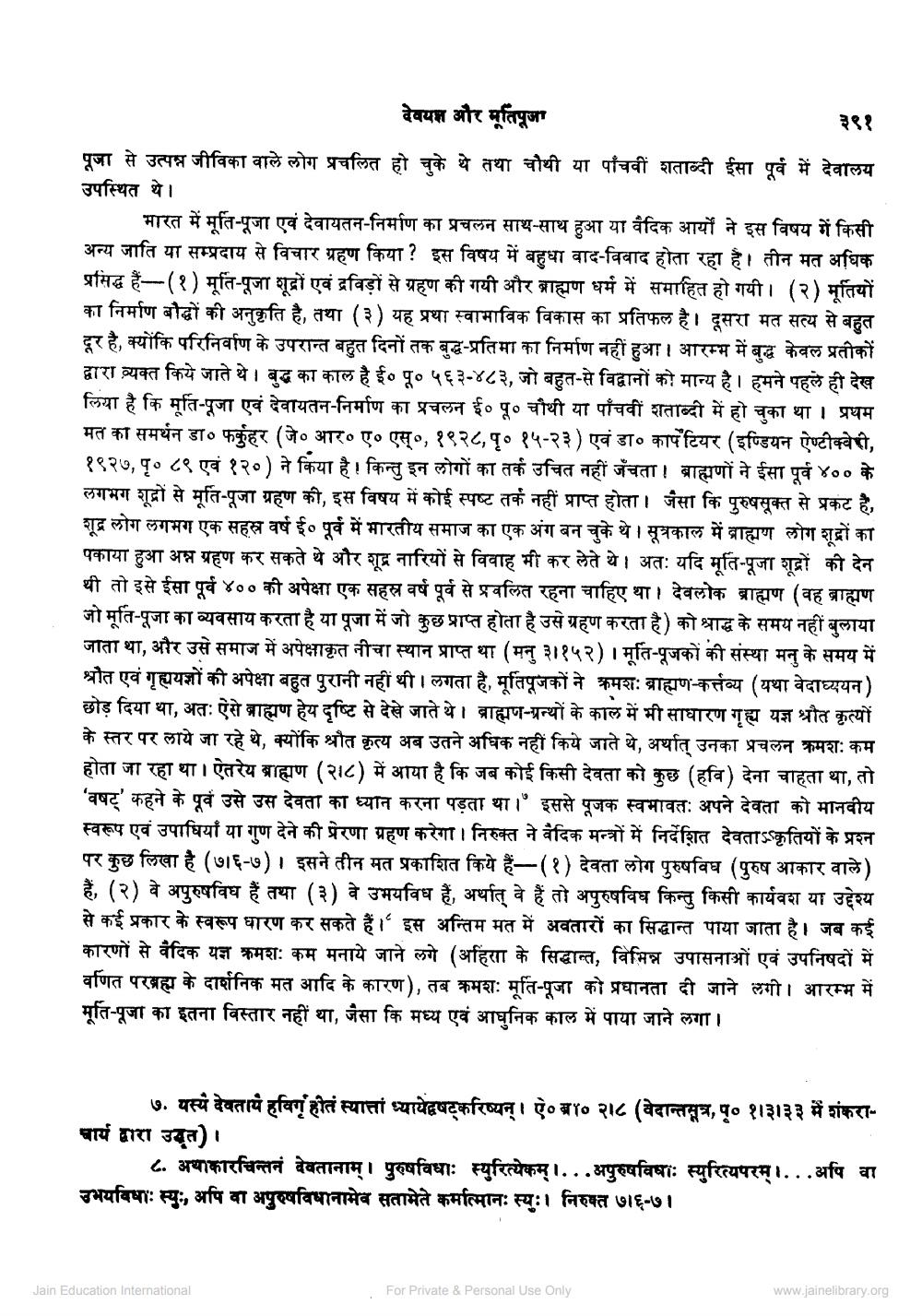________________
देवयज्ञ और मूर्तिपूजा
३९१
पूजा से उत्पन्न जीविका वाले लोग प्रचलित हो चुके थे तथा चौथी या पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में देवालय उपस्थित थे।
भारत में मूर्ति पूजा एवं देवायतन- निर्माण का प्रचलन साथ- साथ हुआ या वैदिक आर्यों ने इस विषय में किसी अन्य जाति या सम्प्रदाय से विचार ग्रहण किया ? इस विषय में बहुधा वाद-विवाद होता रहा है। तीन मत अधिक प्रसिद्ध हैं - ( १ ) मूर्ति-पूजा शूद्रों एवं द्रविड़ों से ग्रहण की गयी और ब्राह्मण धर्म में समाहित हो गयी । ( २ ) मूर्तियों का निर्माण बौद्धों की अनुकृति है, तथा ( ३ ) यह प्रथा स्वाभाविक विकास का प्रतिफल है। दूसरा मत सत्य से बहुत दूर है, क्योंकि परिनिर्वाण के उपरान्त बहुत दिनों तक बुद्ध प्रतिमा का निर्माण नहीं हुआ। आरम्भ में बुद्ध केवल प्रतीकों द्वारा व्यक्त किये जाते थे । बुद्ध का काल है ई० पू० ५६३-४८३, जो बहुत से विद्वानों को मान्य है । हमने पहले ही देख लिया है कि मूर्ति पूजा एवं देवायतन- निर्माण का प्रचलन ई० पू० चौथी या पाँचवीं शताब्दी में हो चुका था । प्रथम मत का समर्थन डा० फर्कुहर ( जे० आर० ए० एस्०, १९२८, पृ० १५ - २३ ) एवं डा० कार्पेटियर (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, १९२७, पृ० ८९ एवं १२० ) ने किया है। किन्तु इन लोगों का तर्क उचित नहीं जँचता । ब्राह्मणों ने ईसा पूर्व ४०० के लगभग शूद्रों से मूर्ति पूजा ग्रहण की, इस विषय में कोई स्पष्ट तर्क नहीं प्राप्त होता । जैसा कि पुरुषसूक्त से प्रकट है, शूद्र लोग लगभग एक सहस्र वर्ष ई० पूर्व में भारतीय समाज का एक अंग बन चुके थे। सूत्रकाल में ब्राह्मण लोग शूद्रों का पकाया हुआ अन्न ग्रहण कर सकते थे और शूद्र नारियों से विवाह भी कर लेते थे । अतः यदि मूर्ति-पूजा शूद्रों की देन थी तो इसे ईसा पूर्व ४०० की अपेक्षा एक सहस्र वर्ष पूर्व से प्रवलित रहना चाहिए था। देवलोक ब्राह्मण ( वह ब्राह्मण जो मूर्ति पूजा का व्यवसाय करता है या पूजा में जो कुछ प्राप्त होता है उसे ग्रहण करता है) को श्राद्ध के समय नहीं बुलाया जाता था, और उसे समाज में अपेक्षाकृत नीचा स्थान प्राप्त था ( मनु ३ । १५२) । मूर्ति पूजकों की संस्था मनु के समय में श्रत एवं गृह्ययज्ञों की अपेक्षा बहुत पुरानी नहीं थी। लगता है, मूर्तिपूजकों ने क्रमशः ब्राह्मण- कर्त्तव्य ( यथा वेदाध्ययन ) छोड़ दिया था, अतः ऐसे ब्राह्मण हेय दृष्टि से देखे जाते थे । ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल में भी साधारण गृह्य यज्ञ श्रीत कृत्यों के स्तर पर लाये जा रहे थे, क्योंकि श्रौत कृत्य अब उतने अधिक नहीं किये जाते थे, अर्थात् उनका प्रचलन क्रमशः कम होता जा रहा था । ऐतरेय ब्राह्मण ( २८ ) में आया है कि जब कोई किसी देवता को कुछ (हवि ) देना चाहता था, तो 'वषट्' कहने के पूर्व उसे उस देवता का ध्यान करना पड़ता था । इससे पूजक स्वभावतः अपने देवता को मानवीय स्वरूप एवं उपाधियाँ या गुण देने की प्रेरणा ग्रहण करेगा। निरुक्त ने वैदिक मन्त्रों में निर्देशित देवताऽऽकृतियों के प्रश्न पर कुछ लिखा है (७।६-७ ) । इसने तीन मत प्रकाशित किये हैं- ( १ ) देवता लोग पुरुषविध ( पुरुष आकार वाले) हैं, (२) वे अपुरुषविघ हैं तथा (३) वे उभयविध हैं, अर्थात् वे हैं तो अपुरुषविध किन्तु किसी कार्यवश या उद्देश्य से कई प्रकार के स्वरूप धारण कर सकते हैं।" इस अन्तिम मत में अवतारों का सिद्धान्त पाया जाता है। जब कई कारणों से वैदिक यज्ञ क्रमशः कम मनाये जाने लगे (अहिंसा के सिद्धान्त, विभिन्न उपासनाओं एवं उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म के दार्शनिक मत आदि के कारण ), तब क्रमशः मूर्ति पूजा को प्रधानता दी जाने लगी। आरम्भ में मूर्ति-पूजा का इतना विस्तार नहीं था, जैसा कि मध्य एवं आधुनिक काल में पाया जाने लगा ।
७. यस्यै देवतायं हविर्गृ होतं स्यात्तां ध्यायेद्वषट्करिष्यन् । ऐ० ब्र४० २।८ ( वेदान्तसूत्र, पू० १।३।३३ में शंकराचार्य द्वारा उद्धृत)।
८. अाकारचिन्तनं देवतानाम् । पुरुषविधाः स्युरित्येकम् । उभयविषाः स्युः अपि वा अपुरुषविधानामेव सतामेते कर्मात्मानः स्युः । निरुक्त ७ ६-७ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
अपुरुषविषाः स्युरित्यपरम् । अपि वा
www.jainelibrary.org