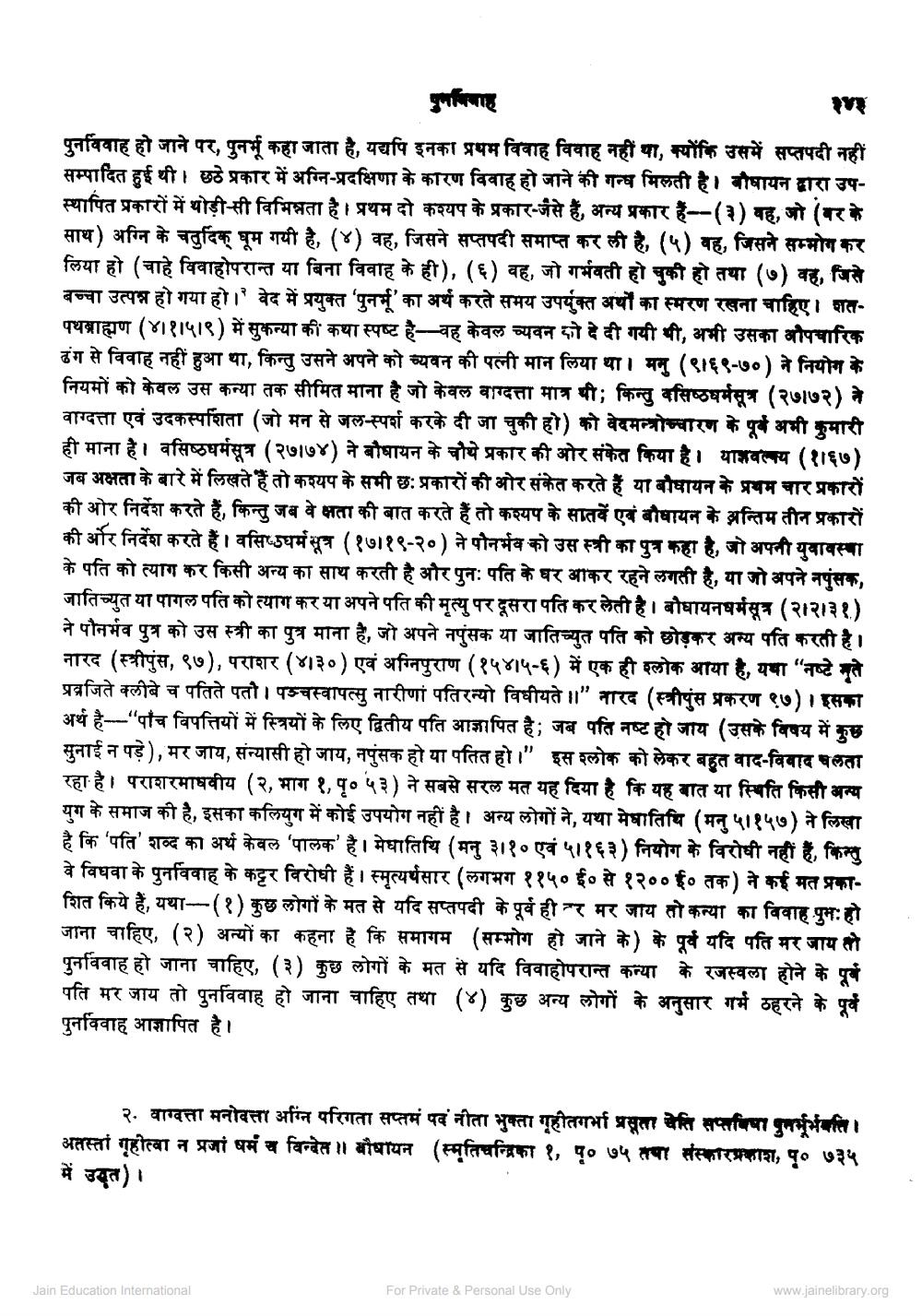________________
पुनर्विवाह पुनर्विवाह हो जाने पर, पुन' कहा जाता है, यद्यपि इनका प्रथम विवाह विवाह नहीं था, क्योंकि उसमें सप्तपदी नहीं सम्पादित हुई थी। छठे प्रकार में अग्नि-प्रदक्षिणा के कारण विवाह हो जाने की गन्ध मिलती है। बौधायन द्वारा उपस्थापित प्रकारों में थोड़ी-सी विभिन्नता है। प्रथम दो कश्यप के प्रकार-जैसे हैं, अन्य प्रकार हैं--(३) वह, जो (बर के साथ) अग्नि के चतुर्दिक् घूम गयी है, (४) वह, जिसने सप्तपदी समाप्त कर ली है, (५) वह, जिसने सम्भोग कर लिया हो (चाहे विवाहोपरान्त या बिना विवाह के ही), (६) वह, जो गर्भवती हो चुकी हो तथा (७) वह, जिते बच्चा उत्पन्न हो गया हो। वेद में प्रयुक्त 'पुनर्मू' का अर्थ करते समय उपर्युक्त अर्थों का स्मरण रखना चाहिए। शतपथब्राह्मण (४।१।५।९) में सुकन्या की कथा स्पष्ट है-वह केवल च्यवन को दे दी गयी थी, अभी उसका बीपचारिक ढंग से विवाह नहीं हुआ था, किन्तु उसने अपने को च्यवन की पत्नी मान लिया था। मनु (९।६९-७०) ने नियोग के नियमों को केवल उस कन्या तक सीमित माना है जो केवल वाग्दत्ता मात्र थी; किन्तु वसिष्ठधर्मसूत्र (२७१७२) ने वाग्दत्ता एवं उदकस्पर्शिता (जो मन से जल-स्पर्श करके दी जा चुकी हो) को वेदमन्त्रोच्चारण के पूर्व अभी कुमारी ही माना है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२७१७४) ने बौधायन के चौथे प्रकार की ओर संकेत किया है। याज्ञवल्क्य (२०६७) जब अक्षता के बारे में लिखते हैं तो कश्यप के समी छ: प्रकारों की ओर संकेत करते हैं या बौधायन के प्रथम चार प्रकारों की ओर निर्देश करते हैं, किन्तु जब वे क्षता की बात करते हैं तो कश्यप के सातवें एवं बौधायन के अन्तिम तीन प्रकारों की और निर्देश करते हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।१९-२०) ने पोनर्भव को उस स्त्री का पुत्र कहा है, जो अपनी युवावस्था के पति को त्याग कर किसी अन्य का साथ करती है और पुनः पति के घर आकर रहने लगती है, या जो अपने नपुंसक, जातिच्युत या पागल पति को त्याग कर या अपने पति की मृत्यु पर दूसरा पति कर लेती है। बौधायनधर्मसूत्र (२।२।३१) ने पौनर्मव पुत्र को उस स्त्री का पुत्र माना है, जो अपने नपुंसक या जातिच्युत पति को छोड़कर अन्य पति करती है। नारद (स्त्रीपुंस, ९७), पराशर (४।३०) एवं अग्निपुराण (१५४।५-६) में एक ही श्लोक आया है, यथा “नष्टे मृते प्रवजिते क्लीबे च पतिते पतो। पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥" नारद (स्त्रीपुंस प्रकरण ९७)। इसका अर्थ है-"पाँच विपत्तियों में स्त्रियों के लिए द्वितीय पति आज्ञापित है; जब पति नष्ट हो जाय (उसके विषय में कुछ सुनाई न पड़े), मर जाय, संन्यासी हो जाय, नपुंसक हो या पतित हो।" इस श्लोक को लेकर बहुत वाद-विवाद चलता रहा है। पराशरमाधवीय (२, भाग १, पृ० ५३) ने सबसे सरल मत यह दिया है कि यह बात या स्थिति किसी अन्य युग के समाज की है, इसका कलियुग में कोई उपयोग नहीं है। अन्य लोगों ने, यथा मेधातिथि (मनु ५।१५७) ने लिखा है कि 'पति' शब्द का अर्थ केवल 'पालक' है। मेधातिथि (मनु ३।१० एवं ५।१६३) नियोग के विरोधी नहीं हैं, किन्तु वे विधवा के पुनर्विवाह के कट्टर विरोधी हैं। स्मृत्यर्थसार (लगभग ११५० ई० से १२००६० तक) ने कई मत प्रकाशित किये हैं, यथा-(१) कुछ लोगों के मत से यदि सप्तपदी के पूर्व हीटर मर जाय तो कन्या का विक जाना चाहिए, (२) अन्यों का कहना है कि समागम (सम्भोग हो जाने के) के पूर्व यदि पति मर जाय तो पुनर्विवाह हो जाना चाहिए, (३) कुछ लोगों के मत से यदि विवाहोपरान्त कन्या के रजस्वला होने के पूर्व पति मर जाय तो पुनर्विवाह हो जाना चाहिए तथा (४) कुछ अन्य लोगों के अनुसार गर्भ ठहरने के पूर्व पुनर्विवाह आज्ञापित है।
२. वाग्वत्ता मनोवत्ता अग्नि परिगता सप्तमं पदं नीता भुक्ता गृहीतगर्भा प्रसूता येति सप्तविया पुनर्भवति । अतस्तां गृहीत्वा न प्रजा धर्म च विन्देत॥ बौधायन (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ७५ तथा संस्कारप्रकाश, पृ० ७३५ में उपत)।
Jain Education International
www.jainelibrary.org
For Private & Personal Use Only
Jain Education International