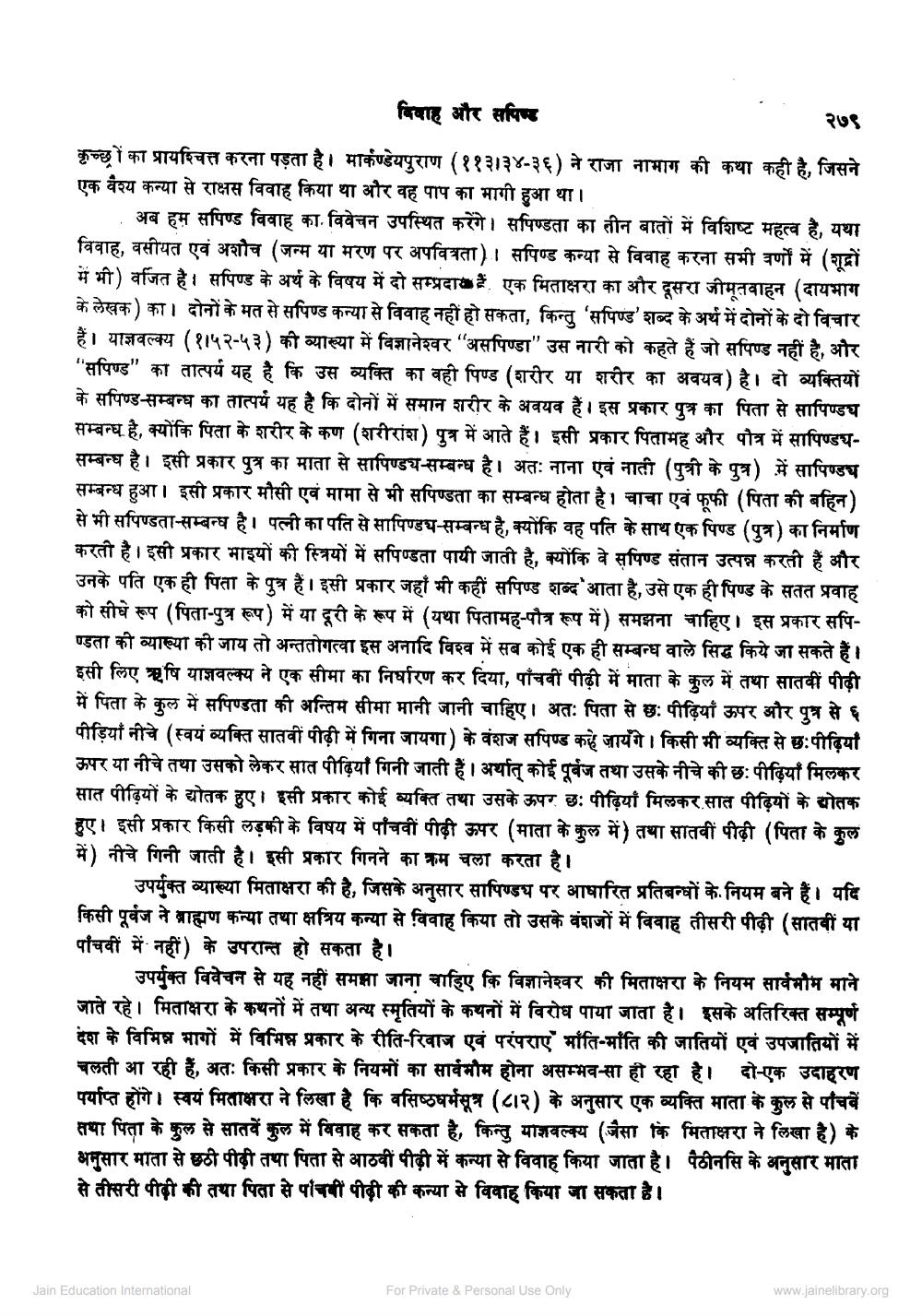________________
विवाह और सपिट
२७९ कृच्छों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मार्कण्डेयपुराण (११३॥३४-३६) ने राजा नामाग की कथा कही है, जिसने एक वैश्य कन्या से राक्षस विवाह किया था और वह पाप का भागी हुआ था।
.. अब हम सपिण्ड विवाह का विवेचन उपस्थित करेंगे। सपिण्डता का तीन बातों में विशिष्ट महत्व है, यथा विवाह, वसीयत एवं अशौच (जन्म या मरण पर अपवित्रता)। सपिण्ड कन्या से विवाह करना सभी वर्गों में (शूद्रों में भी) वजित है। सपिण्ड के अर्थ के विषय में दो सम्प्रदा एक मिताक्षरा का और दूसरा जीमूतवाहन (दायभाग के लेखक) का। दोनों के मत से सपिण्ड कन्या से विवाह नहीं हो सकता, किन्तु 'सपिण्ड' शब्द के अर्थ में दोनों के दो विचार हैं। याज्ञवल्क्य (११५२-५३) की व्याख्या में विज्ञानेश्वर "असपिण्डा" उस नारी को कहते हैं जो सपिण्ड नहीं है, और "सपिण्ड" का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति का वही पिण्ड (शरीर या शरीर का अवयव) है। दो व्यक्तियों के सपिण्ड-सम्बन्ध का तात्पर्य यह है कि दोनों में समान शरीर के अवयव हैं। इस प्रकार पुत्र का पिता से सापिण्डय सम्बन्ध है, क्योंकि पिता के शरीर के कण (शरीरांश) पुत्र में आते हैं। इसी प्रकार पितामह और पौत्र में सापिण्डयसम्बन्ध है। इसी प्रकार पुत्र का माता से सापिण्ड्य-सम्बन्ध है। अतः नाना एवं नाती (पुत्री के पुत्र) में सापिण्डप सम्बन्ध हुआ। इसी प्रकार मौसी एवं मामा से भी सपिण्डता का सम्बन्ध होता है। चाचा एवं फूफी (पिता की बहिन) से भी सपिण्डता-सम्बन्ध है। पत्नी का पति से सापिण्डय-सम्बन्ध है, क्योंकि वह पति के साथ एक पिण्ड (पुत्र) का निर्माण करती है। इसी प्रकार भाइयों की स्त्रियों में सपिण्डता पायी जाती है, क्योंकि वे सपिण्ड संतान उत्पन्न करती हैं और उनके पति एक ही पिता के पुत्र हैं। इसी प्रकार जहाँ भी कहीं सपिण्ड शब्द आता है, उसे एक ही पिण्ड के सतत प्रवाह को सीधे रूप (पिता-पुत्र रूप) में या दूरी के रूप में (यथा पितामह-पौत्र रूप में) समझना चाहिए। इस प्रकार सपिण्डता की व्याख्या की जाय तो अन्ततोगत्वा इस अनादि विश्व में सब कोई एक ही सम्बन्ध वाले सिद्ध किये जा सकते हैं। इसी लिए ऋषि याज्ञवल्क्य ने एक सीमा का निर्धारण कर दिया, पाँचवीं पीढ़ी में माता के कुल में तथा सातवीं पीढ़ी में पिता के कुल में सपिण्डता की अन्तिम सीमा मानी जानी चाहिए। अतः पिता से छ: पीढ़ियाँ ऊपर और पुत्र से ६ पीड़ियाँ नीचे (स्वयं व्यक्ति सातवीं पीढ़ी में गिना जायगा) के वंशज सपिण्ड कहे जायंगे। किसी भी व्यक्ति से छ:पीढ़ियाँ ऊपर या नीचे तथा उसको लेकर सात पीढ़ियां गिनी जाती हैं । अर्थात् कोई पूर्वज तथा उसके नीचे की छः पीढ़ियाँ मिलकर सात पीढ़ियों के द्योतक हुए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति तथा उसके ऊपर छ: पीढ़ियाँ मिलकर सात पीढ़ियों के द्योतक हुए। इसी प्रकार किसी लड़की के विषय में पांचवीं पीढ़ी ऊपर (माता के कुल में) तथा सातवीं पीढ़ी (पिता के कुल में) नीचे गिनी जाती है। इसी प्रकार गिनने का क्रम चला करता है।
उपर्युक्त व्याख्या मिताक्षरा की है, जिसके अनुसार सापिण्डय पर आधारित प्रतिबन्धों के नियम बने हैं। यदि किसी पूर्वज ने ब्राह्मण कन्या तथा क्षत्रिय कन्या से विवाह किया तो उसके वंशजों में विवाह तीसरी पीढ़ी (सातवीं या पांचवीं में नहीं) के उपरान्त हो सकता है।
उपर्युक्त विवेचन से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा के नियम सार्वभौम माने जाते रहे। मिताक्षरा के कथनों में तथा अन्य स्मृतियों के कथनों में विरोध पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के रीति-रिवाज एवं परंपराएं भांति-भांति की जातियों एवं उपजातियों में चलती आ रही हैं, अतः किसी प्रकार के नियमों का सार्वभौम होना असम्भव-सा ही रहा है। दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। स्वयं मिताक्षरा ने लिखा है कि वसिष्ठधर्मसूत्र (८२) के अनुसार एक व्यक्ति माता के कुल से पांचवें तथा पिता के कुल से सातवें कुल में विवाह कर सकता है, किन्तु याज्ञवल्क्य (जैसा कि मिताक्षरा ने लिखा है) के अनुसार माता से छठी पीढ़ी तथा पिता से आठवीं पीढ़ी में कन्या से विवाह किया जाता है। पैठीनसि के अनुसार माता से तीसरी पीढ़ी की तथा पिता से पांचवीं पीढ़ी की कन्या से विवाह किया जा सकता है।
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org