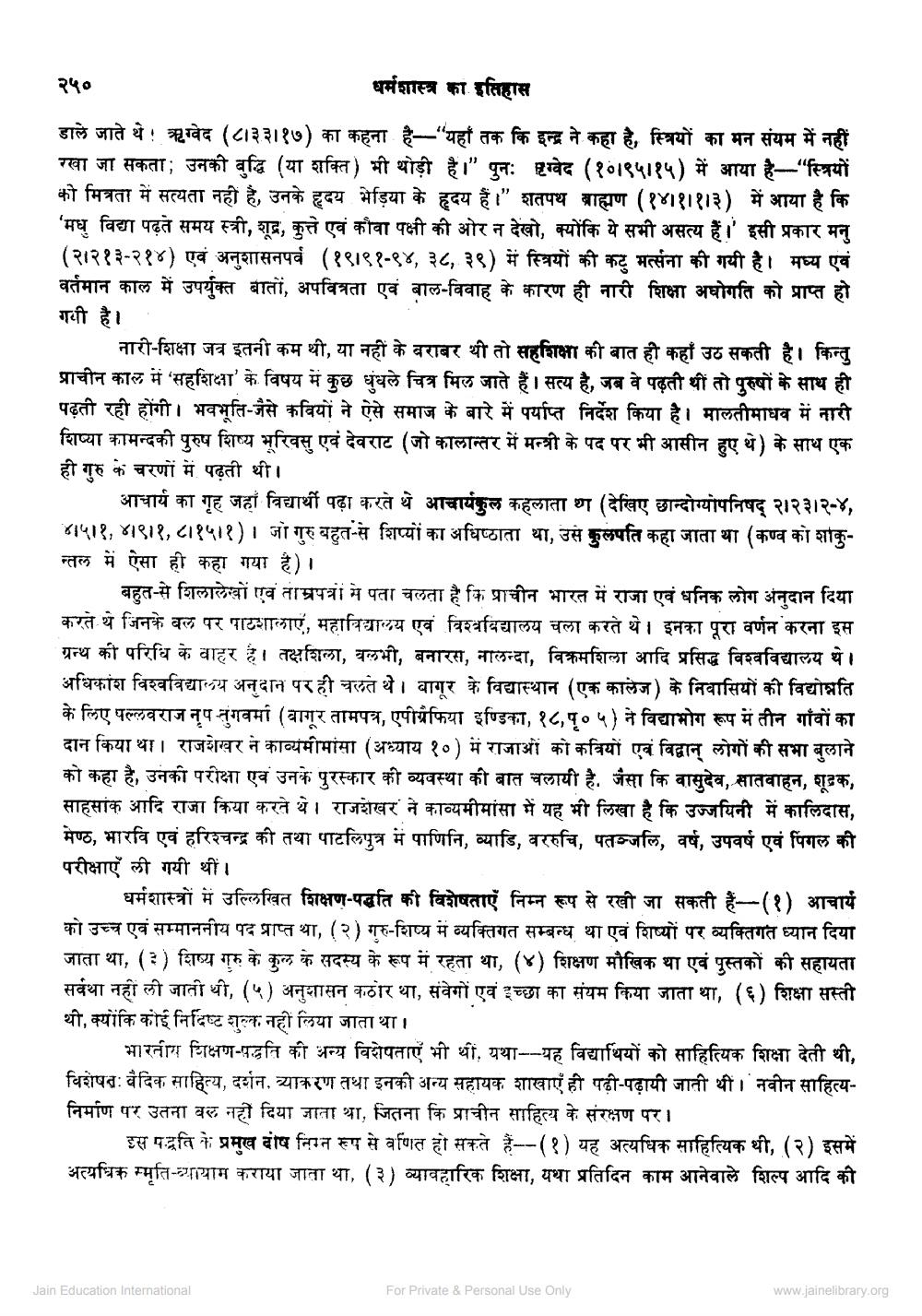________________
धर्मशास्त्र का इतिहास
२५०
डाले जाते थे ! ऋग्वेद ( ८|३३|१७ ) का कहना है- "यहाँ तक कि इन्द्र ने कहा है, स्त्रियों का मन संयम में नहीं रखा जा सकता; उनकी बुद्धि ( या शक्ति) भी थोड़ी है।" पुनः टग्वेद ( १० । ९५/१५ ) में आया है - "स्त्रियों की मित्रता में सत्यता नहीं हैं, उनके हृदय भेड़िया के हृदय हैं।" शतपथ ब्राह्मण ( १४|१|१|३) में आया है कि 'मधु विद्या पढ़ते समय स्त्री, शूद्र, कुत्ते एवं कौवा पक्षी की ओर न देखो, क्योंकि ये सभी असत्य हैं।' इसी प्रकार मनु (२।२१३-२१४) एवं अनुशासनपर्व ( १९९१ ९४, ३८, ३९) में स्त्रियों की कटु भर्त्सना की गयी है। मध्य एवं वर्तमान काल में उपर्युक्त बातों, अपवित्रता एवं बाल विवाह के कारण ही नारी शिक्षा अघोगति को प्राप्त हो गयी है ।
नारी-शिक्षा जब इतनी कम थी, या नहीं के बराबर थी तो सहशिक्षा की बात ही कहाँ उठ सकती है। किन्तु प्राचीन काल में 'सहशिक्षा' के विषय में कुछ धुंधले चित्र मिल जाते हैं। सत्य है, जब वे पढ़ती थीं तो पुरुषों के साथ ही पढ़ती रही होंगी । भवभूति-जैसे कवियों ने ऐसे समाज के बारे में पर्याप्त निर्देश किया है। मालतीमाधव में नारी शिष्या कामन्दकी पुरुष शिष्य भूरिवसु एवं देवराट ( जो कालान्तर में मन्त्री के पद पर भी आसीन हुए थे) के साथ एक ही गुरु के चरणों में पढ़ती थी ।
आचार्य का गृह जहाँ विद्यार्थी पढ़ा करते थे आचार्यकुल कहलाता था (देखिए छान्दोग्योपनिषद् २।२३।२-४, ४४५।१, ४।९।१, ८।१५।१) । जो गुरु बहुत-से शिष्यों का अधिष्ठाता था, उसे कुलपति कहा जाता था ( कण्व को शाकुन्तल में ऐसा ही कहा गया है ) ।
बहुत से शिलालेखों एवं ताम्रपत्रों में पता चलता है कि प्राचीन भारत में राजा एवं धनिक लोग अनुदान दिया करते थे जिनके बल पर पाठशालाएं, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय चला करते थे । इनका पूरा वर्णन करना इस ग्रन्थ की परिधि के बाहर है। तक्षशिला, बलभी, बनारस, नालन्दा, विक्रमशिला आदि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे । afrasia विश्वविद्यालय अनुदान पर ही चलते थे । बागूर के विद्यास्थान (एक कालेज) के निवासियों की विद्योन्नति के लिए पल्लवराज नृप तुंगवर्मा (बागूर तामपत्र, एपीग्रैफिया इण्डिका, १८, पृ० ५ ) ने विद्याभोग रूप में तीन गाँवों का दान किया था। राजशेखर ने काव्यमीमांसा (अध्याय १०) में राजाओं को कत्रियों एवं विद्वान् लोगों की सभा बुलाने को कहा है, उनकी परीक्षा एवं उनके पुरस्कार की व्यवस्था की बात चलायी है. जैसा कि वासुदेव, सातवाहन, शूद्रक, साहसांक आदि राजा किया करते थे । राजशेखर ने काव्यमीमांसा में यह भी लिखा है कि उज्जयिनी में कालिदास, मेण्ठ, भारवि एवं हरिश्चन्द्र की तथा पाटलिपुत्र में पाणिनि, व्याडि, वररुचि, पतञ्जलि, वर्ष, उपवर्ष एवं पिंगल की परीक्षाएँ ली गयी थीं ।
धर्मशास्त्रों में उल्लिखित शिक्षण-पद्धति की विशेषताएँ निम्न रूप से रखी जा सकती हैं - (१) आचार्य को उच्च एवं सम्माननीय पद प्राप्त था, (२) गुरु-शिष्य में व्यक्तिगत सम्बन्ध था एवं शिष्यों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था, (३) शिष्य गुरु के कुल के सदस्य के रूप में रहता था, (४) शिक्षण मौखिक था एवं पुस्तकों की सहायता सर्वथा नहीं ली जाती थी, (५) अनुशासन कठोर था, संवेगों एवं इच्छा का संयम किया जाता था, (६) शिक्षा सस्ती थी, क्योंकि कोई निर्दिष्ट शुल्क नहीं लिया जाता था ।
भारतीय शिक्षण-पद्धति की अन्य विशेषताएँ भी थीं, यथा-यह विद्यार्थियों को साहित्यिक शिक्षा देती थी, विशेषत: वैदिक साहित्य, दर्शन, व्याकरण तथा इनकी अन्य सहायक शाखाएँ ही पढ़ी-पढ़ायी जाती थीं। नवीन साहित्यनिर्माण पर उतना बल नहीं दिया जाता था, जितना कि प्राचीन साहित्य के संरक्षण पर ।
इस पद्धति के प्रमुख दोष निम्न रूप से वर्णित हो सकते हैं -- ( १ ) यह अत्यधिक साहित्यिक थी, (२) इसमें अत्यधिक स्मृति व्यायाम कराया जाता था, (३) व्यावहारिक शिक्षा, यथा प्रतिदिन काम आनेवाले शिल्प आदि की
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org