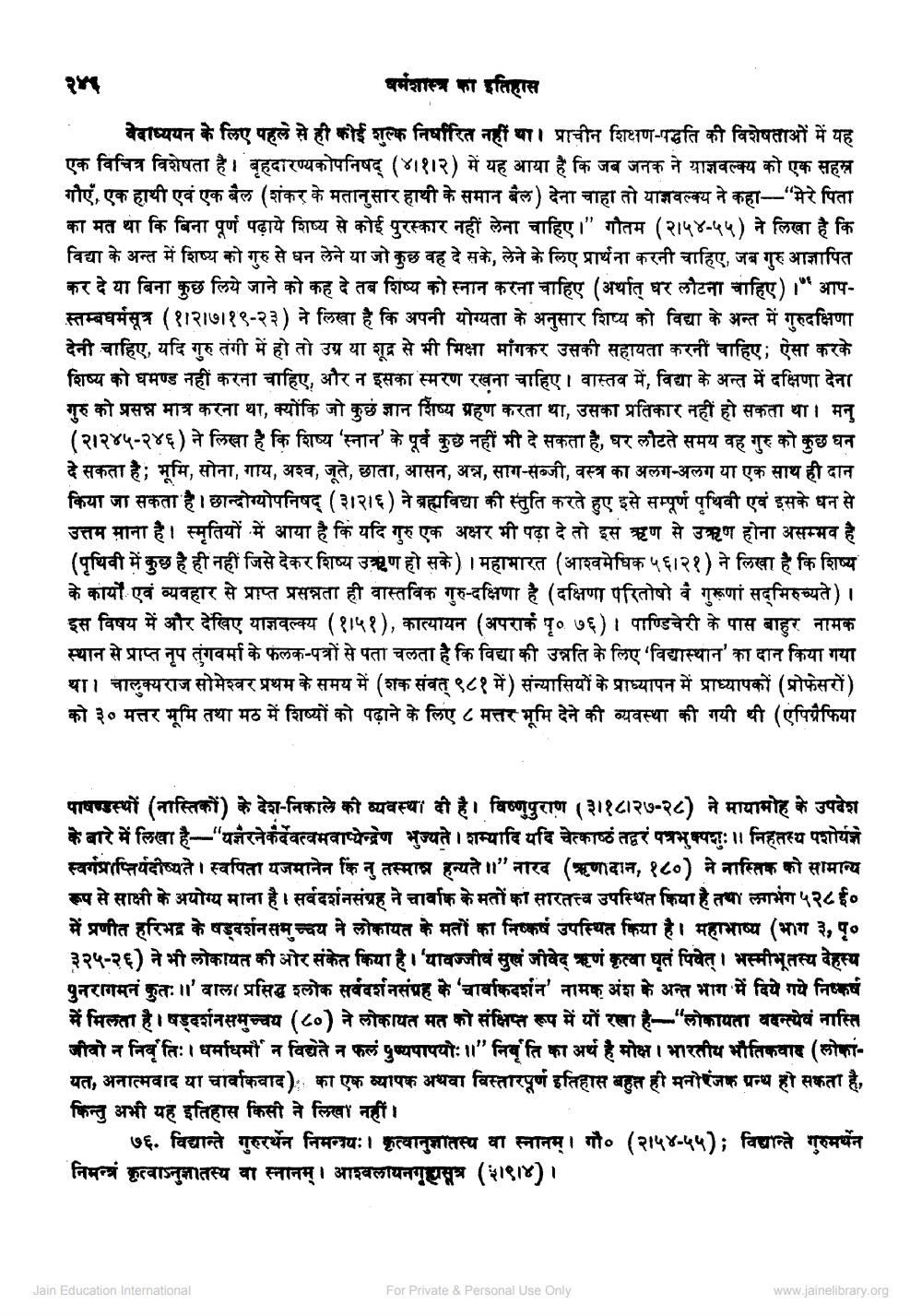________________
धर्मशास्त्र का इतिहास - वेदाध्ययन के लिए पहले से ही कोई शुल्क निर्धारित नहीं था। प्राचीन शिक्षण-पद्धति की विशेषताओं में यह एक विचित्र विशेषता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।१।२) में यह आया है कि जब जनक ने याज्ञवल्क्य को एक सहन गौएँ, एक हाथी एवं एक बैल (शंकर के मतानुसार हाथी के समान बैल) देना चाहा तो याज्ञवल्क्य ने कहा-"मेरे पिता का मत था कि बिना पूर्ण पढ़ाये शिष्य से कोई पुरस्कार नहीं लेना चाहिए।" गौतम (२१५४-५५) ने लिखा है कि विद्या के अन्त में शिष्य को गुरु से धन लेने या जो कुछ वह दे सके, लेने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जब गुरु आज्ञापित कर दे या बिना कुछ लिये जाने को कह दे तब शिष्य को स्नान करना चाहिए (अर्थात् घर लौटना चाहिए)।" आपस्तम्बधर्मसूत्र (११२।७।१९-२३) ने लिखा है कि अपनी योग्यता के अनुसार शिष्य को विद्या के अन्त में गुरुदक्षिणा देनी चाहिए, यदि गुरु तंगी में हो तो उग्र या शूद्र से भी भिक्षा मांगकर उसकी सहायता करनी चाहिए; ऐसा करके शिष्य को घमण्ड नहीं करना चाहिए, और न इसका स्मरण रखना चाहिए। वास्तव में, विद्या के अन्त में दक्षिणा देना गुरु को प्रसन्न मात्र करना था, क्योंकि जो कुछ ज्ञान शिष्य ग्रहण करता था, उसका प्रतिकार नहीं हो सकता था। मनु (२।२४५-२४६) ने लिखा है कि शिष्य 'स्नान' के पूर्व कुछ नहीं भी दे सकता है, घर लौटते समय वह गुरु को कुछ धन दे सकता है ; भूमि, सोना, गाय, अश्व, जूते, छाता, आसन, अन्न, साग-सब्जी, वस्त्र का अलग-अलग या एक साथ ही दान किया जा सकता है। छान्दोग्योपनिषद् (३।२।६) ने ब्रह्मविद्या की स्तुति करते हुए इसे सम्पूर्ण पृथिवी एवं इसके धन से उत्तम माना है। स्मृतियों में आया है कि यदि गुरु एक अक्षर भी पढ़ा दे तो इस ऋण से उऋण होना असम्भव है (पृथिवी में कुछ है ही नहीं जिसे देकर शिष्य उऋण हो सके) । महाभारत (आश्वमेधिक ५६।२१) ने लिखा है कि शिष्य के कार्यो एवं व्यवहार से प्राप्त प्रसन्नता ही वास्तविक गुरु-दक्षिणा है (दक्षिणा परितोषो वै गुरूणां सद्भिरुच्यते) । इस विषय में और देखिए याज्ञवल्क्य (११५१), कात्यायन (अपरार्क पृ० ७६) । पाण्डिचेरी के पास बाहुर नामक स्थान से प्राप्त नृप तुंगवर्मा के फलक-पत्रों से पता चलता है कि विद्या की उन्नति के लिए 'विद्यास्थान' का दान किया गया था। चालुक्यराज सोमेश्वर प्रथम के समय में (शक संवत् ९८१ में) संन्यासियों के प्राध्यापन में प्राध्यापकों (प्रोफेसरों) को ३० मत्तर भूमि तथा मठ में शिष्यों को पढ़ाने के लिए ८ मत्तर भूमि देने की व्यवस्था की गयी थी (एपिप्रैफिया
पाषण्डस्थों (नास्तिकों) के देश-निकाले को व्यवस्था दी है। विष्णुपुराण (३।१८।२७-२८) ने मायामोह के उपदेश के बारे में लिखा है-"यहरनेकर्देवत्वमवाप्येन्द्रेण भुज्यते । शम्यादि यदि चेत्काष्ठं तद्वरं पत्रभुक्पशुः ॥ निहतस्य पशोर्यज्ञे स्वर्गप्राप्तिर्यदीष्यते। स्वपिता यजमानेन किं नु तस्मान हन्यते ॥" नारद (ऋणादान, १८०) ने नास्तिक को सामान्य रूप से साक्षी के अयोग्य माना है। सर्वदर्शनसंग्रह ने चार्वाक के मतों का सारतत्त्व उपस्थित किया है तथा लगभंग ५२८ ई० में प्रणीत हरिभद्र के षड्दर्शनसमुच्चय ने लोकायत के मतों का निष्कर्ष उपस्थित किया है। महाभाष्य (भाग ३, पृ० ३२५-२६) ने भी लोकायत की ओर संकेत किया है। यावज्जीवं सुखं जीवेद ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥' वाला प्रसिद्ध श्लोक सर्वदर्शनसंग्रह के 'चार्वाकदर्शन' नामक अंश के अन्त भाग में दिये गये निष्कर्ष में मिलता है। षड्दर्शनसमुच्चय (८०) ने लोकायत मत को संक्षिप्त रूप में यों रखा है-"लोकायता वदन्त्येवं नास्ति जीवो न निवृतिः। धर्माधमौ न विद्यते न फलं पुण्यपापयोः॥" निर्वृति का अर्थ है मोक्ष । भारतीय भौतिकवाद (लोकायत, अनात्मवाद या चार्वाकवाद) का एक व्यापक अथवा विस्तारपूर्ण इतिहास बहुत ही मनोरंजक ग्रन्थ हो सकता है, किन्तु अभी यह इतिहास किसी ने लिखा नहीं।
७६. विद्यान्ते गुरुरर्थेन निमन्त्रयः। कृत्वानुज्ञातस्य वा स्नानम्। गौ० (२१५४-५५); विद्यान्ते गुरुमन निमन्त्रं कृत्वाऽनुज्ञातस्य वा स्नानम् । आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।९।४)।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org