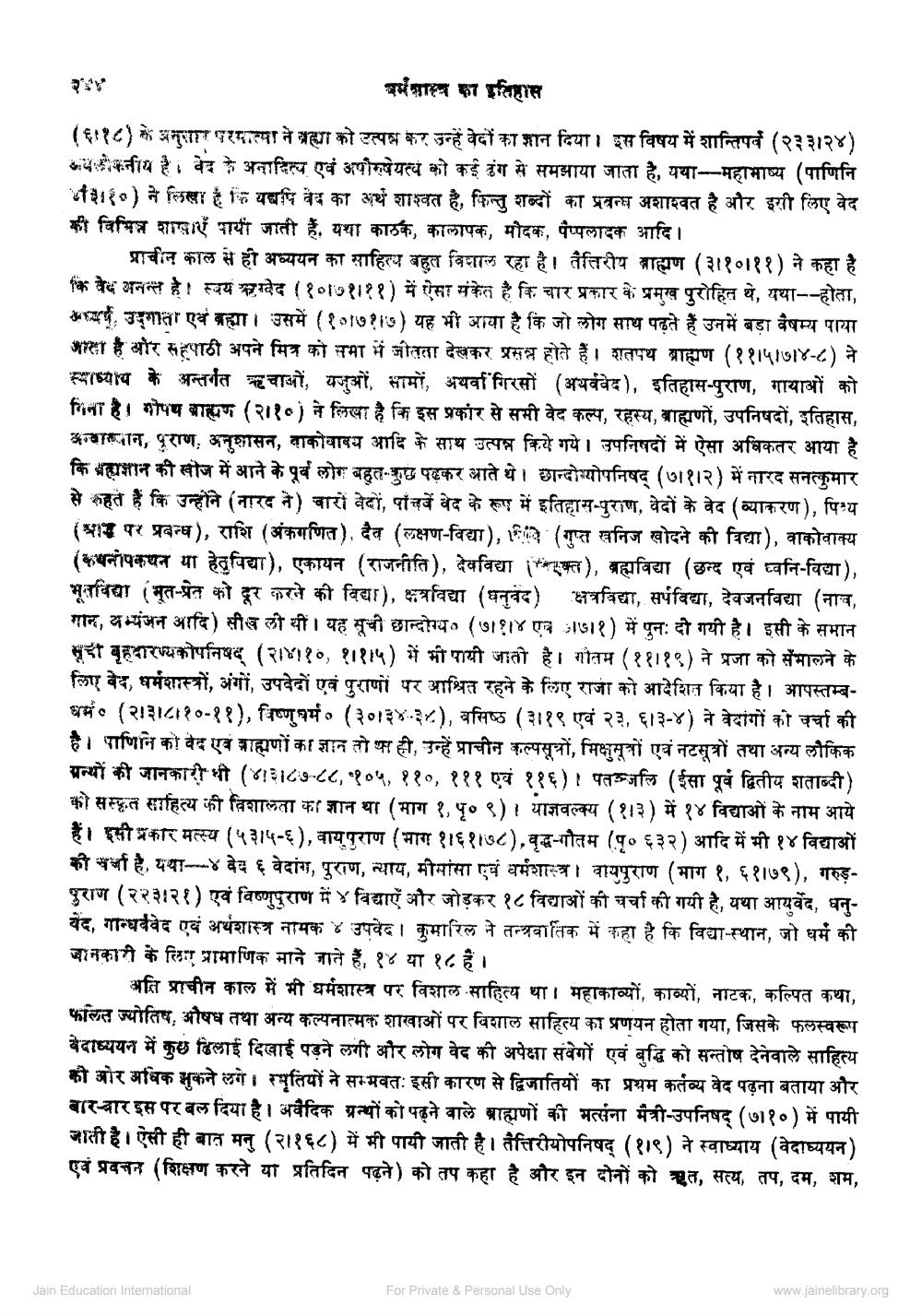________________
मंत्र का इतिहास
(६११८) के अनुसार परमात्मा ने ब्रह्मा को उत्पन्न कर उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। इस विषय में शान्तिपर्व ( २३३।२४ ) नीय है। वेद के अनादित्य एवं अपौरुषेयत्व को कई ढंग से समझाया जाता है, यथा -- महाभाष्य ( पाणिनि १०) ने लिखा है कि यद्यपि वेद का अर्थ शाश्वत है, किन्तु शब्दों का प्रवन्ध अशाश्वत है और इसी लिए वेद की विभिन्न शाखाएँ पायी जाती हैं, यथा काठक, कालापक, मोदक, पैप्पलादक आदि ।
२०४
प्राचीन काल से ही अध्ययन का साहित्य बहुत विशाल रहा है । तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३|१०|११ ) ने कहा है कि वे अनन्त है। स्वयं ऋग्वेद (१०।७१।११) में ऐसा संकेत हैं कि चार प्रकार के प्रमुख पुरोहित थे, यथा-- होता, उद्गाता एवं ब्रह्मा। उसमें (१०/७१1७) यह भी जावा है कि जो लोग साथ पढ़ते हैं उनमें बड़ा वैषम्य पाया जाता है और सहपाठी अपने मित्र को सभा में जीतता देखकर प्रसन्न होते हैं। शतपथ ब्राह्मण (११।५।७१४-८) ने स्वाध्याय के अन्तर्गत ऋचाओं, यजुओं, सामों, अथर्वा गिरसों (अथर्ववेद), इतिहास-पुराण, गाथाओं को दिना है। गोपथ ब्राह्मण (२०१०) ने लिखा है कि इस प्रकार से सभी वेद कल्प, रहस्य, ब्राह्मणों, उपनिषदों, इतिहास, अवास्थान, पुराण, अनुशासन, वाकोवाक्य आदि के साथ उत्पन्न किये गये। उपनिषदों में ऐसा अधिकतर आया है। कि ब्रह्मज्ञान की खोज में आने के पूर्व लोग बहुत कुछ पढ़कर आते थे। छान्दोग्योपनिषद् (७।१।२) में नारद सनत्कुमार से कहते हैं कि उन्होंने (नारद ने ) चारों वेदों, पाँचवें वेद के रूप में इतिहास-पुराण, वेदों के वेद (व्याकरण), पिश्य ( श्राद्ध पर प्रबन्ध), राशि (अंकगणित), दैव (लक्षण-विद्या), (गुप्त खनिज खोदने की विद्या), वाकोवाक्य ( कथोपकथन या हेतुविद्या ), एकायन (राजनीति), देवविद्या (मुक्त), ब्रह्मविद्या (छन्द एवं ध्वनि - विद्या), भूतविद्या ( भूत-प्रेत को दूर करने की विद्या), क्षत्रविद्या (धनुबंद ) गान, अभ्पंजन आदि) सीख ली थीं। यह सूची छान्दोग्य० (७११।४ एव मृदा बृहदारण्यकोपनिषद् ( २/४११०, ११११५) में भी पायी जाती है। लिए वेद, धर्मशास्त्रों, अंगों, उपवेदों एवं पुराणों पर आश्रित रहने के लिए राजा को आदेशित किया है। आपस्तम्बधर्म० (२३८)१०-११), विष्णुधर्म० (३०/३४-३८), वसिष्ठ ( ३|१९ एवं २३, ६।३-४ ) ने वेदांगों की चर्चा की है । पाणिनि को वेद एवं ब्राह्मणों का ज्ञान तो था ही, उन्हें प्राचीन कल्पसूत्रों, भिक्षुसूत्रों एवं नटसूत्रों तथा अन्य लौकिक ग्रन्थों की जानकारी भी (४१३१८७-८८, १०५, ११०, १११ एवं ११६) । पतञ्जलि (ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी) को संस्कृत साहित्य की विशालता का ज्ञान था (भाग १, पृ० ९ ) । याज्ञवल्क्य ( ११३ ) में १४ विद्याओं के नाम आये हैं। इसी प्रकार मत्स्य (५३।५-६), वायुपुराण ( भाग ११६१०७८), वृद्ध-गौतम ( पृ० ६३२) आदि में भी १४ विद्याओं की चर्चा है, यथा---४ वेद ६ वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धर्मशास्त्र । वायुपुराण (भाग १, ६१।७९), गरुड़पुराण (२२३।२१) एवं विष्णुपुराण में ४ विद्याएँ और जोड़कर १८ विद्याओं की चर्चा की गयी है, यथा आयुर्वेद, धनुवेद, गान्धर्ववेद एवं अर्थशास्त्र नामक ४ उपवेद । कुमारिल ने तन्त्रवार्तिक में कहा है कि विद्या- स्थान, जो धर्म की जानकारी के लिए प्रामाणिक माने जाते हैं, १४ या १८ हैं ।
क्षत्रविद्या, सर्पविद्या, देवजनविद्या (नाव, ।७।१) में पुनः दी गयी है। इसी के समान गौतम (११।१९ ) ने प्रजा को सँभालने के
अति प्राचीन काल में भी धर्मशास्त्र पर विशाल साहित्य था । महाकाव्यों, काव्यों, नाटक, कल्पित कथा, फलित ज्योतिष, औषध तथा अन्य कल्पनात्मक शाखाओं पर विशाल साहित्य का प्रणयन होता गया, जिसके फलस्वरूप वेदाध्ययन में कुछ ढिलाई दिखाई पड़ने लगी और लोग वेद की अपेक्षा संवेगों एवं बुद्धि को सन्तोष देनेवाले साहित्य की ओर अधिक झुकने लगे। स्मृतियों ने सम्भवत: इसी कारण से द्विजातियों का प्रथम कर्तव्य वेद पढ़ना बताया और बार-बार इस पर बल दिया है। अवैदिक ग्रन्थों को पढ़ने वाले ब्राह्मणों की भत्संना मैत्री - उपनिषद् (७।१०) में पायी जाती है। ऐसी ही बात मनु ( २।१६८ ) में भी पायी जाती है। तैत्तिरीयोपनिषद् (१।९ ) ने स्वाध्याय ( वेदाध्ययन ) एवं प्रवचन ( शिक्षण करने या प्रतिदिन पढ़ने) को तप कहा है और इन दोनों को ऋॠत, सत्य, तप, दम, शम,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org