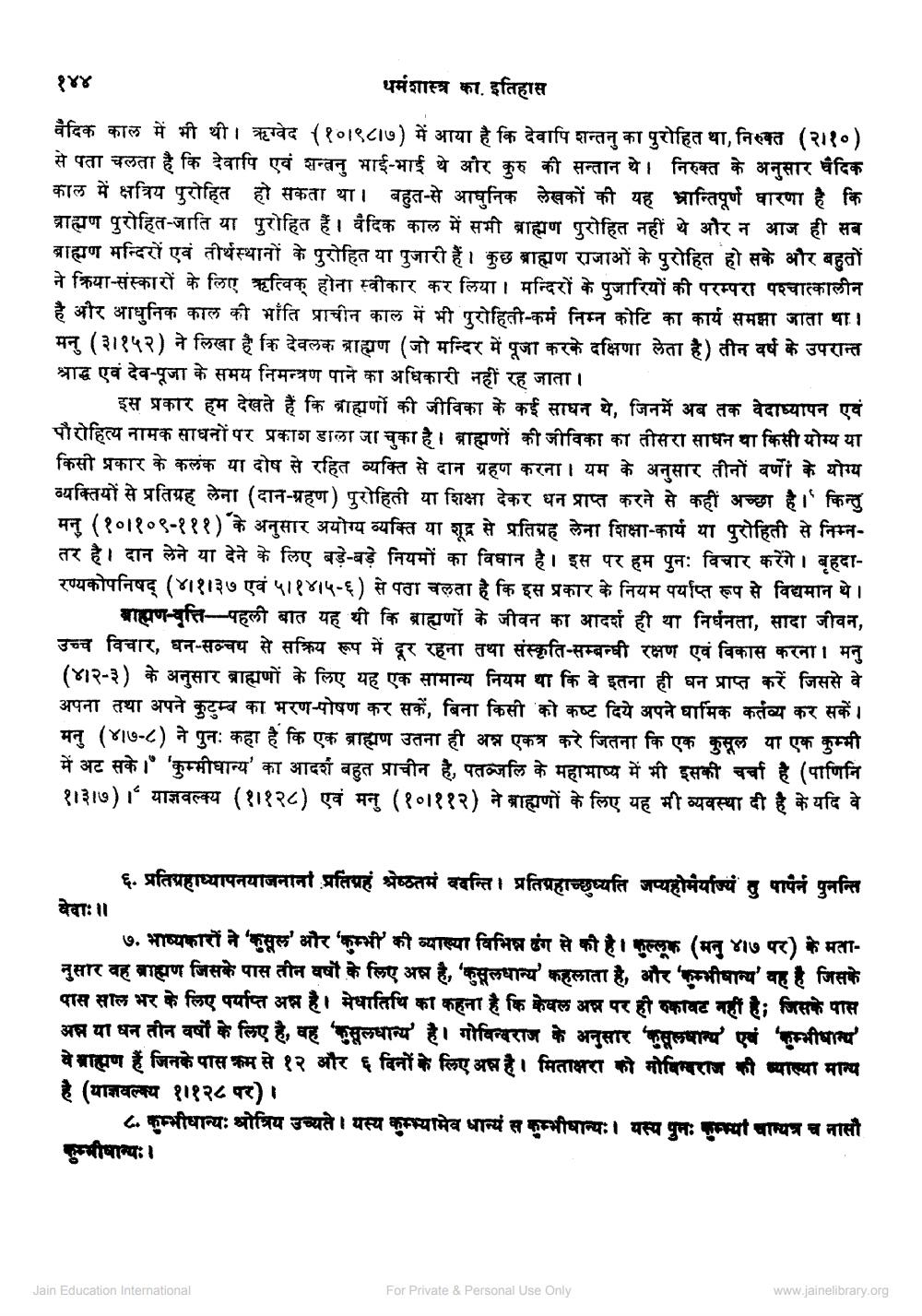________________
१४४
धर्मशास्त्र का इतिहास
वैदिक काल में भी थी । ऋग्वेद ( १० | ९८१७) में आया है कि देवापि शन्तनु का पुरोहित था, निरुक्त ( २०१० ) से पता चलता है कि देवापि एवं शन्तनु भाई-भाई थे और कुरु की सन्तान थे। निरुक्त के अनुसार वैदिक काल में क्षत्रिय पुरोहित हो सकता था । बहुत-से आधुनिक लेखकों की यह भ्रान्तिपूर्ण धारणा है कि ब्राह्मण पुरोहित-जाति या पुरोहित हैं । वैदिक काल में सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं थे और न आज ही सब ब्राह्मण मन्दिरों एवं तीर्थस्थानों के पुरोहित या पुजारी हैं। कुछ ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित हो सके और बहुतों ने क्रिया-संस्कारों के लिए ऋत्विक् होना स्वीकार कर लिया। मन्दिरों के पुजारियों की परम्परा पश्चात्कालीन है और आधुनिक काल की भाँति प्राचीन काल में भी पुरोहिती - कर्म निम्न कोटि का कार्य समझा जाता था । मनु ( ३|१५२ ) ने लिखा है कि देवलक ब्राह्मण ( जो मन्दिर में पूजा करके दक्षिणा लेता है) तीन वर्ष के उपरान्त श्राद्ध एवं देव पूजा के समय निमन्त्रण पाने का अधिकारी नहीं रह जाता ।
इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की जीविका के कई साधन थे, जिनमें अब तक वेदाध्यापन एवं पौरोहित्य नामक साधनों पर प्रकाश डाला जा चुका है । ब्राह्मणों की जीविका का तीसरा साधन या किसी योग्य या किसी प्रकार के कलंक या दोष से रहित व्यक्ति से दान ग्रहण करना । यम के अनुसार तीनों वर्णों के योग्य व्यक्तियों से प्रतिग्रह लेना ( दान - ग्रहण) पुरोहिती या शिक्षा देकर धन प्राप्त करने से कहीं अच्छा है।' किन्तु मनु (१०।१०९-१११ ) के अनुसार अयोग्य व्यक्ति या शूद्र से प्रतिग्रह लेना शिक्षा कार्य या पुरोहिती से निम्नतर है। दान लेने या देने के लिए बड़े-बड़े नियमों का विधान है। इस पर हम पुनः विचार करेंगे। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।१।३७ एवं ५।१४।५-६ ) से पता चलता है कि इस प्रकार के नियम पर्याप्त रूप से विद्यमान थे । ब्राह्मण-वृत्ति-पहली बात यह थी कि ब्राह्मणों के जीवन का आदर्श ही या निर्धनता, सादा जीवन, उच्च विचार, धन सञ्चय से सक्रिय रूप में दूर रहना तथा संस्कृति सम्बन्धी रक्षण एवं विकास करना । मनु (४/२ - ३ ) के अनुसार ब्राह्मणों के लिए यह एक सामान्य नियम था कि वे इतना ही धन प्राप्त करें जिससे वे अपना तथा अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण कर सकें, बिना किसी को कष्ट दिये अपने धार्मिक कर्तव्य कर सकें । मनु ( ४१७- ८ ) ने पुन: कहा है कि एक ब्राह्मण उतना ही अन्न एकत्र करे जितना कि एक कुसूल या एक कुम्मी में अट सके । ' कुम्मीधान्य' का आदर्श बहुत प्राचीन है, पतञ्जलि के महाभाष्य में भी इसकी चर्चा है ( पाणिनि १।३।७) । याज्ञवल्क्य (१।१२८) एवं मनु (१०।११२ ) ने ब्राह्मणों के लिए यह भी व्यवस्था दी है के यदि वे
६. प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानां प्रतिग्रहं श्रेष्ठतमं वदन्ति । प्रतिग्रहाच्छुष्यति जप्यहोमंर्याज्यं तु पापनं पुनन्ति
देवाः ॥
७. भाष्यकारों ने 'कुसूल' और 'कुम्भी' की व्याख्या विभिन्न ढंग से की है। कुल्लूक (मनु ४।७ पर) के मतानुसार वह ब्राह्मण जिसके पास तीन वर्षों के लिए अन्न है, 'कुसलधान्य' कहलाता है, और 'कुम्भीषान्य' वह है जिसके पास साल भर के लिए पर्याप्त अन्न है। मेधातिथि का कहना है कि केवल अन पर ही वकावट नहीं है; जिसके पास अन या धन तीन वर्षों के लिए है, वह 'कुसुलधान्य' है । गोविन्दराज के अनुसार 'कुसूलधान्य' एवं 'कुम्भीधान्य' वे ब्राह्मण हैं जिनके पास क्रम से १२ और ६ दिनों के लिए अस है। मिताक्षरा को मोविम्वराज की व्याल्या मान्य है ( याज्ञवल्क्य १।१२८ पर)।
८. कुम्भीधान्यः श्रोत्रिय उच्यते । यस्य कुम्भ्यामेव धान्यं स कुम्भीधान्यः । यस्य पुनः कुम्भ्यां चान्यत्र च नासौ कुम्भीषान्यः ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org