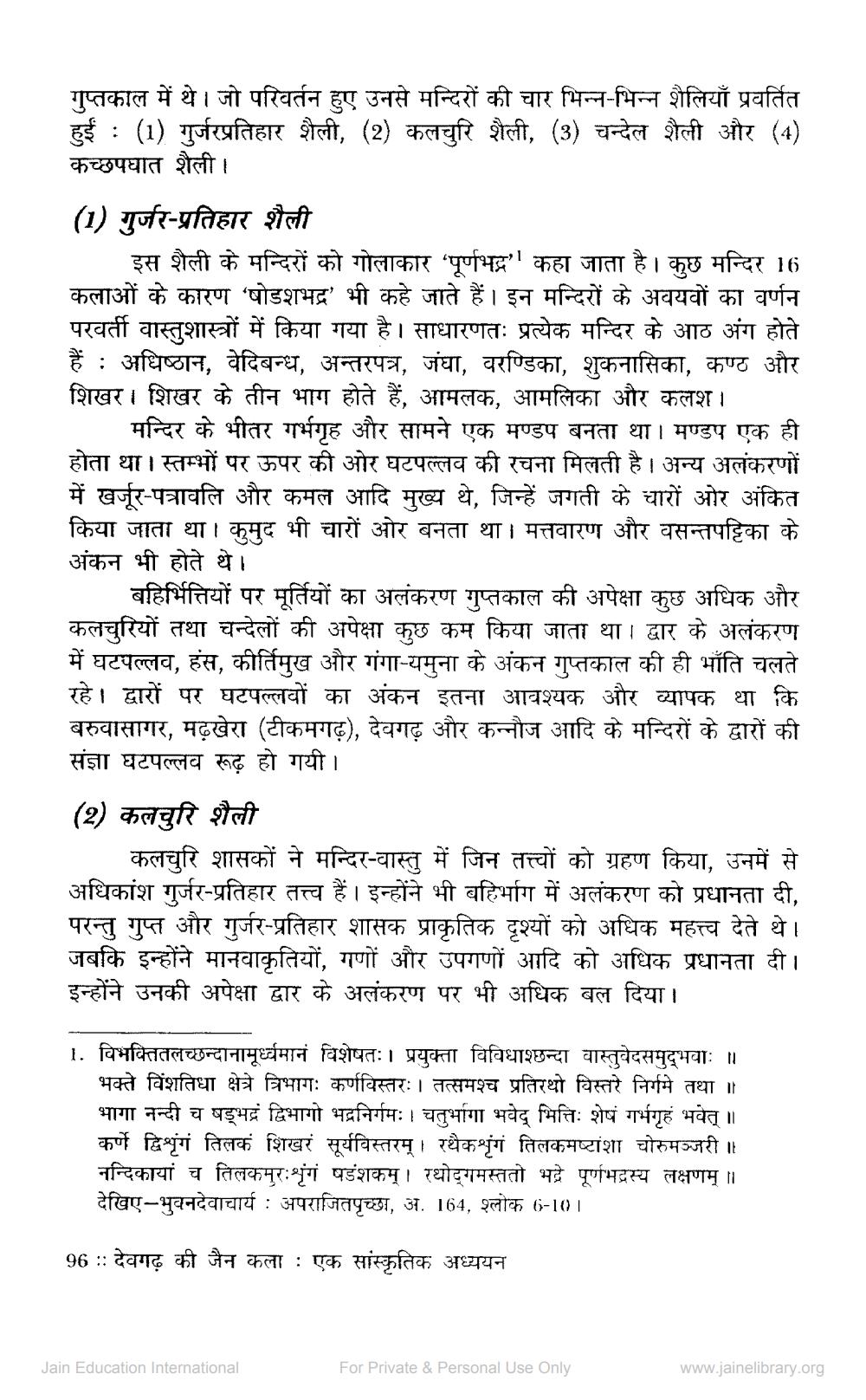________________
गुप्तकाल में थे। जो परिवर्तन हुए उनसे मन्दिरों की चार भिन्न-भिन्न शैलियाँ प्रवर्तित हुईं : (1) गुर्जरप्रतिहार शैली, (2) कलचुरि शैली, (3) चन्देल शैली और (4) कच्छपघात शैली। (1) गुर्जर-प्रतिहार शैली
__इस शैली के मन्दिरों को गोलाकार ‘पूर्णभद्र' कहा जाता है। कुछ मन्दिर 16 कलाओं के कारण 'षोडशभद्र' भी कहे जाते हैं। इन मन्दिरों के अवयवों का वर्णन परवर्ती वास्तुशास्त्रों में किया गया है। साधारणतः प्रत्येक मन्दिर के आठ अंग होते हैं : अधिष्ठान, वेदिबन्ध, अन्तरपत्र, जंघा, वरण्डिका, शुकनासिका, कण्ट और शिखर । शिखर के तीन भाग होते हैं, आमलक, आमलिका और कलश।
मन्दिर के भीतर गर्भगृह और सामने एक मण्डप बनता था। मण्डप एक ही होता था। स्तम्भों पर ऊपर की ओर घटपल्लव की रचना मिलती है। अन्य अलंकरणों में खजूर-पत्रावलि और कमल आदि मुख्य थे, जिन्हें जगती के चारों ओर अंकित किया जाता था। कुमुद भी चारों ओर बनता था। मत्तवारण और वसन्तपट्टिका के अंकन भी होते थे।
बहिर्भित्तियों पर मूर्तियों का अलंकरण गुप्तकाल की अपेक्षा कुछ अधिक और कलचुरियों तथा चन्देलों की अपेक्षा कुछ कम किया जाता था। द्वार के अलंकरण में घटपल्लव, हंस, कीर्तिमुख और गंगा-यमुना के अंकन गुप्तकाल की ही भाँति चलते रहे। द्वारों पर घटपल्लवों का अंकन इतना आवश्यक और व्यापक था कि बरुवासागर, मढ़खेरा (टीकमगढ़), देवगढ़ और कन्नौज आदि के मन्दिरों के द्वारों की संज्ञा घटपल्लव रूढ़ हो गयी। (2) कलचुरि शैली
कलचुरि शासकों ने मन्दिर-वास्तु में जिन तत्त्वों को ग्रहण किया, उनमें से अधिकांश गुर्जर-प्रतिहार तत्त्व हैं। इन्होंने भी बहिर्भाग में अलंकरण को प्रधानता दी, परन्तु गुप्त और गुर्जर-प्रतिहार शासक प्राकृतिक दृश्यों को अधिक महत्त्व देते थे। जबकि इन्होंने मानवाकृतियों, गणों और उपगणों आदि को अधिक प्रधानता दी। इन्होंने उनकी अपेक्षा द्वार के अलंकरण पर भी अधिक बल दिया।
1. विभक्तितलच्छन्दानामूर्ध्वमानं विशेषतः। प्रयुक्ता विविधाश्छन्दा वास्तुवेदसमुद्भवाः ॥
भक्ते विंशतिधा क्षेत्रे त्रिभागः कर्णविस्तरः। तत्समश्च प्रतिरथो विस्तरे निर्गमे तथा ॥ भागा नन्दी च षड्भद्रं द्विभागो भद्रनिर्गमः । चतुर्भागा भवेद् भित्तिः शेषं गर्भगृहं भवेत् ॥ कर्णे द्विशृंगं तिलकं शिखरं सूर्यविस्तरम् । रथैकशृंगं तिलकमष्टांशा चोरुमञ्जरी ॥ नन्दिकायां च तिलकमरःशृंगं षडंशकम्। रथोद्गमस्ततो भद्रे पूर्णभद्रस्य लक्षणम् ॥ देखिए-भुवनदेवाचार्य : अपराजितपृच्छा, अ. 164, श्लोक (5-10 |
96 :: देवगढ़ की जैन कला : एक सांस्कृतिक अध्ययन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org