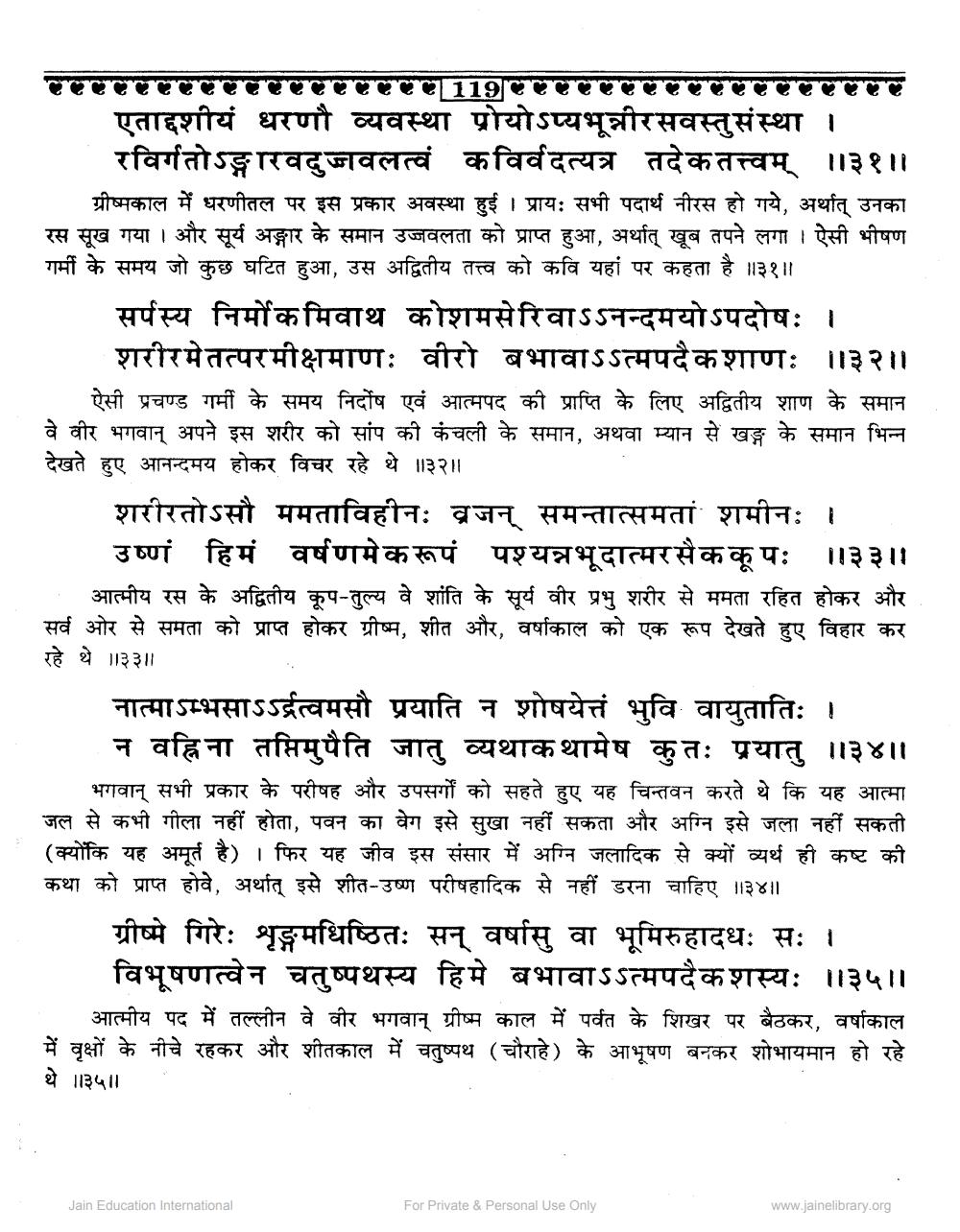________________
୧୯୯୯୯୯୯୯୯୯୯୯୯୯୪୧୦a[119୧୦୯୯୯୯୯୯୯୯୯୯୯୯୯୯୯୯
एताद्दशीयं धरणी व्यवस्था प्रोयोऽप्यभून्नीरसवस्तुसंस्था ।
रविर्गतोऽङ्गारवदुज्जवलत्वं कविर्वदत्यत्र तदेकतत्त्वम् ॥३१॥ ग्रीष्मकाल में धरणीतल पर इस प्रकार अवस्था हुई । प्रायः सभी पदार्थ नीरस हो गये, अर्थात् उनका रस सूख गया । और सूर्य अङ्गार के समान उज्जवलता को प्राप्त हुआ, अर्थात् खूब तपने लगा । ऐसी भीषण गर्मी के समय जो कछ घटित हआ, उस अद्वितीय तत्त्व को कवि यहां पर कहता है ॥३१॥
सर्पस्य निर्मोक मिवाथ कोशमसेरिवाऽऽनन्दमयोऽपदोषः । शरीर मेतत्पर मीक्षमाणः वीरो बभावाऽऽत्मपदैक शाणः ॥३२॥ ऐसी प्रचण्ड गर्मी के समय निर्दोष एवं आत्मपद की प्राप्ति के लिए अद्वितीय शाण के समान वे वीर भगवान् अपने इस शरीर को सांप की कंचली के समान, अथवा म्यान से खङ्ग के समान भिन्न देखते हुए आनन्दमय होकर विचर रहे थे ॥३२॥
शरीरतोऽसौ ममताविहीनः व्रजन् समन्तात्समतां शमीनः । उष्णं हिमं वर्षणमेक रूपं पश्यन्नभूदात्मर सैक कूपः ॥३३॥
आत्मीय रस के अद्वितीय कूप-तुल्य वे शांति के सूर्य वीर प्रभु शरीर से ममता रहित होकर और सर्व ओर से समता को प्राप्त होकर ग्रीष्म, शीत और, वर्षाकाल को एक रूप देखते हुए विहार कर रहे थे ॥३३॥
नात्माऽम्भसाऽऽर्द्रत्वमसौ प्रयाति न शोषयेत्तं भुवि वायुतातिः ।
न वह्निना तप्तिमुपैति जातु व्यथाक थामेष कुतः प्रयातु ॥३४॥ भगवान् सभी प्रकार के परीषह और उपसर्गों को सहते हुए यह चिन्तवन करते थे कि यह आत्मा जल से कभी गीला नहीं होता, पवन का वेग इसे सुखा नहीं सकता और अग्नि इसे जला नहीं सकती (क्योंकि यह अमूर्त है) । फिर यह जीव इस संसार में अग्नि जलादिक से क्यों व्यर्थ ही कष्ट की कथा को प्राप्त होवे, अर्थात् इसे शीत-उष्ण परीषहादिक से नहीं डरना चाहिए ॥३४॥
ग्रीष्मे गिरेः शृङ्गमधिष्ठितः सन् वर्षासु वा भूमिरुहादधः सः । विभूषणत्वेन चतुष्पथस्य हि मे बभावाऽऽत्मपदैक शस्यः ॥३५।।
आत्मीय पद में तल्लीन वे वीर भगवान् ग्रीष्म काल में पर्वत के शिखर पर बैठकर, वर्षाकाल में वृक्षों के नीचे रहकर और शीतकाल में चतुष्पथ (चौराहे) के आभूषण बनकर शोभायमान हो रहे थे ॥३५॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org