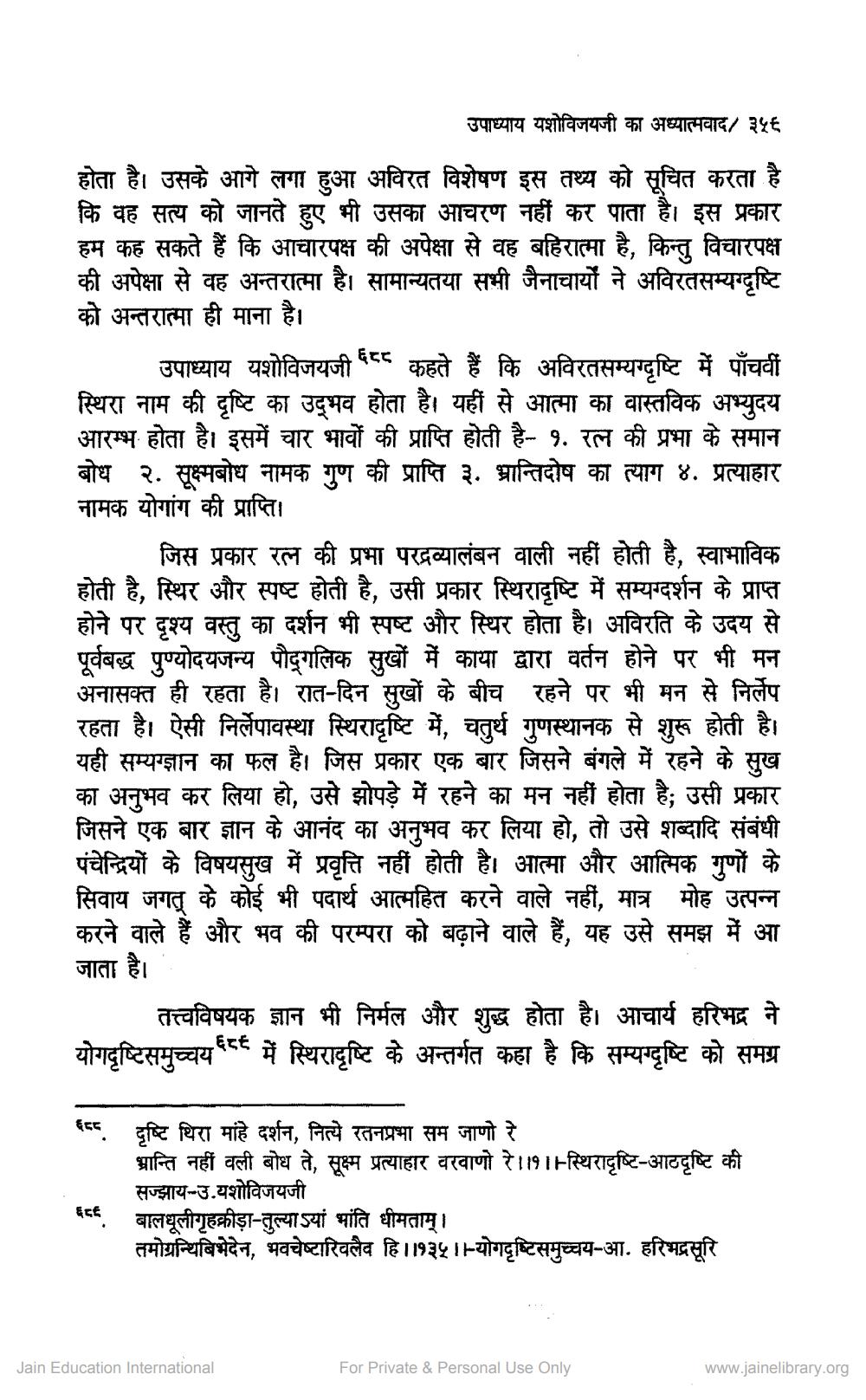________________
उपाध्याय यशोविजयजी का अध्यात्मवाद/ ३५६
होता है। उसके आगे लगा हुआ अविरत विशेषण इस तथ्य को सूचित करता है कि वह सत्य को जानते हुए भी उसका आचरण नहीं कर पाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचारपक्ष की अपेक्षा से वह बहिरात्मा है, किन्तु विचारपक्ष की अपेक्षा से वह अन्तरात्मा है। सामान्यतया सभी जैनाचार्यों ने अविरतसम्यग्दृष्टि को अन्तरात्मा ही माना है।
उपाध्याय यशोविजयजी ६६८ कहते हैं कि अविरतसम्यग्दृष्टि में पाँचवीं स्थिरा नाम की दृष्टि का उद्भव होता है। यहीं से आत्मा का वास्तविक अभ्युदय
आरम्भ होता है। इसमें चार भावों की प्राप्ति होती है- १. रन की प्रभा के समान बोध २. सूक्ष्मबोध नामक गुण की प्राप्ति ३. भ्रान्तिदोष का त्याग ४. प्रत्याहार नामक योगांग की प्राप्ति।
जिस प्रकार रत्न की प्रभा परद्रव्यालंबन वाली नहीं होती है, स्वाभाविक होती है, स्थिर और स्पष्ट होती है, उसी प्रकार स्थिरादृष्टि में सम्यग्दर्शन के प्राप्त होने पर दृश्य वस्तु का दर्शन भी स्पष्ट और स्थिर होता है। अविरति के उदय से पूर्वबद्ध पुण्योदयजन्य पौद्गलिक सुखों में काया द्वारा वर्तन होने पर भी मन अनासक्त ही रहता है। रात-दिन सुखों के बीच रहने पर भी मन से निर्लेप रहता है। ऐसी निर्लेपावस्था स्थिरादृष्टि में, चतुर्थ गुणस्थानक से शुरू होती है। यही सम्यग्ज्ञान का फल है। जिस प्रकार एक बार जिसने बंगले में रहने के सुख का अनुभव कर लिया हो, उसे झोपड़े में रहने का मन नहीं होता है; उसी प्रकार जिसने एक बार ज्ञान के आनंद का अनुभव कर लिया हो, तो उसे शब्दादि संबंधी पंचेन्द्रियों के विषयसुख में प्रवृत्ति नहीं होती है। आत्मा और आत्मिक गुणों के सिवाय जगत् के कोई भी पदार्थ आत्महित करने वाले नहीं, मात्र मोह उत्पन्न करने वाले हैं और भव की परम्परा को बढ़ाने वाले हैं, यह उसे समझ में आ जाता है।
तत्त्वविषयक ज्ञान भी निर्मल और शुद्ध होता है। आचार्य हरिभद्र ने योगदृष्टिसमुच्चय ६६ में स्थिरादृष्टि के अन्तर्गत कहा है कि सम्यग्दृष्टि को समग्र
६८८. दृष्टि थिरा माहे दर्शन, नित्ये रतनप्रभा सम जाणो रे
भ्रान्ति नहीं वली बोध ते, सूक्ष्म प्रत्याहार वरवाणो रे।।१। स्थिरादृष्टि-आठदृष्टि की सज्झाय-उ.यशोविजयजी बालधूलीगृहक्रीड़ा-तुल्याऽयां भांति धीमताम्। तमोग्रन्थिबिभेदेन, भवचेष्टारिवलैव हि।।१३५।। योगदृष्टिसमुच्चय-आ. हरिभद्रसूरि
६८६.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org