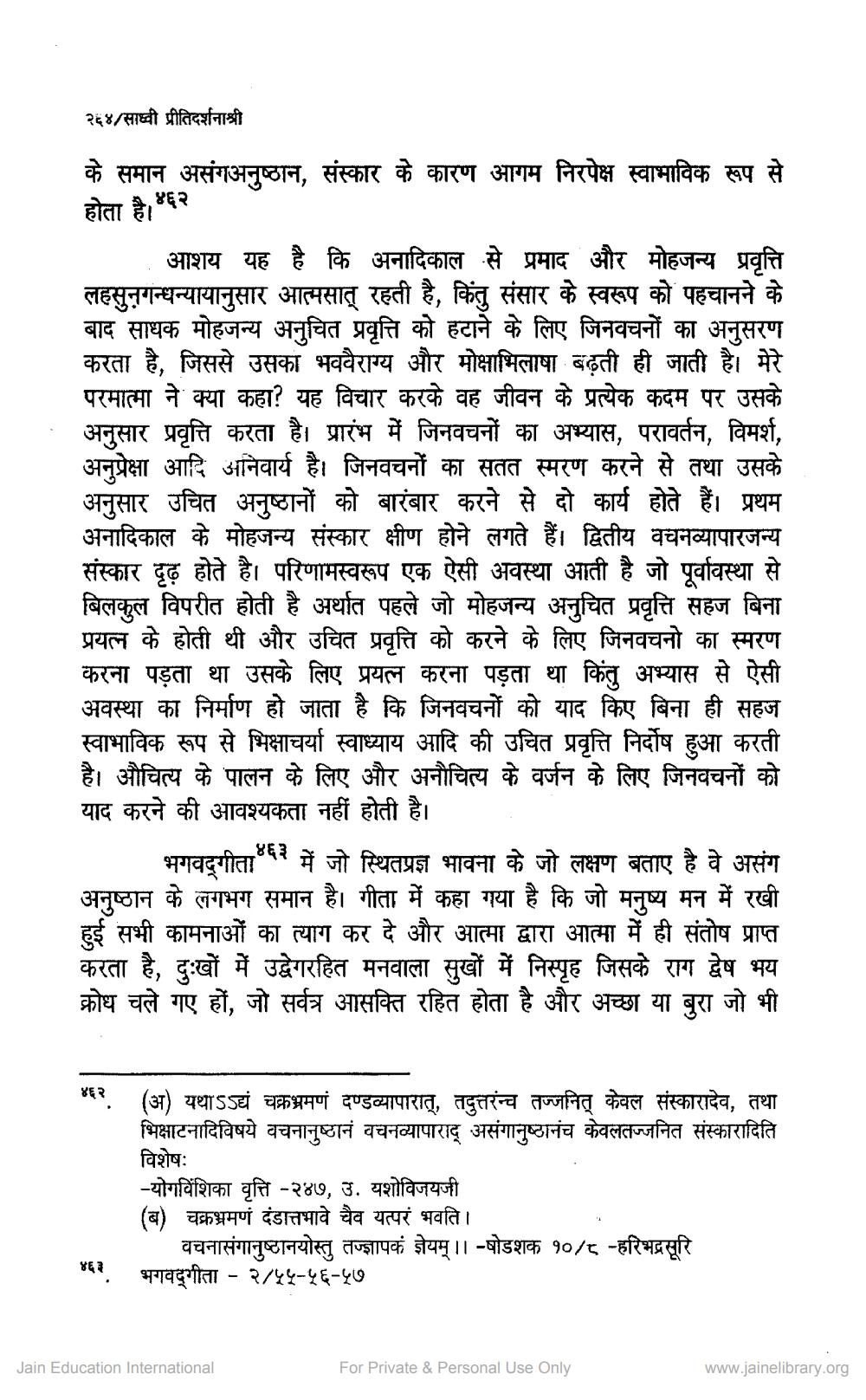________________
२६४/साध्वी प्रीतिदर्शनाश्री
के समान असंगअनुष्ठान, संस्कार के कारण आगम निरपेक्ष स्वाभाविक रूप से होता है।४६२
. आशय यह है कि अनादिकाल से प्रमाद और मोहजन्य प्रवृत्ति लहसुनगन्धन्यायानुसार आत्मसात् रहती है, किंतु संसार के स्वरूप को पहचानने के बाद साधक मोहजन्य अनुचित प्रवृत्ति को हटाने के लिए जिनवचनों का अनुसरण करता है, जिससे उसका भववैराग्य और मोक्षाभिलाषा बढ़ती ही जाती है। मेरे परमात्मा ने क्या कहा? यह विचार करके वह जीवन के प्रत्येक कदम पर उसके अनुसार प्रवृत्ति करता है। प्रारंभ में जिनवचनों का अभ्यास, परावर्तन, विमर्श, अनुप्रेक्षा आदि आनेवार्य है। जिनवचनों का सतत स्मरण करने से तथा उसके अनुसार उचित अनुष्ठानों को बारंबार करने से दो कार्य होते हैं। प्रथम अनादिकाल के मोहजन्य संस्कार क्षीण होने लगते हैं। द्वितीय वचनव्यापारजन्य संस्कार दृढ़ होते है। परिणामस्वरूप एक ऐसी अवस्था आती है जो पूर्वावस्था से बिलकुल विपरीत होती है अर्थात पहले जो मोहजन्य अनुचित प्रवृत्ति सहज बिना प्रयत्न के होती थी और उचित प्रवृत्ति को करने के लिए जिनवचनो का स्मरण करना पड़ता था उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता था किंतु अभ्यास से ऐसी अवस्था का निर्माण हो जाता है कि जिनवचनों को याद किए बिना ही सहज स्वाभाविक रूप से भिक्षाचर्या स्वाध्याय आदि की उचित प्रवृत्ति निर्दोष हुआ करती है। औचित्य के पालन के लिए और अनौचित्य के वर्जन के लिए जिनवचनों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है।
भगवद्गीता ५२ में जो स्थितप्रज्ञ भावना के जो लक्षण बताए है वे असंग अनुष्ठान के लगभग समान है। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य मन में रखी हुई सभी कामनाओं का त्याग कर दे और आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, दुःखों में उद्वेगरहित मनवाला सुखों में निस्पृह जिसके राग द्वेष भय क्रोध चले गए हों, जो सर्वत्र आसक्ति रहित होता है और अच्छा या बुरा जो भी
४६२. (अ) यथाऽऽद्यं चक्रभ्रमणं दण्डव्यापारात्, तदुत्तरंन्च तज्जनित् केवल संस्कारादेव, तथा
भिक्षाटनादिविषये वचनानुष्ठानं वचनव्यापाराद् असंगानुष्ठानंच केवलतज्जनित संस्कारादिति विशेषः -योगविंशिका वृत्ति -२४७, उ. यशोविजयजी (ब) चक्रभ्रमणं दंडात्तभावे चैव यत्परं भवति।
वचनासंगानुष्ठानयोस्तु तज्ज्ञापकं ज्ञेयम् ।। -षोडशक १०/८ -हरिभद्रसूरि ४६३. भगवद्गीता - २/५५-५६-५७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org