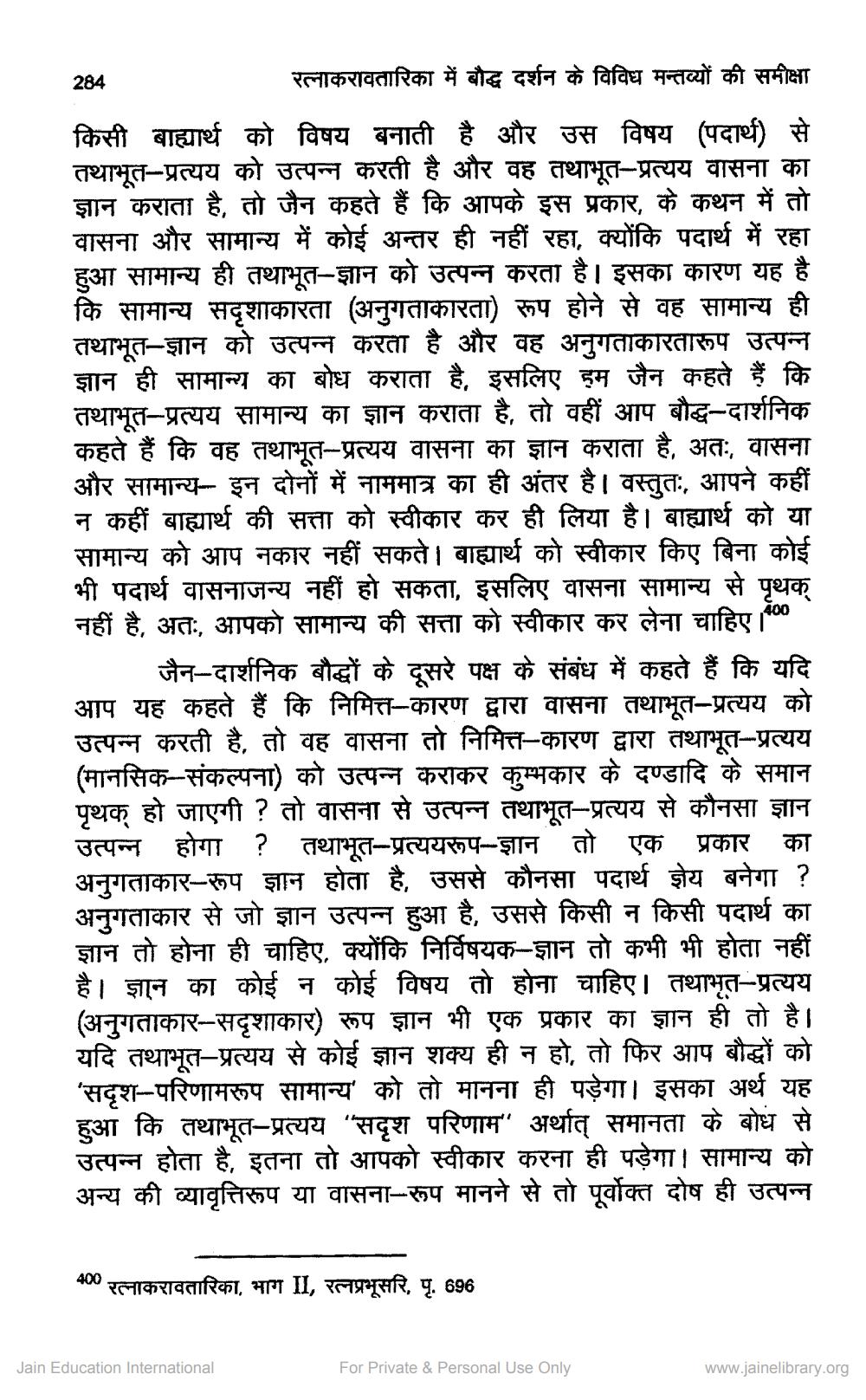________________
284
रत्नाकरावतारिका में बौद्ध दर्शन के विविध मन्तव्यों की समीक्षा
किसी बाह्यार्थ को विषय बनाती है और उस विषय (पदार्थ) से तथाभूत-प्रत्यय को उत्पन्न करती है और वह तथाभूत-प्रत्यय वासना का ज्ञान कराता है, तो जैन कहते हैं कि आपके इस प्रकार, के कथन में तो वासना और सामान्य में कोई अन्तर ही नहीं रहा, क्योंकि पदार्थ में रहा हुआ सामान्य ही तथाभूत-ज्ञान को उत्पन्न करता है। इसका कारण यह है कि सामान्य सदृशाकारता (अनुगताकारता) रूप होने से वह सामान्य ही तथाभूत-ज्ञान को उत्पन्न करता है और वह अनुगताकारतारूप उत्पन्न ज्ञान ही सामान्य का बोध कराता है, इसलिए हम जैन कहते हैं कि तथाभूत-प्रत्यय सामान्य का ज्ञान कराता है, तो वहीं आप बौद्ध-दार्शनिक कहते हैं कि वह तथाभूत-प्रत्यय वासना का ज्ञान कराता है, अतः, वासना और सामान्य- इन दोनों में नाममात्र का ही अंतर है। वस्तुतः, आपने कहीं न कहीं बाह्यार्थ की सत्ता को स्वीकार कर ही लिया है। बाह्यार्थ को या सामान्य को आप नकार नहीं सकते। बाह्यार्थ को स्वीकार किए बिना कोई भी पदार्थ वासनाजन्य नहीं हो सकता, इसलिए वासना सामान्य से पृथक् नहीं है, अतः, आपको सामान्य की सत्ता को स्वीकार कर लेना चाहिए। 00
जैन-दार्शनिक बौद्धों के दूसरे पक्ष के संबंध में कहते हैं कि यदि आप यह कहते हैं कि निमित्त-कारण द्वारा वासना तथाभूत-प्रत्यय को उत्पन्न करती है, तो वह वासना तो निमित्त-कारण द्वारा तथाभूत-प्रत्यय (मानसिक-संकल्पना) को उत्पन्न कराकर कुम्भकार के दण्डादि के समान पृथक हो जाएगी ? तो वासना से उत्पन्न तथाभूत-प्रत्यय से कौनसा ज्ञान उत्पन्न होगा ? तथाभूत-प्रत्ययरूप-ज्ञान तो एक प्रकार का अनुगताकार-रूप ज्ञान होता है, उससे कौनसा पदार्थ ज्ञेय बनेगा ? अनुगताकार से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उससे किसी न किसी पदार्थ का ज्ञान तो होना ही चाहिए, क्योंकि निर्विषयक-ज्ञान तो कभी भी होता नहीं है। ज्ञान का कोई न कोई विषय तो होना चाहिए। तथाभूत-प्रत्यय (अनुगताकार-सदृशाकार) रूप ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान ही तो है। यदि तथाभूत-प्रत्यय से कोई ज्ञान शक्य ही न हो, तो फिर आप बौद्धों को 'सदृश-परिणामरूप सामान्य' को तो मानना ही पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि तथाभूत-प्रत्यय “सदृश परिणाम' अर्थात् समानता के बोध से उत्पन्न होता है, इतना तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। सामान्य को अन्य की व्यावृत्तिरूप या वासना-रूप मानने से तो पूर्वोक्त दोष ही उत्पन्न
400 रत्नाकरावतारिका, भाग II, रत्नप्रभूसरि, पृ. 696
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org