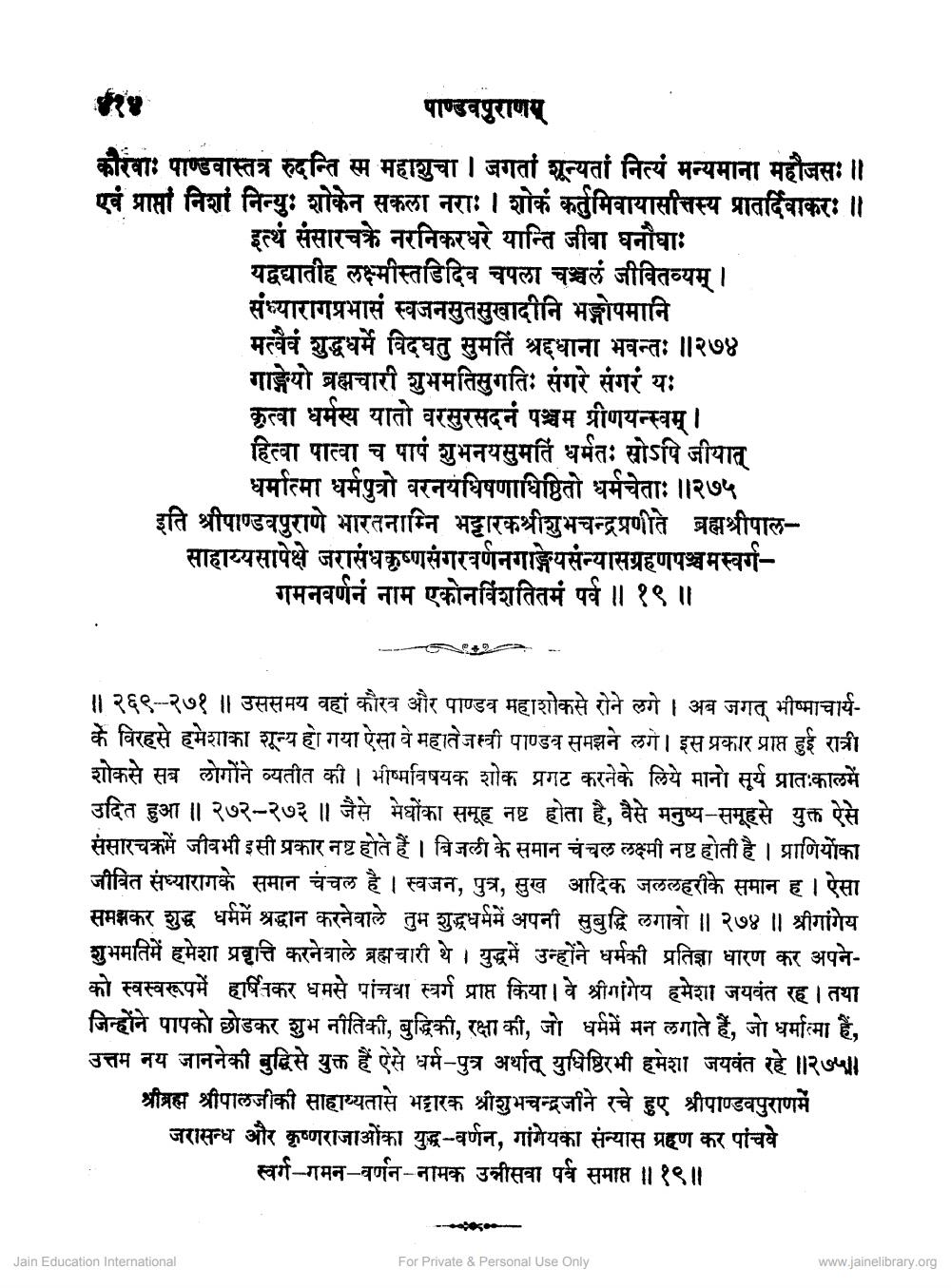________________
पाण्डवपुराणम् कौरवाः पाण्डवास्तत्र रुदन्ति स्म महाशुचा । जगतां शून्यतां नित्यं मन्यमाना महौजसः ।। एवं प्राप्तां निशां निन्युः शोकेन सकला नराः । शोकं कर्तुमिवायासीत्तस्य प्रातर्दिवाकरः ॥
इत्थं संसारचक्रे नरनिकरधरे यान्ति जीवा घनौषाः यद्वद्यातीह लक्ष्मीस्तडिदिव चपला चञ्चलं जीवितव्यम् । संध्यारागप्रभासं स्वजनसुतसुखादीनि भङ्गोपमानि मत्वैवं शुद्धधर्मे विदघतु सुमतिं श्रद्दधाना भवन्तः ॥२७४ गाङ्गेयो ब्रह्मचारी शुभमतिसुगतिः संगरे संगरं यः कृत्वा धर्मस्य यातो वरसुरसदनं पञ्चम प्रीणयन्स्वम् । हित्वा पात्वा च पापं शुभनयसुमतिं धर्मतः सोऽपि जीयात्
धर्मात्मा धर्मपुत्रो वरनयंधिषणाधिष्ठितो धर्मचेताः॥२७५ इति श्रीपाण्डवपुराणे भारतनाम्नि भट्टारकश्रीशुभचन्द्रप्रणीते ब्रह्मश्रीपालसाहाय्यसापेक्षे जरासंधकृष्णसंगरवर्णनगाङ्गेयसंन्यासग्रहणपञ्चमस्वर्ग
___ गमनवर्णनं नाम एकोनविंशतितमं पर्व ॥ १९ ॥
।। २६९-२७१ ।। उससमय वहां कौरव और पाण्डव महाशोकसे रोने लगे । अब जगत् भीष्माचार्यके विरहसे हमेशाका शून्य हो गया ऐसा वे महातेजस्वी पाण्डव समझने लगे। इस प्रकार प्राप्त हुई रात्री शोकसे सब लोगोंने व्यतीत की । भीष्मविषयक शोक प्रगट करनेके लिये मानो सूर्य प्रातःकालमें उदित हुआ ॥ २७२-२७३ ।। जैसे मेघोंका समूह नष्ट होता है, वैसे मनुष्य-समूहसे युक्त ऐसे संसारचक्र जीवभी इसी प्रकार नष्ट होते हैं । बिजली के समान चंचल लक्ष्मी नष्ट होती है । प्राणियोंका जीवित संध्यारागके समान चंचल है । स्वजन, पुत्र, सुख आदिक जललहरीके समान ह । ऐसा समझकर शुद्ध धर्ममें श्रद्धान करनेवाले तुम शुद्धधर्ममें अपनी सुबुद्धि लगावो || २७४ ॥ श्रीगांगेय शुभमतिमें हमेशा प्रवृत्ति करनेवाले ब्रह्मचारी थे। युद्धमें उन्होंने धर्मकी प्रतिज्ञा धारण कर अपनेको स्वस्वरूपमें हर्षितकर धमसे पांचवा स्वर्ग प्राप्त किया। वे श्रीगांगेय हमेशा जयवंत रह । तथा जिन्होंने पापको छोडकर शुभ नीतिकी, बुद्धिकी, रक्षा की, जो धर्ममें मन लगाते हैं, जो धर्मात्मा हैं, उत्तम नय जाननेकी बुद्धिसे युक्त हैं ऐसे धर्म-पुत्र अर्थात् युधिष्ठिरभी हमेशा जयवंत रहे ॥२७५॥
श्रीब्रह्म श्रीपालजीकी साहाय्यतासे भट्टारक श्रीशुभचन्द्र ने रचे हुए श्रीपाण्डवपुराणमें जरासन्ध और कृष्णराजाओंका युद्ध-वर्णन, गांगेयका संन्यास ग्रहण कर पांचवे
स्वर्ग-गमन-वर्णन-नामक उन्नीसवा पर्व समाप्त ॥१९॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org