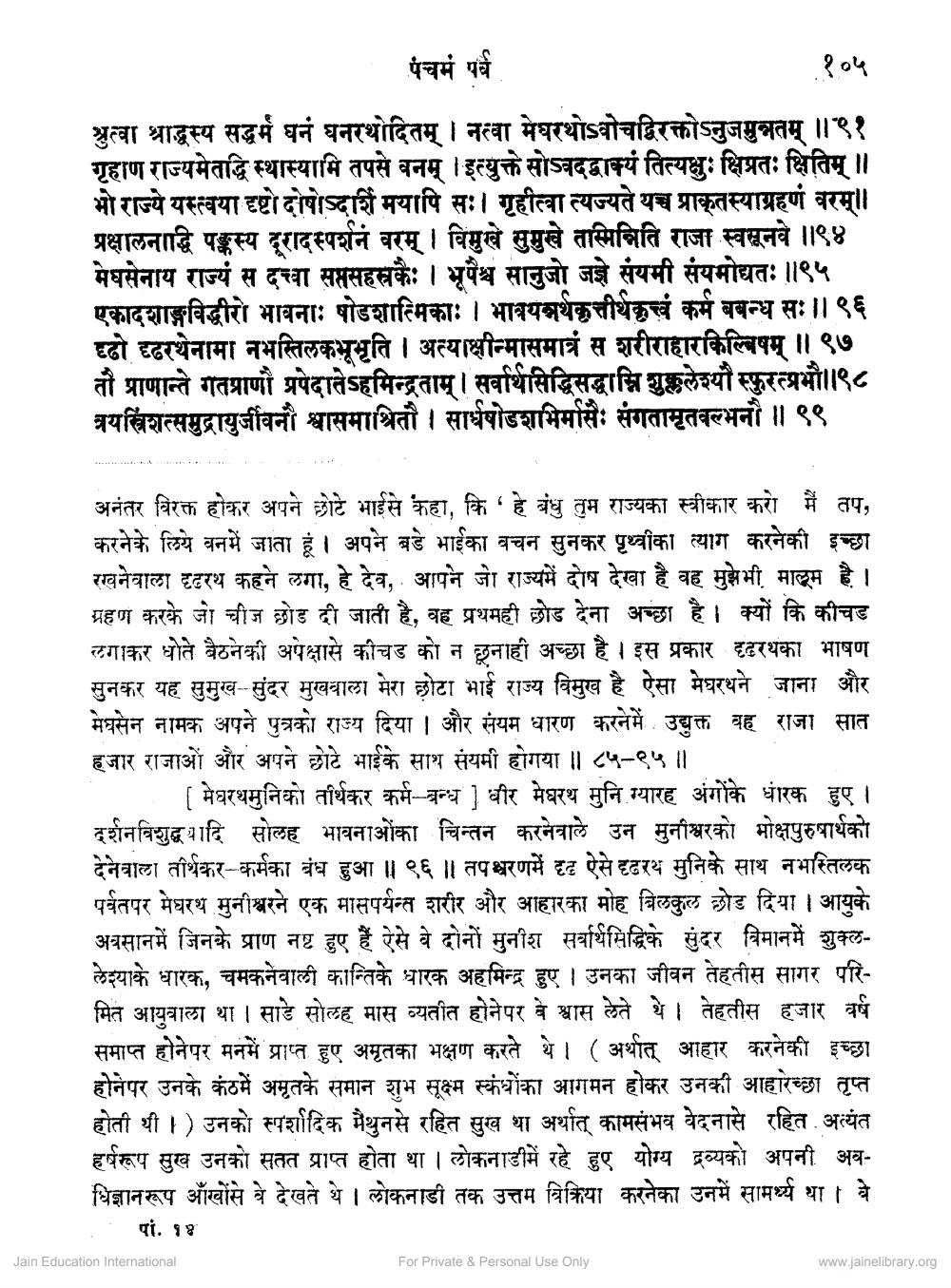________________
.१०५
पंचमं पर्व श्रुत्वा श्राद्धस्य सद्धर्म धनं धनरथोदितम् । नत्वा मेघरथोऽवोचद्विरक्तोऽनुजमुन्नतम् ॥९१ गृहाण राज्यमेतद्धि स्थास्यामि तपसे वनम् । इत्युक्ते सोजदद्वाक्यं तित्यक्षुः क्षिप्रतः क्षितिम् ॥ भोराज्ये यस्त्वया दृष्टो दोषोऽदार्श मयापि सः। गृहीत्वा त्यज्यते यच्च प्राक्तस्याग्रहणं वरम्।। प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् । विमुखे सुमुखे तस्मिन्निति राजा स्वसूनवे ॥९४ मेघसेनाय राज्यं स दत्त्वा सप्तसहस्रकैः । भूपैश्च सानुजो जज्ञे संयमी संयमोद्यतः ॥९५ एकादशाङ्गविद्धीरो भावनाः षोडशात्मिकाः । भावयनर्थकृतीर्थकृत्वं कर्म बबन्ध सः।। ९६ दृढो दृढरथेनामा नभस्तिलकभूभृति । अत्याक्षीन्मासमात्रं स शरीराहारकिल्विषम् ॥ ९७ तौ प्राणान्ते गतप्राणौ प्रपेदातेऽहमिन्द्रताम् । सर्वार्थसिद्धिसद्धानि शुक्ललेश्यौ स्फुरत्प्रभौ।।९८ त्रयस्त्रिंशत्समुद्रायुर्जीवनौ श्वासमाश्रितौ । सार्धषोडशभिर्मासैः संगतामृतवल्भनौ ।। ९९
अनंतर विरक्त होकर अपने छोटे भाईसे कहा, कि ' हे बंधु तुम राज्यका स्वीकार करो मैं तप, करनेके लिये वनमें जाता हूं। अपने बड़े भाईका वचन सुनकर पृथ्वीका त्याग करनेकी इच्छा रखनेवाला दृढरथ कहने लगा, हे देव, आपने जो राज्यमें दोष देखा है वह मुझेभी मालूम है। ग्रहण करके जो चीज छोड दी जाती है, वह प्रथमही छोड देना अच्छा है। क्यों कि कीचड लगाकर धोते बैठने की अपेक्षासे कीचड को न छूनाही अच्छा है । इस प्रकार दृढरथका भाषण सुनकर यह सुमुख-सुंदर मुखवाला मेरा छोटा भाई राज्य विमुख है ऐसा मेघरथने जाना और मेघसेन नामक अपने पुत्रको राज्य दिया । और संयम धारण करनेमें उद्युक्त वह राजा सात हजार राजाओं और अपने छोटे भाईके साथ संयमी होगया ॥ ८५-९५ ॥
[ मेघरथमुनिको तीर्थकर कर्म-बन्ध ] धीर मेघरथ मुनि ग्यारह अंगोंके धारक हुए। दर्शनविशुद्धयादि सोलह भावनाओंका चिन्तन करनेवाले उन मुनीश्वरको मोक्षपुरुषार्थको देनेवाला तीर्थकर-कर्मका बंध हुआ ॥ ९६ ॥ तपश्चरणमें दृढ ऐसे दृढरथ मुनिके साथ नभस्तिलक पर्वतपर मेघरथ मुनीश्वरने एक मासपर्यन्त शरीर और आहारका मोह बिलकुल छोड दिया । आयुके अवसानमें जिनके प्राण नष्ट हुए हैं ऐसे वे दोनों मुनीश सर्वार्थसिद्धिके सुंदर विमानमें शुक्ललेझ्याके धारक, चमकनेवाली कान्तिके धारक अहमिन्द्र हुए । उनका जीवन तेहतीस सागर परिमित आयुवाला था । साडे सोलह मास व्यतीत होनेपर वे श्वास लेते थे। तेहतीस हजार वर्ष समाप्त होनेपर मनमें प्राप्त हुए अमृतका भक्षण करते थे। ( अर्थात् आहार करनेकी इच्छा होनेपर उनके कंठमें अमृतके समान शुभ सूक्ष्म स्कंधोंका आगमन होकर उनकी आहारेच्छा तृप्त होती थी। ) उनको स्पर्शादिक मैथुनसे रहित सुख था अर्थात् कामसंभव वेदनासे रहित अत्यंत हर्षरूप सुख उनको सतत प्राप्त होता था । लोकनाडीमें रहे हुए योग्य द्रव्यको अपनी अवविज्ञानरूप आँखोंसे वे देखते थे । लोकनाडी तक उत्तम विक्रिया करनेका उनमें सामर्थ्य था। वे
पां. १४
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org