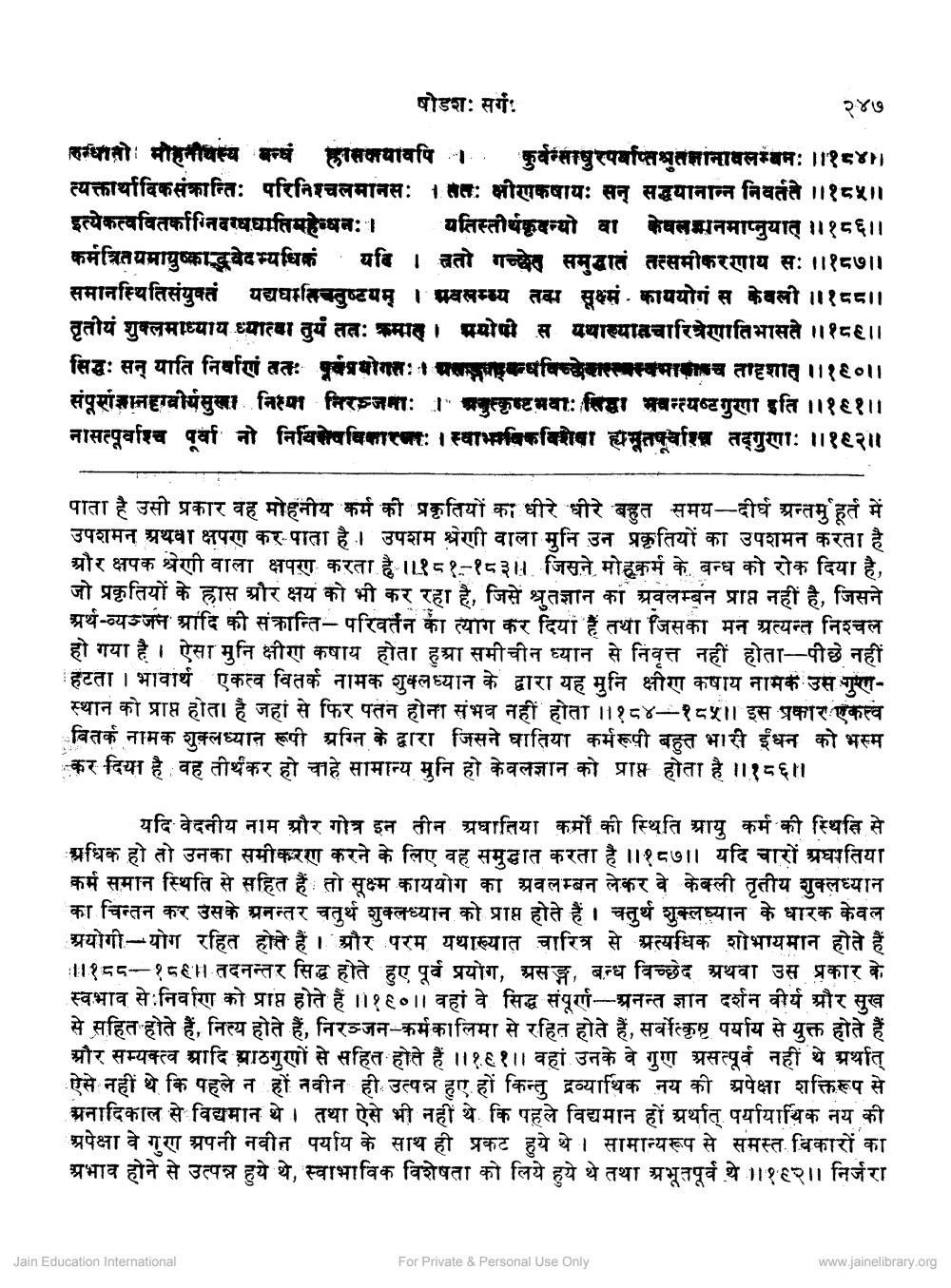________________
षोडशः सर्गः
२४७ सिन्धातोः मोहनीवस्य बन्धं हासमयावपि । कुर्वन्साधुरपप्तिश्रुतमानावलम्बनः ।।१४।। त्यक्तार्थादिकसंक्रान्ति: परिनिश्चलमानसः । सत: क्षीणकषायः सन् सद्धयानान्न निवर्तते ।।१८५॥ इत्येकत्ववितर्काग्निवग्धघातिमहेन्धनः। यतिस्तीर्यकृदन्यो वा केवलहानमाप्नुयात् ॥१८६।। कर्मत्रितयमायुष्काद्भवेदभ्यधिकं । यदि । ततो गच्छेत समुखातं तत्समीकरणाय सः ।।१८७॥ समानस्थितिसंयुक्तं यद्यपातिचतुष्टयम् । अवलम्म्य तका सूक्ष्म . काययोगं स केवली ॥१८८।। तृतीयं शुक्लमाध्याय ध्यात्या तुर्य ततः क्रमात् । प्रयोफी स यथाख्यातचारित्रेणातिभासते ॥१८६।। सिद्धः सन् याति निर्वाणं ततः पूर्वप्रयोगतः सनाधविच्छेनारास्वमाकच तादृशात् ।।१६।। संपूर्णजातहग्वीर्यसुखा निस्या निरजमाः । अनुत्कृष्टमवा: लिखा भवन्त्यष्टगुणा इति ।।१६१।। नासत्पूर्वाश्च पूर्वा नो निविशेषविकारणाः । स्वाभाविकविशेषा ह्यभूतपूरिन तद्गुणाः ॥१९॥
पाता है उसी प्रकार वह मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का धीरे धीरे बहुत समय-दीर्घ अन्तमुहर्त में उपशमन अथवा क्षपण कर पाता है। उपशम श्रेणी वाला मुनि उन प्रकृतियों का उपशमन करता है और क्षपक श्रेणी वाला क्षपण करता है ।।१८१-१८३।। जिसने मोहकर्म के बन्ध को रोक दिया है, जो प्रकृतियों के ह्रास और क्षय को भी कर रहा है, जिसे श्रुतज्ञान का अवलम्बन प्राप्त नहीं है, जिसने अर्थ-व्यञ्जन आदि की संक्रान्ति-परिवर्तन का त्याग कर दिया है तथा जिसका मन अत्यन्त निश्चल हो गया है। ऐसा मुनि क्षीण कषाय होता हुआ समीचीन ध्यान से निवृत्त नहीं होता-पीछे नहीं हटता । भावार्थ एकत्व वितर्क नामक शुक्लध्यान के द्वारा यह मुनि क्षीण कषाय नामक उस गुणस्थान को प्राप्त होता है जहां से फिर पतन होना संभव नहीं होता ।।१८४-१८५। इस प्रकार एकत्त्व वितर्क नामक शुक्लध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिसने घातिया कर्मरूपी बहुत भारी ईंधन को भस्म कर र दिया है वह तीर्थकर हो चाहे सामान्य मुनि हो केवलज्ञान को प्राप्त होता है ।।१८६॥
यदि वेदनीय नाम और गोत्र इन तीन अधातिया कर्मों की स्थिति आयु कर्म की स्थिति से अधिक हो तो उनका समीकरण करने के लिए वह समुद्धात करता है ॥१८७।। यदि चारों अघातिया कर्म समान स्थिति से सहित हैं तो सूक्ष्म काययोग का अवलम्बन लेकर वे केवली तृतीय शुक्लध्यान का चिन्तन कर उसके अनन्तर चतुर्थ शुक्लध्यान को प्राप्त होते हैं। चतुर्थ शुक्लध्यान के धारक केवल अयोगी-योग रहित होते हैं। और परम यथाख्यात चारित्र से अत्यधिक शोभायमान होते हैं ॥१८८-१८६।। तदनन्तर सिद्ध होते हुए पूर्व प्रयोग, असङ्ग, बन्ध विच्छेद अथवा उस प्रकार के स्वभाव से निरिण को प्राप्त होते हैं ।।१६० ।। वहां वे सिद्ध संपूर्ण-अनन्त ज्ञान दर्शन वीर्य और सुख से सहित होते हैं, नित्य होते हैं, निरञ्जन-कर्मकालिमा से रहित होते हैं, सर्वोत्कृष्ट पर्याय से युक्त होते हैं और सम्यक्त्व आदि प्राठगुरणों से सहित होते हैं ।।१६।। वहां उनके वे गुण असत्पूर्व नहीं थे अर्थात् ऐसे नहीं थे कि पहले न हों नवीन ही उत्पन्न हुए हों किन्तु द्रव्याथिक नय की अपेक्षा शक्तिरूप से अनादिकाल से विद्यमान थे। तथा ऐसे भी नहीं थे कि पहले विद्यमान हों अर्थात् पर्यायाथिक नय की अपेक्षा वे गुरण अपनी नवीन पर्याय के साथ ही प्रकट हुये थे। सामान्यरूप से समस्त विकारों का अभाव होने से उत्पन्न हुये थे, स्वाभाविक विशेषता को लिये हुये थे तथा अभूतपूर्व थे ॥१९२।। निर्जरा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org