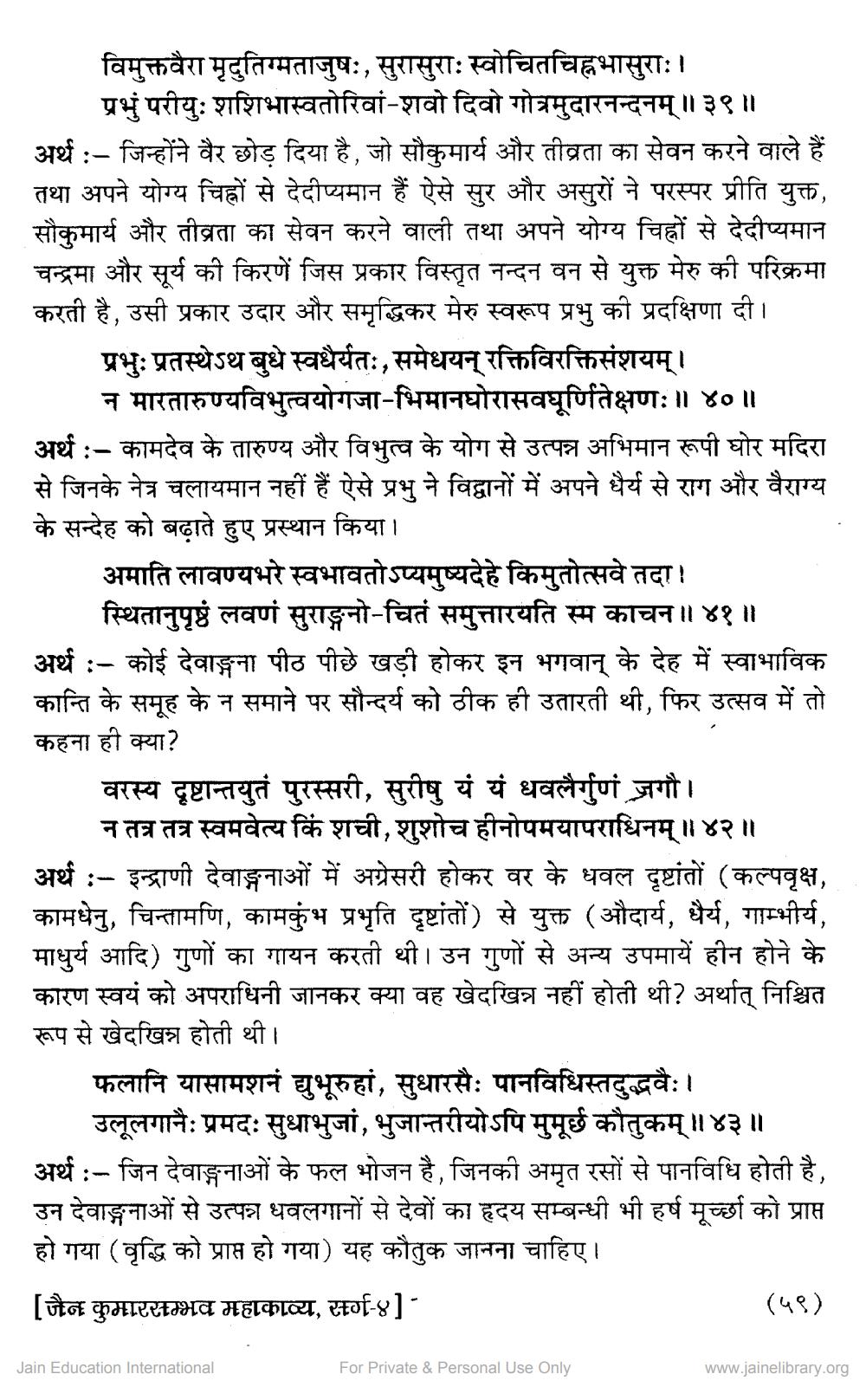________________
विमुक्तवैरा मृदुतिग्मताजुषः, सुरासुराः स्वोचितचिह्नभासुराः ।
प्रभुं परीयुः शशिभास्वतोरिवां शवो दिवो गोत्रमुदारनन्दनम् ॥ ३९॥
-
अर्थ :- जिन्होंने वैर छोड़ दिया है, जो सौकुमार्य और तीव्रता का सेवन करने वाले हैं तथा अपने योग्य चिह्नों से देदीप्यमान हैं ऐसे सुर और असुरों ने परस्पर प्रीति युक्त, सौकुमार्य और तीव्रता का सेवन करने वाली तथा अपने योग्य चिह्नों से देदीप्यमान चन्द्रमा और सूर्य की किरणें जिस प्रकार विस्तृत नन्दन वन से युक्त मेरु की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार उदार और समृद्धिकर मेरु स्वरूप प्रभु की प्रदक्षिणा दी ।
प्रभुः प्रतस्थेऽथ बुधे स्वधैर्यतः, समेधयन् रक्तिविरक्तिसंशयम् । मारतारुण्यविभुत्वयोगजा-भिमानघोरासवघूर्णितेक्षणः ॥ ४० ॥
न
अर्थ :- कामदेव के तारुण्य और विभुत्व के योग से उत्पन्न अभिमान रूपी घोर मदिरा से जिनके नेत्र चलायमान नहीं हैं ऐसे प्रभु ने विद्वानों में अपने धैर्य से राग और वैराग्य के सन्देह को बढ़ाते हुए प्रस्थान किया।
अमाति लावण्यभरे स्वभावतोऽप्यमुष्यदेहे किमुतोत्सवे तदा । स्थितानुपृष्ठं लवणं सुराङ्गनो-चितं समुत्तारयति स्म काचन ॥ ४१ ॥
अर्थ :कोई देवाङ्गना पीठ पीछे खड़ी होकर इन भगवान् के देह में स्वाभाविक कान्ति के समूह के न समाने पर सौन्दर्य को ठीक ही उतारती थी, फिर उत्सव में तो कहना ही क्या ?
वरस्य दृष्टान्तयुतं पुरस्सरी, सुरीषु यं यं धवलैर्गुणं जगौ ।
न तत्र तत्र स्वमवेत्य किं शची, शुशोच हीनोपमयापराधिनम् ॥ ४२ ॥
अर्थ :इन्द्राणी देवाङ्गनाओं में अग्रेसरी होकर वर के धवल दृष्टांतों ( कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिन्तामणि, कामकुंभ प्रभृति दृष्टांतों) से युक्त ( औदार्य, धैर्य, गाम्भीर्य, माधुर्य आदि) गुणों का गायन करती थी । उन गुणों से अन्य उपमायें हीन होने के कारण स्वयं को अपराधिनी जानकर क्या वह खेदखिन्न नहीं होती थी? अर्थात् निश्चित रूप से खेदखिन्न होती थी ।
फलानि यासामशनं द्युभूरुहां, सुधारसैः पानविधिस्तदुद्भवैः ।
उलूलगानैः प्रमदः सुधाभुजां, भुजान्तरीयोऽपि मुमूर्छ कौतुकम् ॥ ४३ ॥ अर्थ :- जिन देवाङ्गनाओं के फल भोजन है, जिनकी अमृत रसों से पानविधि होती है, उन देवाङ्गनाओं से उत्पन्न धवलगानों से देवों का हृदय सम्बन्धी भी हर्ष मूर्च्छा को प्राप्त हो गया (वृद्धि को प्राप्त हो गया) यह कौतुक जानना चाहिए।
[जैन कुमारसम्भव महाकाव्य, सर्ग - ४ ] -
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
(५९)
www.jainelibrary.org