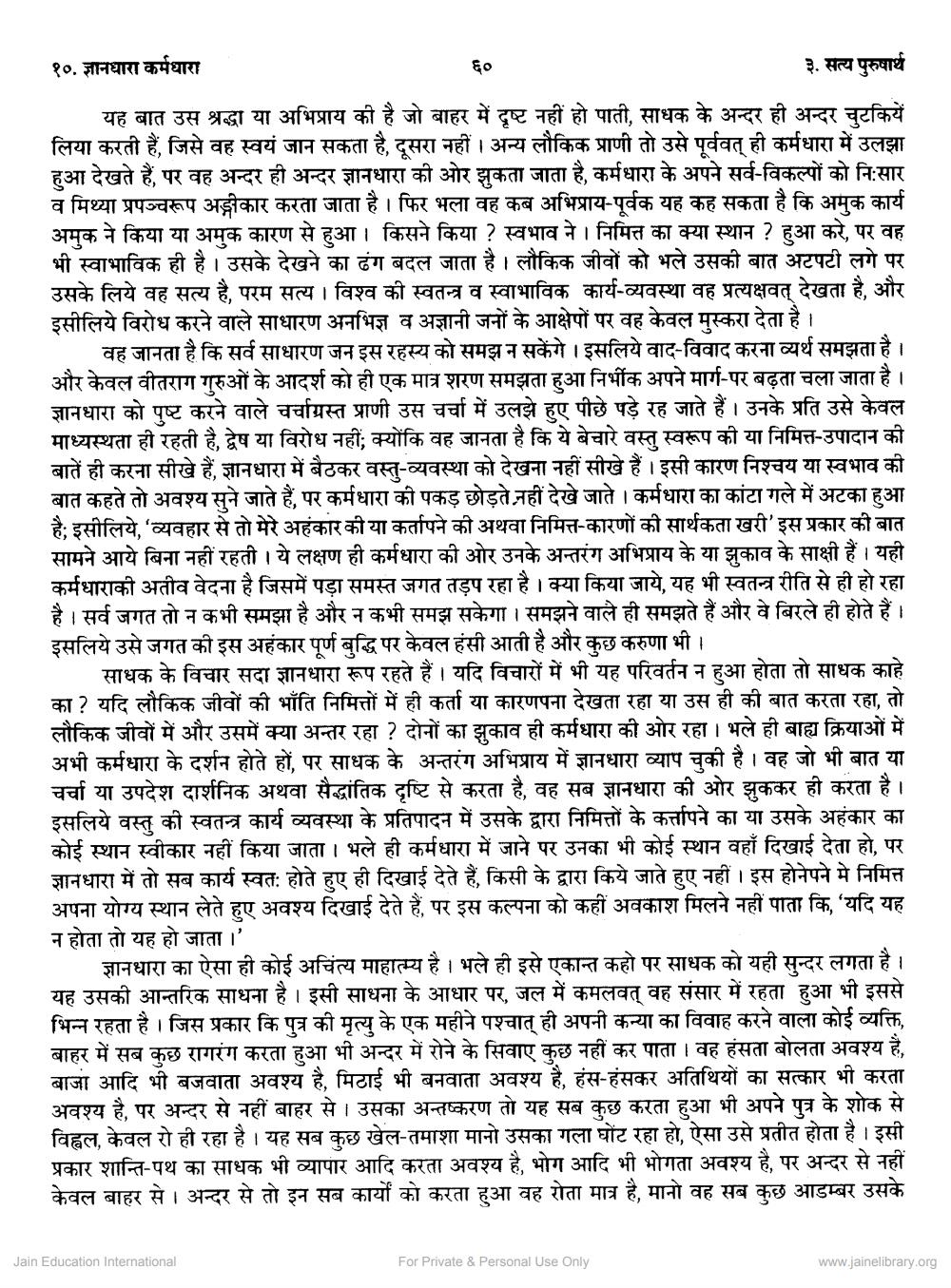________________
१०. ज्ञानधारा कर्मधारा
३. सत्य पुरुषार्थ
यह बात उस श्रद्धा या अभिप्राय की है जो बाहर में दृष्ट नहीं हो पाती, साधक के अन्दर ही अन्दर चुटकियें लिया करती हैं. जिसे वह स्वयं जान सकता है. दसरा नहीं। अन्य लौकिक प्राणी तो उसे पर्ववत ही कर्मधारा में उलझा हआ देखते हैं. पर वह अन्दर ही अन्दर ज्ञानधारा की ओर झकता जाता है. कर्मधारा के अपने सर्व-विकल व मिथ्या प्रपञ्चरूप अङ्गीकार करता जाता है। फिर भला वह कब अभिप्राय-पूर्वक यह कह सकता है कि अमुक कार्य अमुक ने किया या अमुक कारण से हुआ। किसने किया? स्वभाव ने । निमित्त का क्या स्थान? हुआ करे, पर वह भी स्वाभाविक ही है। उसके देखने का ढंग बदल जाता है । लौकिक जीवों को भले उसकी बात अटपटी लगे पर उसके लिये वह सत्य है, परम सत्य । विश्व की स्वतन्त्र व स्वाभाविक कार्य-व्यवस्था वह प्रत्यक्षवत् देखता है, और इसीलिये विरोध करने वाले साधारण अनभिज्ञ व अज्ञानी जनों के आक्षेपों पर वह केवल मुस्करा देता है।
वह जानता है कि सर्व साधारण जन इस रहस्य को समझ न सकेंगे । इसलिये वाद-विवाद करना व्यर्थ समझता है। और केवल वीतराग गुरुओं के आदर्श को ही एक मात्र शरण समझता हुआ निर्भीक अपने मार्ग-पर बढ़ता चला जाता है । ज्ञानधारा को पुष्ट करने वाले चर्चाग्रस्त प्राणी उस चर्चा में उलझे हुए पीछे पड़े रह जाते हैं। उनके प्रति उसे केवल माध्यस्थता ही रहती है, द्वेष या विरोध नहीं; क्योंकि वह जानता है कि ये बेचारे वस्तु स्वरूप की या निमित्त-उपादान की बातें ही करना सीखे हैं, ज्ञानधारा में बैठकर वस्तु-व्यवस्था को देखना नहीं सीखे हैं । इसी कारण निश्चय या स्वभाव की बात कहते तो अवश्य सुने जाते हैं, पर कर्मधारा की पकड़ छोड़ते नहीं देखे जाते । कर्मधारा का कांटा गले में अटका हुआ है; इसीलिये, 'व्यवहार से तो मेरे अहंकार की या कर्तापने की अथवा निमित्त-कारणों की सार्थकता खरी' इस प्रकार की बात सामने आये बिना नहीं रहती। ये लक्षण ही कर्मधारा की ओर उनके अन्तरंग अभिप्राय के या झुकाव के साक्षी हैं । यही कर्मधाराकी अतीव वेदना है जिसमें पडा समस्त जगत तड़प रहा है। क्या किया जाये, यह भी स्वतन्त्र रीति से ही हो रहा है। सर्व जगत तो न कभी समझा है और न कभी समझ सकेगा। समझने वाले ही समझते हैं और वे बिरले ही होते हैं। इसलिये उसे जगत की इस अहंकार पूर्ण बुद्धि पर केवल हंसी आती है और कुछ करुणा भी।
साधक के विचार सदा ज्ञानधारा रूप रहते हैं। यदि विचारों में भी यह परिवर्तन न हुआ होता तो साधक काहे का? यदि लौकिक जीवों की भाँति निमित्तों में ही कर्ता या कारणपना देखता रहा या उस ही की बात करता रहा, तो लौकिक जीवों में और उसमें क्या अन्तर रहा ? दोनों का झुकाव ही कर्मधारा की ओर रहा। भले ही बाह्य क्रियाओं में अभी कर्मधारा के दर्शन होते हों, पर साधक के अन्तरंग अभिप्राय में ज्ञानधारा व्याप चुकी है। वह जो भी बात या चर्चा या उपदेश दार्शनिक अथवा सैद्धांतिक दृष्टि से करता है, वह सब ज्ञानधारा की ओर झुककर ही करता है। इसलिये वस्तु की स्वतन्त्र कार्य व्यवस्था के प्रतिपादन में उसके द्वारा निमित्तों के कर्तापने का या उसके अहंकार का कोई स्थान स्वीकार नहीं किया जाता। भले ही कर्मधारा में जाने पर उनका भी कोई स्थान वहाँ दिखाई देता हो, पर ज्ञानधारा में तो सब कार्य स्वत: होते हुए ही दिखाई देते हैं, किसी के द्वारा किये जाते हुए नहीं। इस होनेपने मे निमित्त अपना योग्य स्थान लेते हुए अवश्य दिखाई देते हैं, पर इस कल्पना को कहीं अवकाश मिलने नहीं पाता कि, 'यदि यह न होता तो यह हो जाता।'
ज्ञानधारा का ऐसा ही कोई अचिंत्य माहात्म्य है। भले ही इसे एकान्त कहो पर साधक को यही सुन्दर लगता है। यह उसकी आन्तरिक साधना है। इसी साधना के आधार पर, जल में कमलवत् वह संसार में रहता हुआ भी इससे भिन्न रहता है । जिस प्रकार कि पुत्र की मृत्यु के एक महीने पश्चात् ही अपनी कन्या का विवाह करने वाला कोई व्यक्ति, बाहर में सब कुछ रागरंग करता हुआ भी अन्दर में रोने के सिवाए कुछ नहीं कर पाता । वह हंसता बोलता अवश्य है, बाजा आदि भी बजवाता अवश्य है, मिठाई भी बनवाता अवश्य है, हंस-हंसकर अतिथियों का सत्कार भी करता अवश्य है, पर अन्दर से नहीं बाहर से । उसका अन्तष्करण तो यह सब कुछ करता हुआ भी अपने पुत्र के शोक से विह्वल, केवल रो ही रहा है। यह सब कुछ खेल-तमाशा मानो उसका गला घोंट रहा हो, ऐसा उसे प्रतीत होता है । इसी प्रकार शान्ति-पथ का साधक भी व्यापार आदि करता अवश्य है, भोग आदि भी भोगता अवश्य है, पर अन्दर से नहीं केवल बाहर से । अन्दर से तो इन सब कार्यों को करता हुआ वह रोता मात्र है, मानो वह सब कुछ आडम्बर उसके
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org