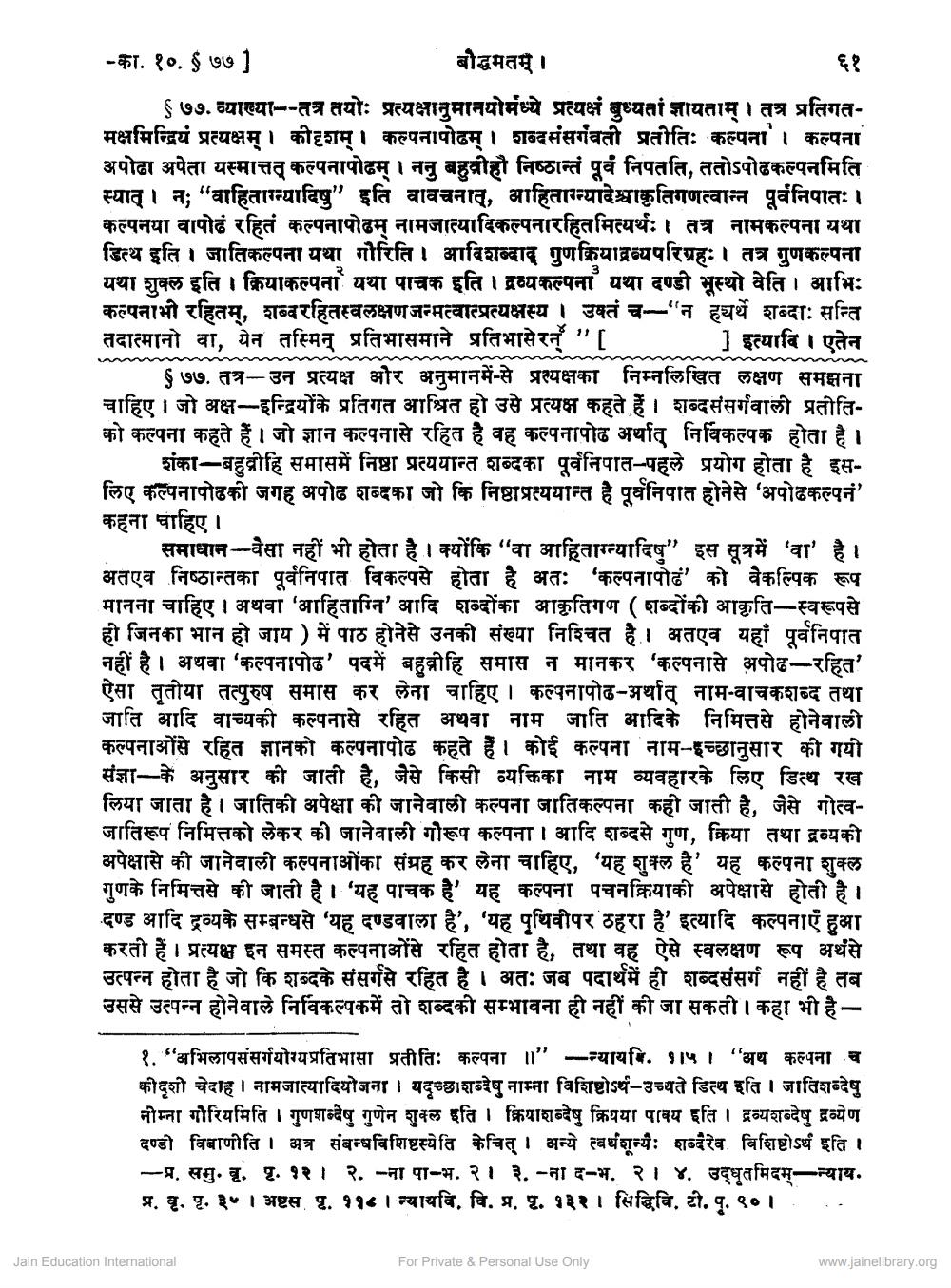________________
- का. १०. § ७७ ]
बोद्धमतम् ।
६१
1
९ ७७. व्याख्या -- तत्र तयोः प्रत्यक्षानुमानयोर्मध्ये प्रत्यक्षं बुध्यतां ज्ञायताम् । तत्र प्रतिगतमक्षमिन्द्रियं प्रत्यक्षम् । कीदृशम् । कल्पनापोढम् । शब्दसंसर्गवती प्रतीतिः कल्पना' | कल्पना अपोढा अपेता यस्मात्तत् कल्पनापोढम् । ननु बहुव्रीहौ निष्ठान्तं पूर्वं निपतति, ततोऽपोढकल्पनमिति स्यात् । न; " वाहिताग्न्यादिषु" इति वावचनात्, आहिताग्न्यादेचाकृतिगणत्वान्न पूर्वनिपातः । कल्पनया वापोढं रहितं कल्पनापोढम् नामजात्यादिकल्पनारहितमित्यर्थः । तत्र नामकल्पना यथा डित्य इति । जातिकल्पना यथा गौरिति । आविशब्दाद् गुणक्रियाद्रव्यपरिग्रहः । तत्र गुणकल्पना यथा शुक्ल इति । क्रियाकल्पना यथा पाचक इति । द्रव्यकल्पना यथा दण्डी भूस्थो वेति । अभिः कल्पनाभी रहितम्, शब्द रहितस्वलक्षण जन्मत्वात्प्रत्यक्षस्य । उक्तं च--" न हयर्थे शब्दाः सन्ति तदात्मानो वा, येन तस्मिन् प्रतिभासमाने प्रतिभासेरन् " [ ] इत्यादि । एतेन
§ ७७. तत्र - उन प्रत्यक्ष और अनुमानमें से प्रत्यक्षका निम्नलिखित लक्षण समझना चाहिए । जो अक्ष- इन्द्रियोंके प्रतिगत आश्रित हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । शब्दसंसर्गवाली प्रतीतिको कल्पना कहते हैं । जो ज्ञान कल्पनासे रहित है वह कल्पनापोढ अर्थात् निर्विकल्पक होता है | शंका - बहुव्रीहि समासमें निष्ठा प्रत्ययान्त शब्दका पूर्वनिपात- पहले प्रयोग होता है इसलिए कल्पनापोढकी जगह अपोढ शब्दका जो कि निष्ठाप्रत्ययान्त है पूर्वनिपात होनेसे 'अपोढकल्पनं ' कहना चाहिए ।
समाधान - वैसा नहीं भी होता है । क्योंकि “वा आहिताग्न्यादिषु" इस सूत्र में 'वा' है । अतएव निष्ठान्तका पूर्वनिपात विकल्पसे होता है अत: 'कल्पनापोढं' को वैकल्पिक रूप मानना चाहिए । अथवा 'आहिताग्नि' आदि शब्दोंका आकृतिगण ( शब्दोंकी आकृति - स्वरूप से ही जिनका भान हो जाय ) में पाठ होनेसे उनकी संख्या निश्चित है। अतएव यहाँ पूर्वनिपात नहीं है । अथवा 'कल्पनापोढ' पदमें बहुव्रीहि समास न मानकर 'कल्पनासे अपोढ - रहित ' ऐसा तृतीया तत्पुरुष समास कर लेना चाहिए। कल्पनापोढ अर्थात् नाम-वाचकशब्द तथा जाति आदि वाच्यकी कल्पनासे रहित अथवा नाम जाति आदिके निमित्तसे होनेवाली कल्पनाओंसे रहित ज्ञानको कल्पनापोढ कहते हैं । कोई कल्पना नाम- इच्छानुसार की गयी संज्ञा - के अनुसार की जाती है, जैसे किसी व्यक्तिका नाम व्यवहारके लिए डित्थ रख लिया जाता है । जातिकी अपेक्षा की जानेवाली कल्पना जातिकल्पना कही जाती है, जैसे गोत्वजातिरूप निमित्तको लेकर की जानेवाली गोरूप कल्पना । आदि शब्दसे गुण, क्रिया तथा द्रव्यकी अपेक्षासे की जानेवाली कल्पनाओंका संग्रह कर लेना चाहिए, 'यह शुक्ल है' यह कल्पना शुक्ल गुण निमित्तसे की जाती है। 'यह पाचक है' यह कल्पना पचनक्रियाको अपेक्षासे होती है । दण्ड आदि द्रव्य के सम्बन्धसे 'यह दण्डवाला है', 'यह पृथिवीपर ठहरा है' इत्यादि कल्पनाएँ हुआ करती हैं । प्रत्यक्ष इन समस्त कल्पनाओंसे रहित होता है, तथा वह ऐसे स्वलक्षण रूप अर्थसे उत्पन्न होता है जो कि शब्दके संसर्गसे रहित है । अतः जब पदार्थ में ही शब्दसंसर्ग नहीं है तब उससे उत्पन्न होनेवाले निर्विकल्पकमें तो शब्द की सम्भावना ही नहीं की जा सकती। कहा भी है
-
१. " अभिलापसंसर्ग योग्य प्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना ॥" न्यायवि ११५ । " अथ कल्पना च कीदृशी चेदाह | नामजात्यादियोजना । यदृच्छा शब्देषु नाम्ना विशिष्टोऽर्थ - उच्यते डित्य इति । जातिशब्देषु नीना गौरियमिति । गुणशब्देषु गुणेन शुक्ल इति । क्रियाशब्देषु क्रियया पाक्य इति । द्रव्यशब्देषु द्रव्येण cost विवाणीति । अत्र संबन्धविशिष्टस्येति केचित् । अन्ये त्वर्थशून्यैः शब्दैरेव विशिष्टोऽर्थं इति । - प्र. समु. वृ. पृ. १२ । २. ना पा-भ. २ । ३. - नाद-भ. २ । ४. उद्धृतमिदम् — न्याय. प्र. वृ. पृ. ३५ । अष्टस पृ. ११८ । न्यायवि. वि. प्र. पू. १३२ । सिद्धिवि. टी. पू. ९० ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org