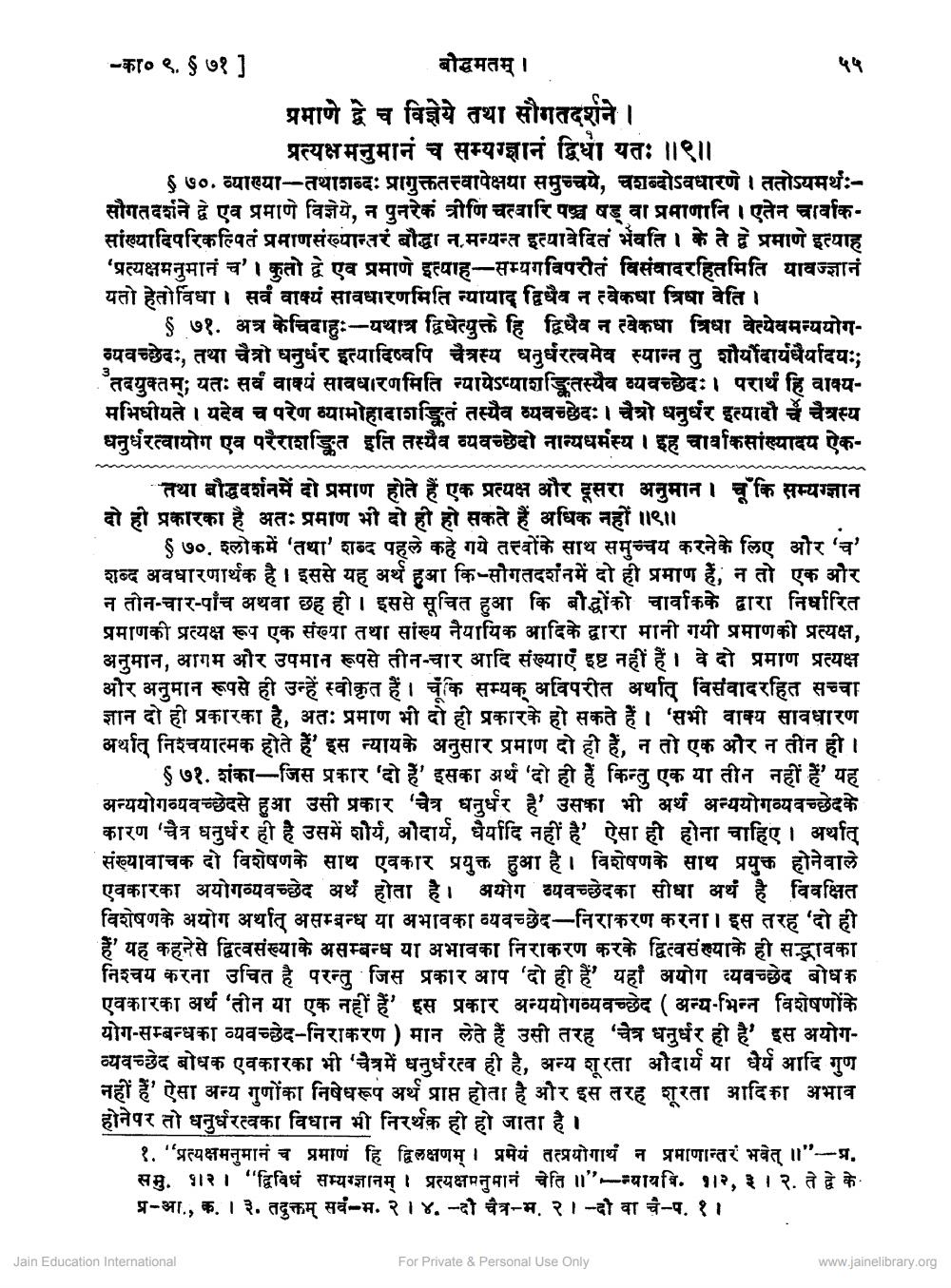________________
- का० ९. ६ ७१ ]
मतम् ।
प्रमाणे द्वे च विज्ञेये तथा सौगतदर्शने ।
प्रत्यक्षमनुमानं च सम्यग्ज्ञानं द्विधा यतः ॥ ९ ॥
$ ७०. व्याख्या - तथाशब्दः प्रागुक्ततत्वापेक्षया समुच्चये, चशब्दोऽवधारणे । ततोऽयमर्थःसौगतदर्शने द्वे एव प्रमाणे विज्ञेये, न पुनरेकं त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् वा प्रमाणानि । एतेन चार्वाकसांख्यादिपरिकल्पितं प्रमाणसंख्यान्तरं बौद्धा न मन्यन्त इत्यावेदितं भवति । के ते द्वे प्रमाणे इत्याह 'प्रत्यक्षमनुमानं च' । कुतो द्वे एव प्रमाणे इत्याह- सम्यगविपरीतं विसंवादरहितमिति यावज्ज्ञानं यतो हेतोर्विधा । सर्वं वाक्यं सावधारणमिति न्यायाद् द्विधैव न त्वेकधा त्रिधा वेति ।
$ ७१. अत्र केचिदाहुः - यथात्र द्विधेत्युक्ते हि द्विधैव न त्वेकधा त्रिधा वेत्येवमन्ययोगव्यवच्छेदः, तथा चैत्रो धनुर्धर इत्यादिष्वपि चैत्रस्य धनुर्धरत्वमेव स्यान्न तु शौर्योदार्यधैर्यादयः; " तदयुक्तम्; यतः सर्वं वाक्यं सावधारणमिति न्यायेऽप्याशङ्कितस्यैव व्यवच्छेदः । परार्थं हि वाक्यमभिधीयते । यदेव च परेण व्यामोहादाशङ्कितं तस्यैव व्यवच्छेदः । चैत्रो धनुर्धर इत्यादौ चै चैत्रस्य धनुर्धरत्वायोग एव परैराशङ्कित इति तस्यैव व्यवच्छेदो नान्यधर्मस्य । इह चार्वाक सांख्यादय ऐक
५५
तथा बौद्धदर्शन में दो प्रमाण होते हैं एक प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान | चूँकि सम्यग्ज्ञान दो ही प्रकारका है अतः प्रमाण भी दो ही हो सकते हैं अधिक नहीं ॥९॥
§ ७०. श्लोकमें ‘तथा' शब्द पहले कहे गये तत्वोंके साथ समुच्चय करनेके लिए और 'च' शब्द अवधारणार्थक है । इससे यह अर्थ हुआ कि -सोगतदर्शन में दो ही प्रमाण हैं, न तो एक और न तोन-चार-पाँच अथवा छह हो। इससे सूचित हुआ कि बौद्धोंको चार्वाकके द्वारा निर्धारित प्रमाणकी प्रत्यक्ष रूप एक संख्या तथा सांख्य नैयायिक आदिके द्वारा मानी गयी प्रमाणकी प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान रूपसे तीन-चार आदि संख्याएं इष्ट नहीं हैं । वे दो प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान रूपसे ही उन्हें स्वीकृत हैं । चूँकि सम्यक् अविपरीत अर्थात् विसंवादरहित सच्चा ज्ञान दो ही प्रकारका है, अतः प्रमाण दो ही प्रकार के हो सकते हैं। 'सभी वाक्य सावधारण अर्थात् निश्चयात्मक होते हैं' इस न्यायके अनुसार प्रमाण दो ही हैं, न तो एक और न तीन ही । ७१. शंका - जिस प्रकार 'दो हैं' इसका अर्थ 'दो ही हैं किन्तु एक या तीन नहीं हैं' यह अन्ययोगव्यवच्छेदसे हुआ उसी प्रकार 'चैत्र धनुर्धर है' उसका भी अर्थ अन्ययोगव्यवच्छेद के कारण 'चैत्र धनुर्धर ही है उसमें शौर्य, औदार्य, धैर्यादि नहीं है' ऐसा ही होना चाहिए । अर्थात् संख्यावाचक दो विशेषणके साथ एवकार प्रयुक्त हुआ है । विशेषणके साथ प्रयुक्त होनेवाले एवकारका अयोगव्यवच्छेद अर्थ होता है। अयोग व्यवच्छेदका सीधा अर्थ है विवक्षित विशेषणके आयोग अर्थात् असम्बन्ध या अभावका व्यवच्छेद - निराकरण करना । इस तरह 'दो ही हैं' यह कहने से द्वित्वसंख्या के असम्बन्ध या अभावका निराकरण करके द्वित्वसंख्याके ही सद्भावका निश्चय करना उचित है परन्तु जिस प्रकार आप 'दो ही हैं' यहाँ अयोग व्यवच्छेद बोधक एवकारका अर्थ 'तीन या एक नहीं हैं' इस प्रकार अन्ययोगव्यवच्छेद ( अन्य-भिन्न विशेषणोंके योग-सम्बन्धका व्यवच्छेद - निराकरण ) मान लेते हैं उसी तरह 'चैत्र धनुर्धर ही है' इस अयोगव्यवच्छेद बोधक एवकारका भी 'चैत्र में धनुर्धरत्व ही है, अन्य शूरता औदार्य या धैर्य आदि गुण नहीं हैं' ऐसा अन्य गुणोंका निषेधरूप अर्थ प्राप्त होता है और इस तरह शूरता आदिका अभाव होनेपर तो धनुर्धरत्वका विधान भी निरर्थक हो हो जाता है ।
१. " प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं हि द्विलक्षणम् । प्रमेयं तत्प्रयोगार्थं न प्रमाणान्तरं भवेत् ॥ " -- प्र. समु. ११२ । " द्विविधं सम्यग्ज्ञानम् । प्रत्यक्षमनुमानं चेति ॥” - न्यायवि. ११२, ३ । २. ते द्वे के प्र-आ. क. । ३. तदुक्तम् सर्व-म. २ । ४. -दो चैत्र-म. २ । दो वा चै प. १ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org