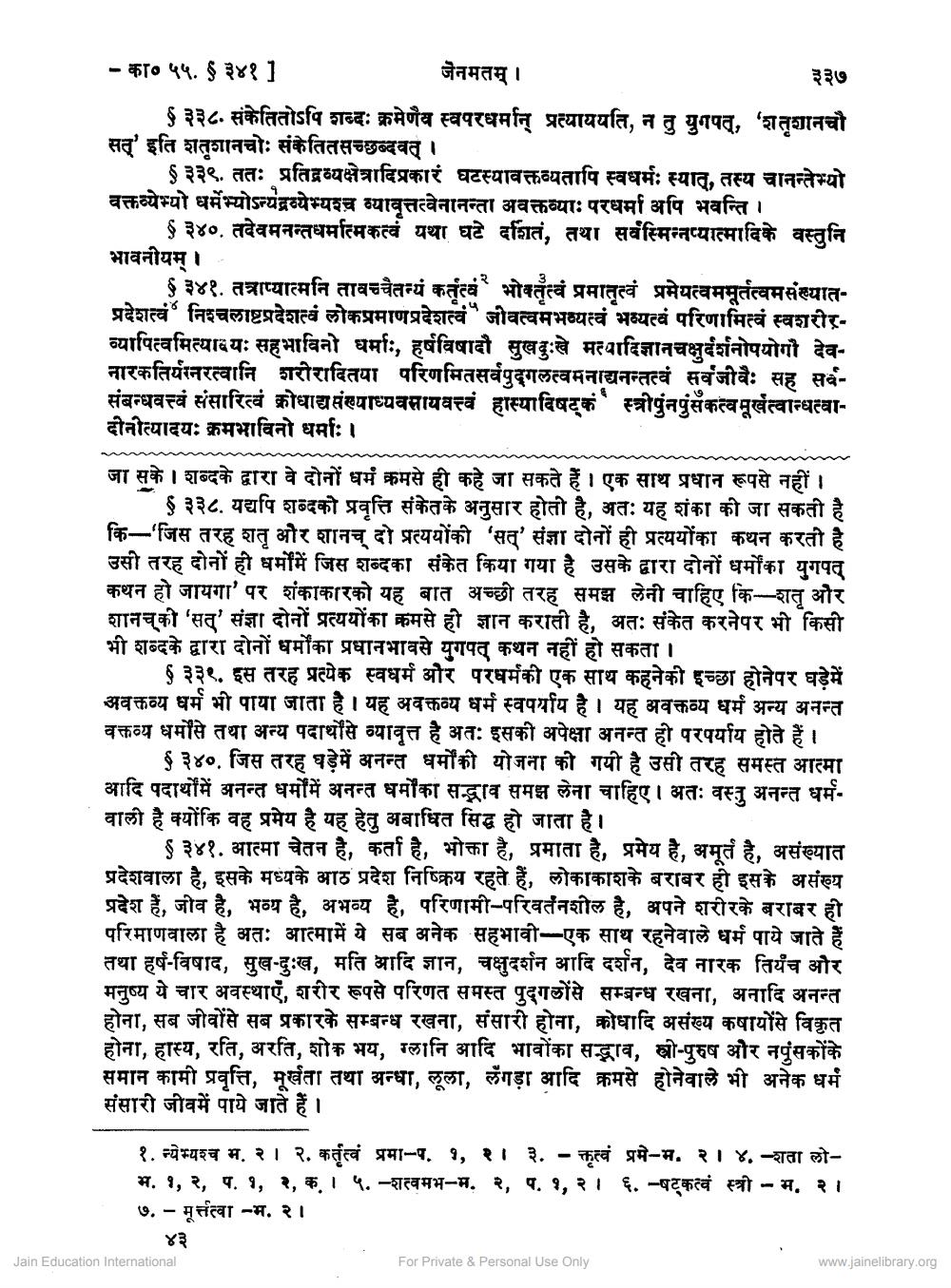________________
- का० ५५. ६ ३४१] जैनमतम् ।
३३७ ६३३८. संकेतितोऽपि शब्दः क्रमेणैव स्वपरधर्मान् प्रत्याययति, न तु युगपत्, ‘शतृशानचौ सत्' इति शतशानचोः संकेतितसच्छब्दवत् ।
६३३९. ततः प्रतिद्रव्यक्षेत्रादिप्रकारं घटस्यावक्तव्यतापि स्वधर्मः स्यात, तस्य चानन्तेभ्यो वक्तव्येभ्यो धर्मेभ्योऽन्यद्रव्येभ्यश्च व्यावृत्तत्वेनानन्ता अवक्तव्याः परधर्मा अपि भवन्ति ।
६३४०. तदेवमनन्तधर्मात्मकत्वं यथा घटे दर्शितं, तथा सर्वस्मिन्नप्यात्मादिके वस्तुनि भावनीयम्।।
६३४१. तत्राप्यात्मनि तावच्चैतन्यं कर्तृत्व भोक्तृत्वं प्रमातृत्वं प्रमेयत्वममूर्तत्वमसंख्यातप्रदेशत्वं निश्चलाष्टप्रदेशत्वं लोकप्रमाणप्रदेशत्वं जीवत्वमभव्यत्वं भव्यत्वं परिणामित्वं स्वशरीरव्यापित्वमित्यादयः सहभाविनो धर्माः, हर्षविषादौ सुखदुःखे मत्यादिज्ञानचक्षुर्दर्शनोपयोगी देवनारकतिर्यग्नरत्वानि शरीरादितया परिणमितसर्वपुदगलत्वमनाद्यनन्तत्वं सर्वजीवैः सह सर्वसंबन्धवत्त्वं संसारित्वं क्रोधाद्य संख्याध्यवसायवत्त्वं हास्याविषट्कं' स्त्रीपुंनपुंसकत्वमूर्खत्वान्धत्वादोनीत्यादयः क्रमभाविनो धर्माः।
जा सके। शब्दके द्वारा वे दोनों धर्म क्रमसे ही कहे जा सकते हैं। एक साथ प्रधान रूपसे नहीं।
६३३८. यद्यपि शब्दको प्रवृत्ति संकेतके अनुसार होती है, अतः यह शंका की जा सकती है कि-'जिस तरह शतृ और शानच दो प्रत्ययोंकी 'सत्' संज्ञा दोनों ही प्रत्ययोंका कथन करती है उसी तरह दोनों ही धर्मों में जिस शब्दका संकेत किया गया है उसके द्वारा दोनों धर्मोंका युगपत् कथन हो जायगा' पर शंकाकारको यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि-शतृ और शानचकी 'सत्' संज्ञा दोनों प्रत्ययोंका क्रमसे ही ज्ञान कराती है, अतः संकेत करनेपर भी किसी भी शब्दके द्वारा दोनों धर्मोंका प्रधानभावसे युगपत् कथन नहीं हो सकता।
३३१. इस तरह प्रत्येक स्वधर्म और परधर्मकी एक साथ कहनेकी इच्छा होनेपर घडेमें अवक्तव्य धर्म भी पाया जाता है । यह अवक्तव्य धर्म स्वपर्याय है। यह अवक्तव्य धर्म अन्य अनन्त वक्तव्य धर्मोंसे तथा अन्य पदार्थोंसे व्यावृत्त है अत: इसकी अपेक्षा अनन्त हो परपर्याय होते हैं।
६३४०. जिस तरह घड़ेमें अनन्त धर्मोंकी योजना की गयी है उसी तरह समस्त आत्मा आदि पदार्थों में अनन्त धर्मों में अनन्त धर्मोका सद्भाव समझ लेना चाहिए। अतः वस्तु अनन्त धर्मवाली है क्योंकि वह प्रमेय है यह हेतु अबाधित सिद्ध हो जाता है।
३४१. आत्मा चेतन है, कर्ता है, भोक्ता है, प्रमाता है, प्रमेय है, अमूर्त है, असंख्यात प्रदेशवाला है, इसके मध्यके आठ प्रदेश निष्क्रिय रहते हैं, लोकाकाशके बराबर ही इसके असंख्य प्रदेश हैं, जीव है, भव्य है, अभव्य है, परिणामी-परिवर्तनशील है, अपने शरीरके बराबर ही परिमाणवाला है अतः आत्मामें ये सब अनेक सहभावी-एक साथ रहनेवाले धर्म पाये जाते हैं तथा हर्ष-विषाद, सुख-दुःख, मति आदि ज्ञान, चक्षुदर्शन आदि दर्शन, देव नारक तिथंच और मनुष्य ये चार अवस्थाएं, शरीर रूपसे परिणत समस्त पुद्गलोंसे सम्बन्ध रखना, अनादि अनन्त होना, सब जीवोंसे सब प्रकारके सम्बन्ध रखना, संसारी होना, क्रोधादि असंख्य कषायोंसे विकृत होना, हास्य, रति, अरति, शोक भय, ग्लानि आदि भावोंका सद्भाव, खो-पुरुष और नपुंसकोंके समान कामी प्रवृत्ति, मूर्खता तथा अन्धा, लूला, लंगड़ा आदि क्रमसे होनेवाले भी अनेक धर्म संसारी जीवमें पाये जाते हैं।
१. न्येभ्यश्च म. २ । २. कर्तृत्वं प्रमा-प. १, । ३. - क्तत्वं प्रमे-म. २। ४.-शता लोम. १, २, प. १, २, क । ५.-शत्वमभ-म. २, प.१,२। ६. -षटकत्वं स्त्री-म, ३। ७. - मूर्त्तत्वा -म. २।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org