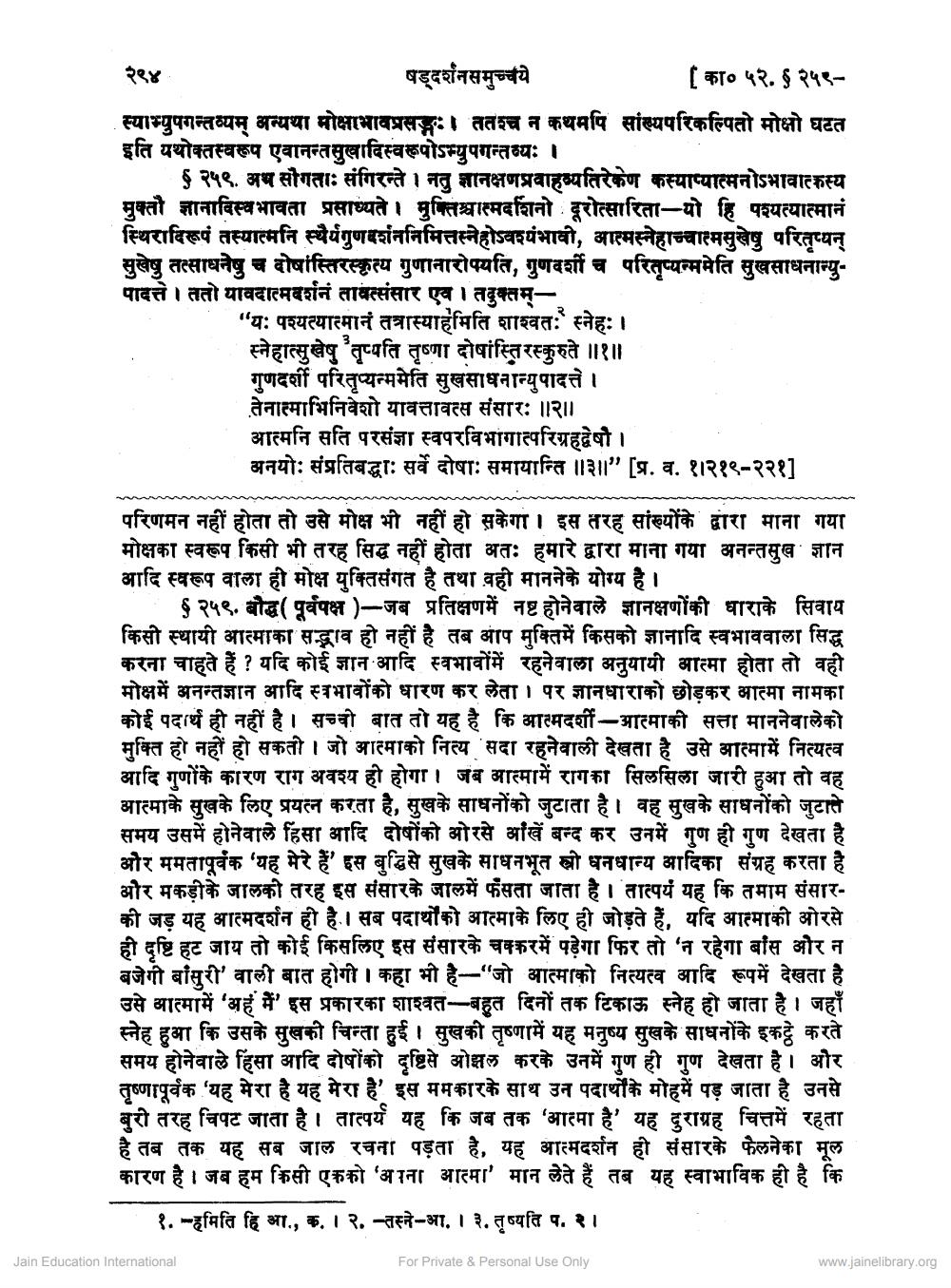________________
२९४ षड्दर्शनसमुच्चये
[का० ५२.६२५९स्याभ्युपगन्तव्यम् अन्यथा मोक्षाभावप्रसङ्गः। ततश्च न कथमपि सांख्यपरिकल्पितो मोक्षो घटत इति यथोक्तस्वरूप एवानन्तसुखादिस्वरूपोऽभ्युपगन्तव्यः ।
5२५९. अब सौगताः संगिरन्ते । नतु ज्ञानक्षणप्रवाहव्यतिरेकेण कस्याप्यात्मनोऽभावात्कस्य मुक्तौ ज्ञानाविस्वभावता प्रसाध्यते। मुक्तिश्चात्मशिनो दूरोत्सारिता-यो हि पश्यत्यात्मानं स्थिरादिरूपं तस्यात्मनि स्थैर्यगुणदर्शननिमित्तस्नेहोऽवश्यंभावी, आत्मस्नेहाच्चारमसुखेषु परितृप्यन् सुखेषु तत्साधनेषु च दोषास्तिरस्कृत्य गुणानारोपयति, गुणदर्शी च परितृप्यन्ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते । ततो यावदात्मवर्शनं तावत्संसार एव । तदुक्तम्
"यः पश्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति शाश्वतः स्नेहः। स्नेहात्सुखेषु तृप्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥१॥ गुणदर्शी परितृप्यन्ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते । तेनात्माभिनिवेशो यावत्तावत्स संसारः ॥२॥ आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहद्वेषौ । अनयोः संप्रतिबद्धाः सर्वे दोषाः समायान्ति ॥३॥" [प्र. व. ११२१९-२२१]
परिणमन नहीं होता तो उसे मोक्ष भी नहीं हो सकेगा। इस तरह सांख्योंके द्वारा माना गया मोक्षका स्वरूप किसी भी तरह सिद्ध नहीं होता अतः हमारे द्वारा माना गया अनन्तसुख ज्ञान आदि स्वरूप वाला ही मोक्ष युक्तिसंगत है तथा वही माननेके योग्य है।
२५९. बौद्ध(पूर्वपक्ष)-जब प्रतिक्षणमें नष्ट होनेवाले ज्ञानक्षणोंकी धाराके सिवाय किसी स्थायी आत्माका सद्भाव हो नहीं है तब आप मुक्तिमें किसको ज्ञानादि स्वभाववाला सिद्ध करना चाहते हैं ? यदि कोई ज्ञान आदि स्वभावोंमें रहनेवाला अनुयायी आत्मा होता तो वही मोक्षमें अनन्तज्ञान आदि स्वभावोंको धारण कर लेता। पर ज्ञानधाराको छोड़कर आत्मा नामका कोई पदार्थ ही नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि आत्मदर्शी-आत्माकी सत्ता माननेवालेको मुक्ति हो नहीं हो सकती। जो आत्माको नित्य सदा रहनेवाली देखता है उसे आत्मामें नित्यत्व आदि गुणोंके कारण राग अवश्य ही होगा। जब आत्मामें रागका सिलसिला जारी हुआ तो वह आत्माके सुखके लिए प्रयत्न करता है, सुखके साधनोंको जुटाता है। वह सुखके साधनोंको जुटाते समय उसमें होनेवाले हिंसा आदि दोषोंको ओरसे आँखें बन्द कर उनमें गुण ही गुण देखता है और ममतापूर्वक 'यह मेरे हैं। इस बुद्धिसे सुखके साधनभूत स्त्री धनधान्य आदिका संग्रह करता है और मकड़ीके जालकी तरह इस संसारके जालमें फंसता जाता है। तात्पर्य यह कि तमाम संसारकी जड़ यह आत्मदर्शन ही है । सब पदार्थोको आत्माके लिए ही जोड़ते हैं, यदि आत्माको ओरसे ही दृष्टि हट जाय तो कोई किसलिए इस संसारके चक्करमें पड़ेगा फिर तो 'न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी' वाली बात होगी । कहा भी है-"जो आत्माको नित्यत्व आदि रूपमें देखता है उसे आत्मामें 'अहं मैं' इस प्रकारका शाश्वत-बहुत दिनों तक टिकाऊ स्नेह हो जाता है । जहाँ स्नेह हुआ कि उसके सुखको चिन्ता हुई। सुखकी तृष्णामें यह मनुष्य सुखके साधनोंके इकट्ठे करते समय होनेवाले हिंसा आदि दोषोंको दृष्टिसे ओझल करके उनमें गुण ही गुण देखता है। और तृष्णापूर्वक 'यह मेरा है यह मेरा है' इस ममकारके साथ उन पदार्थोके मोहमें पड़ जाता है उनसे बुरी तरह चिपट जाता है। तात्पर्य यह कि जब तक 'आत्मा है' यह दुराग्रह चित्तमें रहता है तब तक यह सब जाल रचना पड़ता है, यह आत्मदर्शन ही संसारके फैलनेका मल कारण है । जब हम किसी एकको 'अपना आत्मा' मान लेते हैं तब यह स्वाभाविक ही है कि
१. -हमिति हि आ., क. । २. -तस्ने-आ. । ३. तृष्यति प. १।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org