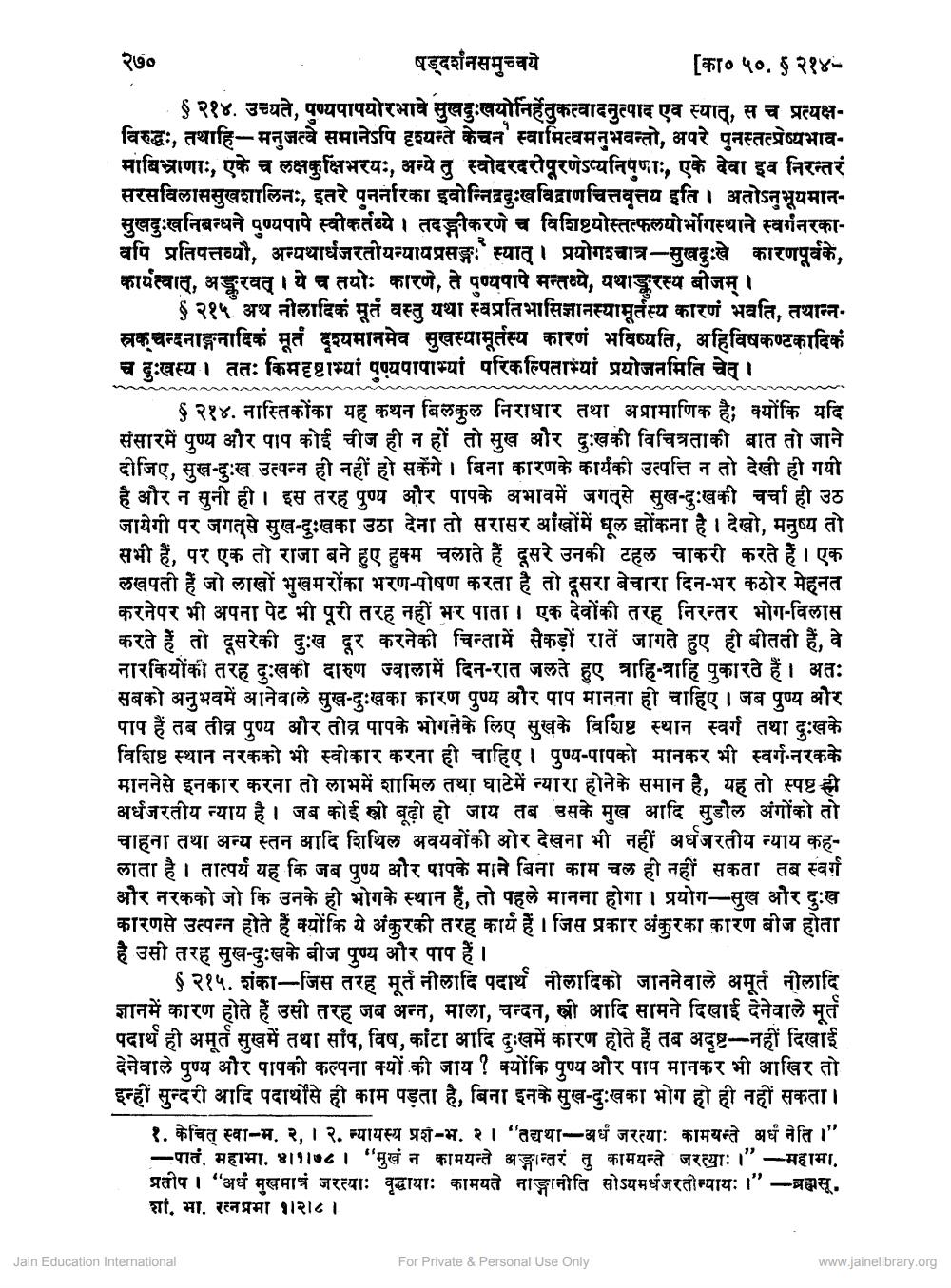________________
२७० षड्दर्शनसमुच्चये
[का०५०.६२१४६२१४. उच्यते, पुण्यपापयोरभावे सुखदुःखयोनिर्हेतुकत्वादनुत्पाद एव स्यात्, स च प्रत्यक्षविरुद्धः, तथाहि-मनुजत्वे समानेऽपि दृश्यन्ते केचन स्वामित्वमनुभवन्तो, अपरे पुनस्तत्प्रेष्यभावमाबिभ्राणाः, एके च लक्षकुक्षिभरयः, अन्ये तु स्वोदरदरीपूरणेऽप्यनिपुणाः, एके देवा इव निरन्तरं सरसविलाससुखशालिनः, इतरे पुनारका इवोन्निद्रदुःखविद्राणचित्तवृत्तय इति । अतोऽनुभूयमानसुखदुःखनिबन्धने पुण्यपापे स्वीकर्तव्ये । तदङ्गीकरणे च विशिष्टयोस्तत्फलयो गस्थाने स्वर्गनरकावपि प्रतिपत्तव्यौ, अन्यथार्धजरतीयन्यायप्रसङ्ग स्यात् । प्रयोगश्चात्र-सुखदुःखे कारणपूर्वके, कार्यत्वात्, अङ्करवत् । ये च तयोः कारणे, ते पुण्यपापे मन्तव्ये, यथाङ्करस्य बीजम् ।
$ २१५ अथ नीलादिकं मूर्त वस्तु यथा स्वप्रतिभासिज्ञानस्यामूर्तस्य कारणं भवति, तथान्नस्रकचन्दनाङ्गनादिकं मूतं दृश्यमानमेव सुखस्यामूर्तस्य कारणं भविष्यति, अहिविषकण्टकादिकं च दुःखस्य। ततः किमदृष्टाभ्यां पुण्यपापाभ्यां परिकल्पिताभ्यां प्रयोजनमिति चेत् ।
६२१४. नास्तिकोंका यह कथन बिलकुल निराधार तथा अप्रामाणिक है; क्योंकि यदि संसारमें पुण्य और पाप कोई चीज ही न हों तो सुख और दुःखकी विचित्रताकी बात तो जाने दीजिए, सुख-दुःख उत्पन्न ही नहीं हो सकेंगे। बिना कारणके कार्यको उत्पत्ति न तो देखी ही गयी है और न सुनी ही। इस तरह पुण्य और पापके अभावमें जगत्से सुख-दुःखकी चर्चा ही उठ जायेगी पर जगत्से सुख-दुःखका उठा देना तो सरासर आंखोंमें धूल झोंकना है । देखो, मनुष्य तो सभी हैं, पर एक तो राजा बने हए हक्म चलाते हैं दूसरे उनकी टहल चाकरी करते हैं। एक लखपती हैं जो लाखों भुखमरोंका भरण-पोषण करता है तो दूसरा बेचारा दिन-भर कठोर मेहनत करनेपर भी अपना पेट भी पूरी तरह नहीं भर पाता। एक देवोंकी तरह निरन्तर भोग-विलास करते हैं तो दूसरेकी दुःख दूर करनेकी चिन्तामें सैकड़ों रातें जागते हुए ही बीतती हैं, वे नारकियोंकी तरह दुःखको दारुण ज्वालामें दिन-रात जलते हुए त्राहि-त्राहि पुकारते हैं। अतः सबको अनुभवमें आनेवाले सुख-दुःखका कारण पुण्य और पाप मानना ही चाहिए । जब पुण्य और पाप हैं तब तीन पुण्य और तीव्र पापके भोगनेके लिए सुखके विशिष्ट स्थान स्वर्ग तथा दुःखके विशिष्ट स्थान नरकको भी स्वीकार करना ही चाहिए। पुण्य-पापको मानकर भी स्वर्ग-नरकके माननेसे इनकार करना तो लाभमें शामिल तथा घाटेमें न्यारा होने के समान है, यह तो स्पष्ट ही अर्धजरतीय न्याय है। जब कोई स्त्री बूढ़ी हो जाय तब उसके मुख आदि सुडौल अंगोंको तो चाहना तथा अन्य स्तन आदि शिथिल अवयवोंकी ओर देखना भी नहीं अर्धजरतीय न्याय कहलाता है। तात्पर्य यह कि जब पुण्य और पापके माने बिना काम चल ही नहीं सकता तब स्वर्ग
और नरकको जो कि उनके हो भोगके स्थान हैं, तो पहले मानना होगा। प्रयोग-सुख और दुःख कारणसे उत्पन्न होते हैं क्योंकि ये अंकुरकी तरह कार्य हैं । जिस प्रकार अंकुरका कारण बीज होता है उसी तरह सुख-दुःखके बीज पुण्य और पाप हैं।
२१५. शंका-जिस तरह मूर्त नीलादि पदार्थ नीलादिको जाननेवाले अमूर्त नीलादि ज्ञानमें कारण होते हैं उसी तरह जब अन्न, माला, चन्दन, स्त्री आदि सामने दिखाई देनेवाले मूर्त पदार्थ ही अमूर्त सुख में तथा साँप, विष, कांटा आदि दुःखमें कारण होते हैं तब अदृष्ट नहीं दिखाई देनेवाले पुण्य और पापकी कल्पना क्यों की जाय ? क्योंकि पुण्य और पाप मानकर भी आखिर तो इन्हीं सुन्दरी आदि पदार्थों से ही काम पड़ता है, बिना इनके सुख-दुःखका भोग हो ही नहीं सकता।
१. केचित् स्वा-म. २, । २. न्यायस्य प्रश-भ. २ । "तद्यथा-अर्धं जरत्याः कामयन्ते अर्ध नेति ।" -पातं. महामा. ४011८। "मुखं न कामयन्ते अङ्गान्तरं तु कामयन्ते जरत्याः।" -महामा. प्रतीप । “अधं मुखमात्र जरत्याः वृद्धायाः कामयते नाङ्गानीति सोऽयमर्धजरतीन्यायः ।" -ब्रह्मसू, शां. भा. रत्नप्रमा १२।८।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org