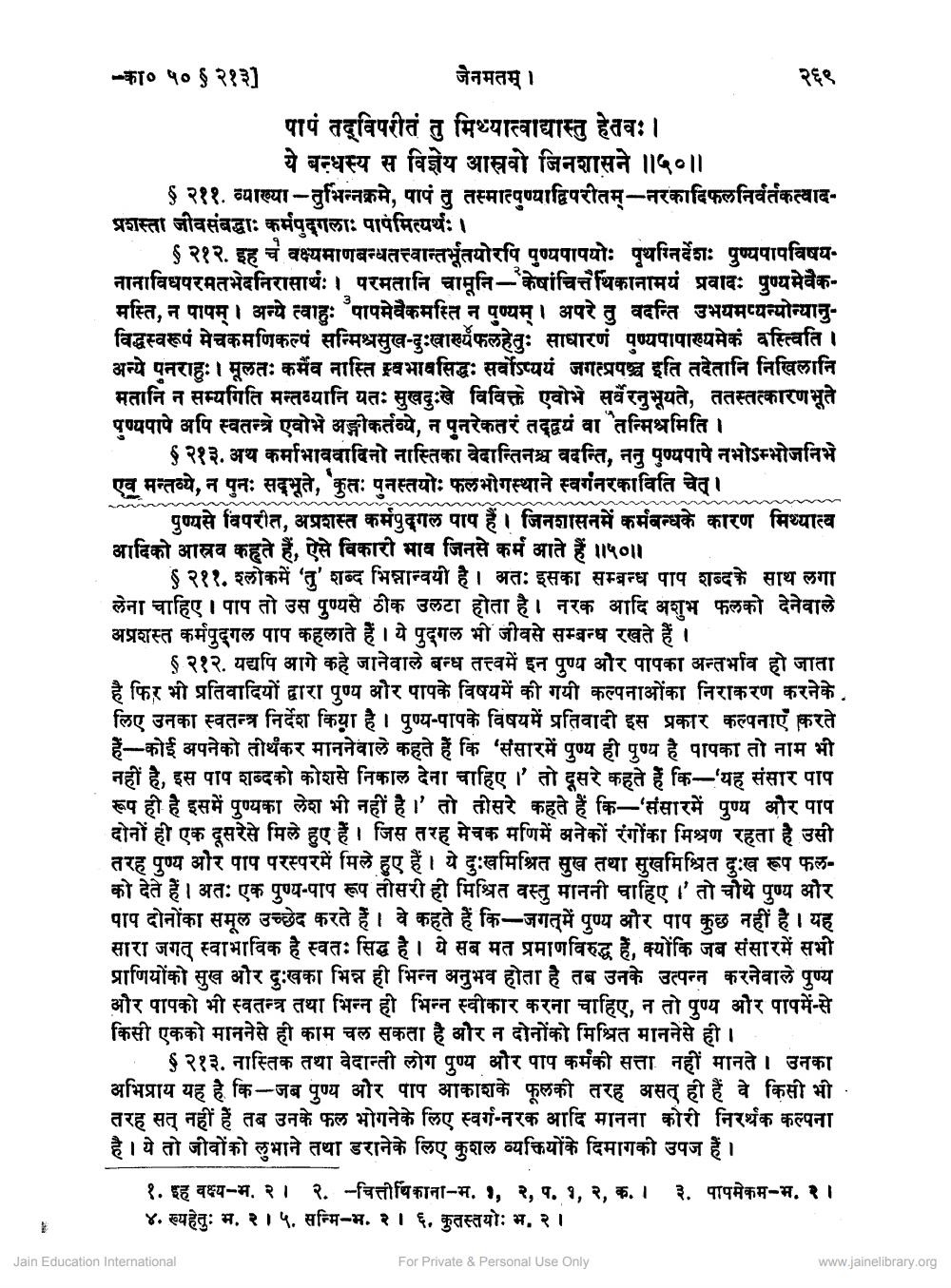________________
- का० ५० ६ २१३]
जैनमतम् ।
पापं तद्विपरीतं तु मिथ्यात्वाद्यास्तु हेतवः ।
ये बन्धस्य स विज्ञेय आस्रवो जिनशासने ॥५०॥
२६९
$ २११. व्याख्या - - तुभिन्नक्रमे पापं तु तस्मात्पुण्याद्विपरीतम् - नरकादिफलनिर्वर्तकत्वादप्रशस्ता जीव संबद्धाः कर्मपुद्गलाः पापमित्यर्थः ।
$ २१२. इह च वक्ष्यमाणबन्ध तत्त्वान्तर्भूतयोरपि पुण्यपापयोः पृथग्निर्देशः पुण्यपापविषयनानाविधपर मतभेदनिरासार्थः । परमतानि चामूनि - केषांचित्तैथिकानामयं प्रवादः पुण्यमेवैकमस्ति, न पापम् । अन्ये त्वाहुः पापमेवैकमस्ति न पुण्यम् । अपरे तु वदन्ति उभयमप्यन्योन्यानुविद्धस्वरूपं मेचकमणिकल्पं सन्मिश्रसुख-दुःखाख्यै फलहेतुः साधारणं पुण्यपापाख्यमेकं वस्त्विति । अन्ये पुनराहुः । मूलतः कर्मैव नास्ति स्वभावसिद्धः सर्वोऽप्ययं जगत्प्रपञ्च इति तदेतानि निखिलानि मतानि न सम्यगिति मन्तव्यानि यतः सुखदुःखे विविक्ते एवोभे सर्वैरनुभूयते, ततस्तत्कारणभू पुण्यपापे अपि स्वतन्त्रे एवोभे अङ्गीकर्तव्ये, न पुनरेकतरं तद्वयं वा तन्मिश्रमिति ।
६ २१३. अथ कर्माभाववादिनो नास्तिका वेदान्तिनश्च वदन्ति, ननु पुण्यपापे नभोऽम्भोजनिभे एव मन्तव्ये, न पुनः सभूते, कुतः पुनस्तयोः फलभोगस्थाने स्वर्गनरका विति चेत् ।
gora fवपरीत, अप्रशस्त कर्मपुद्गल पाप हैं। जिनशासन में कर्मबन्धके कारण मिथ्यात्व आदिको आस्रव कहते हैं, ऐसे विकारी भाव जिनसे कर्म आते हैं ॥५०॥
$ २११. श्लोकमें 'तु' शब्द भिन्नान्वयी है । अत: इसका सम्बन्ध पाप शब्द के साथ लगा लेना चाहिए । पाप तो उस पुण्यसे ठीक उलटा होता है। नरक आदि अशुभ फलको देनेवाले अप्रशस्त कर्मपुद्गल पाप कहलाते हैं । ये पुद्गल भी जीवसे सम्बन्ध रखते हैं ।
$ २१२. यद्यपि आगे कहे जानेवाले बन्ध तत्त्वमें इन पुण्य और पापका अन्तर्भाव हो जाता है फिर भी प्रतिवादियों द्वारा पुण्य और पापके विषयमें की गयी कल्पनाओंका निराकरण करनेके . लिए उनका स्वतन्त्र निर्देश किया है। पुण्य-पापके विषय में प्रतिवादी इस प्रकार कल्पनाएँ करते हैं- कोई अपनेको तीर्थंकर माननेवाले कहते हैं कि 'संसार में पुण्य ही पुण्य है पापका तो नाम भी नहीं है, इस पाप शब्दको कोशसे निकाल देना चाहिए ।' तो दूसरे कहते हैं कि - 'यह संसार पाप रूप ही है इसमें पुण्यका लेश भी नहीं है।' तो तीसरे कहते हैं कि - 'संसार में पुण्य और पाप दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। जिस तरह मेचक मणिमें अनेकों रंगों का मिश्रण रहता है उसी तरह पुण्य और पाप परस्पर में मिले हुए हैं। ये दुःखमिश्रित सुख तथा सुखमिश्रित दुःख रूप फल
।
देते हैं। अत: एक पुण्य-पाप रूप तीसरी ही मिश्रित वस्तु माननी चाहिए ।' तो चौथे पुण्य और पाप दोनोंका समूल उच्छेद करते हैं। वे कहते हैं कि-जगत् में पुण्य और पाप कुछ नहीं है । यह सारा जगत् स्वाभाविक है स्वतः सिद्ध है । ये सब मत प्रमाणविरुद्ध हैं, क्योंकि जब संसारमें सभी प्राणियोंको सुख और दुःखका भिन्न ही भिन्न अनुभव होता है तब उनके उत्पन्न करनेवाले पुण्य और पापको भी स्वतन्त्र तथा भिन्न हो भिन्न स्वीकार करना चाहिए, न तो पुण्य और पापमें से किसी एकको मानने से ही काम चल सकता है और न दोनोंको मिश्रित माननेसे ही ।
$ २१३. नास्तिक तथा वेदान्ती लोग पुण्य और पाप कर्मकी सत्ता नहीं मानते । उनका अभिप्राय यह है कि - जब पुण्य और पाप आकाशके फूलकी तरह असत् ही हैं वे किसी भी तरह सत् नहीं हैं तब उनके फल भोगनेके लिए स्वर्ग-नरक आदि मानना कोरी निरर्थक कल्पना है । ये तो जीवों को लुभाने तथा डरानेके लिए कुशल व्यक्तियोंके दिमागकी उपज हैं ।
Jain Education International
१. इह वक्ष्य-म २ । २. - चित्तीर्थिकाना-म. १, २, प. १, २, क. ३. पापमेकम-म. २ । ४. ख्यहेतुः म २ । ५. सन्मि-भ. २ । ६. कुतस्तयोः भ २ ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org