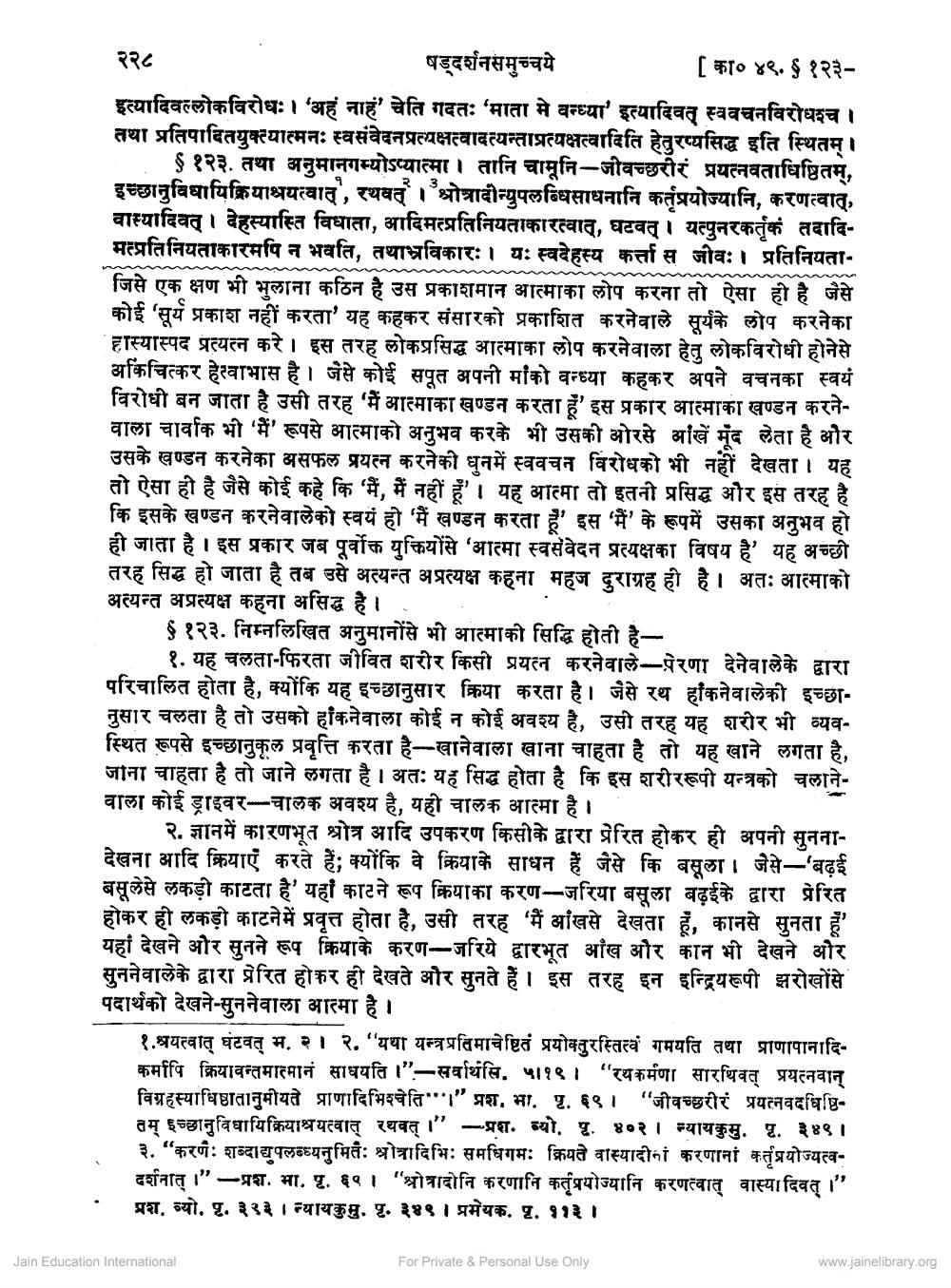________________
२२८
षड्दर्शनसमुच्चये
[ का० ४९.६ १२३इत्यादिवल्लोकविरोधः । 'अहं नाहं' चेति गदतः 'माता मे वन्ध्या' इत्यादिवत् स्ववचनविरोधश्च । तथा प्रतिपादितयुक्त्यात्मनः स्वसंवेदनप्रत्यक्षत्वादत्यन्ताप्रत्यक्षत्वादिति हेतुरप्यसिद्ध इति स्थितम् ।
$१२३. तथा अनुमानगम्योऽप्यात्मा। तानि चामूनि-जीवच्छरीरं प्रयत्नवताधिष्ठितम्, इच्छानुविधायिक्रियाश्रयत्वात्', रथवत् । श्रोत्रादीन्युपलब्धिसाधनानि कर्तृप्रयोज्यानि, करणत्वात्, वास्यादिवत् । देहस्यास्ति विधाता, आदिमत्प्रतिनियताकारत्वात्, घटवत् । यत्पुनरकर्तृकं तदादिमत्प्रतिनियताकारमपि न भवति, तथाभ्रविकारः। यः स्वदेहस्य कर्ता स जीवः। प्रतिनियताजिसे एक क्षण भी भुलाना कठिन है उस प्रकाशमान आत्माका लोप करना तो ऐसा ही है जैसे कोई 'सूर्य प्रकाश नहीं करता' यह कहकर संसारको प्रकाशित करनेवाले सूर्यके लोप करनेका हास्यास्पद प्रत्यत्न करे। इस तरह लोकप्रसिद्ध आत्माका लोप करनेवाला हेतु लोकविरोधी होनेसे अकिंचित्कर हेत्वाभास है। जैसे कोई सपूत अपनी मांको वन्ध्या कहकर अपने वचनका स्वयं विरोधी बन जाता है उसी तरह 'मैं आत्माका खण्डन करता हूँ' इस प्रकार आत्माका खण्डन करने
चार्वाक भी 'मैं' रूपसे आत्माको अनुभव करके भी उसकी ओरसे आंखें मंद लेता है और उसके खण्डन करनेका असफल प्रयत्न करनेकी धुनमें स्ववचन विरोधको भी नहीं देखता। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि 'मैं, मैं नहीं हूँ'। यह आत्मा तो इतनी प्रसिद्ध और इस तरह है कि इसके खण्डन करनेवालेको स्वयं हो 'मैं खण्डन करता है' इस 'मैं' के रूपमें उसका अनुभव हो ही जाता है । इस प्रकार जब पूर्वोक्त युक्तियोंसे 'आत्मा स्वसेवेदन प्रत्यक्षका विषय है' यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है तब उसे अत्यन्त अप्रत्यक्ष कहना महज दुराग्रह ही है। अतः आत्माको अत्यन्त अप्रत्यक्ष कहना असिद्ध है। . .
६१२३. निम्नलिखित अनुमानोंसे भी आत्माको सिद्धि होती है
१. यह चलता-फिरता जीवित शरीर किसी प्रयत्न करनेवाले-प्रेरणा देनेवालेके द्वारा परिचालित होता है, क्योंकि यह इच्छानुसार क्रिया करता है। जैसे रथ हांकनेवालेकी इच्छानुसार चलता है तो उसको हांकनेवाला कोई न कोई अवश्य है, उसी तरह यह शरीर भी व्यवस्थित रूपसे इच्छानुकूल प्रवृत्ति करता है-खानेवाला खाना चाहता है तो यह खाने लगता है, जाना चाहता है तो जाने लगता है । अतः यह सिद्ध होता है कि इस शरीररूपी यन्त्रको चलानेवाला कोई ड्राइवर-चालक अवश्य है, यही चालक आत्मा है।
२. ज्ञानमें कारणभूत श्रोत्र आदि उपकरण किसीके द्वारा प्रेरित होकर ही अपनी सुननादेखना आदि क्रियाएं करते हैं; क्योंकि वे क्रियाके साधन हैं जैसे कि बसूला। जैसे–'बढ़ई बसूलेसे लकड़ी काटता है' यहां काटने रूप क्रियाका करण-जरिया बसूला बढ़ईके द्वारा प्रेरित होकर ही लकड़ी काटने में प्रवत्त होता है, उसी तरह 'मैं आंखसे देखता है. कानसे सुनता है' यहां देखने और सुनने रूप क्रियाके करण-जरिये द्वारभूत आँख और कान भी देखने और सुननेवालेके द्वारा प्रेरित होकर ही देखते और सुनते हैं। इस तरह इन इन्द्रियरूपी झरोखोंसे पदार्थको देखने-सुननेवाला आत्मा है।
१.श्रयत्वात् घंटवत् म. २ । २. "यथा यन्त्रप्रतिमाचेष्टितं प्रयोक्तुरस्तित्वं गमयति तथा प्राणापानादिकर्मापि क्रियावन्तमात्मानं साधयति ।"-सर्वार्थसि. ५।१९। "रथकर्मणा सारथिवत् प्रयत्नवान विग्रहस्याधिष्ठातानुमीयते प्राणादिभिश्चेति""प्रश, भा. पृ. ६९। "जीवच्छरीरं प्रयत्नवदधिष्ठितम इच्छानुविधायिक्रियाश्रयत्वात् रथवत् ।" -प्रश. ब्यो, पृ. ४०२। न्यायकुमु. पृ. ३४९ । ३. “करणः शब्दाद्यपलब्ध्यनुमितः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते वास्यादीनां करणानां कर्तप्रयोज्यत्वदर्शनात ।" -प्रश. भा. पृ. ६५ । "श्रोत्रादोनि करणानि कर्तृप्रयोज्यानि करणत्वात् वास्यादिवत् ।" प्रश. व्यो. पृ. ३१३ । न्यायकुमु. पृ. ३४९ । प्रमेयक. पृ. ११३।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org