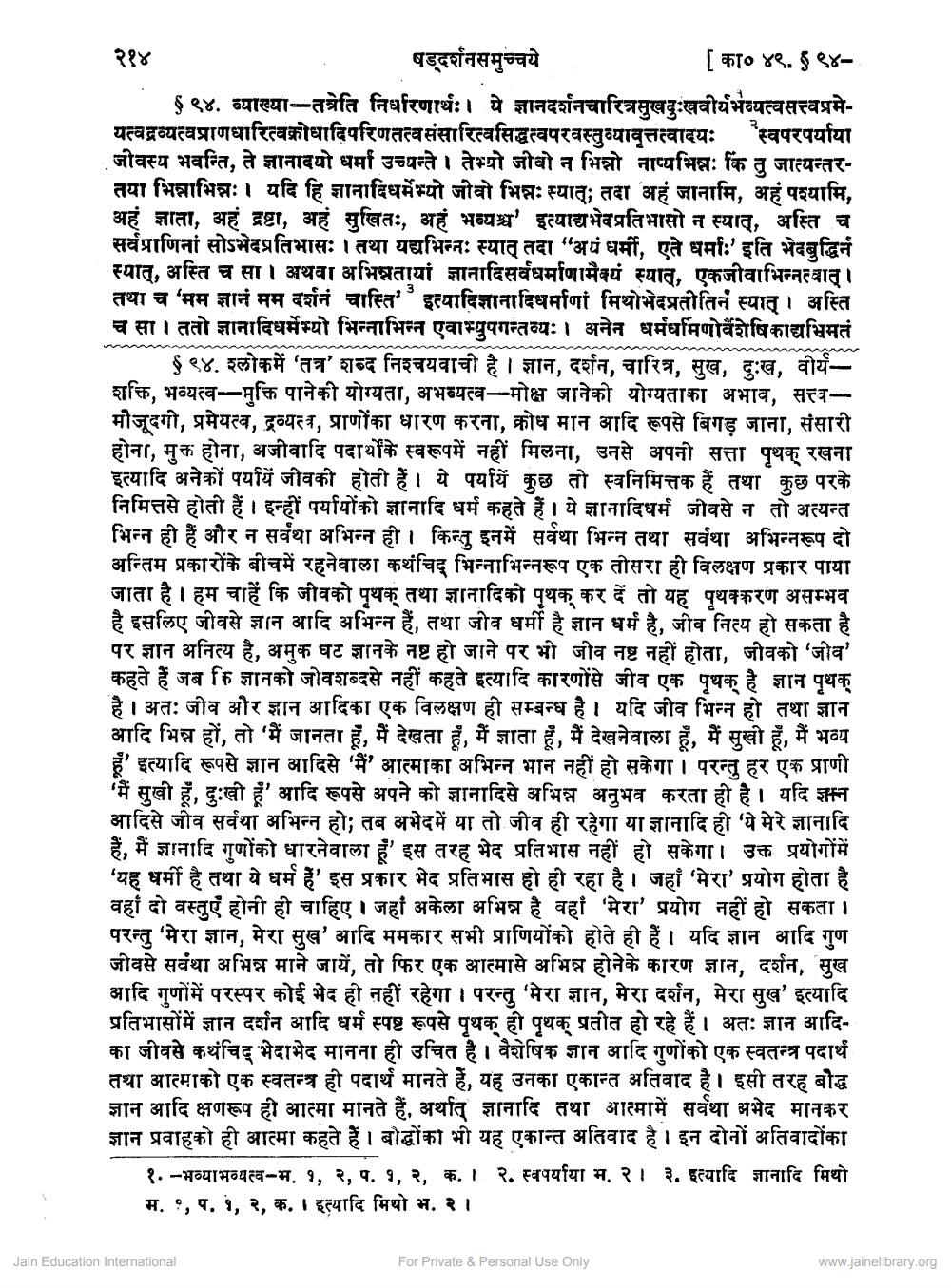________________
षड्दर्शनसमुच्चये
[ का० ४९. १९४
स्वपरपर्याया
९४. व्याख्या - तत्रेति निर्धारणार्थः । ये ज्ञानदर्शनचारित्रसुखदुःखवीर्य भेव्यत्व सत्त्वप्रमेयत्वद्रव्यत्वप्राणधारित्वक्रोधादिपरिणतत्व संसारित्व सिद्धत्व पर वस्तुव्यावृत्तत्वादयः . जीवस्य भवन्ति, ते ज्ञानादयो धर्मा उच्यन्ते । तेभ्यो जीवो न भिन्नो नाप्यभिन्नः किं तु जात्यन्तरतया भिन्नाभिन्नः । यदि हि ज्ञानादिधर्मेभ्यो जीवो भिन्नः स्यात्; तदा अहं जानामि, अहं पश्यामि, अहं ज्ञाता, अहं द्रष्टा, अहं सुखितः, अहं भव्यश्च' इत्याद्यभेदप्रतिभासो न स्यात्, अस्ति च सर्वप्राणिनां सोऽभेदप्रतिभासः । तथा यद्यभिन्नः स्यात् तदा " अयं धर्मो, एते धर्माः' इति भेदबुद्धिर्न स्यात्, अस्ति च सा । अथवा अभिन्नतायां ज्ञानादिसर्वधर्माणामैक्यं स्यात्, एकजीवाभिन्नत्वात् । तथा च 'मम ज्ञानं मम दर्शनं चास्ति' इत्यादिज्ञानादिधर्माणां मिथोभेदप्रतीतिनं स्यात् । अस्ति च सा । ततो ज्ञानादिधर्मेभ्यो भिन्नाभिन्न एवाभ्युपगन्तव्यः । अनेन धर्मधर्मणोवैशेषिकाद्यभिमतं
२१४
$ ९४. श्लोक में 'तत्र' शब्द निश्चयवाची है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, दुःख, वीर्यशक्ति, भव्यत्व - मुक्ति पाने की योग्यता, अभव्यत्व - मोक्ष जानेको योग्यताका अभाव, सत्त्वमोजूदगी, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्राणोंका धारण करना, क्रोध मान आदि रूपसे बिगड़ जाना, संसारी होना, मुक्त होना, अजीवादि पदार्थोंके स्वरूपमें नहीं मिलना, उनसे अपनी सत्ता पृथक् रखना इत्यादि अनेकों पर्यायें जीवकी होती हैं। ये पर्यायें कुछ तो स्वनिमित्तक हैं तथा कुछ परके निमित्तसे होती हैं । इन्हीं पर्यायोंको ज्ञानादि धर्म कहते हैं । ये ज्ञानादिधर्म जीवसे न तो अत्यन्त भिन्न ही हैं और न सर्वथा अभिन्न हो । किन्तु इनमें सर्वथा भिन्न तथा सर्वथा अभिन्नरूप दो अन्तिम प्रकारों के बीच में रहनेवाला कथंचिद् भिन्नाभिन्नरूप एक तीसरा ही विलक्षण प्रकार पाया जाता है । हम चाहें कि जीवको पृथक् तथा ज्ञानादिको पृथक कर दें तो यह पृथक्करण असम्भव है इसलिए जीवसे ज्ञान आदि अभिन्न हैं, तथा जीव धर्मी है ज्ञान धर्म है, जीव नित्य हो सकता है पर ज्ञान अनित्य है, अमुक घट ज्ञानके नष्ट हो जाने पर भी जीव नष्ट नहीं होता, जीवको 'जीव' कहते हैं जबकि ज्ञानको जीवशब्दसे नहीं कहते इत्यादि कारणोंसे जीव एक पृथक् है ज्ञान पृथक् है । अत: जीव और ज्ञान आदिका एक विलक्षण ही सम्बन्ध है । यदि जीव भिन्न हो तथा ज्ञान आदि भिन्न हों, तो 'मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं देखनेवाला हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं भव्य हूँ' इत्यादि रूपसे ज्ञान आदिसे 'मैं' आत्माका अभिन्न भान नहीं हो सकेगा। परन्तु हर एक प्राणी 'मैं सुखी हूँ, दुःखी हूँ' आदि रूपसे अपने को ज्ञानादिसे अभिन्न अनुभव करता ही है । यदि ज्ञान आदि जीव सर्वथा अभिन्न हो; तब अभेद में या तो जीव ही रहेगा या ज्ञानादि ही 'ये मेरे ज्ञानादि हैं, मैं ज्ञानादि गुणोंको धारनेवाला हूँ' इस तरह भेद प्रतिभास नहीं हो सकेगा। उक्त प्रयोगों में 'यह धर्मी है तथा ये धर्म हैं' इस प्रकार भेद प्रतिभास हो ही रहा है । जहाँ 'मेरा' प्रयोग होता है वहाँ दो वस्तुएँ होनी ही चाहिए। जहाँ अकेला अभिन्न है वहाँ 'मेरा' प्रयोग नहीं हो सकता । परन्तु 'मेरा ज्ञान, मेरा सुख' आदि ममकार सभी प्राणियोंको होते ही हैं । यदि ज्ञान आदि गुण जीवसे सर्वथा अभिन्न माने जायें, तो फिर एक आत्मासे अभिन्न होनेके कारण ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुणों में परस्पर कोई भेद ही नहीं रहेगा। परन्तु 'मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा सुख' इत्यादि प्रतिभासों में ज्ञान दर्शन आदि धर्म स्पष्ट रूपसे पृथक् ही पृथक् प्रतीत हो रहे हैं । अतः ज्ञान आदिका जीवसे कथंचिद् भेदाभेद मानना ही उचित है । वैशेषिक ज्ञान आदि गुणों को एक स्वतन्त्र पदार्थ तथा आत्माको एक स्वतन्त्र ही पदार्थ मानते हैं, यह उनका एकान्त अतिवाद है । इसी तरह बौद्ध ज्ञान आदि क्षणरूप ही आत्मा मानते हैं, अर्थात् ज्ञानादि तथा आत्मामें सर्वथा अभेद मानकर ज्ञान प्रवाहको ही आत्मा कहते हैं । बौद्धों का भी यह एकान्त अतिवाद है । इन दोनों अतिवादों का
१. - भव्या भव्यत्व - म. १, २, प. १, २, क. । २. स्वपर्याया म २। ३ इत्यादि ज्ञानादि मिथो म.९, प. १, २, क. । इत्यादि मिथो भ. २ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org