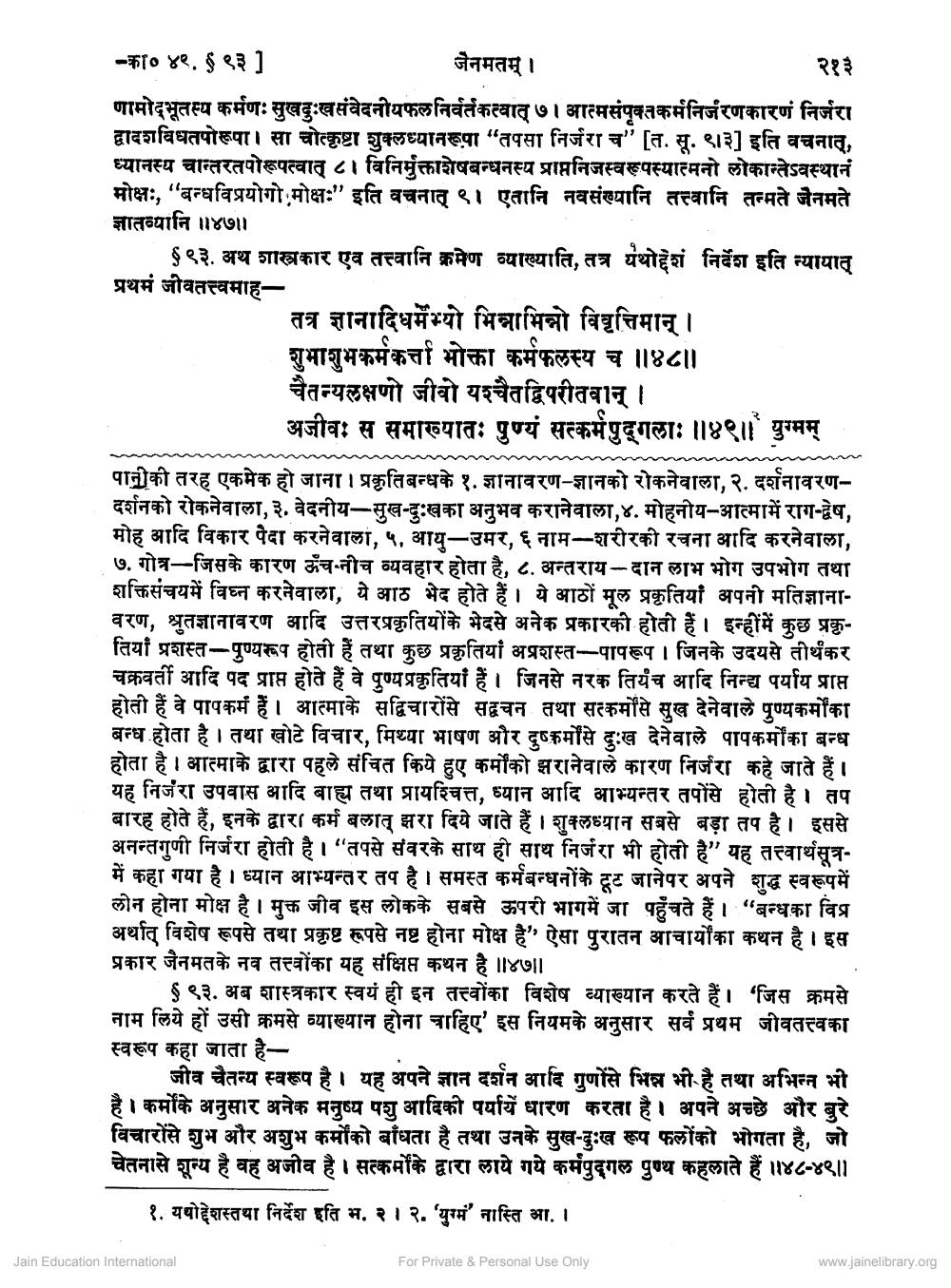________________
- का० ४९. $ ९३ ]
जैनमतम् ।
२१३
मोद्भूतस्य कर्मणः सुखदुःख संवेदनीयफल निर्वर्तकत्वात् ७ । आत्मसंपृक्त कर्मनिर्जरणकारणं निर्जरा द्वादशविधतपोरूपा । सा चोत्कृष्टा शुक्लध्यानरूपा " तपसा निर्जरा च" [त. सू. ९३] इति वचनात्, ध्यानस्य चान्तरत पोरूपत्वात् ८ । विनिर्मुक्ताशेषबन्धनस्य प्राप्तनिजस्वरूपस्यात्मनो लोकान्तेऽवस्थानं मोक्षः, "बन्धविप्रयोगो मोक्षः" इति वचनात् ९ । एतानि नवसंख्यानि तत्त्वानि तन्मते जैनमते ज्ञातव्यानि ॥४७॥
१९३. अथ शास्त्रकार एव तत्त्वानि क्रमेण व्याख्याति, तत्र येथेोद्देशं निर्देश इति न्यायात् प्रथमं जीवतत्त्वमाह -
तत्र ज्ञानादिधर्मेभ्यो भिन्नाभिन्नो विवृत्तिमान् । शुभाशुभकर्मकर्त्ता भोक्ता कर्मफलस्य च ॥ ४८ ॥ चैतन्यलक्षणो जीवो यश्चैतद्विपरीतवान् ।
अजीवः स समाख्यातः पुण्यं सत्कर्म पुद्गलाः ॥ ४९ ॥ युग्मम्
पानी की तरह एकमेक हो जाना । प्रकृतिबन्धके १. ज्ञानावरण-ज्ञानको रोकनेवाला, २. दर्शनावरणदर्शनको रोकनेवाला, ३. वेदनीय - सुख-दुःखका अनुभव करानेवाला, ४. मोहनीय - आत्मा में राग-द्वेष, मोह आदि विकार पैदा करनेवाला, ५ आयु - उमर, ६ नाम - शरीरकी रचना आदि करनेवाला, ७. गोत्र - जिसके कारण ऊँच-नीच व्यवहार होता है, ८. अन्तराय - दान लाभ भोग उपभोग तथा शक्तिसंचय में विघ्न करनेवाला, ये आठ भेद होते हैं । ये आठों मूल प्रकृतियाँ अपनी मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण आदि उत्तरप्रकृतियोंके भेदसे अनेक प्रकारको होती हैं। इन्हीं में कुछ प्रकृतियाँ प्रशस्त - पुण्यरूप होती हैं तथा कुछ प्रकृतियां अप्रशस्त - पापरूप | जिनके उदयसे तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि पद प्राप्त होते हैं वे पुण्यप्रकृतियां हैं। जिनसे नरक तियंच आदि निन्द्य पर्याय प्राप्त होती हैं वे पापकर्म हैं। आत्माके सद्विचारोंसे सद्वचन तथा सत्कर्मोंसे सुख देनेवाले पुण्यकर्मोंका बन्ध होता है । तथा खोटे विचार, मिथ्या भाषण और दुष्कर्मोसे दुःख देनेवाले पापकर्मीका बन्ध होता है। आत्मा द्वारा पहले संचित किये हुए कर्मोंको झरानेवाले कारण निर्जरा कहे जाते हैं । यह निर्जरा उपवास आदि बाह्य तथा प्रायश्चित्त, ध्यान आदि आभ्यन्तर तपोंसे होती है । तप बारह होते हैं, इनके द्वारा कर्म बलात् झरा दिये जाते हैं। शुक्लध्यान सबसे बड़ा तप है। इससे अनन्तगुणी निर्जरा होती है । " तपसे संवरके साथ ही साथ निर्जरा भी होती है" यह तत्त्वार्थसूत्रमें कहा गया है | ध्यान आभ्यन्तर तप है । समस्त कर्मबन्धनों के टूट जानेपर अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होना मोक्ष है | मुक्त जीव इस लोकके सबसे ऊपरी भागमें जा पहुँचते हैं। "बन्धका विप्र अर्थात् विशेष रूपसे तथा प्रकृष्ट रूपसे नष्ट होना मोक्ष है" ऐसा पुरातन आचार्योंका कथन है । इस प्रकार जैनमतके नव तत्त्वोंका यह संक्षिप्त कथन है ||४७||
$ ९३. अब शास्त्रकार स्वयं ही इन तत्वोंका विशेष व्याख्यान करते हैं । 'जिस क्रमसे नाम लिये हों उसी क्रमसे व्याख्यान होना चाहिए' इस नियमके अनुसार सर्व प्रथम जीवतत्त्वका स्वरूप कहा जाता है
जीव चैतन्य स्वरूप है । यह अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणोंसे भिन्न भी है तथा अभिन्न भी है | कर्मों अनुसार अनेक मनुष्य पशु आदिको पर्यायें धारण करता है । अपने अच्छे और बुरे विचारोंसे शुभ और अशुभ कर्मोंको बाँधता है तथा उनके सुख-दुःख रूप फलोंको भोगता है, जो चेतना शून्य है वह अजीव है । सत्कर्मोंके द्वारा लाये गये कर्मपुद्गल पुण्य कहलाते हैं ||४८-४९ ॥
१. यथोद्देशस्तथा निर्देश इति भ. २ । २. 'युग्मं' नास्ति आ. ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org