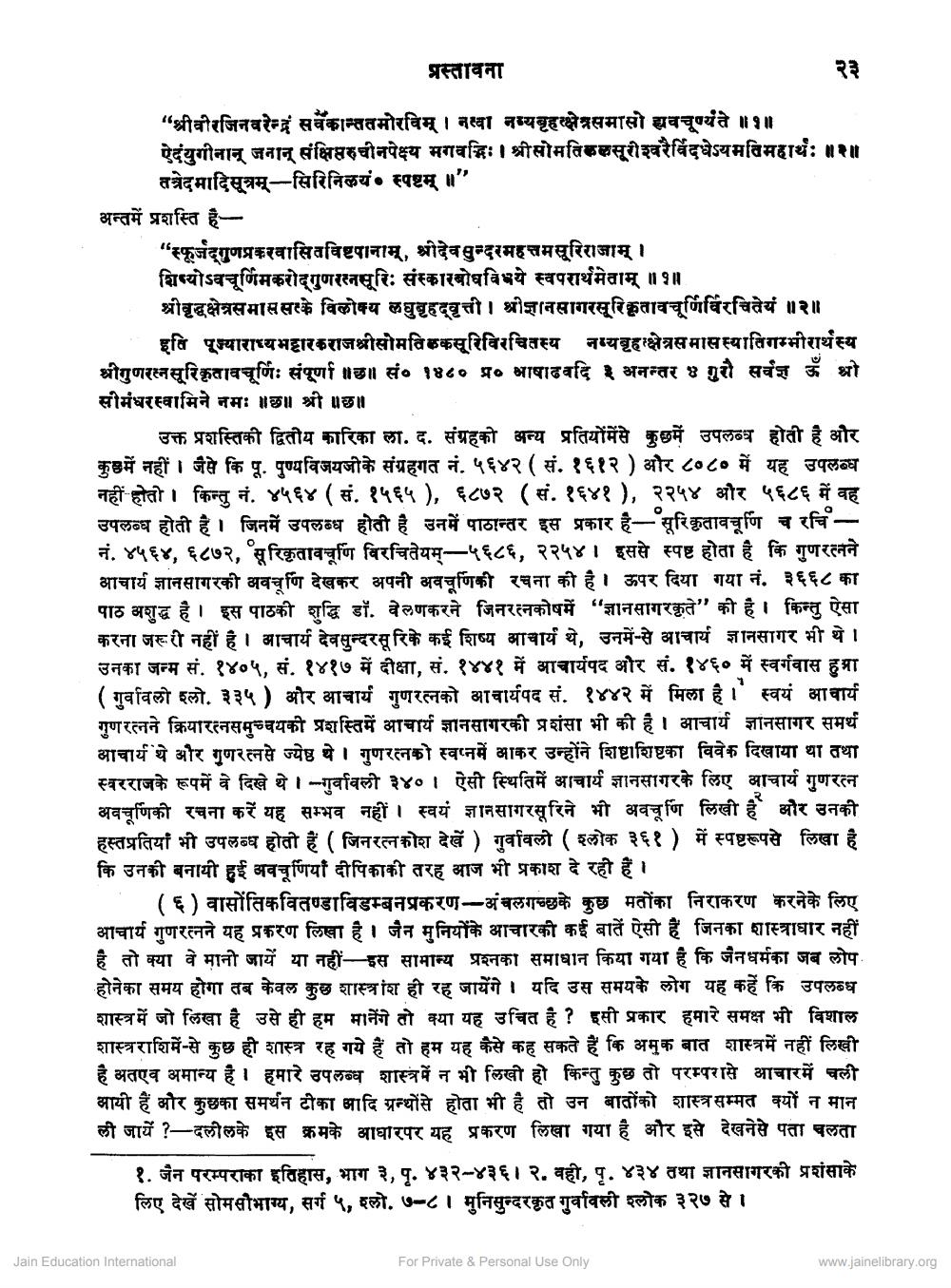________________
प्रस्तावना
२३
"श्रीवीरजिनवरेन्द्रं सर्वकान्ततमोरविम् । नवा नम्यबृहत्क्षेत्रसमासो रवचूयते ॥१॥ ऐदंयुगीनान् जनान् संक्षिप्तरुचीनपेक्ष्य मगवद्भिः। श्रीसोमतिकलसूरीश्वरैर्विदधेऽयमतिमहार्थः
तत्रेदमादिसूत्रम्-सिरिनिलयं• स्पष्टम् ॥" अन्तमें प्रशस्ति है
"स्फूर्जद्गुणप्रकरवासितविष्टपानाम्, श्रीदेवसुन्दरमहत्तमसूरिराजाम् । शिष्योऽवचूर्णिमकरोद्गुणरत्नसूरिः संस्कारबोधविषये स्वपरार्थमेताम् ॥१॥ श्रीवृद्धक्षेत्रसमाससके विलोक्य लघुबहवृत्ती। श्रीज्ञानसागरसूरिकृतावचूर्णिविरचितेयं ॥२॥
इति पूज्याराज्यभट्टारकराजश्रीसोमविलकसूरिविरचितस्य नग्यबृहरक्षेत्रसमासस्यातिगम्भीरार्थस्य श्रीगुणरत्नसूरिकृतावचूर्णिः संपूर्णा ॥छ॥ सं० १४४० प्र० भाषाढवदि ३ अनन्तर ४ गुरौ सर्वज्ञ ॐ श्री सीमंधरस्वामिने नमः ॥छ॥ श्री छ॥
उक्त प्रशस्तिकी द्वितीय कारिका ला. द. संग्रहको अन्य प्रतियोंमेंसे कुछमें उपलब्ध होती है और कुछमें नहीं । जैसे कि पू. पुण्यविजयजीके संग्रहगत नं. ५६४२ ( सं. १६१२ ) और ८०८० में यह उपलब्ध नहीं होती। किन्तु नं. ४५६४ (सं. १५६५), ६८७२ (सं. १६४१), २२५४ और ५६८६ में वह उपलब्ध होती है। जिनमें उपलब्ध होती है उनमें पाठान्तर इस प्रकार है-सूरि कृतावणि च रचिनं. ४५६४, ६८७२, सूरिकृतावचूणि विरचितेयम्-५६८६, २२५४ । इससे स्पष्ट होता है कि गुणरत्नने आचार्य ज्ञानसागरकी अवणि देखकर अपनी अवणिकी रचना की है। ऊपर दिया गया नं. ३६६८ का पाठ अशुद्ध है। इस पाठकी शद्धि डॉ. वेलणकरने जिनरत्नकोषमें "ज्ञानसागरकृते" की है। किन्तु ऐसा करना जरूरी नहीं है। आचार्य देवसुन्दरसूरिके कई शिष्य आचार्य थे, उनमें-से आचार्य ज्ञानसागर भी थे। उनका जन्म सं. १४०५, सं. १४१७ में दीक्षा, सं. १४४१ में आचार्यपद और सं. १४६० में स्वर्गवास हुआ (गुर्वावलो श्लो. ३३५) और आचार्य गुणरत्नको आचार्यपद सं. १४४२ में मिला है। स्वयं आचार्य गुणरत्नने क्रियारत्नसमुच्चयकी प्रशस्तिमें आचार्य ज्ञानसागरकी प्रशंसा भी की है। आचार्य ज्ञानसागर समर्थ आचार्य थे और गुणरत्नसे ज्येष्ठ थे। गुणरत्नको स्वप्नमें आकर उन्होंने शिष्टाशिष्टका विवेक दिखार स्वरराजके रूपमें वे दिखे थे। -गविली ३४०। ऐसी स्थितिमें आचार्य ज्ञानसागरके लिए आचार्य गुणरत्न अवचूर्णिकी रचना करें यह सम्भव नहीं। स्वयं ज्ञानसागरसूरिने भी अवचूणि लिखी है और उनकी हस्तप्रतियां भी उपलब्ध होती हैं (जिनरत्नकोश देखें ) गुर्वावलो (श्लोक ३६१) में स्पष्टरूपसे लिखा है कि उनकी बनायी हुई अवचूणियाँ दीपिकाकी तरह आज भी प्रकाश दे रही हैं।
(६) वासोंतिकवितण्डाविडम्बनप्रकरण-अंचलगच्छके कुछ मतोंका निराकरण करनेके लिए आचार्य गुणरत्नने यह प्रकरण लिखा है। जैन मुनियोंके आचारकी कई बातें ऐसी हैं जिनका शास्त्राधार नहीं है तो क्या वे मानो जायें या नहीं इस सामान्य प्रश्नका समाधान किया गया है कि जैनधर्मका जब लोप होनेका समय होगा तब केवल कुछ शास्त्रांश ही रह जायेंगे। यदि उस समयके लोग यह कहें कि उपलब्ध शास्त्र में जो लिखा है उसे ही हम मानेंगे तो क्या यह उचित है ? इसी प्रकार हमारे समक्ष भी विशाल शास्त्रराशिमें-से कुछ ही शास्त्र रह गये हैं तो हम यह कैसे कह सकते है कि अमुक बात शास्त्रमें नहीं लिखी है अतएव अमान्य है। हमारे उपलब्ध शास्त्र में न भी लिखी हो किन्तु कुछ तो परम्परासे आचारमें चली आयी हैं और कुछका समर्थन टीका आदि ग्रन्थोंसे होता भी है तो उन बातोंको शास्त्रसम्मत क्यों न मान ली जायें ?-दलीलके इस क्रमके आधारपर यह प्रकरण लिखा गया है और इसे देखनेसे पता चलता
१. जैन परम्पराका इतिहास, भाग ३, पृ. ४३२-४३६ । २. वही, पृ. ४३४ तथा ज्ञानसागरकी प्रशंसाके लिए देखें सोमसौभाग्य, सर्ग ५, श्लो. ७-८ । मुनिसुन्दरकृत गुर्वावली श्लोक ३२७ से ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org