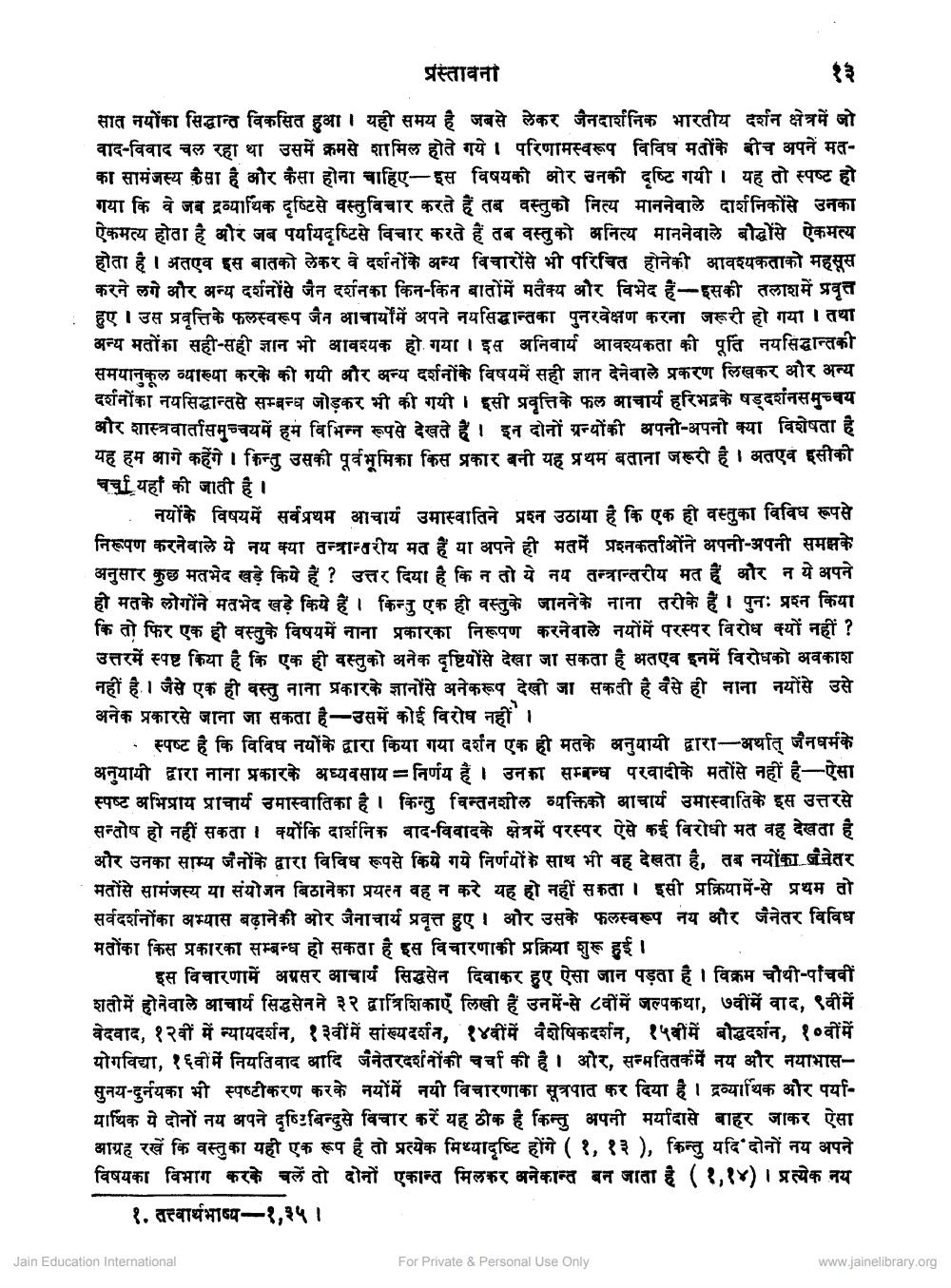________________
प्रस्तावना
सात नयोंका सिद्धान्त विकसित हुआ। यही समय है जबसे लेकर जैनदार्शनिक भारतीय दर्शन क्षेत्र में जो वाद-विवाद चल रहा था उसमें क्रमसे शामिल होते गये । परिणामस्वरूप विविध मतोंके बीच अपनें मतका सामंजस्य कैसा है और कैसा होना चाहिए-इस विषयकी ओर उनकी दृष्टि गयी। यह तो स्पष्ट हो गया कि वे जब द्रव्याथिक दृष्टिसे वस्तुविचार करते हैं तब वस्तुको नित्य माननेवाले दार्शनिकोंसे उनका ऐकमत्य होता है और जब पर्यायदृष्टिसे विचार करते हैं तब वस्तुको अनित्य माननेवाले बौद्धोंसे ऐकमत्य होता है । अतएव इस बातको लेकर वे दर्शनोंके अन्य विचारोंसे भी परिचित होनेकी आवश्यकताको महसूस करने लगे और अन्य दर्शनोंसे जैन दर्शनका किन-किन बातोंमें मतैक्य और विभेद है-इसकी तलाशमें प्रवृत्त हुए । उस प्रवृत्तिके फलस्वरूप जैन आचार्यों में अपने नयसिद्धान्तका पुनरवेक्षण करना जरूरी हो गया । तथा अन्य मतोंका सही-सही ज्ञान भी आवश्यक हो गया। इस अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति नयसिद्धान्तकी समयानुकूल व्याख्या करके को गयी और अन्य दर्शनोंके विषयमें सही ज्ञान देनेवाले प्रकरण लिखकर और अन्य दर्शनोंका नयसिद्धान्तसे सम्बन्ध जोडकर भी की गयी। इसी प्रवृत्तिके फल आचार्य हरिभद्रके षड्दर्शनसमुच्चय और शास्त्रवार्तासमुच्चयमें हम विभिन्न रूपसे देखते हैं। इन दोनों ग्रन्योंकी अपनी-अपनी क्या विशेषता है यह हम आगे कहेंगे । किन्तु उसकी पूर्वभूमिका किस प्रकार बनी यह प्रथम बताना जरूरी है । अतएव इसीको चर्चा यहां की जाती है।
. नयोंके विषयमें सर्वप्रथम आचार्य उमास्वातिने प्रश्न उठाया है कि एक ही वस्तुका विविध रूपसे निरूपण करनेवाले ये नय क्या तन्त्रान्तरीय मत हैं या अपने ही मतमें प्रश्नकर्ताओंने अपनी-अपनी समझके अनुसार कुछ मतभेद खड़े किये हैं ? उत्तर दिया है कि न तो ये नय तन्त्रान्तरीय मत हैं और न ये अपने हो मतके लोगोंने मतभेद खड़े किये हैं। किन्तु एक ही वस्तुके जानने के नाना तरीके हैं। पुनः प्रश्न किया कि तो फिर एक ही वस्तुके विषयमें नाना प्रकारका निरूपण करनेवाले नयोंमें परस्पर विरोध क्यों नहीं? उत्तरमें स्पष्ट किया है कि एक ही वस्तुको अनेक दृष्टियोंसे देखा जा सकता है अतएव इनमें विरोधको अवकाश नहीं है । जैसे एक ही वस्तु नाना प्रकारके ज्ञानोंसे अनेकरूप देखी जा सकती है वैसे ही नाना नयोंसे उसे अनेक प्रकारसे जाना जा सकता है-उसमें कोई विरोध नहीं ।
• स्पष्ट है कि विविध नयों के द्वारा किया गया दर्शन एक ही मतके अनुयायी द्वारा अर्थात् जैनधर्मके अनुयायी द्वारा नाना प्रकारके अध्यवसाय = निर्णय है। उनका सम्बन्ध परवादीके मतोंसे नहीं है-ऐसा स्पष्ट अभिप्राय प्राचार्य उमास्वातिका है। किन्तु चिन्तनशील व्यक्तिको आचार्य उमास्वातिके इस उत्तरसे सन्तोष हो नहीं सकता। क्योंकि दार्शनिक वाद-विवादके क्षेत्रमें परस्पर ऐसे कई विरोधी मत वह देखता है और उनका साम्य जैनोंके द्वारा विविध रूपसे किये गये निर्णयों के साथ भी वह देखता है, तब नयोंका जैनेतर
सामंजस्य या संयोजन बिठानेका प्रयत्न वह न करे यह हो नहीं सकता। इसी प्रक्रिया में से प्रथम तो सर्वदर्शनोंका अभ्यास बढ़ाने की ओर जैनाचार्य प्रवृत्त हए। और उसके फलस्वरूप नय और जैनेतर विविध मतोंका किस प्रकारका सम्बन्ध हो सकता है इस विचारणाकी प्रक्रिया शुरू हुई।
इस विचारणामें अग्रसर आचार्य सिद्धसेन दिवाकर हए ऐसा जान पड़ता है । विक्रम चौथी-पांचवीं शतीमें होनेवाले आचार्य सिद्धसेनने ३२ द्वात्रिशिकाएँ लिखी हैं उनमें से ८वों में जल्पकथा, ७वीमें वाद, ९वीं में वेदवाद, १२वीं में न्यायदर्शन, १३वों में सांख्यदर्शन, १४वीं में वैशेषिकदर्शन, १५वीमें बौद्धदर्शन, १०वोंमें योगविद्या, १६वों में नियतिवाद आदि जैनेतरदर्शनोंकी चर्चा की है। और, सन्मतितर्कमें नय और नयाभाससुनय-दुर्नयका भी स्पष्टीकरण करके नयोंमें नयी विचारणाका सूत्रपात कर दिया है। द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक ये दोनों नय अपने दृष्टिबिन्दुसे विचार करें यह ठीक है किन्तु अपनी मर्यादासे बाहर जाकर ऐसा आग्रह रखें कि वस्तु का यही एक रूप है तो प्रत्येक मिथ्यादष्टि होंगे (१,१३ ), किन्तु यदि दोनों नय अपने विषयका विभाग करके चलें तो दोनों एकान्त मिलकर अनेकान्त बन जाता है (१,१४) । प्रत्येक नय
१. तत्त्वार्थभाष्य-१,३५ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org