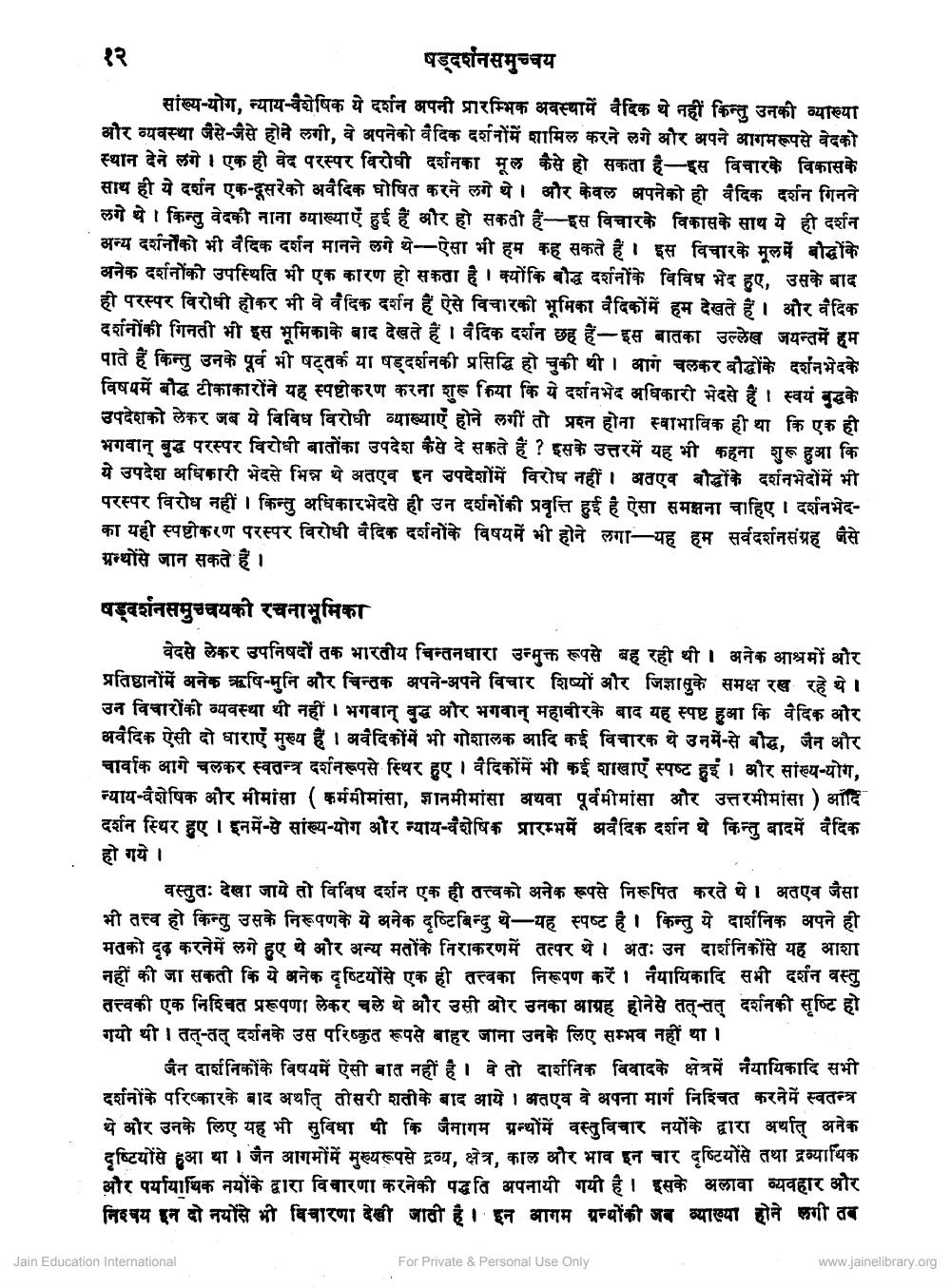________________
षड्दर्शनसमुच्चय
सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक ये दर्शन अपनी प्रारम्भिक अवस्थामें वैदिक थे नहीं किन्तु उनकी व्याख्या और व्यवस्था जैसे-जैसे होने लगी, वे अपनेको वैदिक दर्शनोंमें शामिल करने लगे और अपने आगमरूपसे वेदको स्थान देने लगे। एक ही वेद परस्पर विरोधी दर्शनका मूल कैसे हो सकता है-इस विचारके विकासके साथ ही ये दर्शन एक-दूसरेको अवैदिक घोषित करने लगे थे। और केवल अपनेको हो वैदिक दर्शन गिनने लगे थे। किन्तु वेदकी नाना व्याख्याएँ हुई हैं और हो सकती है-इस विचारके विकासके साथ ये ही दर्शन अन्य दर्शनोंको भी वैदिक दर्शन मानने लगे थे-ऐसा भी हम कह सकते हैं। इस विचारके मूल में बौद्धोंके अनेक दर्शनोंको उपस्थिति भी एक कारण हो सकता है । क्योंकि बौद्ध दर्शनोंके विविध भेद हए, उसके बाद ही परस्पर विरोधी होकर भी वे वैदिक दर्शन हैं ऐसे विचारको भूमिका वैदिकोंमें हम देखते हैं। और वैदिक दर्शनोंकी गिनती भी इस भूमिकाके बाद देखते हैं । वैदिक दर्शन छह हैं-इस बातका उल्लेख जयन्तमें हम पाते हैं किन्तु उनके पूर्व भी षट्तर्क या षड्दर्शनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी। आगे चलकर बौद्धोंके दर्शनभेदके विषयमें बौद्ध टीकाकारोंने यह स्पष्टीकरण करना शुरू किया कि ये दर्शनभेद अधिकारी भेदसे हैं। स्वयं बुद्धके उपदेशको लेकर जब ये विविध विरोधी व्याख्याएं होने लगी तो प्रश्न होना स्वाभाविक ही था कि एक ही भगवान् बुद्ध परस्पर विरोधी बातोंका उपदेश कैसे दे सकते हैं ? इसके उत्तरमें यह भी कहना शुरू हुआ कि ये उपदेश अधिकारी भेदसे भिन्न थे अतएव इन उपदेशोंमें विरोध नहीं। अतएव बौद्धोंके दर्शनभेदोंमें भी परस्पर विरोध नहीं। किन्तु अधिकारभेदसे ही उन दर्शनोंकी प्रवृत्ति हुई है ऐसा समझना चाहिए । दर्शनभेदका यही स्पष्टीकरण परस्पर विरोधी वैदिक दर्शनोंके विषय में भी होने लगा-यह हम सर्वदर्शनसंग्रह जैसे ग्रन्थोंसे जान सकते है।
षड्दर्शनसमुच्चयको रचनाभूमिका
वेदसे लेकर उपनिषदों तक भारतीय चिन्तनधारा उन्मुक्त रूपसे बह रही थी। अनेक आश्रमों और प्रतिष्ठानोंमें अनेक ऋषि-मुनि और चिन्तक अपने-अपने विचार शिष्यों और जिज्ञासुके समक्ष रख रहे थे। उन विचारोंकी व्यवस्था थी नहीं । भगवान् बुद्ध और भगवान् महावीरके बाद यह स्पष्ट हुआ कि वैदिक और अवैदिक ऐसी दो धाराएँ मुख्य है। अवैदिकों में भी गोशालक आदि कई विचारक थे उनमें-से बौद्ध, जैन और चार्वाक आगे चलकर स्वतन्त्र दर्शनरूपसे स्थिर हुए । वैदिकोंमें भी कई शाखाएं स्पष्ट हुई। और सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक और मीमांसा (कर्ममीमांसा, ज्ञानमीमांसा अथवा पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा) आदि दर्शन स्थिर हुए। इनमें से सांख्य-योग और न्याय-वैशेषिक प्रारम्भमें अवैदिक दर्शन थे किन्तु बादमें वैदिक हो गये।
वस्तुतः देखा जाये तो विविध दर्शन एक ही तत्त्वको अनेक रूपसे निरूपित करते थे। अतएव जैसा भी तत्त्व हो किन्तु उसके निरूपणके ये अनेक दृष्टिबिन्दु थे—यह स्पष्ट है। किन्तु ये दार्शनिक अपने ही मतको दृढ़ करने में लगे हुए थे और अन्य मतोंके निराकरणमें तत्पर थे। अतः उन दार्शनिकोंसे यह आशा नहीं की जा सकती कि ये अनेक दृष्टियोंसे एक ही तत्त्वका निरूपण करें। नैयायिकादि सभी दर्शन वस्तु तत्त्वकी एक निश्चित प्ररूपणा लेकर चले थे और उसी ओर उनका आग्रह होनेसे तत-तत् दर्शनकी सृष्टि हो गयी थी। तत-तत् दर्शनके उस परिष्कृत रूपसे बाहर जाना उनके लिए सम्भव नहीं था।
जैन दार्शनिकोंके विषयमें ऐसी बात नहीं है। वे तो दार्शनिक विवादके क्षेत्रमें नैयायिकादि सभी दर्शनोंके परिष्कारके बाद अर्थात तीसरी शतीके बाद आये। अतएव वे अपना मार्ग निश्चित करने में स्वतन्त्र थे और उनके लिए यह भी सुविधा थी कि जैमागम ग्रन्थोंमें वस्तुविचार नयोंके द्वारा अर्थात् अनेक दृष्टियोंसे हुआ था। जैन आगमोंमें मुख्यरूपसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चार दृष्टियोंसे तथा द्रव्यार्थिक और पर्यायाथिक नयोंके द्वारा विचारणा करनेकी पद्धति अपनायी गयी है। इसके अलावा व्यवहार और निश्चय इन दो नयोंसे भी विचारणा देखी जाती है। इन आगम ग्रन्थोंकी जब व्याख्या होने लगी तब
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org