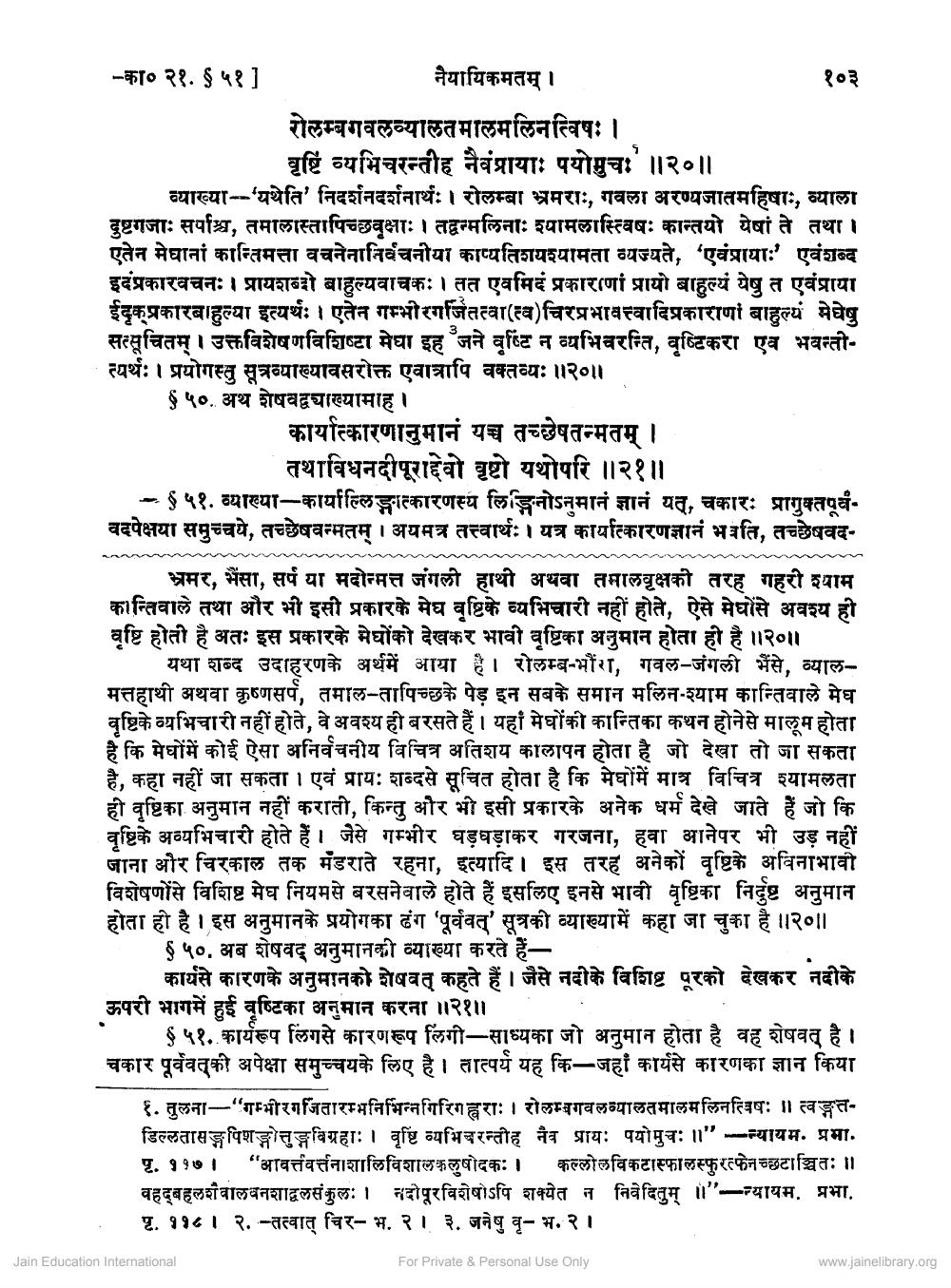________________
-का० २१. ६५१] नैयायिकमतम् ।
१०३ रोलम्बगवलव्यालतमालमलिनत्विषः ।
वृष्टिं व्यभिचरन्तीह नैवंप्रायाः पयोमुचा ॥२०॥ व्याख्या--'यथेति' निदर्शनदर्शनार्थः । रोलम्बा भ्रमराः, गवला अरण्यजातमहिषाः, व्याला दुष्टगजाः सपश्चि, तमालास्तापिच्छवृक्षाः । तद्वन्मलिनाः श्यामलास्त्विषः कान्तयो येषां ते तथा । एतेन मेघानां कान्तिमत्ता वचनेनानिर्वचनीया काप्यतिशयश्यामता व्यज्यते, 'एवंप्रायाः' एवंशब्द इदंप्रकारवचनः। प्रायशब्दो बाहुल्यवाचकः । तत एवमिदं प्रकाराणां प्रायो बाहुल्यं येषु त एवंप्राया ईदृकप्रकारबाहुल्या इत्यर्थः । एतेन गम्भीरगजितत्वा(त्व)चिरप्रभावत्वादिप्रकाराणां बाहुल्यं मेघेषु सत्सूचितम् । उक्तविशेषणविशिष्टा मेघा इह जने वृष्टि न व्यभिवरन्ति, वृष्टिकरा एव भवन्तीत्यर्थः । प्रयोगस्तु सूत्रव्याख्यावसरोक्त एवात्रापि वक्तव्यः ॥२०॥ ६५०. अथ शेषवद्वयाख्यामाह।
कार्याकारणानुमानं यच्च तच्छेषतन्मतम् ।
तथाविधनदीपूराद्देवो वृष्टो यथोपरि ॥२१॥ - ६५१. व्याख्या-कार्याल्लिङ्गात्कारणस्य लिङ्गिनोऽनुमानं ज्ञानं यत्, चकारः प्रागुक्तपूर्ववदपेक्षया समुच्चये, तच्छेषवन्मतम् । अयमत्र तत्त्वार्थः। यत्र कार्यात्कारणज्ञानं भवति, तच्छेषवद
भ्रमर, भैंसा, सर्प या मदोन्मत्त जंगली हाथी अथवा तमालवृक्षको तरह गहरी श्याम कान्तिवाले तथा और भी इसी प्रकारके मेघ वृष्टिके व्यभिचारी नहीं होते, ऐसे मेघोंसे अवश्य ही वृष्टि होती है अतः इस प्रकारके मेघोंको देखकर भावी वृष्टिका अनुमान होता ही है ॥२०॥ ___यथा शब्द उदाहरणके अर्थमें आया है। रोलम्ब-भौंरा, गवल-जंगली भैंसे, व्यालमत्तहाथी अथवा कृष्णसर्प, तमाल-तापिच्छके पेड़ इन सबके समान मलिन-श्याम कान्तिवाले मेघ
भचारी नहीं होते, वे अवश्य ही बरसते हैं। यहाँ मेघोंकी कान्तिका कथन होनेसे मालूम होता है कि मेघोंमें कोई ऐसा अनिर्वचनीय विचित्र अतिशय कालापन होता है जो देखा तो जा सकता है, कहा नहीं जा सकता । एवं प्रायः शब्दसे सूचित होता है कि मेघोंमें मात्र विचित्र श्यामलता ही वृष्टिका अनुमान नहीं कराती, किन्तु और भी इसी प्रकारके अनेक धर्म देखे जाते हैं जो कि वृष्टिके अव्यभिचारी होते हैं। जैसे गम्भीर घड़घड़ाकर गरजना, हवा आनेपर भी उड़ नहीं जाना और चिरकाल तक मंडराते रहना, इत्यादि। इस तरह अनेकों वृष्टिके अविनाभावी विशेषणोंसे विशिष्ट मेघ नियमसे बरसनेवाले होते हैं इसलिए इनसे भावी वृष्टिका निदृष्ट अनुमान होता ही है । इस अनुमानके प्रयोगका ढंग 'पूर्ववत्' सूत्रकी व्याख्या में कहा जा चुका है ॥२०॥
६५०. अब शेषवद् अनुमानकी व्याख्या करते हैं
कार्यसे कारणके अनुमानको शेषवत् कहते हैं। जैसे नदीके विशिष्ट पूरको देखकर नदीके ऊपरी भागमें हुई वृष्टिका अनुमान करना ॥२१॥
५१. कार्यरूप लिंगसे कारणरूप लिंगी-साध्यका जो अनुमान होता है वह शेषवत् है। चकार पूर्ववत्की अपेक्षा समुच्चयके लिए है। तात्पर्य यह कि-जहाँ कार्यसे कारणका ज्ञान किया
१. तुलना-“गम्भीरगजितारम्भनिभिन्नगिरिगह्वराः । रोलम्बगवलव्यालतमालमलिनत्विषः ॥ त्वङ्गतडिल्लतासङ्गपिशङ्गोत्तुङ्गविग्रहाः । वृष्टिं व्यभिचरन्तीह नैव प्रायः पयोमुचः॥"-न्यायम. प्रमा. पृ. ११७। "आवर्त्तवर्त्तनाशालिविशालकलुषोदकः। कल्लोलविकटास्फालस्फुरत्फेनच्छटाञ्चितः ॥ वहद्बहलशैवालवनशाद्वलसंकुलः । नदोपूरविशेषोऽपि शक्येत न निवेदितुम् ॥"-न्यायम. प्रभा. पृ. ११८। २. -तत्वात् चिर- भ. २। ३. जनेषु वृ-भ.२।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org