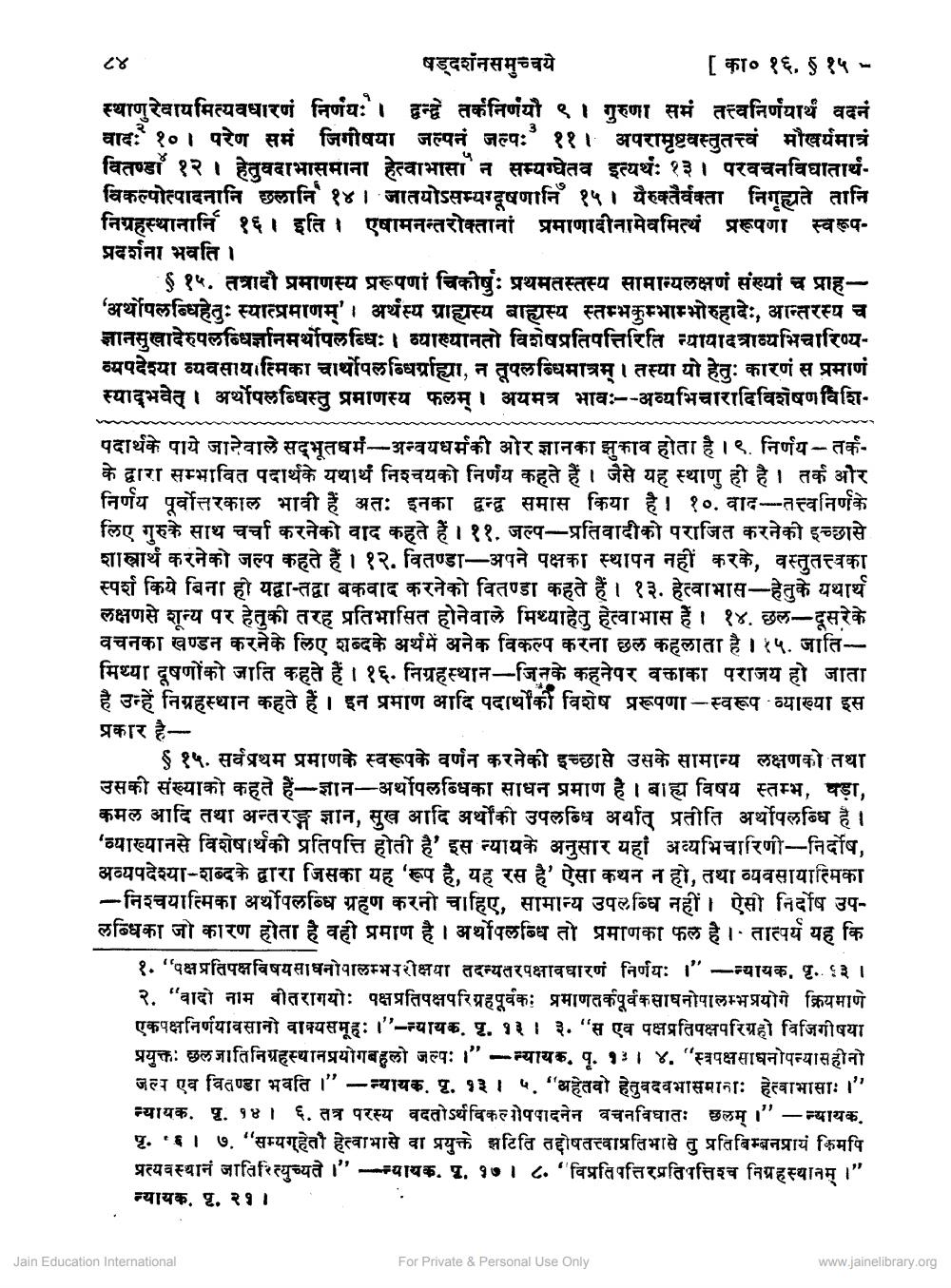________________
८४
षड्दर्शनसमुच्चय
[ का० १६, ६ १५ - स्थाणुरेवायमित्यवधारणं निर्णयः। द्वन्द्वे तर्कनिर्णयौ ९ । गुरुणा समं तत्त्वनिर्णयार्थं वदनं वादः १०। परेण समं जिगीषया जल्पनं जल्पः ११। अपरामृष्टवस्तुतत्त्वं मौखर्यमात्रं वितण्डा १२ । हेतुवदाभासमाना हेत्वाभासा न सम्यग्घेतव इत्यर्थः १३। परवचनविघातार्थविकल्पोत्पादनानि छलानि १४ । जातयोऽसम्यग्दूषणानि १५ । यैरुक्तैर्वक्ता निगृह्यते तानि निग्रहस्थानानि १६ । इति । एषामनन्तरोक्तानां प्रमाणादीनामेवमित्थं प्ररूपणा स्वरूपप्रदर्शना भवति।
१५. तत्रादौ प्रमाणस्य प्ररूपणां चिकीर्षुः प्रथमतस्तस्य सामान्यलक्षणं संख्यां च प्राह'अर्थोपलब्धिहेतुः स्यात्प्रमाणम्'। अर्थस्य ग्राह्यस्य बाह्यस्य स्तम्भकुम्भाम्भोरुहादेः, आन्तरस्य च ज्ञानसुखादेरुपलब्धिर्ज्ञानमर्थोपलब्धिः। व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरिति न्यायादत्राव्यभिचारिण्यव्यपदेश्या व्यवसायात्मिका चार्थोपलब्धिाह्या, न तूपलब्धिमात्रम् । तस्या यो हेतुः कारणं स प्रमाणं स्याद्भवेत् । अर्थोपलब्धिस्तु प्रमाणस्य फलम् । अयमत्र भाव:--अव्यभिचारादिविशेषणविशिपदार्थके पाये जानेवाले सद्भूतधर्म-अन्वयधर्मकी ओर ज्ञानका झुकाव होता है । ९. निर्णय- तर्कके द्वारा सम्भावित पदार्थके यथार्थ निश्चयको निर्णय कहते हैं। जैसे यह स्थाणु ही है। तर्क और निर्णय पूर्वोत्तरकाल भावी हैं अतः इनका द्वन्द्व समास किया है। १०. वाद-तत्त्वनिर्णके लिए गरुके साथ चर्चा करनेको वाद कहते हैं। ११. जल्प-प्रतिवादीको पराजित करनेकी इच्छासे शास्त्रार्थ करनेको जल्प कहते हैं । १२. वितण्डा-अपने पक्षका स्थापन नहीं करके, वस्तुतत्त्वका स्पर्श किये बिना हो यद्वा-तद्वा बकवाद करनेको वितण्डा कहते हैं । १३. हेत्वाभास-हेतुके यथार्थ लक्षणस शन्य पर हेतूकी तरह प्रतिभासित होनेवाले मिथ्याहेतू हेत्वाभास हैं। १४. छल-दुसरेके वचनका खण्डन करने के लिए शब्दके अर्थ में अनेक विकल्प करना छल कहलाता है । १५. जातिमिथ्या दूषणोंको जाति कहते हैं । १६. निग्रहस्थान-जिनके कहनेपर वक्ताका पराजय हो जाता है उन्हें निग्रहस्थान कहते हैं। इन प्रमाण आदि पदार्थोंकी विशेष प्ररूपणा-स्वरूप व्याख्या इस प्रकार है
१५. सर्वप्रथम प्रमाणके स्वरूपके वर्णन करनेकी इच्छासे उसके सामान्य लक्षणको तथा उसकी संख्याको कहते हैं-ज्ञान-अर्थोपलब्धिका साधन प्रमाण है । बाह्य विषय स्तम्भ, घड़ा, कमल आदि तथा अन्तरङ्ग ज्ञान, सुख आदि अर्थों की उपलब्धि अर्थात् प्रतीति अर्थोपलब्धि है। 'व्याख्यानसे विशेषार्थको प्रतिपत्ति होती है' इस न्यायके अनुसार यहाँ अव्यभिचारिणी-निर्दोष, अव्यपदेश्या-शब्दके द्वारा जिसका यह 'रूप है. यह रस है ऐसा कथन न हो. तथा व्यवसायात्मिका -निश्चयात्मिका अर्थोपलब्धि ग्रहण करनी चाहिए, सामान्य उपलब्धि नहीं। ऐसो निर्दोष उपलब्धिका जो कारण होता है वही प्रमाण है । अर्थोपलब्धि तो प्रमाणका फल है। तात्पर्य यह कि
१. "पक्षप्रतिपक्षविषयसाधनोपालम्भपरीक्षया तदन्यतरपक्षावधारणं निर्णयः ।" -न्यायक, पृ.. ३ । २. “वादो नाम वीतरागयोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहपूर्वकः प्रमाणतर्कपूर्वकसाधनोपालम्भप्रयोगे क्रियमाणे एकपक्षनिर्णयावसानो वाक्यसमूहः।"-न्यायक. पृ. १३ । ३. "स एव पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो विजिगीषया प्रयुक्तः छल जातिनिग्रहस्थानप्रयोगबहुलो जल्पः ।" -न्यायक. पृ. १। ४. “स्वपक्षसाधनोपन्यासहीनो जल्म एव वितण्डा भवति ।" -न्यायक. पृ. १३ । ५."अहेतवो हेतुवदवभासमाना: हेत्वाभासाः।" न्यायक. पू. १४ । ६. तत्र परस्य वदतोऽर्थविकल्पोपपादनेन वचनविघातः छलम् ।" -न्यायक. पृ. ६ । ७. "सम्यगहेतौ हेत्वाभासे वा प्रयुक्त झटिति तद्दोषतत्त्वाप्रतिभासे तु प्रतिबिम्बनप्रायं किमपि प्रत्यवस्थानं जातिरित्युच्यते।" -न्यायक. पू. १७। ८. "विप्रतिपतिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम् ।" न्यायक. पृ. २१॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org