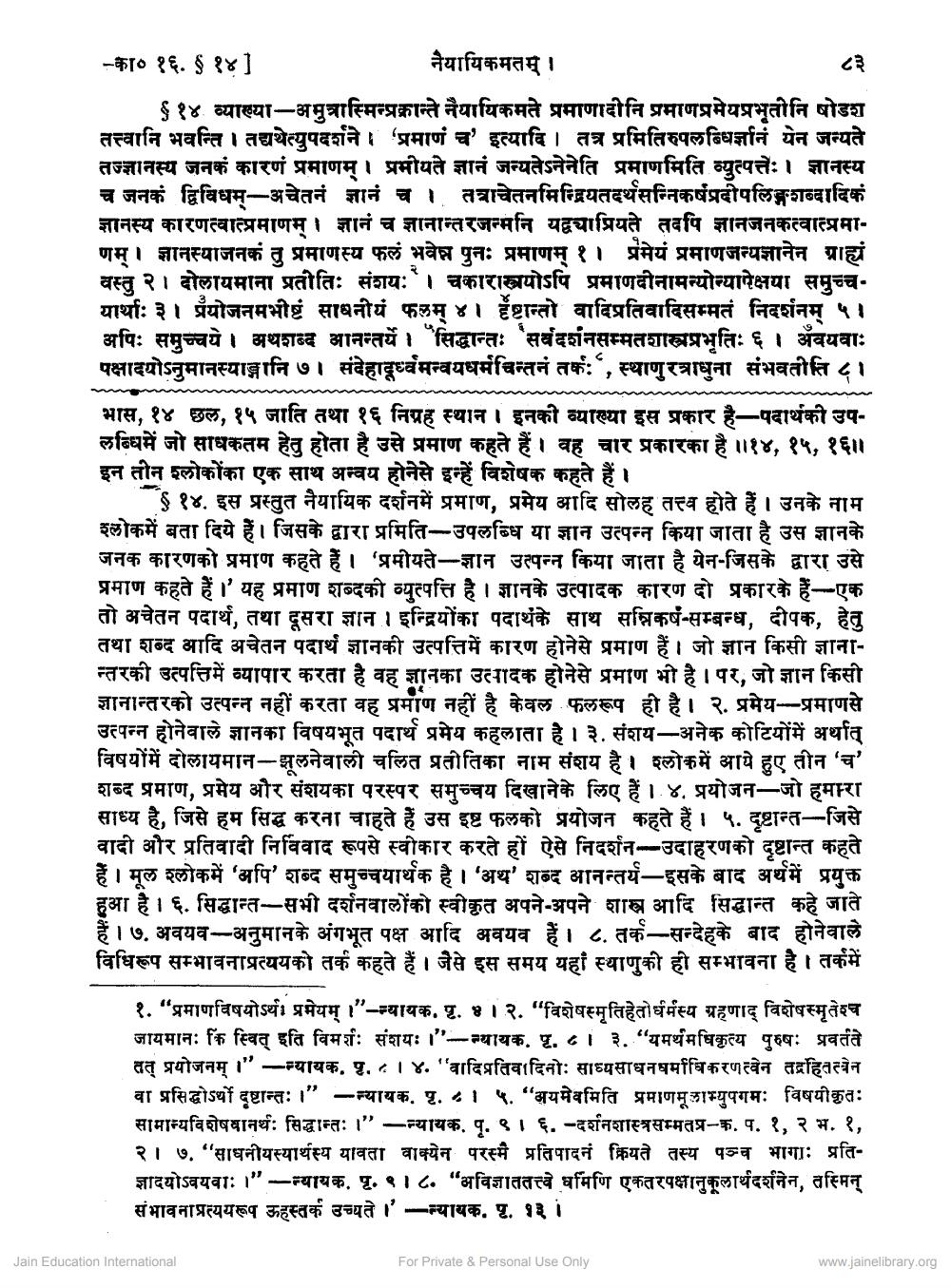________________
-का० १६. ६ १४]
नैयायिकमतम् । ११४ व्याख्या-अमुत्रास्मिन्प्रक्रान्ते नैयायिकमते प्रमाणादीनि प्रमाणप्रमेयप्रभृतीनि षोडश तत्त्वानि भवन्ति । तद्यथेत्युपदर्शने। 'प्रमाणं च' इत्यादि । तत्र प्रमितिरुपलब्धिर्ज्ञानं येन जन्यते तज्ज्ञानस्य जनकं कारणं प्रमाणम् । प्रमीयते ज्ञानं जन्यतेऽनेनेति प्रमाणमिति व्युत्पत्तेः। ज्ञानस्य च जनकं द्विविधम्-अचेतनं ज्ञानं च । तत्राचेतनमिन्द्रियतदर्थसन्निकर्षप्रदीपलिङ्गशब्दादिकं ज्ञानस्य कारणत्वात्प्रमाणम् । ज्ञानं च ज्ञानान्तरजन्मनि ययाप्रियते तदपि ज्ञानजनकत्वात्प्रमाणम् । ज्ञानस्याजनकं तु प्रमाणस्य फलं भवेन पुनः प्रमाणम् १। प्रमेयं प्रमाणजन्यज्ञानेन ग्राह्यं वस्तु २। दोलायमाना प्रतीतिः संशयः । चकारास्त्रयोऽपि प्रमाणदीनामन्योन्यापेक्षया समुच्च. यार्थाः ३। प्रयोजनमभीष्टं साधनीयं फलम् ४ । दृष्टान्तो वादिप्रतिवादिसम्मतं निदर्शनम् ५। अपिः समुच्चये। अथशब्द आनन्तर्ये । सिद्धान्तः सर्वदर्शनसम्मतशास्त्रप्रभृतिः ६ । अवयवाः पक्षादयोऽनुमानस्याङ्गानि ७। संदेहादूर्ध्वमन्वयधर्मचिन्तनं तर्कः, स्थाणुरत्राधुना संभवतीति ८। भास, १४ छल, १५ जाति तथा १६ निग्रह स्थान । इनकी व्याख्या इस प्रकार है-पदार्थकी उपलब्धिमें जो साधकतम हेतु होता है उसे प्रमाण कहते हैं। वह चार प्रकारका है ॥१४, १५, १६॥ इन तीन श्लोकोंका एक साथ अन्वय होनेसे इन्हें विशेषक कहते हैं।
१४. इस प्रस्तुत नैयायिक दर्शनमें प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह तत्त्व होते हैं। उनके नाम श्लोकमें बता दिये हैं। जिसके द्वारा प्रमिति-उपलब्धि या ज्ञान उत्पन्न किया जाता है उस ज्ञानके जनक कारणको प्रमाण कहते हैं । 'प्रमीयते-ज्ञान उत्पन्न किया जाता है येन-जिसके द्वारा उसे प्रमाण कहते हैं।' यह प्रमाण शब्दको व्युत्पत्ति है । ज्ञानके उत्पादक कारण दो प्रकारके हैं-एक तो अचेतन पदार्थ, तथा दूसरा ज्ञान । इन्द्रियोंका पदार्थके साथ सन्निकर्ष-सम्बन्ध, दीपक, हेतु तथा शब्द आदि अचेतन पदार्थ ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होनेसे प्रमाण हैं। जो ज्ञान किसी ज्ञानान्तरकी उत्पत्ति में व्यापार करता है वह ज्ञानका उत्सादक होनेसे प्रमाण भी है । पर, जो ज्ञान किसी ज्ञानान्तरको उत्पन्न नहीं करता वह प्रमाण नहीं है केवल फलरूप ही है। २. प्रमेय-प्रमाणसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानका विषयभूत पदार्थ प्रमेय कहलाता है । ३. संशय-अनेक कोटियोंमें अर्थात् विषयोंमें दोलायमान-झूलनेवाली चलित प्रतीतिका नाम संशय है। श्लोकमें आये हुए तीन 'च' शब्द प्रमाण, प्रमेय और संशयका परस्पर समुच्चय दिखानेके लिए हैं। ४. प्रयोजन-जो हमारा साध्य है, जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं उस इष्ट फलको प्रयोजन कहते हैं। ५. दृष्टान्त-जिसे वादी और प्रतिवादी निर्विवाद रूपसे स्वीकार करते हों ऐसे निदर्शन-उदाहरणको दृष्टान्त कहते हैं। मूल श्लोकमें 'अपि' शब्द समुच्चयार्थक है । 'अथ' शब्द आनन्तर्य-इसके बाद अर्थमें प्रयुक्त हआ है। ६.सिद्धान्त-सभी दर्शनवालोंको स्वीकृत अपने-अपने शास्त्र आदि सिद्धान्त कहे जाते हैं । ७. अवयव-अनुमानके अंगभूत पक्ष आदि अवयव हैं। ८. तर्क-सन्देहके बाद होनेवाले विधिरूप सम्भावनाप्रत्ययको तर्क कहते हैं। जैसे इस समय यहां स्थाणुकी ही सम्भावना है। तर्कमें
१. "प्रमाणविषयोऽर्थः प्रमेयम् ।"-न्यायक. पृ. ४ । २. "विशेषस्मृतिहेतोधर्मस्य ग्रहणाद् विशेषस्मृतेश्च जायमानः किं स्वित् इति विमर्शः संशयः।"-न्यायक. पृ. ८। ३. “यमर्थमधिकृत्य पुरुषः प्रवर्तते तत् प्रयोजनम् ।" -न्यायक. पृ. । । ४. "वादिप्रतिवादिनोः साध्यसाधनधर्माधिकरणत्वेन तद्रहितत्वेन वा प्रसिद्धोऽर्थो दृष्टान्तः ।" -न्यायक. पृ. ।। ५. "अयमेवमिति प्रमाणमूलाभ्युपगमः विषयीकृतः सामान्यविशेषवानर्थः सिद्धान्तः ।" -न्यायक. पृ. ९ । ६. -दर्शनशास्त्रसम्मतप्र-क.प. १, २ भ. १, २। ७. "साधनीयस्यार्थस्य यावता वाक्येन परस्मै प्रतिपादनं क्रियते तस्य पञ्च भागाः प्रतिज्ञादयोऽवयवाः ।" -न्यायक. पृ.। ८. "अविज्ञाततत्त्वे धर्मिणि एकतरपक्षानुकूलार्थदर्शनेन, तस्मिन् संभावनाप्रत्ययरूप ऊहस्तर्क उच्यते।'-न्यायक. पू. १३ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org