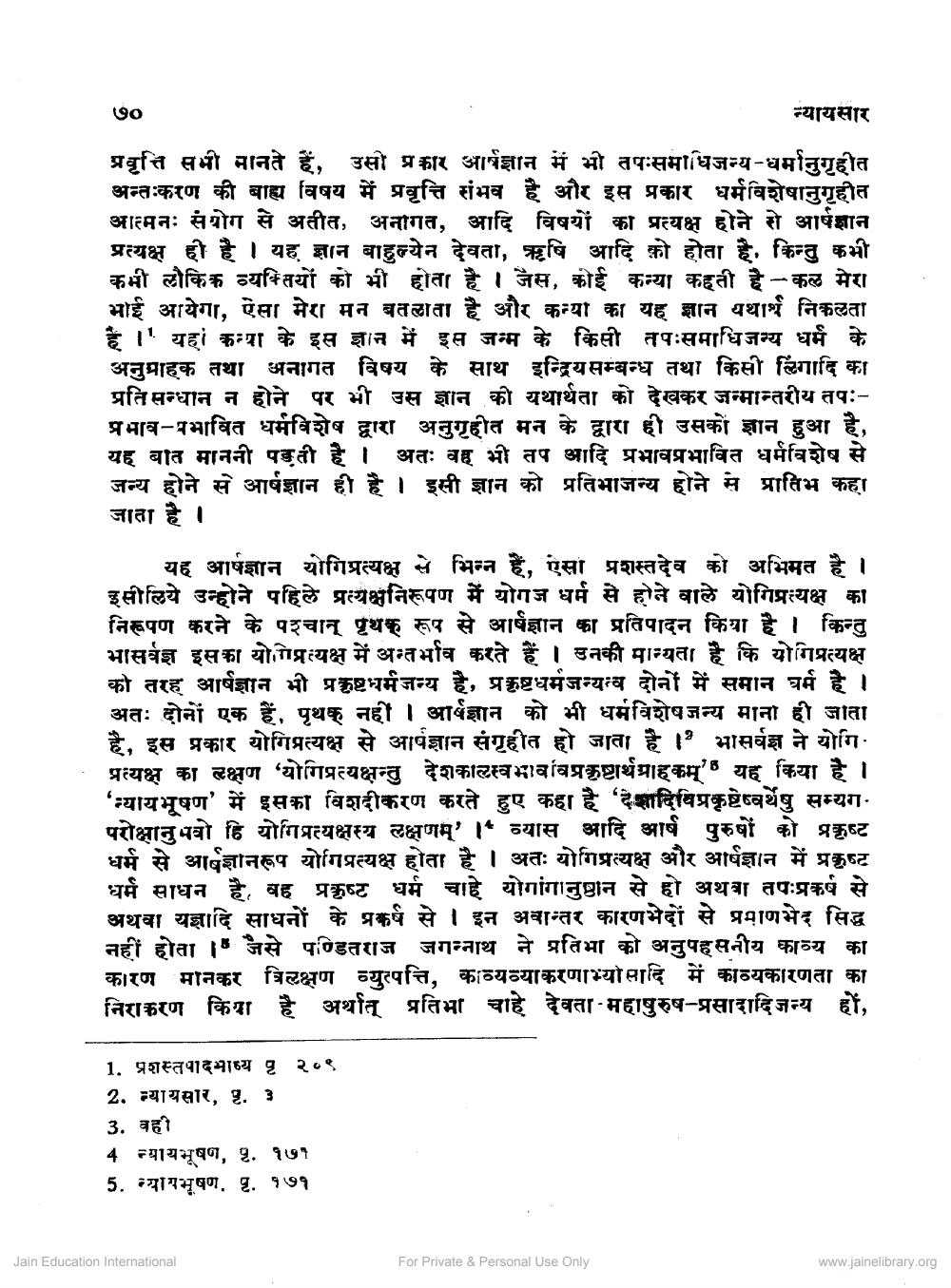________________
७०
न्यायसार प्रवृत्ति सभी मानते हैं, उसी प्रकार आर्यज्ञान में भी तपासमाधिजन्य-धर्मानुगृहीत अन्तःकरण की बाह्य विषय में प्रवृत्ति संभव है और इस प्रकार धर्मविशेषानुगृहीत आत्मनः संयोग से अतीत, अनागत, आदि विषयों का प्रत्यक्ष होने से आर्षज्ञान प्रत्यक्ष ही है। यह ज्ञान बाहत्येन देवता. ऋषि आदि को होता है. किन्त कर्म कभी लौकिक व्यक्तियों को भी होता है । जैस, कोई कन्या कहती है-कल मेरा भाई आयेगा, ऐसा मेरा मन बतलाता है और कन्या का यह ज्ञान यथार्थ निकलता है। यहां कन्या के इस ज्ञान में इस जन्म के किसी तपःसमाधिजन्य धर्म के अनुग्राहक तथा अनागत विषय के साथ इन्द्रिय सम्बन्ध तथा किसी लिंगादि का प्रतिसन्धान न होने पर भी उस ज्ञान को यथार्थता को देखकर जन्मान्तरीय तपःप्रभाव-प्रभावित धर्मविशेष द्वारा अनुगृहीत मन के द्वारा ही उसको ज्ञान हुआ है, यह बात माननी पड़ती है। अतः वह भी तप आदि प्रभावप्रभावित धर्मविशेष से जन्य होने से आर्षज्ञान ही है। इसी ज्ञान को प्रतिभाजन्य होने से प्रातिभ कहा जाता है।
__ यह आषज्ञान योगिप्रत्यक्ष से भिन्न हैं, ऐसा प्रशस्तदेव को अभिमत है। इसीलिये उन्होने पहिले प्रत्यक्षनिरूपण में योगज धर्म से होने वाले योगिप्रत्यक्ष का निरूपण करने के पश्चान् पृथक रूप से आर्षज्ञान का प्रतिपादन किया है। किन्तु भासर्वज्ञ इसका यो प्रत्यक्ष में अन्तर्भाव करते हैं । उनकी मान्यता है कि योगिप्रत्यक्ष को तरह आर्षज्ञान भी प्रकृष्टधर्मजन्य है, प्रकृष्टधर्मजन्यत्व दोनों में समान धर्म है। अतः दोनों एक हैं, पृथक् नहीं । आषज्ञान को भी धर्मविशेष जन्य माना ही जाता है, इस प्रकार योगिप्रत्यक्ष से आषज्ञान संगृहीत हो जाता है। भासर्वज्ञ ने योगिः प्रत्यक्ष का लक्षण 'योगिप्रत्यक्षन्तु देशकालस्वभावविप्रकृष्टार्थग्राहकम्' यह किया है। 'न्यायभूषण' में इसका विशदीकरण करते हुए कहा है 'देशादिविप्रकृष्टेष्वर्थेषु सम्यग. परोक्षानुभवो हि योगिप्रत्यक्षस्य लक्षणम्' । व्यास आदि आर्ष पुरुषों को प्रकृष्ट धर्म से आईज्ञानरूप योगिप्रत्यक्ष होता है । अतः योगिप्रत्यक्ष और आर्षज्ञान में प्रकृष्ट धर्म साधन है, वह प्रकृष्ट धर्म चाहे योगांगानुष्ठान से हो अथवा तपःप्रकर्ष से अथवा यज्ञादि साधनों के प्रकर्ष से । इन अवान्तर कारणभेदों से प्रमाणभेद सिद्ध नहीं होता। जैसे पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रतिभा को अनुपहसनीय काव्य का कारण मानकर विलक्षण व्युत्पत्ति, काव्यव्याकरणाभ्योसादि में काव्यकारणता का निराकरण किया है अर्थात् प्रतिभा चाहे देवता-महापुरुष-प्रसादादिजन्य हों,
1. प्रशस्तपादभाध्य पृ २०९ 2. न्यायसार, पृ. ३ 3. वही 4 न्यायभूषण, पृ. १७१ 5. न्यायभूषण. पृ. १७१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org