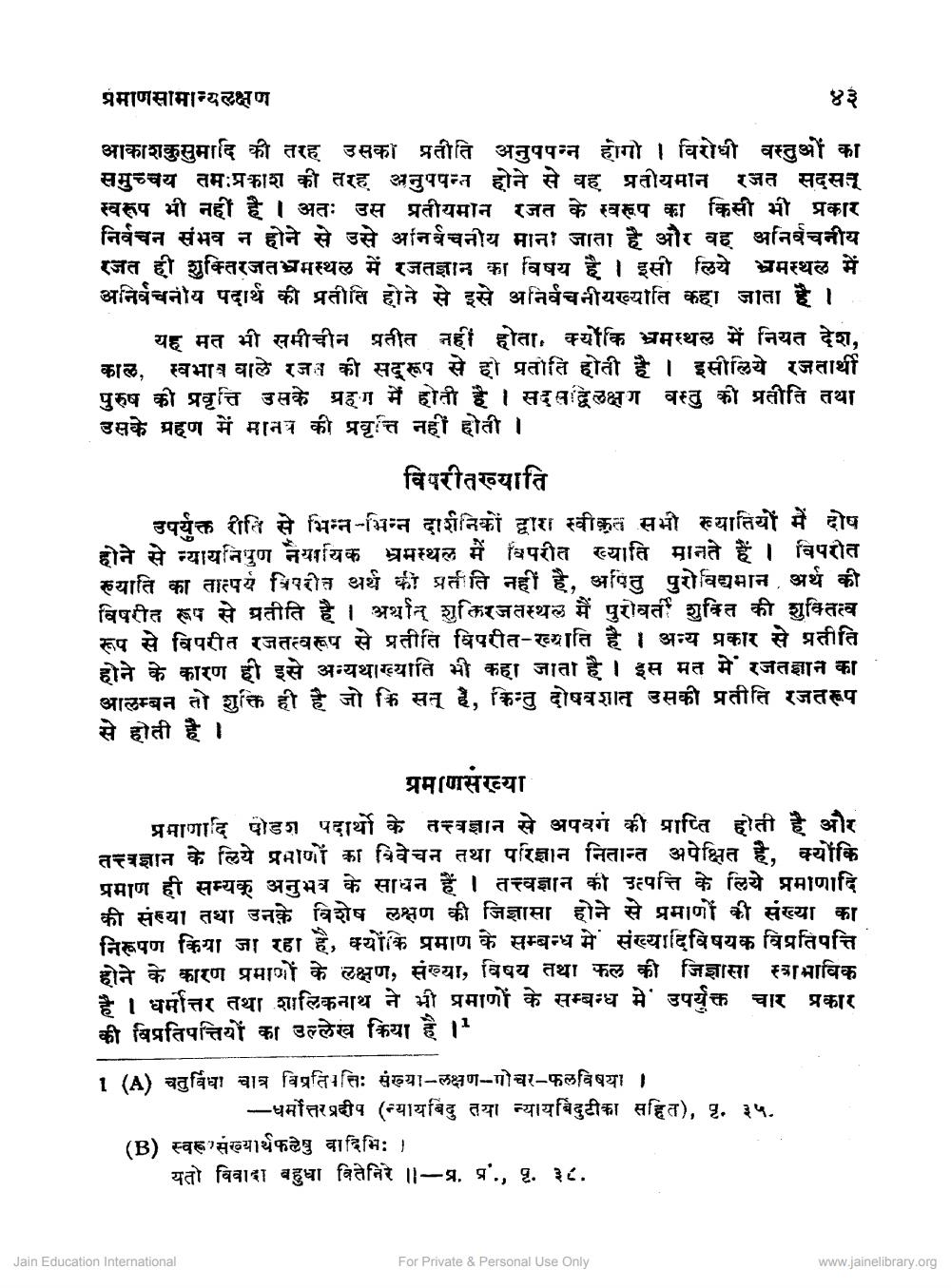________________
प्रमाणसामान्यलक्षण
४३
आकाशकुसुमादि की तरह उसका प्रतीति अनुपपन्न होगो । विरोधी वस्तुओं का समुच्चय तमः प्रकाश की तरह अनुपपन्न होने से वह प्रतीयमान रजत सदसत् स्वरूप भी नहीं है । अतः उस प्रतीयमान रजत के स्वरूप का किसी भी प्रकार निर्वाचन संभव न होने उसे अनिर्वचनीय माना जाता है और वह अनिर्वचनीय रजत ही शुक्तिरजतभ्रमस्थल में रजतज्ञान का विषय है । इसी लिये भ्रमस्थल में अनिर्वचनीय पदार्थ की प्रतीति होने से इसे अनिर्वचनीयख्याति कहा जाता है ।
यह मत भी समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि भ्रमस्थल में नियत देश, काल, स्वभाव वाले रजत की सद्रूप से हो प्रतोति होती है । इसीलिये रजतार्थी पुरुष की प्रवृत्ति उसके ग्रहग में होती है । सदसद्विलक्षग वस्तु की प्रतीति तथा उसके ग्रहण में मानव की प्रवृत्ति नहीं होती ।
विपरीतख्याति
उपर्युक्त रीति से भिन्न-भिन्न दार्शनिकों द्वारा स्वीकृत सभी ख्यातियों में दोष होने से न्यायनिपुण नैयायिक भ्रमस्थल में विपरीत ख्याति मानते हैं । विपरीत ख्याति का तात्पर्यविपरीत अर्थ की प्रतीति नहीं है, अपितु पुरोविद्यमान अर्थ की विपरीत रूप से प्रतीति है । अर्थात् शुक्तिरजतस्थल मैं पुरोवर्ती शुक्ति की शुक्तित्व रूप से विपरीत रजतत्वरूप से प्रतीति विपरीत ख्याति है । अन्य प्रकार से प्रतीति होने के कारण ही इसे अन्यथाख्याति भी कहा जाता है । इस मत में रजतज्ञान का आलम्बन तो शुक्ति ही है जो कि सत् हैं, किन्तु दोषवशात उसकी प्रतीति रजतरूप से होती है ।
माणसंख्या
प्रमाणादि पोड पदार्थो के तत्वज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है और ज्ञान के लिये प्रमाणों का विवेचन तथा परिज्ञान नितान्त अपेक्षित है, क्योंकि प्रमाण ही सम्यक् अनुभव के साधन हैं । तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति के लिये प्रमाणादि की संख्या तथा उनके विशेष लक्षण की जिज्ञासा होने से प्रमाणों की संख्या का निरूपण किया जा रहा है, क्योंकि प्रमाण के सम्बन्ध में संख्यादिविषयक विप्रतिपत्ति होने के कारण प्रमाणों के लक्षण, संख्या, विषय तथा फल की जिज्ञासा स्वाभाविक है । धर्मोत्तर तथा शालिकनाथ ने भी प्रमाणों के सम्बन्ध में उपर्युक्त चार प्रकार की विप्रतिपत्तियों का उल्लेख किया है । '
1 (A) चतुर्विधा चात्र विप्रतिपत्तिः संख्या - लक्षण - गोचर - फलविषया ।
- धर्मोत्तर प्रदीप ( न्याय बिंदु तया न्याय बिंदुटीका सहित), पृ. ३५. (B) स्वरू' संख्यार्थ फलेषु वादिभिः ।
यतो विवाद बहुधा वितेनिरे ॥ प्र. प्र., पृ. ३८.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org