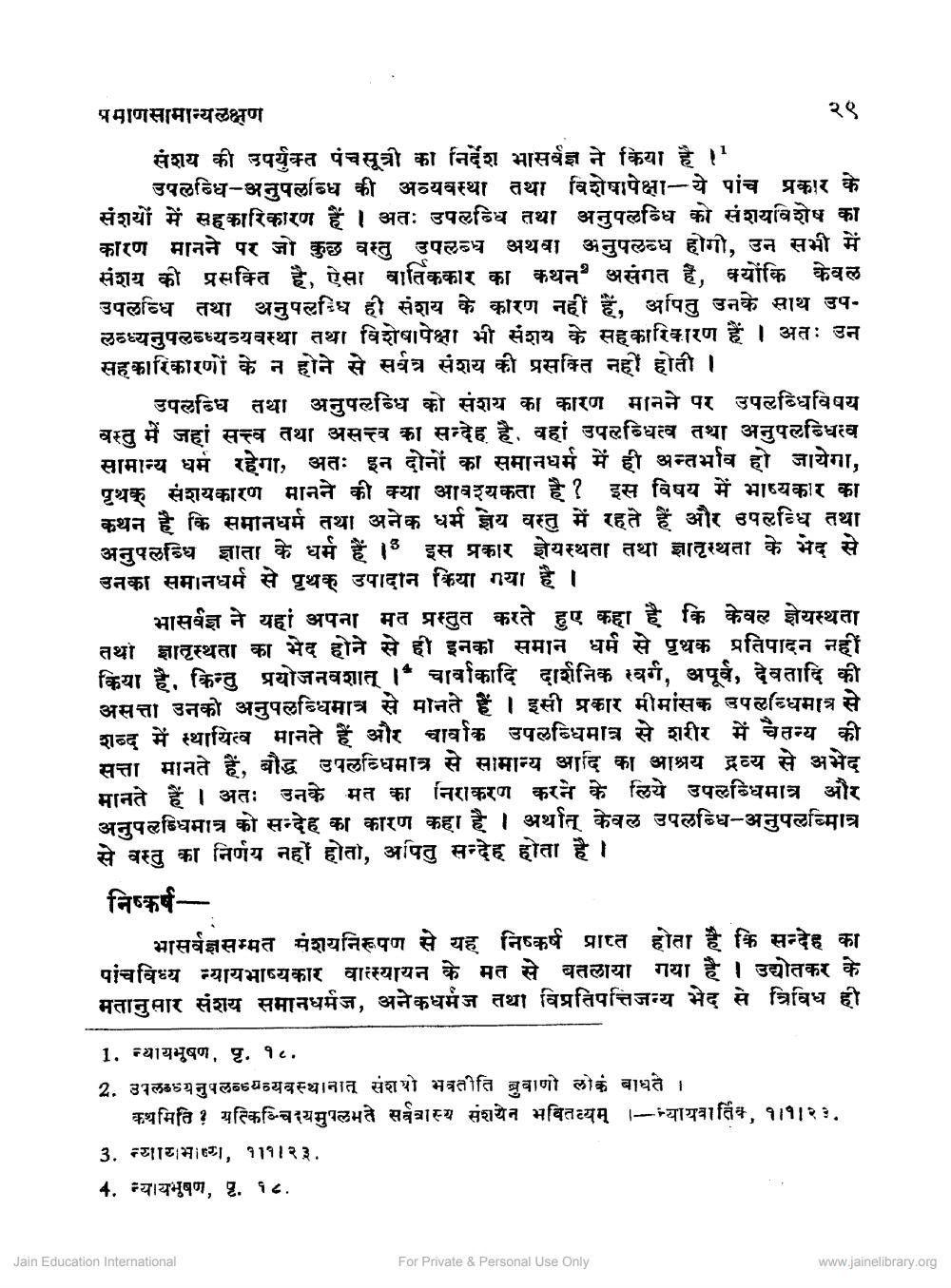________________
प्रमाणसामान्यलक्षण
संशय की उपर्युक्त पंचसूत्री का निर्देश भासर्वज्ञ ने किया है।
उपलब्धि-अनुपलब्धि की अव्यवस्था तथा विशेषापेक्षा-ये पांच प्रकार के संशयों में सहकारिकारण हैं । अतः उपलब्धि तथा अनुपलब्धि को संशयविशेष का कारण मानने पर जो कुछ वस्तु उपलब्ध अथवा अनुपलब्ध होगी, उन सभी में संशय की प्रसक्ति है, ऐसा वातिककार का कथन' असंगत हैं, क्योंकि केवल उपलब्धि तथा अनुपलब्धि ही संशय के कारण नहीं हैं, अपितु उनके साथ उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्था तथा विशेषापेक्षा भी संशय के सहकारिकारण हैं । अतः उन सहकारिकारणों के न होने से सर्वत्र संशय की प्रसक्ति नहीं होती।
उपलब्धि तथा अनुपलब्धि को संशय का कारण मानने पर उपलब्धिविनय वस्त में जहां सत्व तथा असत्व का सन्देह है, वहां उपलब्धित्व तथा अनपर सामान्य धर्म रहेगा, अतः इन दोनों का समानधर्म में ही अन्तर्भाव हो जायेगा, पृथक् संशयकारण मानने की क्या आवश्यकता है ? इस विषय में भाष्यकार का कथन है कि समानधर्म तथा अनेक धर्म ज्ञेय वस्तु में रहते हैं और उपलब्धि तथा अनुपलब्धि ज्ञाता के धर्म हैं। इस प्रकार ज्ञेयस्थता तथा ज्ञातृस्थता के भेद से उनका समानधर्म से पृथक् उपादान किया गया है।
भासर्वज्ञ ने यहां अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि केवल ज्ञेयस्थता तथा ज्ञातृस्थता का भेद होने से ही इनका समान धर्म से पृथक प्रतिपादन नहीं किया है, किन्तु प्रयोजनवशात् ।' चार्वाकादि दार्शनिक स्वर्ग, अपूर्व, देवतादि की असत्ता उनको अनुपलब्धिमात्र से मानते हैं। इसी प्रकार मीमांसक उपलब्धिमात्र से शब्द में स्थायित्व मानते हैं और चार्वाक उपलब्धिमात्र से शरीर में चैतन्य की सत्ता मानते हैं, बौद्ध उपलब्धिमात्र से सामान्य आदि का आश्रय द्रव्य से अभेद मानते हैं । अतः उनके मत का निराकरण करने के लिये उपलब्धिमात्र और अनुपलब्धिमात्र को सन्देह का कारण कहा है । अर्थात् केवल उपलब्धि-अनुपलब्मिात्र से वस्तु का निर्णय नहीं होतो, अपितु सन्देह होता है। निष्कर्ष
भासर्वज्ञसम्मत संशयनिरूपण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सन्देह का पांचविध्य न्यायभाष्यकार वात्स्यायन के मत से बतलाया गया है । उद्योतकर के मतानुसार संशय समानधर्मज, अनेकधर्मज तथा विप्रतिपत्तिजन्य भेद से त्रिविध ही
1. न्यायभूषण, पृ. १८. 2. उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थानात् संशयो भवतीति ब्रुवाणो लोकं बाधते । __ कथमिति ? यत्किञ्चित्यमुपलभते सर्वास्य संशयेन भवितव्यम् ।-न्यायवार्तिक, ११॥२३. 3. न्यायभाया, १११।२३. 4. न्यायभुषण, पृ. १८.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org