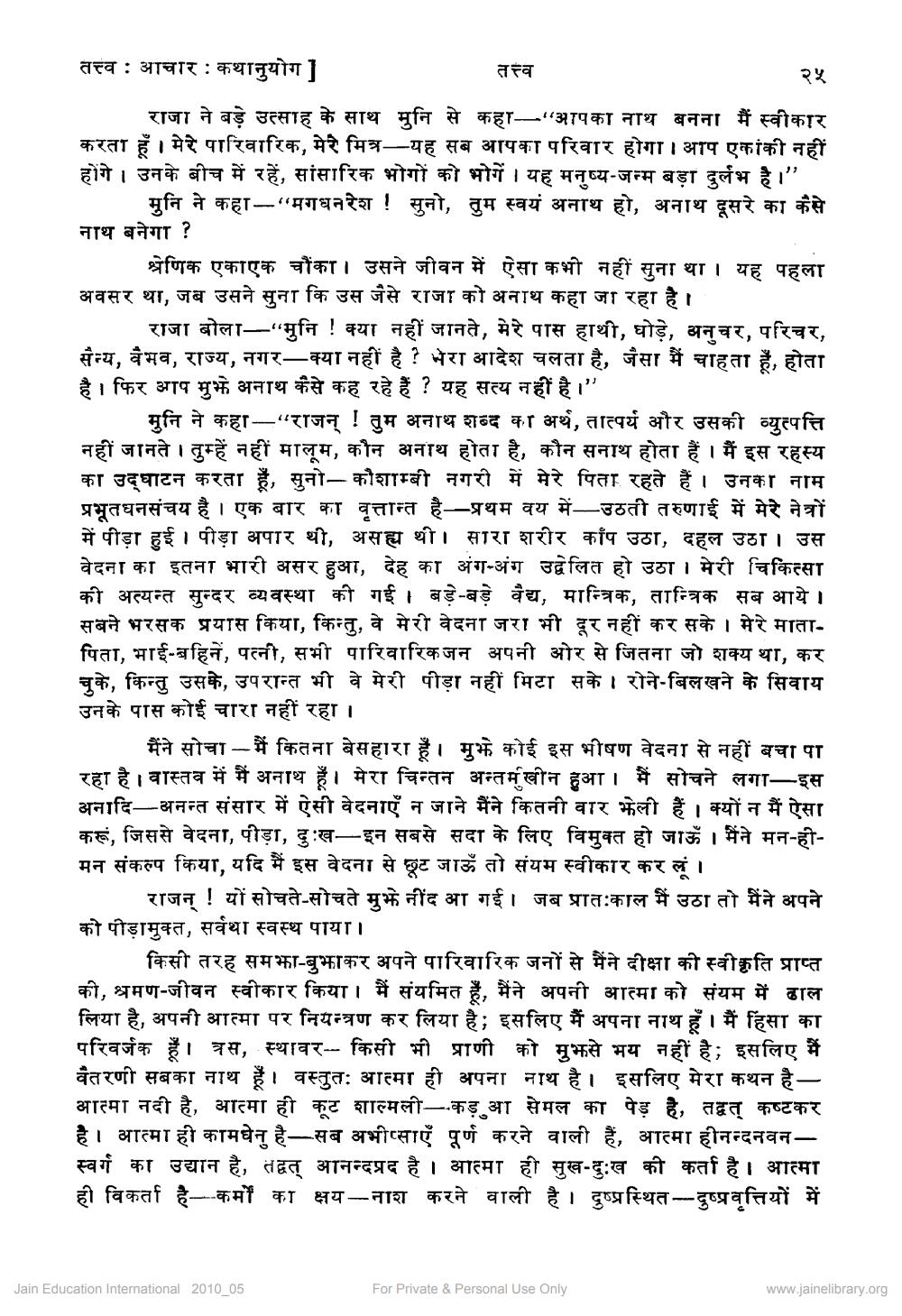________________
तत्त्व : आचार : कथानुयोग]
तत्त्व
२५
राजा ने बड़े उत्साह के साथ मुनि से कहा- "आपका नाथ बनना मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे पारिवारिक, मेरे मित्र—यह सब आपका परिवार होगा। आप एकांकी नहीं होंगे। उनके बीच में रहें, सांसारिक भोगों को भोगें । यह मनुष्य-जन्म बड़ा दुर्लभ है।"
मुनि ने कहा- “मगधनरेश ! सुनो, तुम स्वयं अनाथ हो, अनाथ दूसरे का कैसे नाथ बनेगा ?
श्रेणिक एकाएक चौंका। उसने जीवन में ऐसा कभी नहीं सुना था। यह पहला अवसर था, जब उसने सुना कि उस जैसे राजा को अनाथ कहा जा रहा है।
राजा बोला- "मुनि ! क्या नहीं जानते, मेरे पास हाथी, घोड़े, अनुचर, परिचर, सैन्य, वैभव, राज्य, नगर-क्या नहीं है ? भेरा आदेश चलता है, जैसा मैं चाहता हूँ, होता है। फिर आप मुझे अनाथ कैसे कह रहे हैं ? यह सत्य नहीं है।"
मुनि ने कहा- "राजन् ! तुम अनाथ शब्द का अर्थ, तात्पर्य और उसकी व्युत्पत्ति नहीं जानते । तुम्हें नहीं मालूम, कौन अनाथ होता है, कौन सनाथ होता हैं । मैं इस रहस्य का उद्घाटन करता हूँ, सुनो- कौशाम्बी नगरी में मेरे पिता रहते हैं। उनका नाम प्रभूतधनसंचय है । एक बार का वृत्तान्त है-प्रथम वय में-उठती तरुणाई में मेरे नेत्रों में पीड़ा हुई। पीड़ा अपार थी, असह्य थी। सारा शरीर काँप उठा, दहल उठा। उस वेदना का इतना भारी असर हुआ, देह का अंग-अंग उद्वेलित हो उठा। मेरी चिकित्सा की अत्यन्त सुन्दर व्यवस्था की गई। बड़े-बड़े वैद्य, मान्त्रिक, तान्त्रिक सब आये। सबने भरसक प्रयास किया, किन्तु, वे मेरी वेदना जरा भी दूर नहीं कर सके। मेरे मातापिता, भाई-बहिनें, पत्नी, सभी पारिवारिक जन अपनी ओर से जितना जो शक्य था, कर चुके, किन्तु उसके, उपरान्त भी वे मेरी पीड़ा नहीं मिटा सके। रोने-बिलखने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं रहा ।
मैंने सोचा -मैं कितना बेसहारा हूँ। मुझे कोई इस भीषण वेदना से नहीं बचा पा रहा है। वास्तव में मैं अनाथ हूँ। मेरा चिन्तन अन्तर्मुखीन हुआ। मैं सोचने लगा-इस अनादि-अनन्त संसार में ऐसी वेदनाएँ न जाने मैंने कितनी वार झेली हैं। क्यों न मैं ऐसा करूं, जिससे वेदना, पीड़ा, दु:ख-इन सबसे सदा के लिए विमुक्त हो जाऊँ । मैंने मन-हीमन संकल्प किया, यदि मैं इस वेदना से छूट जाऊँ तो संयम स्वीकार कर लें।
राजन् ! यों सोचते-सोचते मुझे नींद आ गई। जब प्रातःकाल मैं उठा तो मैंने अपने को पीड़ामुक्त, सर्वथा स्वस्थ पाया।
किसी तरह समझा-बुझाकर अपने पारिवारिक जनों से मैंने दीक्षा की स्वीकृति प्राप्त की, श्रमण-जीवन स्वीकार किया। मैं संयमित हैं, मैंने अपनी आत्मा को संयम में ढाल लिया है, अपनी आत्मा पर नियन्त्रण कर लिया है। इसलिए मैं अपना नाथ हूँ। मैं हिंसा का परिवर्जक हूँ। त्रस, स्थावर-- किसी भी प्राणी को मुझसे भय नहीं है। इसलिए मैं वैतरणी सबका नाथ हूँ। वस्तुत: आत्मा ही अपना नाथ है। इसलिए मेरा कथन हैआत्मा नदी है, आत्मा ही कूट शाल्मली-कड़ आ सेमल का पेड़ है, तद्वत् कष्टकर है। आत्मा ही कामधेनु है-सब अभीप्साएँ पूर्ण करने वाली हैं, आत्मा हीनन्दनवनस्वर्ग का उद्यान है, तद्वत् आनन्दप्रद है । आत्मा ही सुख-दु:ख की कर्ता है। आत्मा ही विकर्ता है---कर्मों का क्षय-नाश करने वाली है। दुष्प्रस्थित-दुष्प्रवृत्तियों में
____Jain Education International 2010_05
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org